समय आ गया है कि हम भाषा के सवाल को गंभीरता से लें। भाषा मनुष्य होने की शर्त है। इसे सिर्फ अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में सीमित करना मुनासिब नहीं। भाषा के लिए सभ्य और असभ्य, विकसित और अविकसित, संपन्न और दरिद्र जैसे पैमाने लागू करना भी ठीक नहीं है। इन्हीं मान्यताओं के चलते हम अपनी भाषिक संपदा को गंवाते चले आ रहे हैं। हमारे औपनिवेशिक प्रभुओं ने बताया कि हमारी मातृभाषाएं असभ्य, अविकसित और दरिद्र हैं। इस औपनिवेशिक ज्ञान ने मातृभाषाओं के प्रति एक सहज अवमानना का भाव पैदा कर दिया। हम सभ्य, विकसित और संपन्न होने के लिए दूसरी भाषाओं का मुंह जोहने लगे और इस चक्कर में अपनी मातृभाषाओं से विमुख होते चले गए। मातृभाषाओं की जगह राष्ट्रभाषा हिंदी हमारे सामने आई। दुर्भाग्य से हम हिंदी को लेकर खास तरह की बेपरवाही बरतते रहे हैं। अंगरेजी के लिए सम्मान जरूर है, लेकिन उसके मूल में भाषा प्रेम नहीं है। हमें अंगरेजी सिर्फ रोजी-रोजगार के लिए नहीं, बल्कि प्रभुत्व और प्रभुता के लिए चाहिए।
मातृभाषा से विमुखता की प्रवृत्ति भाषा विहीनता की ओर ले जाती है। यह भाषा विहीनता हमारी मनुष्यता को विकलांग बना रही है। धीरे-धीरे हम ऐसे समाज में बदल रहे हैं, जो मातृभाषाओं से पीछा छुड़ाने को बेताब, हिंदी के प्रति बेपरवाह और अंगरेजी के सामने लाचार है। यह तथ्य हमें समझना होगा कि अंगरेजी हो या संसार की कोई अन्य भाषा, मातृभाषा के रास्ते ही हम उस तक पंहुच सकते हैं।
मातृभाषाओं के माध्यम से हम बहुत कुछ ऐसा सीखते हैं जो हमें सामाजिक और समावेशी बनाता है। मातृभाषाओं में एक खास तरह की सामूहिकता होती है। वह हमें समावेशी होना सिखाती है। आज दुनिया भौतिक उन्नति और विकास के पीछे पागल हो रही है, बिना यह परवाह किए कि अंत:करण का आयतन संक्षिप्त होता जा रहा है। भाषा से अंत:करण का निर्माण होता है, उसे गहराई मिलती है। भाषा के प्रति हमारी बेपरवाही से हमारा अंत:करण छीज रहा है। आलम यह है कि हम दिनोंदिन भाषाई संपदा को नष्ट हो जाने दे रहे हैं।
भाषाविद गणेश देवी के सर्वे के मुताबिक भारत में तकरीबन नौ सौ भाषाएं बोली जाती हैं। 1961 की जनगणना के अनुसार भारत में सोलह-सत्रह सौ भाषाएं थीं। पिछले पचास-साठ वर्षों में यह संख्या आधी रह गई है। आशंका व्यक्त की गई है कि आने वाले पचास वर्षों में इनमे से लगभग एक तिहाई भाषाएं खत्म हो जाएंगी।
भाषाओं के खत्म होने के साथ हमारा मनुष्य होना ही खतरे में पड़ गया है। भारत की भाषा बहुलता हमारी थाती है। सत्ताएं इसे समझने में नाकाम रही हैं। वे भाषा बहुलता को समस्या समझती और भाषा को वर्चस्व का हथियार बनाती हैं। वर्चस्व से जुड़ कर भाषा अपनी मूल प्रकृति- संवादधर्मिता- से अलग हो जाती और वैमनस्य पैदा करती है। इसलिए मातृभाषाओं का सवाल हमारे मनुष्य बने रहने के सवाल से जुड़ा है।
साम्राज्य और पूंजी के वर्चस्व वाली आधुनिक दुनिया भाषाओं के बारे में बेहद असंवेदनशील हुई है। पिछली शताब्दी में दुनिया की असंख्य भाषाएं या तो विलुप्त हो गई हैं या फिर होने के कगार पर हैं। फिलहाल पूरी दुनिया में तीन हजार भाषाएं हैं। ऐसी आशंका है कि शताब्दी के अंत तक उनमें से केवल तीन सौ बचें। शायद इसीलिए उन्नीस सौ निन्यानबे में यूनेस्को ने मातृभाषाओं को संरक्षित और विकसित करने की जरूरत पर बल दिया और इक्कीस फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप मनाने का प्रस्ताव पारित किया। इसके लिए इक्कीस फरवरी की तिथि इसलिए निश्चित की गई क्योंकि इसी दिन 1952 में बांग्लादेश (तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान) में ढाका विश्वविद्यालय के बांग्ला भाषा को मान्यता देने की मांग करते हुए चार प्रदर्शनकारी छात्र शहीद हो गए। आगे चल कर मातृभाषा के लिए शुरू हुए इस आंदोलन की परिणति बांग्लादेश के उदय में हुई।
प्रत्येक भाषा की अपनी विश्व दृष्टि होती है, अपना देशज ज्ञान, प्रतिभा कोश और साहित्य होता है, जो भाषाओं के साथ नष्ट हो जाता है। भाषाओं के नष्ट होने की एक वजह उनको बोलने वाले लोगों का जीवन स्तर है। कुछ भाषाओं के साथ पिछड़ा, गंवारू होने की चिप्पी लगा दी गई है। इसलिए लोग उन भाषाओं से अपना संबंध छिपाते हैं। यह भी नहीं कि जिन भाषाओं के बोलने वालों की संख्या कम है, उन्हीं पर खत्म होने का खतरा मड़रा रहा है। भेदभाव का शिकार होने के नाते भी भाषाओं का अस्तित्व खतरे में है।
भाषा की बहुलता हमारी थाती है, जबकि सत्ताएं भाषा बहुलता को समस्या समझने की भूल करती हैं और भाषा को वर्चस्व का हथियार बनाती हैं। इसी से भाषाओं को लेकर हीनताबोध उपजता है। भाषाओं के बीच संवाद नहीं हो पाता। जबकि भाषा की प्रकृति संवादधर्मी है। इसलिए जरूरत भाषाओं के बीच वैमनस्य पैदा करने वाली शक्तियों को पहचानने और उन्हें व्यर्थ करने की है। महान अफ्रीकी लेखक न्गूगी वा थ्यांगो कहते हैं- अनेक भाषाओं वाला विश्व विभिन्न रंगों वाले फूलों के मैदान जैसा होना चाहिए। कोई ऐसा फूल नहीं है, जो अपने रंग या आकार के कारण दूसरे फूल से बढ़ कर हो। ऐसे सभी फूल अपने रंगों और आकारों की विविधता में अपने सामूहिक पुष्पत्व को व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार हमारी विभिन्न भाषाएं एक सामूहिकता के बोध को व्यक्त कर सकती हैं और उन्हें करना चाहिए। भाषाएं इस तरह मिलें जैसे नदियां मिलती हैं। हमें भाषाओं के लोकतंत्र को समझाना चाहिए और उसकी अवतारणा करनी चाहिए। तभी हम भाषा की निधि को नष्ट होने से बचा सकेंगे और उसे भावी पीढ़ी को सौंप सकेंगे।
स्वाधीनता आंदोलन के साथ ही वासुदेवशरण अग्रवाल, राहुल संकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे मनीषियों ने जनपदीय आंदोलन की बात की थी। यह जनपदीय भावना भाषाई वैमनस्य नहीं, भाषाओं के सामंजस्य की बात करती है। इन मनीषियों की सोच थी कि जनपदों में विकसित हुआ साहित्य, संगीत-कला कौशल, ज्ञान-विज्ञान उपेक्षा की वस्तु नहीं है। उनमें हजारों वर्ष का मानवीय संघर्ष, अनुभव और चेतना का इतिहास संचित है। इसलिए जनपदीय साहित्य का अध्ययन और मूल्यांकन किया जाना चाहिए। देखना यह चाहिए कि इस निधि के भीतर ऐसा क्या है, जो हमारे आधुनिक जीवन को बेहतर बनाने के काम आ सकता है।
हमारे विश्वविद्यालयों में देशी भाषाएं प्राय: लोक साहित्य के रूप में पढ़ाई जाती हैं। कुछ-कुछ कृपा भाव से। यह नाकाफी ही नहीं, बल्कि चिंताजनक है। अपने परिवेश की इतिहास चेतना से रहित और मातृभाषा से वंचित और भाषाई विपन्नता के शिकार हो चुके पढ़े-लिखे लोगों ने भाषा की बहुआयामी निधि को गंवा दिया है। यह निधि, यह संपदा भाषा का यह सौंदर्य कहां बचा है? गांवों में। जिसे बे-पढ़ी-लिखी जनता कहा जाता है उसने इस संपत्ति को बचाया है। इसलिए भी इस महान संपदा का संरक्षण और संवर्धन जनपदीय अध्ययन के रास्ते ही संभव है। भूमि, उस पर बसने वाला जन और उस जन की संस्कृति का त्रिकोणात्मक अध्ययन करना होगा। इस अध्ययन से हम यह सीख सकेंगे कि विविधता अभिशाप नहीं है। बल्कि यह पृथ्वी के साथ घनिष्ठ रूप से संबद्ध होने के कारण है। मातृभाषाओं को उपयोग और उपभोग के नजरिए से ऊपर उठ कर जनपदीय अध्ययन के नजरिए से देखने-जानने की जरूरत है।
अवसरः मातृभाषाओं को बचाने की जरूरत
कुछ भाषाओं के साथ पिछड़ा, गंवारू होने की चिप्पी लगा दी गई है। इसलिए लोग उन भाषाओं से अपना संबंध छिपाते हैं। यह भी नहीं कि जिन भाषाओं के बोलने वालों की संख्या कम है, उन्हीं पर खत्म होने का खतरा मडरा रहा है। भेदभाव का शिकार होने के नाते भी भाषाओं का अस्तित्व खतरे में है।
Written by जनसत्ता
Updated:
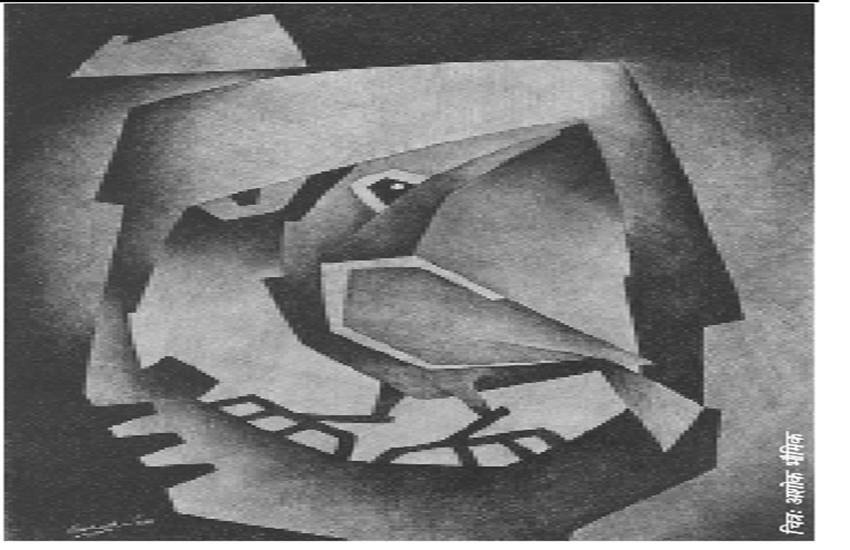
Jansatta.com पर पढ़े ताज़ा रविवारीय स्तम्भ समाचार (Sundaycolumn News), लेटेस्ट हिंदी समाचार (Hindi News), बॉलीवुड, खेल, क्रिकेट, राजनीति, धर्म और शिक्षा से जुड़ी हर ख़बर। समय पर अपडेट और हिंदी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए जनसत्ता की हिंदी समाचार ऐप डाउनलोड करके अपने समाचार अनुभव को बेहतर बनाएं ।
First published on: 21-02-2016 at 03:33 IST