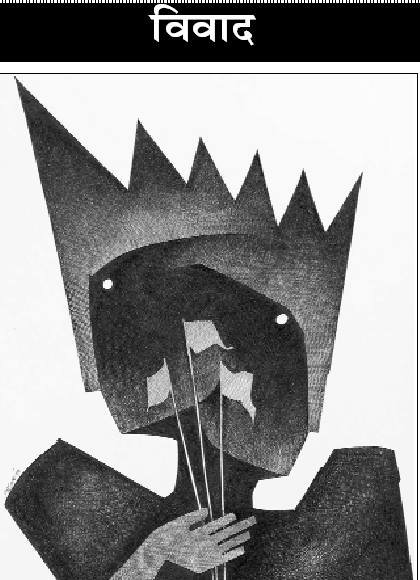विपरीत विचारधारा के सत्ता में होने पर अक्सर रचनाकार सरकारी या सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं के समारोहों, सम्मानों-पुरस्कारों का विरोध करते देखे जाते हैं। अनेक मौकों पर यह भी देखा जाता है कि जब कोई समानधर्मा रचनाकार ऐसे किसी मंच पर शिरकत करता है तो उसकी लानत-मलामत में कोर-कसर नहीं छोड़ी जाती। यहां तक कि उस पर व्यक्तिगत हमले भी शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही हुआ पिछले दिनों, जब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने मूर्धन्य आलोचक नामवर सिंह के जन्मदिन पर पूरे दिन का एक कार्यक्रम आयोजित किया। नामवर सिंह वामपंथी हैं और चूंकि केंद्र में इस समय दक्षिणपंथी सरकार है और वामपंथी रचनाकार उसकी रीति-नीति से सहमत नहीं हैं, इसलिए उनमें से बहुतों को नामवर सिंह का राष्ट्रीय कला केंद्र का न्योता स्वीकार करना नागवार गुजरा। सिद्धांतों की दुहाई दी जाने लगी। उस कार्यक्रम में जाने वालों की मजम्मत भी खूब हुई। सरकारी संस्थाओं को लेकर ऐसी वैचारिक छुआछूत कहां तक उचित है! फिर ऐसा क्या है कि सिर्फ हिंदी साहित्य के रचनाकार इन संस्थाओं को लेकर अधिक आग्रही दिखते हैं। चित्रकला, संगीत, रंगमंच आदि से जुड़े लोग ऐसी छुआछूत बरतते प्राय: नहीं देखे जाते, बेशक वे किसी मुद्दे पर सहमति-असहमति का स्वर साहित्यकारों के साथ मिलाते हैं। इन्हीं सवालों से जूझती ये टिप्पणियां। – सं.
लेखकों को सरकारी संस्थाओं में हिस्सा लेना चाहिए या उनका बहिष्कार करना चाहिए, यह प्रश्न परिस्थिति-सापेक्ष है। जब-जब लेखकों के आम रुझान और सरकार की नीतियों में अंतर्विरोध उभरता है, तब-तब यह प्रश्न उठ खड़ा होता है। इससे यह तो साफ होता ही है कि लेखक समुदाय सरकार के चाटुकारों का समुदाय नहीं है। वह कुछ मूल्यों और नीतियों के आधार पर सहयोग या असहयोग का रुख अपनाता है। सहयोग की स्थितियों में लाभ-लोभ की सीमाएं भी आ मिलती हों, यह संभव है। लेकिन इसी आधार पर कोई सरकार यह नहीं मान सकती कि लेखक तो लाभ के लिए आतुर और लालायित है, इसलिए जैसा चाहो करो, उसका समर्थन मिलेगा ही!
कभी-कभी विरोध और बहिष्कार के अन्य कारण भी होते हैं। भोपाल गैसकांड के बाद फोर्ड फाउंडेशन के आर्थिक सहयोग को लेकर भारत भवन का विरोध क्रमश: तेज होता गया। इसमें सरकार से अधिक एक संस्था की नीति का प्रश्न था। लेकिन यहां यह स्मरण करना उचित है कि आजादी के बाद सबसे पहले यह बहस शुरू हुई प्रगतिशीलों और प्रयोगवादियों के बीच ‘सेठाश्रय’ बनाम ‘राज्याश्रय’ को लेकर। कुछ प्रगतिशील लेखक सरकारी संस्थाओं में नियुक्त हुए थे और कुछ प्रयोगवदी लेखक निजी संस्थानों में। यह बहस सरकार से लेखकों के सीधे विवाद का द्योतक न था। इसका वैचारिक स्रोत था नेहरू के प्रति कुछ मार्क्सवादियों का सकारात्मक और लोहियावादियों का नकारात्मक रुख।
सरकारी संस्थाओं के बहिष्कार की व्यापक स्थिति बनी आपातकाल में, जब अनेक लेखकों ने, अधिकतर प्रगतिशील लेखकों ने, विरोध का स्वर ऊंचा किया- किसी ने पत्रिका के पृष्ठ काले छापे, कोई जेल गया। लेकिन तब बहिष्कार को लेकर यह बहस नहीं हुई। शायद दो कारणों से।
आपातकाल की बंदिशों के कारण; और दक्षिण-वाम सब तरह के लेखकों में आपातकाल के बारे में लगभग आम सहमति के कारण। पिछले कुछ दिनों से सहयोग बनाम बहिष्कार का मुद्दा फिर प्रासंगिक हो गया है। कभी असहिष्णुता के प्रश्न पर, कभी ‘देशद्रोह’ के मुद्दे पर। इस स्थिति में विभिन्न संस्थाओं के प्रति सहयोग और बहिष्कार के सवाल पर एक सैद्धांतिक नजरिया आवश्यक हो जाता है।
संस्थाएं किसी एक प्रकार की नहीं हैं। सरकारी, संवैधानिक, स्वायत्त, जनतांत्रिक, सार्वजनिक क्षेत्र की और निजी, अनेक प्रकार की संस्थाएं हैं, उनके बारे में एक समान रुख अपनाना मुश्किल है। फिर भी, एक सैद्धांतिक आधार के बिना यह मसला निरंतर समस्या पैदा करता रहेगा। सर्वसम्मति तो शायद ही बने, लेकिन व्यापक सहमति बनाने का प्रयास किया जाना आवश्यक है।
अक्सर देखा जाता है कि विरोधी विचारधारा के लेखक नहीं, सहयोगी धारा के लेखक ही बहिष्कार न करने वाले रचनाकार का विरोध करते हैं। हिंदी के मूर्धन्य आलोचक और विचारक रामविलास शर्मा को दो अवसरों पर ऐसी आलोचना का शिकार होना पड़ा। पहला अवसर था दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर में हिंदी जाति की अवधारणा पर दो दिवसीय संगोष्ठी में उनके शामिल होने का, दूसरा था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पत्र ‘पांचजन्य’ में उनके साक्षात्कार का। ‘पांचजन्य’ ने साक्षात्कार में कई मनमाने जोड़-तोड़ किए थे, जिसका ब्योरा उनके लिखित साक्षात्कार की मूल प्रति के आधार पर ‘आज के सवाल और मार्क्सवाद’ में कर दिया गया था। खुद रामविलासजी ने अपनी आत्मकथा में इस बारे में स्पष्ट किया था: ‘…लेनिन ने सिखाया था कि जहां प्रतिक्रियावादी हों, वहां भी मार्क्सवादियों को अपनी बात कहनी चाहिए।’ इस बात का महत्त्व इसलिए है कि अक्सर ऐसे विरोध का स्वर उठाने वालों में मार्क्सवाद से प्रभावित लेखक होते हैं। और, मतिमूढ़ सत्ता प्रतिष्ठान द्वारा अपना विरोध करने वाले सभी लेखकों को एक सपाटे में मार्क्सवादी करार दिया जाता है।
यह सही है कि सत्ता परिवर्तन के साथ कुछ सरकारें अपनी संस्थाओं पर मनचाहे लोगों को बैठाती हैं, भले उनमें संबंधित क्षेत्र की उल्लेखनीय योग्यता न हो। ऐसे पदाधिकारी खुद ही बहुत-से संस्कृतिकर्मियों, खासकर साहित्यकारों को, दूर रखते हैं। लेकिन कभी-कभी लेखक भी ऐसे लोगों के कारण संस्थाओं का बहिष्कार करते हैं। क्या व्यक्तियों के कारण इस तरह का विरोध उचित है? लेखकों के अलावा किसी और क्षेत्र के संस्कृतिकर्मी ऐसा बहिष्कार नहीं करते। रूपंकर कलाओं में शायद कलाकार को लेखकों से अधिक स्वतंत्रता है। वे ‘असहिष्णुता’ का विरोध भी कर सकते हैं और संस्थाओं के कार्य में शामिल भी हो सकते हैं, किसी ‘अयोग्य’ व्यक्ति की नियुक्ति का विरोध भी कर सकते हैं और नियुक्ति करने वाले के कार्यक्रम में अतिथि भी बन सकते हैं। पर साहित्य में ऐसा नहीं होता। यहां लेखक का शील अधिक संवेदनशील है। ‘अवसरवाद’ का तमगा कौन ढोए! अच्छा है, बहिष्कार करो।
इस प्रश्न पर निर्णय की सीधी कसौटी है- लेखक द्वारा किसी संस्था में शामिल होने के लिए कोई समझौता किया गया है या नहीं? अगर अपने विचार, उद्देश्य या सिद्धांत की बलि चढ़ाई गई है, विरोधी बातों पर या जनहितकारी प्रश्नों पर या अनाचार के मामलों पर ‘समझदार मौन’ अपनाया गया है, तब वह हिस्सेदारी निंदनीय है। इसके अलावा बहिष्कार की नीति के बड़े घातक परिणाम होते हैं। संस्थाएं अक्सर अक्षम और निम्नकोटि की प्रतिभाओं के हाथ में केंद्रित हो जाती हैं। परिणामस्वरूप सांस्कृतिक विकृतियां उत्पन्न होती हैं, उन संस्थाओं का जनतांत्रिक स्वरूप नष्ट होता है, जनता का संस्कृति से ही मोहभंग हो जाता है।
कलाकारों को सरकारी या अर्धसरकारी सांस्कृतिक संस्थाओं की स्वायत्तता के लिए संघर्ष करना चाहिए ताकि उनका नियंत्रण संस्कृतिकर्मियों के हाथ में ही रहे, सरकार की निर्णायक दखलंदाजी न होने पाए। कारण, ये सभी संस्थाएं आखिरकार जनता के पैसों से चलती हैं। जिस तरह राजनीतिक संस्थाएं राजनेताओं के नियंत्रण में रहती हैं, उनमें संस्कृतिकर्मियों का दखल नहीं होता, उसी तरह सांस्कृतिक संस्थाओं को संस्कृतिकर्मियों के नियंत्रण में रहना चाहिए, उनमें राजनेताओं का अवांछित दखल नहीं होना चाहिए। इस संघर्ष को वे बाहर रह कर नहीं चला सकते। इसलिए विरोध के और तौर-तरीके अपनाने चाहिए, बहिष्कार कोई अच्छा तरीका नहीं है।
प्राय: देखा जाता है कि जो वामपंथी लेखक संगठन गैर-वामपंथी सरकारों से या अर्ध-सरकारी संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों या निजी न्यासों से आर्थिक स्रोत जुटाने में संकोच नहीं करते, वे सरकारी संस्थाओं के साथ लेखकों के व्यक्तिगत संबंध पर उंगली उठाते हैं। उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए कि अगर वामपंथी पार्टियां अपनी नीतियों का अंतर बनाए रखते हुए संसद में और विभिन्न सरकारी-गैरसरकारी समितियों में दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों के साथ काम कर सकती हैं, तो कोई लेखक या लेखकों का कोई समूह अपने सिद्धांत और अपनी स्वतंत्रता कायम रखते हुए सरकारी, अर्ध-सरकारी, स्वायत्त या सार्वजनिक संस्था से जुड़ कर काम क्यों नहीं कर सकता।
अगर जनतांत्रिक प्रणाली में विभिन्न राजनीतिक संगठन साथ चलने को बाध्य हैं और उसे सैद्धांतिक रूप में भी वे अस्वीकार नहीं करते, तब बहिष्कार का सैद्धांतिक और विचारधारात्मक आधार कहां बचा? दुनिया के एकध्रुवीय होने से पहले साम्राज्यवादी पूंजी से जुड़ी संस्थाओं का बहिष्कार संभव था। अब यह संभव नहीं है। वामपंथी सरकारें भी नव-उदारवादी नीतियां अपना रही हैं। चीन में नहीं, भारत में भी। उत्तर-सोवियत विश्व की यही वास्तविकता है कि नव-उदारवादी आर्थिक नीतियों के परिणाम से साहित्य-संस्कृति का अछूता रहना अकल्पनीय है। उसमें भी, साहित्य के सामने समस्या अधिक है, क्योंकि वह भाषा पर आधारित है और विचारधारा सबसे स्पष्ट रूप में (भाषा के माध्यम से) साहित्य में ही अभिव्यक्त होती है। इन परिस्थितियों में अगर संभव है तो विरोध के नए तौर-तरीके खोजे और अपनाए जाने चाहिए, बहिष्कार का तरीका आज अप्रासंगिक और बासी हो चुका है।
हम विचारधारा के लिहाज से अपने अनुकूल लोगों से संवाद तो करते ही हैं, जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं उनसे भी संवाद करें, ऐसा जनतंत्र का तकाजा है। अपने पांव अपनी जमीन टिकाए रख कर विरोधी विचारधारा के मंच पर भी बोलने में हर्ज नहीं है।
सवाल है कि लेखकों को सरकारी या सरकार पोषित संस्थाओं में जाना चाहिए या नहीं? उन्हें इन संस्थाओं से सम्मानित-पुरस्कृत होना चाहिए या नहीं? इन प्रश्नों का कोई माकूल जवाब देना किसी के लिए भी कठिन है। इसलिए कि लोकतंत्र में हर मंच या संस्था अंतत: जनता की और जनता के लिए है। किसी राजनीतिक दल की सरकार आएगी और जाएगी, लेकिन संस्थाएं बरकरार रहेंगी। फिर भी जब-तब संस्थाओं के बहिष्कार की खबरें आती रहती हैं। कभी भारत भवन, भोपाल के कार्यक्रमों के बहिष्कार का अभियान लेखकों के एक वामपंथी गुट की ओर से चला था। बावजूद इसके कुछ लेखकों को छोड़ कर बाकी लेखक वहां जाते-आते रहे। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मार्गरेट थैचर के हाथों लेने से इनकार करने की मांग भी कुछ लेखकों ने की थी। नागार्जुन से भी इंदिरा गांधी के हाथों पुरस्कार न लेने के लिए कहा गया था। राजेंद्र यादव को बिहार सरकार का शिखर सम्मान मिला तो वामपंथी लेखकों के धड़े ने विरोध किया था। किसी घटना विशेष को ध्यान में रख कर हिंदी अकादेमी और साहित्य अकादेमी का कुछ लेखकों ने विरोध/ बहिष्कार किया, लेकिन किसी लेखक ने ऐसी मांगों के बावजूद पुरस्कार/ सम्मान लेने से मना किया हो या लेखकों के बड़े समुदाय ने किसी संस्था का बहिष्कार किया हो, इसकी याद मुझे नहीं है।
एक लोकतांत्रिक देश में कोई संस्था न तो किसी दल विशेष की होती है और न किसी सरकार विशेष को इनके काम-धाम में अनावश्यक दखल देना चाहिए। इन संस्थाओं के गठन के वक्त आदर्श यही रहा होगा। लेकिन सरकारों के बदलने पर सम्मान/ पुरस्कारों के चयन में कभी-कभार बाहरी दबाव न रहते होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में फिर वही प्रश्न कि लेखकों को सरकार पोषित संस्थाओं के मंचों पर जाना चाहिए या नहीं?
आज का लेखक कबीर, कुंभनदास, तुलसीदास आदि की तरह न तो जीवन जीता है और न कोई उससे वैसी अपेक्षा करेगा। आज के साहित्यकार का घर-परिवार है; उसके लिए उसे कोई न कोई नौकरी या काम करना है। वह जो लिखता है, उसके प्रकाशन, प्रचार-प्रसार के लिए किसी न किसी निजी या सरकार पोषित संस्था की दरकार है। अगर उसने जीवन भर लिखने-पढ़ने का ही काम किया है, तो उसकी सहज मानवीय कमजोरी हो सकती है कि वह साहित्यिक संस्थाओं द्वारा सम्मानित भी हो। लेखकों को पुरस्कृत-सम्मानित करने का काम सरकार पोषित संस्थाएं करती भी रही हैं। अपनी राजनीतिक धारा के लेखकों का भी और अपनी विरोधी राजनीतिक धारा के लेखकों का भी। आज जब कुछ भी राजनीति से परे नहीं है, तब किसी लेखक का किसी सरकार पोषित संस्था द्वारा सम्मान राजनीति से परे नहीं माना जाएगा। भले वह फौरी नहीं, दूरगामी राजनीति हो। तब क्या लेखक को अपनी ही राजनीतिक धारा की सरकार के समय में सरकार पोषित संस्थाओं में जाना चाहिए और सम्मानित होना चाहिए?
किसी लेखक या विपरीत धारा के लेखक का कहीं सम्मानित किया जाना किसी भी लोकतांत्रिक समाज के मुक्त मन का परिचायक है। अपनी आलोचना किए जाने का माहौल लोकतंत्र में विश्वास करने वाली सरकारें ही देती हैं। जो सरकारें विचारधारा की तानाशाही के आधार पर सत्ता में आती हैं वे लेखकों की अभिव्यक्ति पर पहरा बिठा देती हैं। नात्सी जर्मनी में भी लेखकों-कलाकारों को यातनाएं झेलनी पड़ीं और स्तालिनकालीन सोवियत रूस में भी। ऐसी सरकारों द्वारा पोषित संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जाना कोई स्वतंत्रचेता लेखक कैसे पसंद करेगा? करना भी नहीं चाहिए। इन देशों में भी लेखकों-कलाकारों ने तानाशाही का विरोध किया था और यातनाएं झेली थीं। अपने देश में भी आपातकाल में जब अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध लगा तो लेखकों के व्यापक समुदाय ने उसका विरोध किया था। हालांकि सीपीआइ/ प्रलेस से जुड़े लेखक तब या तो आपात्काल के समर्थन में थे या चतुराई पूर्वक चुप थे।
कोई लेखक जब किसी संस्था द्वारा सम्मानित होता है तो अंतत: उसकी रचना सम्मानित होती है। रचना के पीछे लेखक की अपनी जीवन-दृष्टि होती है; रचना में निहित उसके मौन या मुखर विचार होते हैं। जेनुइन लेखक सम्मान से अधिक अपनी रचना के साथ होता है। संस्थाएं ऐसे लेखकों का सम्मान करके खुद सम्मानित होना चाहती हैं; अपना उदार चेहरा प्रस्तुत करना चाहती हैं। कई बार सत्ताधारी दल ऐसा करके लेखक से अपने अनुकूल बनने की अपेक्षा भी रखता है। सरकार पोषित संस्थाओं के मंचों पर जब ऐसे लेखकों को बुलाया जाता है तो यह भी अपेक्षा होती है कि लेखक संस्था या सत्ता के लिए असुविधाजनक वक्तव्य न दे। अवसरवादी लेखक अनुकूलन के शिकार होते भी हैं, लेकिन जेनुइन लेखक वही बोलता है, जो साहित्य का स्वाभाविक धर्म होता है। कहने की जरूरत नहीं कि एक लेखक का स्वाभाविक धर्म जनता की पीड़ा का सही चित्रण है, उस पीड़ा का पक्षधर होना है। इसलिए किसी लेखक का असली काम है सत्ता के विपक्ष में होना।
राममनोहर लोहिया कहते थे कि उनके दल की भी सरकार बनी तब भी वे विपक्ष की भूमिका में रहना पसंद करेंगे; ताकि अपने दल की सरकार के प्रति आलोचनात्मक रुख रख सकें। आज के दिन कौन-सा दल या कौन-सा नेता ऐसे आदर्श को जीना पसंद करेगा, कहना कठिन है, लेकिन एक लेखक को तो सतत विपक्ष में होना ही चाहिए। जो वह लिखता है उसमें उसका विपक्षी तेवर साहित्यिक भाषा और सलीके के साथ साफ-साफ दिखना चाहिए। जब वह किसी मंच पर बोलने के लिए निमंत्रित किया जाता है, तब उसे वही बोलना चाहिए, जो उसका अपना पक्ष है। यह सुविधा और वह माहौल वह मंच मुहैया कराता है, तो उसे अपनी बात बेलाग-लपेट कहने से हिचकना नहीं चाहिए। अगर वह मंच उसे उसकी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं देता तो निश्चित रूप से उसे उसका बहिष्कार करना चाहिए।
वाद-विवाद-संवाद की गुंजाइश जनतांत्रिक समाज में ही होती है। हम विचारधारा के लिहाज से अपने अनुकूल लोगों से संवाद तो करते ही हैं, जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं उनसे भी संवाद करें, ऐसा जनतंत्र का तकाजा है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो अपने से असहमत व्यक्ति के सामने सोच-विचार के लिए कोई दूसरा वैचारिक प्लेटफार्म और दूसरी जीवन-दृष्टि प्रस्तुत करने के दायित्व से अपने को मुक्त कर लेते हैं। अपने पांव अपनी जमीन टिकाए रख कर विरोधी विचारधारा के मंच पर भी बोलने में हर्ज नहीं है। संवाद से वे डरते हैं, जिनके पास दूसरों को प्रभावित करने वाली न तो दृष्टि होती है और न ही चरित्र।
किसी दल की सरकार या किसी संस्था के किसी काम से विरोध हो तो उसका बहिष्कार उसके विरोध का एक तरीका हो सकता है। सामंती समाज में जब किसी व्यक्ति का आचरण अशोभनीय होता था, तो जाति बहिष्कृत करके समाज उसे सजा देता था। लोकतांत्रिक समाज में बहिष्कार विरोध का अंतिम उपाय होना चाहिए। जब तक और जहां तक संभव हो संस्थागत मंच का उपयोग अपना पक्ष रखने में लेखकों को करना चाहिए। इसलिए कि लोकतांत्रिक समाज में सरकार पोषित कोई संस्था किसी एक व्यक्ति, दल या विचारधारा की जागीर नहीं होती। मुक्तिबोध के शब्दों में यह दुनिया अगर कचरे का ढेर नहीं है, तो किसी कुक्कुट को उस पर बैठ कर बांग देने और मसीहा बनने देने से रोकने का आखिर लेखकों के पास उपाय क्या है? सरकार पोषित मंचों पर मौका मिलने पर तब तक बोलना चाहिए जब तक उसकी उदारता का छद्म बेपर्द न हो जाए।