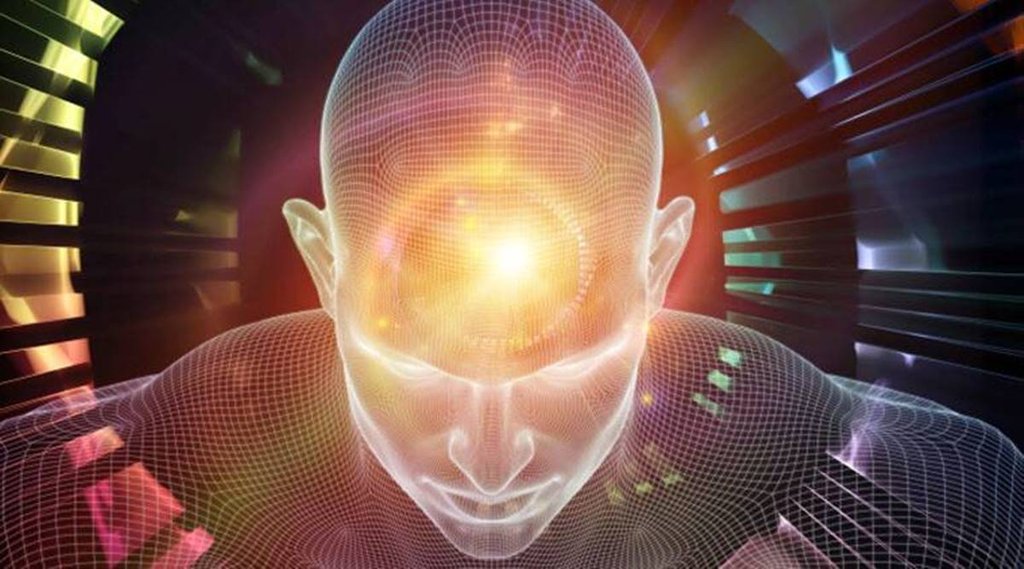अगर एक गधे को बराबर की भूख और प्यास लगी हो और उसे घास और पानी के ठीक बीच में खड़ा कर दिया जाए तो वह पहले अपनी भूख मिटाएगा या फिर प्यास बुझाएगा? दर्शनशास्त्रियों का कहना है कि वह दोनों के बीच में फैसला नहीं कर पाएगा। असमंजस में रहेगा कि घास खाऊं या पानी पीऊं और भूख-प्यास से मर जाएगा।
दर्शनशास्त्र में ऐसे गधे को बुरीदन डंकी कहते हैं। जीन बुरीदन चौदहवी शताब्दीं के फ्रेंच फिलॉसफर थे, जिन्होंने व्यवहार के विरोधाभास को दिखाने की लिए एक काल्पनिक गधे की चर्चा की थी। उनसे पहले ग्रीक दर्शनशास्त्री अरस्तू ने गधे के बजाय ऐसी स्थिति का वर्णन आदमी के संदर्भ में किया था। उन्होंने यह उद्धारण अपने विरोधियों के उस दावे के जवाब में दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार तो जरूर है, पर स्थिर है और इसलिए उस पर हर दिशा से एक-सा दबाव रहता है। मनुष्य इन दबावों के बीच में फंसा रहता है, पृथ्वी की वजह से स्थिर रहता है। अरस्तू ने खाऊं या पीऊं के अनिर्णय की बात करके पृथ्वी की स्थिरता की परिकल्पना को खारिज कर दिया था और कहा था कि वह अपनी धुरी पर घूमती है।
दर्शनशास्त्र की बात जो भी हो, पर हम अपनी जिंदगी में अक्सर बुरीदन वाले गधे की तरह व्यवहार करते हैं। यह करूं या वह करूं की ऊहापोह में फंस जाते हैं और हालांकि काल्पनिक गधे की तरह हम भूख और प्यास से मर तो नहीं जाते, पर कई बार दो एक समान आकर्षण वाले विकल्पों के बीच में ऐसे बंध जाते हैं कि अपने लक्ष्य से चूक जाते हैं।
आम जिंदगी से छोटा-सा उदहारण ले लीजिए। कल मुझसे पूछा गया कि रात के खाने में मैं सब्जी परांठा खाऊंगा या फिर सब्जी रोटी। मुझे परांठा उतना ही पसंद है जितनी कि रोटी। दोनों का आकर्षण एक बराबर है। मैं सोच में पड़ गया था। पहले गरम-गरम खस्ता परांठे का स्वाद याद आया और फिर करारी, घी से चुपड़ी हुई रोटी ने मेरे मुंह में पानी ला दिया। कभी लगता था कि रोटी के लिए हां कर दूं, पर हां निकलने से पहले ही परांठा याद आ जाता था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं किसका स्वाद रात के खाने में लूं। रसोइया मुझे बड़ी देर तक तकता रहा और फिर चिड़चिड़ा कर बोला, आज कुछ मत खाइए। भूखे सो जाइए।
वास्तव में हम विकल्पों की दुनिया में रहते हैं। विकल्प प्रतिस्पर्धात्मक होते हैं। एक विकल्प को त्याग कर दूसरे को चुनना हमारी मुक्त इच्छा (फ्री विल) को दर्शाता है। मुक्त इच्छा का प्रयोग हम अक्सर तर्क के आधार पर करते हैं। अगर हमारे पास दो नौकरियों की पेशकश है, तो हम दोनों के फायदे और नुकसान की तर्कपूर्ण तुलना करते हैं और जिसमें हमें सबसे ज्यादा फायदा दिखता है उसको चुन लेते हैं। पर अगर हर तरह से दोनों ही प्रस्ताव एक जैसे हों तो हम क्या करेंगे?
मेरी रोटी और परांठे के बीच की जद्दोजहद तब खत्म हुई जब रसोइए ने बताया कि उसने सब्जी में रसेदार प्याज के आलू बनाए हैं और साथ में भिंडी की सूखी सब्जी है। नई जानकारी मिलते ही मैंने तपाक से अपना फैसला सुना दिया था- परांठा बना दीजिए। जुबान पर चढ़ा आलू, भिंडी और परांठे का रुचिकर स्वाद रोटी पर हावी हो गया था। स्वाद फैसला लेने का संदर्भ बन गया था। मेरी स्वतंत्र इच्छा परांठे के पक्ष में थी। कोई दूसरा होता तो उसकी इच्छा शायद रोटी होती। और कोई तीसरा, जिसको दोनों का स्वाद नहीं पता है, वह विकल्पों के बीच उलझा रहता और किसी से पूछ कर उसकी राय के अनुसार एक चीज को चुनता। या फिर सिक्का उछाल कर फैसला करता।
तर्क, संदर्भ और स्मरण की सीमाएं हैं। इनका प्रयोग जरूरी तो है, पर इनके आगे सिक्का उछालना ही काम आता है। क्रिकेट को ही ले लीजिए। दो टीमें हैं, पहले कौन बल्लेबाजी करेगा, इसका फैसला किस तर्क पर हो सकता है? मैदान कैसा है के तर्क पर या मौसम के? या फिर किस टीम ने अब तक कितने रन बनाए हैं? दोनों तरफ के खिलाड़ी आपस में बहुत से यह तर्क भी दे सकते हैं कि उनके लिए बल्लेबाजी करना क्यों आवश्यक है। पर खेल फौरन शुरू करने के लिए सिक्का उछालना सबसे अच्छा विकल्प है। अनिश्चिता तुरंत समाप्त हो जाती है।
वैसे, अगर देखा जाए तो हर पल हम अपनी मुक्त इच्छा का प्रयोग सिक्के की स्वतंत्रता के बल पर करते हैं। हमारे पंचानबे प्रतिशत फैसले सहज ज्ञान या सहज बोध के आधार पर होते हैं। कुछ ही ऐसे फैसले होते हैं, जिन पर हम गहराई से सोचते हैं और वे तर्कसंगत हो सकते हैं। बाकी में संदर्भ, स्मरण और सहज बोध होता है। ऐसे सहज फैसले हमारे जीवन की दिशा और दशा हर पल निर्धारित करते हैं। यह हमारी मुक्त इच्छा का साक्ष्य है। सिक्के की चित और पट हमारी जिंदगी का नक्शा बना देती है।
मनुष्य हो या गधा, वह विकल्पों के बीच एक बार ठिठक तो सकता है, पर प्रतिस्पर्धात्मक विकल्प उसको इतना नहीं बांध सकते हैं कि कशमकश में उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाए। इसके होने के बहुत पहले वह एक बेतरतीब फैसला लेगा और अगर वह घास का विकल्प चुनता है, तो पानी से दूर होता जाएगा और घास के पास पहुंच जाएगा। खाने के बाद पानी की तरफ लौटने का विकल्प वह नए तरीके से चुनेगा। वास्तव में बेतरतीब फैसले ऊहापोह से बचने के लिए सहज बोध का तर्क हैं।
यह बात व्यक्ति और समाज दोनों पर एक तरह से लागू होती है। व्यक्तियों से सामाजिक समूह बनता है और जब बहुत सारे लोग एक से बेतरतीब फैसले करने लगते हैं तो वे समाज की दिशा तय कर देते हैं। साधारण संदर्भ और बोध सार्वजनिक ज्ञान बन जाता है और बेअक्ली नए सिक्के की तरह चल निकलती है।
मशहूर शायर इकबाल ने जरूर कहा है ‘गुजर जा अक्ल से आगे कि ये नूर, चरागां-ए-राह है मंजिल नहीं है’, पर मंजिल कौन-सी होगी और उस तक कैसे पंहुचा जाएगा का निर्धारण करने के लिए चरांगा-ए-राह को साथ रखना जरूरी है। गधा घास और पानी के बीच फैसला कर के एक तरफ अपनी जान बचा तो सकता है, पर दूसरी ओर ज्यादा खा-पी कर बीमार पड़ सकता है। कितना खाना है का फैसला न कर पाने की वजह से उसकी जान पर बन आ सकती है। गधे के लिए भी विवेक जरूरी है।