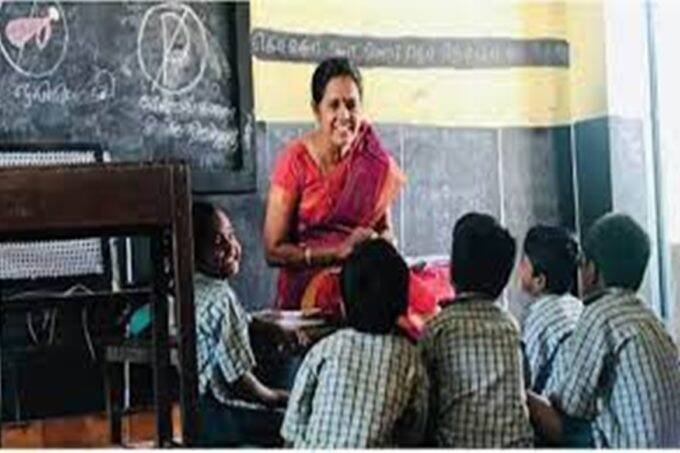गांधीजी ने 1937 में पहली बार औपचारिक रूप से शिक्षा की एक अभिनव व्यवस्था प्रस्तुत की थी। इसे बेसिक शिक्षा या बुनियादी तालीम के नाम से जाना जाता है। आचार्य विनोबा भावे इसे ‘नित्य नई तालीम’ कहते थे। नित्य शब्द के जोड़े जाने से यह स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा की गतिशीलता ही उसकी प्राणदायिनी शक्ति है : ‘नित्य नई तालीम का मतलब है: जो कल थी, वह आज नहीं है और जो आज है, वह कल नहीं रहेगी, जैसे नदी का पानी। वैसे ही रोज के अनुभव के आधार पर जो नित्य बदलती रहती है, वह है नित्य-नई तालीम’।
बदलाव और विकास मानव सभ्यता की एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, जिसका मूल आधार मनुष्य की प्रकृति को जानने, समझने और उसका उपयोग करने की प्रवृत्ति है। इसी से मानवता का ज्ञान भंडार बढ़ता जाता है। समाज, जो आज है, कल बदल चुका होगा। सच्ची तालीम या शिक्षा, वही है जो व्यक्ति को व्यक्तित्व प्रदान कर सके और वह सामाजिक संरचना को नया कलेवर देने में सक्षम हो।
समय के साथ ज्ञानार्जन की प्रक्रिया का वर्तमान स्वरूप- शिक्षा व्यवस्था और नीतियां- हमारे समक्ष उपस्थित हैं, इसकी गतिशीलता परिवर्तन को दिशा देती है। मानव जीवन को सार्थक, सहज, सम्यक और गरिमापूर्ण बनाने में शिक्षा के प्रचार-प्रसार तथा गुणवत्ता संवर्धन का कोई अन्य विकल्प नहीं है।
यूनेस्को ने 1996 में इक्कीसवीं सदी के शिक्षा स्वरूप के लिए जो प्रतिवेदन तैयार कराया था, उसमें शिक्षा को ‘आवश्यक अलभ्य’ लक्ष्य- नेसेसरी यूटोपिया- कहा गया था। शिक्षा हर समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन मनुष्य सबसे पहले उसी में हर समस्या का समाधान ढूंढ़ता है।
इसी प्रक्रिया में शिक्षा व्यवस्था का नया स्वरूप निखरता है। वह शिक्षा ही है, जो संस्कारों को गढ़ती है, जिन्हें पीढ़ी-दर-पीढ़ी संवारा जाता है, मानव के भविष्य को सुनहरा बनाने के प्रयासों में यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण कड़ी है। जब मनुष्य की तार्किक क्षमता और संवेदनात्मक समझ बढ़ती है, तभी वह दास प्रथा, जाति और नस्लभेद, रंगभेद जैसे अस्वीकार्य प्रचलनों से अपने को मुक्त कर पाता है।
इस पृष्ठभूमि को समझने के लिए अत्यंत सार्थक और व्यावहारिक उदाहरण हैं महात्मा गांधी के शैक्षिक विचार, और उनके द्वारा प्रतिपादित शिक्षा की प्रणाली, जिसे पश्चिमी सभ्यता की चमक-दमक में लगभग पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया था। वास्तव में उनका चिंतन भारत की उनकी गहरी समझ पर आधारित था।
विश्व में शिक्षा की विकसित व्यवस्थाएं सिद्धांत रूप में स्वीकार करती हैं कि शिक्षा ही मानव निर्माण की कुंजी है। प्रत्येक मनुष्य के अंतरतम में निहित असीम संभावनाओं और क्षमताओं का प्रस्फुटन शिक्षा द्वारा ही संभव हो सकता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में पूरी तरह से सफल होने के लिए यह स्वीकार करना भी आवश्यक है कि यह तभी संभव होगा जब शिक्षा-व्यवस्था सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से पूरी तरह जुड़ी हो, और उसके द्वारा तैयार किया जाने वाला व्यक्ति सामाजिक अनुशासन को समझता हो, और उसके अंतर्गत अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्वाह के लिए प्रतिबद्ध हो।
वह स्वयं उसका सक्रिय सदस्य बन कर परिवर्तन का भागीदार बन सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि परिवार, समाज और राज्य-व्यवस्था यानी सरकार का संयमित और समेकित दृष्टिकोण नई पीढ़ी के समुचित निर्माण के उत्तरदायित्व को निभाने के लिए एकजुट होकर समर्पित हो, उचित संसाधन उपलब्ध कराए तथा साथ ही शिक्षा की गतिशीलता को सही दिशा और उचित मार्गदर्शन देने को तैयार हो, और व्यावहारिक स्तर पर इसके क्रियान्वयन के प्रति प्रतिबद्ध हो।
जब स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य के अंतरतम में मौजूद पूर्णता का प्रकटीकरण है, तब वे हमारे समक्ष एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण दर्शन प्रस्तुत कर रहे होते हैं: शिक्षा का उद्देश्य, स्वरूप और सारी प्रक्रिया व्यक्ति के सर्वोत्तम गुणों को प्रस्फुटित करने का प्रयास करती रहे।
यह तभी होगा जब व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक क्षमताओं का सहजता से विकास होता रहा हो। वह शिक्षा तो अपूर्ण ही मानी जाएगी, जिसमें बच्चों की आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक शक्तियों के सामंजस्य-युक्त विकास पर समुचित अनुपात में ध्यान न दिया जा रहा हो।
इस समय सारा ध्यान केवल पाठ्य पुस्तकों के अध्याय याद करने और परीक्षा में उसी को लिख कर उत्तर देने और अधिकाधिक अंक प्राप्त करने तक सीमित हो गया है। देश के समक्ष बड़ी चुनौती यही है कि इसे कैसे बदला जाय!
यह समस्या नई नहीं है, यह गांधीजी के समक्ष भी थी। आज वह पहले से बड़े परिमाण में नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन करने वालों के समक्ष उपस्थित है। बुनियादी तालीम के पूर्ण मंतव्य को सभी पूरी तरह 1937 में नहीं समझ सके थे, और आज तो स्थिति यह है कि अनेक लोग उसे तकली तक सीमित मान लेते हैं, या केवल ग्रामीण इलाकों के लिए गांधीजी की एक योजना मान कर बदली हुई परिस्थिति के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त करार दे देते हैं।
ऐसे में यह संतोषप्रद स्थिति मानी जानी चाहिए कि नई शिक्षा नीति चरित्र निर्माण पर बल देती है, पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच कृत्रिम अलगाव को समाप्त करने की संस्तुति करती है और अपेक्षा करती है कि ज्ञान और कौशलों के बीच ‘हानिकारक ऊंच-नीच और परस्पर दूरी तथा असंबद्धता’ को दूर किया जा सकेगा।
अपेक्षा यह होगी कि क्रियान्वयन के समय इस संस्तुति को बुनियादी तालीम की आत्मा से जोड़ कर समझा जाए। इस पर सबसे अधिक ध्यान शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के पाठ्यक्रम निर्माण के समय दिया जान चाहिए।
शिक्षा के त्रिआयामी स्वरूप- शारीरिक, मानसिक और आत्मिक- की समझ अपेक्षित गहराई तक तभी व्यावहारिक स्वरूप लेगी, जब पूरी ईमानदारी से यह स्वीकार किया जाए कि ‘प्रत्येक देश की शिक्षा-व्यवस्था की जड़ें गहराई तक उस देश की संस्कृति से जुड़ी होनी चाहिए, साथ ही उसे नए ज्ञान के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए!’
गांधीजी के शैक्षिक विचार इसी श्रेणी में आते हैं। वे भारत की आवश्यकताओं की समझ को अपने में समेटे हुए हैं: ‘सच्चा विद्याभ्यास वह है, जिसके द्वारा हम आत्मा को, अपने आप को, ईश्वर को, सत्य को पहचानें। इस पहचान के लिए किसी को साहित्य-ज्ञान की आवश्यकता हो सकती है, किसी को भौतिक शास्त्र और किसी को कला की, पर विद्या मात्र का उद्देश्य आत्मा दर्शन होना चाहिए।’
शिक्षा हर व्यक्ति की आवश्यकता है, उसका नैसर्गिक अधिकार है, लेकिन भारत की शिक्षा-व्यवस्था के कुछ विशेष उत्तरदायित्व हैं, जो इतिहास ने उसे प्रदान किए हैं, इन्हें नई शिक्षा नीति स्वीकार करती है : ‘प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन या स्कूल के बाद के जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञानार्जन नहीं, बल्कि पूर्ण आत्मज्ञान और मुक्ति के रूप में माना गया था।
तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे प्राचीन भारत के विश्व-स्तरीय संस्थानों ने अध्ययन के विविध क्षेत्रों में शिक्षण और शोध के प्रतिमान स्थापित किए थे और विभिन्न पृष्ठभूमि और देशों से आने वाले विद्यार्थियों और विद्वानों को लाभान्वित किया था।’ इसके लिए उच्चतर स्तर की तार्किक और समस्या-समाधान जैसी क्षमताओं के विकास पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता को स्वीकर किया गया है।
गांधी जब उद्योग के सहारे लगभग सभी आवश्यक ज्ञान-कौशल, मानवीय मूल्य और चरित्र निर्माण की क्षमता को बुनियादी तालीम के अंतर्गत समाहित देखते थे, तब वे भारत की परंपरागत संवाद-संस्कृति पर अपना विश्वास प्रगट कर रहे होते थे। सार्थक शैक्षिक परिवर्तन के लिए यही सोच अपनानी होगी।