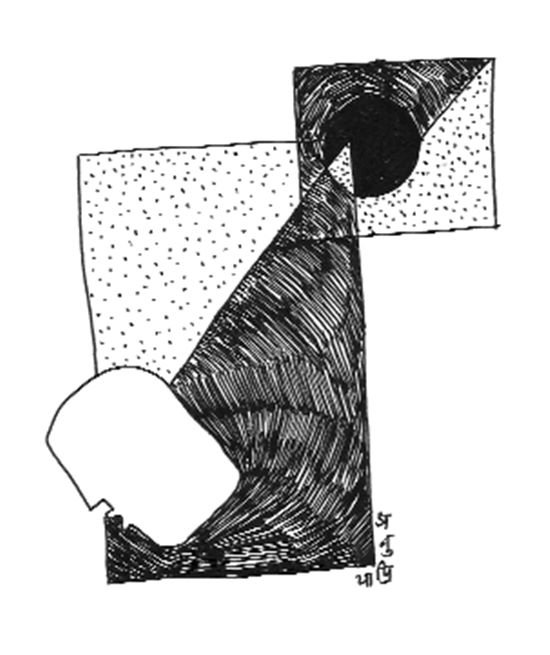विजय बहादुर सिंह
आधी से अधिक शताब्दी की अवधि में विचारधारा का वर्चस्व इतना अधिक बढ़ गया है कि लगता है, सृजन के सौंदर्य की तुलना में विचारधारा का तर्कवाद कहीं अधिक अहम है। तर्कशास्त्र अगर यह कहता है कि मनुष्य एक बौद्धिक पशु है, तो इतना मानता ही है कि मनुष्य में सभ्य होने तक तो ठीक, फिर भी अवशिष्ट अंशों तक अ-सभ्यता उसमें बची ही रह जाती है। कलाओं का जन्म उसके इसी बचे-खुचे अंश से संभव होता है। इसलिए कोई चाहे तो यह तर्क भिड़ा भी सकता है कि समस्त कलाएं उसके इसी अ-सभ्य मानस की उपज हैं। पर ऐसा कहना इतना आसान भी नहीं है। उसका कारण यह कि कलाएं विचारों के संसार से अधिक खूबसूरत मानी जाती हैं। यह अलग बात है कि बड़े-बड़े विचार-शास्त्री अपनी सत्ता कायम करने के लिए उन्हीं कलाओं से जूझने या फिर व्याख्या करने का पौरुष दिखाते रहते हैं। या कहें उनके भी स्वभाव की यह मांग और मजबूरी हो। ऐसों को कला-समीक्षक, सहृदय या फिर आलोचक कहते हैं।
मजेदार बात यह है कि कलात्मक कृतियां तो अपनी जगह रहती हैं पर ये समीक्षक-गण आपस में लड़ा करते हैं। एक कवि को दूसरे कवि या एक कथाकार-नाटककार को दूसरे से लड़ते हुए प्राय: नहीं देखा जाता, पर आलोचकों की तो पहले के आलोचकों की सत्ता ध्वस्त किए बगैर अपनी कोई पहचान नहीं बनती। इसके मूल में क्या है, अगर यह खोजा जाए तो कहना पड़ेगा कि उनकी विचारशीलता। ऐसे में एक पुराने आलोचक का यह कथन बेहद सुसंगत लगता है कि विचारों की एक सीमा होती है, पर भावों की कोई सीमा नहीं होती। कलाओं का क्षेत्र भावों का ही लीला क्षेत्र है। यह अलग बात है कि सर्जक या कलाकार की अपनी सीमाओं या फिर बौद्धिक सजगताओं के चलते कला की हानि हो बैठे। आधुनिक हिंदी कविता में इसके बड़े और प्रामाणिक उदाहरण राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हैं, जिन्होंने ‘साकेत’ जैसे प्रबंध काव्यों में ऐसी स्वाभाविकताओं तक से आंख चुराई, जिनके चलते लक्ष्मण-उर्मिला का मिलन युगल दंपत्ति का नहीं, भाई-बहन के मिलन जैसा लगता है। यहीं प्रसाद उनसे बाजी मार ले जाते हैं ‘कामायनी’ में। कुमार संभव और ‘मेघदूत’ में तो कालिदास इस भावात्मक साहस का अतिक्रामक अपवाद प्रस्तुत करते हैं।
गुप्तजी एक कलाकार के रूप में अपने नैतिक संस्कारों के भय के चलते या फिर दबाववश संवेदनों के उस शिखर का स्पर्श नहीं कर पाते, जिसे कालिदास या प्रसाद कर पाते हैं। न वैसा संतुलन रच पाते हैं जैसा कालिदास ने ‘अभिज्ञान शाकुंतल’ में किया है। गुप्तजी के काव्याचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की सोच और दृष्टि भी उन पर हावी थी। परिणामत: एक खास ऐतिहासिक दौर में वे राष्ट्रीय स्तर पर बेहद उपयोगी कवि साबित हुए। महत्त्व भी मिला। पर निराला भौतिक या दुनियावी स्तर पर विफल होकर भी सार्थक और महान माने गए। इसमें क्या शक कि गुप्तजी पर मर्यादा और नैतिकता की जो दृष्टि प्रबल थी, उसी से उनकी काव्य-साधना उस स्तर का स्पर्श न कर सकी, जिसे प्रसाद या निराला ने पा या छू लिया। यहां प्रयोजन बस इतना है कि क्या विचार या विचारधारा सिद्ध होकर ही कोई कवि या लेखक-सर्जक अहम सृजन कर सकता है? और कोई आलोचक इसी आधार पर उसकी श्रेष्ठता-अश्रेष्ठता या सिद्धता की सिफारिश या वकालत कर सकता है? मानता हूं, उसके मूल्यांकन में यह भी एक मानदंड होगा, पर मात्र इसी बल पर आलोचना के नैतिक फर्ज निभाए नहीं जा सकते। कला अगर एक सौंदर्य-व्यापार है, उसका रिश्ता मानव-मन के मौलिक और अपूर्व अनुभवों से है, तब इन अनुभवों की लीला का सौंदर्य-दर्शन क्या उसका प्राथमिक धर्म नहीं होना चाहिए? फिर उसे यह भी ध्यान में रखना होगा कि वह एक विशेष समाज-व्यवस्था और काल में रची गई कृति है। इनकी अनदेखी कर जो भी कुछ किया जाएगा, वह पंडिताई तो होगी, पर आलोचना नहीं। इसके बड़े उदाहरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जिन्होंने कबीर और सूर पर लिखते हुए जरूरत से ज्यादा पांडित्य और असंयमित भावाकुलता से काम लिया है। वे आलोचना कम, पर विदग्धता से अधिक काम लेते हैं।
इधर जबसे मार्क्सवादी विचाराधारा आई है, धीरे-धीरे विचारधारा वर्चस्वी आलोचना की सक्रियता बढ़ते-बढ़ते इतनी वादग्रस्त हो उठी है कि कतिपय आलोचक सृजन-सौंदर्य और उसके रहस्यों की छान-बीन करने के बजाय वैचारिक मतवादों और आग्रहों को ही कृति पर थोप-थाप कर अपने पौरुष का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा ही एक पौरुष-प्रदर्शन आज से साठ-पैंसठ साल पहले मुक्तिबोध ने किया था ‘कामयनी’ को लेकर। निस्संदेह वह एक असाधारण बौद्धिक विवेचन है, पर है अंतत: आधा-अधूरा ही, सो भी कई जबरिया आरोपों से युक्त और पूर्वपक्ष को सर्वथा नजरअंदाज करते हुए। मसलन, जिस रहस्यवाद से वे कामायनी और प्रसाद के प्रति बेहद आक्रामक हो उठे हैं, उसकी अपनी ओर से कोई व्याख्या वे नहीं करते, जिससे पाठक यह समझ सकें कि किस बिना पर वे विरोध कर रहे हैं। शुक्लजी तक तो फिर भी गनीमत थी कि वे उसे सिरे से खारिज नहीं कर रहे थे। पर मुक्तिबोध ने तो यह जहमत भी नहीं उठाई। अगर ठेठ सौंदर्य-सामग्री का अध्ययन कलावाद है, तो ठेठ विचारधारा या वाद के बल पर किया गया मूल्यांकन वाद-विशेष की राजनीति करना है। इसे और कोई आलोचना की राजनीति या राजनीतिपरक आलोचना कहे तो ठीक ही है। इन दिनों कुछेक अति उत्साही युवा मित्र यही कह रहे हैं।
इन सब कोशिशों में आलोचक रचना और रचनाकार को उसके समस्त संदर्भ और इतिहासबोध से काट कर देखता है। इतना ही नहीं, वह बेहद बर्बर तरीके से अपनी मनमानी पर उतर कर ऐसा आचरण करता है, जिसे मुक्तिबोध ‘पांडित्य का चंद्रत्व’ और ‘चिंतन की चतुरता’ कहते हैं। दरअसल, आलोचक का काम कलाकृति के अंर्तत्त्वों, उसके प्राणतत्त्वों, भावना, कल्पना को ‘हृदयगम करना’ है, ‘और एक विशेष दिशा की ओर प्रवाहित अंतर्धारा की गति को और उसकी अंतिम परिणति को सहानुभूतिपूर्वक अच्छी तरह’ समझ कर उसका विश्लेषण करना है। न कि दुश्मन की तरह कलाकार और कलाकृति को शत्रु-दुर्ग मान ध्वस्त करने पर उतर पड़ना है। गंभीर आलोचना कभी विचार-शून्य नहीं हो सकती। वह तभी दृष्टि-संपन्न मानी जाती है जब एक भरी-पूरी स्वीकार्य जीवन-दृष्टि और दर्शन उसके पीछे काम करता है। आलोचक स्वतंत्र है कि वह उक्त जीवन-दर्शन का समर्थन या विरोध करता हुआ उसकी लोक अहितकारी भूमिकाओं की ओर इशारा करे। पर यह सब करने का औचित्य तभी है, जब वह कलाकृति के तमाम सौंदर्य-रहस्यों की विधिवत खोज खबर कर ले। अपने आप से भी यह सवाल कर ले कि स्वयं उसकी आलोचना का सामाजिक और वैचारिक मूल्य किस कोटि का है? वह वाद-विशेष का प्रवक्ता मात्र है या देशकाल के संदर्भ में उसके शब्दों की कोई स्वीकार्यता भी है?
आलोचकों की आपसी वैचारिक मुठभेड़ें और असहमतियां भी संभव हैं, स्वयं आचोलक और रचनाकार की भी। रहस्यवाद पर प्रसाद और निराला आचार्य शुक्ल से भिड़ कर वैचारिक मुठभेड़ करते हैं। शुक्ल और प्रसाद की गंभीर बहसें हमारे साहित्यिक इतिहास की अमूल्य धरोहरें हैं। छायावादी कविता को लेकर आचार्य शुक्ल की दृष्टि के ठीक विपरीत राय लिए उनकी ही कक्षा के छात्र आचार्य वाजपेयी आते हैं। प्रबंध और प्रगति के मुद्दे पर नीतिवाद और भाववाद के मुद्दों पर भी बहसें की गई हैं। ये सब वैचारिक ही हैं। पर दोनों आलोचकों की जमीन शुद्ध साहित्यिक है। विचारहीन फिर भी नहीं। खतरा तब पैदा होता है जब वादग्रस्त हठवादी रवैया अपना कर लेखक को दुश्मन खेमे का मान कर, किन्हीं राजनीतिक मंसूबों के तहत उसकी छवि ध्वस्त की जाती है। यह तक नहीं सोचा जाता कि अंतत: उसने भरपूर मेहनत और ईमानदारी से अपना काम किया है। संभव है, वह कहीं चूका भी हो। पर आलोचक अगर केवल उसकी चूकों या दुर्बलताओं का निदर्शन करने निकल पड़ा हो, तब वह जितना नुकसान अपना करता है, उतना लेखक का नहीं। लेखक जिस तरह अपनी कलाकृति के बल पर जिंदा रहता है, आलोचक को भी अपनी ही करनी के बल पर जिंदा रहना है। कोई अन्य तो शायद ही कोई मदद कर पाए। जिस तरह सृजन एक सांस्कृतिक सुकर्म है, जीवन की गहरी समाधि में देखा गया सुस्वप्न है, आलोचना भी उसी तरह का एक सुकर्म है। देखना सिर्फ यह है कि उसका काम आने वाली पीढ़ियों के कितने योग्य होगा? होगा भी या नहीं?