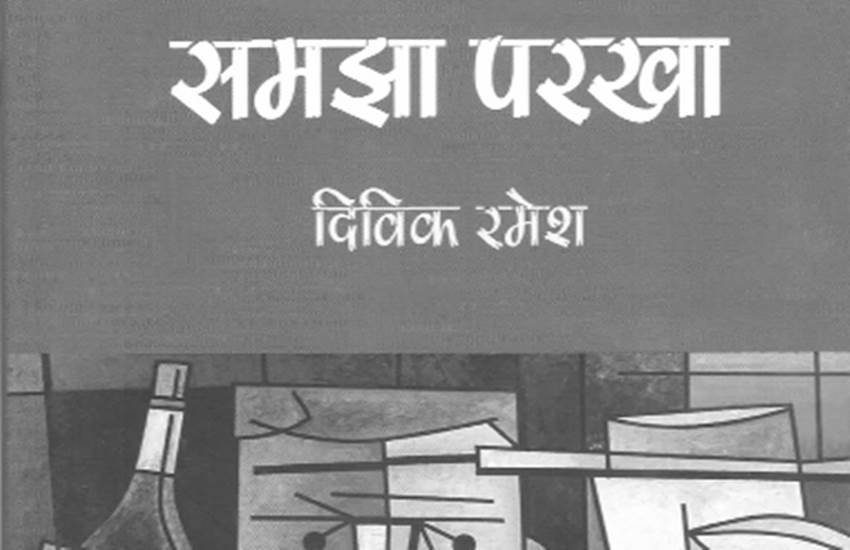आलोचना में संस्मरण और संस्मरण में आलोचना पढ़ने में ललित गद्य-सा सुख देती है। वैसे इसमें यह खतरा भी बना रहता है कि लेखक आत्मपरकता के बहाव में बहता चला जाए और वस्तुनिष्ठता की पतवार उसके हाथ से छूट न जाए। वरिष्ठ कवि दिविक रमेश की ऐसी ही रचनाओं का संग्रह है- समझा परखा। युवावस्था से ही वरिष्ठ लेखकों की निकटता के अनुभवों से लेखक की साहित्य को समझने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। उम्र की प्रौढ़ावस्था में उन्होंने कवि और साहित्य को परखने की प्रक्रिया में उससे काफी मदद ली है।
पुस्तक में शमशेर, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल और जगदीश चतुर्वेदी पर लिखे निबंधों में लेखक ने उनसे जुड़े अपने व्यक्तिगत अनुभवों का समावेश कर इन निबंधों को गहरी आत्मीयता प्रदान की है। इसके अलावा अज्ञेय और मुक्तिबोध के काव्य चिंतन पर भी लेखक ने ठहर कर और गहरी अंतर्दृष्टि के साथ लिखा है।
दिविक रमेश ने किसी भी रचनाकार को समझने के लिए उसके कृतित्व के साथ-साथ व्यक्तित्व को समझने पर भी खासा जोर दिया है। उनकी मान्यता रही है कि ‘रचनाकार यानी व्यक्ति और रचना में तालमेल होना चाहिए। कवि त्रिलोचन को भी मैंने कहते सुना है कि कवि जो लिखता है उसे वैसा ही होना चाहिए। मेरे खयाल में त्रिलोचन के व्यक्तित्व ओर उनकी रचना में जितनी अधिक नजदीकी है वह अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए कवि के व्यतित्व से परिचय पा लेना उनकी रचना और रचना दृष्टि को समझना और कवि की रचना को समझ लेना उनके व्यक्तित्व को समझ लेना आसान कर देता है।’
‘मेरे मित्र मेरे अग्रज: जगदीश चतुर्वेदी’ में भी जगदीश चतुर्वेदी के व्यक्तित्व का चित्रण करते हुए लेखक ने लिखा है: ‘ऐसे सच्चे व्यक्तित्व का प्रभाव रचना को भी सच्चा और प्रामाणिक बनाता है, भले आप रचना और रचनाकार के कुछ बिंदुओं को नापसंद करते हुए उनसे असहमत भी क्यों न हों।’ पूूरी पुस्तक में दिविकजी ने कविता लिखने और कवि होने के निजी अनुभवों का पूरा लाभ उठाया है, जो कहीं-कहीं आत्मप्रक्षेपण-सा लगता है, लेकिन कहीं भी आत्मश्लाघा की हद को नहीं छू पाता।
यथास्थान उन्होंने ऐसी बातों का भी जिक्र किया है, जो उनकी निजी काव्य-यात्रा से जुड़ी हैं। मसलन, उनके पहले कविता संग्रह ‘रास्ते के बीच’ के लिए कविताओं का चयन शमशेरजी ने किया था। इसी संग्रह पर केदारनाथ अग्रवाल ने इक्कीस पृष्ठों की समीक्षा लिखी थी। दिविकजी द्वारा संपादित पत्रिका ‘दिशाबोध’ के प्रवेशांक (जून 1978) में केदारनाथ अग्रवाल की कविताएं और कवि वक्तव्य छपा था। जगदीश चतुर्वेदी ने एक बड़ा पुरस्कार दिलाने में लेखक की मदद की थी। अकविता के निषेधवाद के विरोध में लेखक ने जगदीश चतुर्वेदी से मधुर संबंध होने के बावजूद अकविता के बाद के कवियों की कविताओं का संकलन ‘निषेध के बाद’ संपादित किया था।
उल्लेखनीय है कि 1972 में प्रकाशित जगदीश चतुर्वेदी के एक काव्य संग्रह का नाम ही ‘निषेध’ था। ‘निषेध के बाद’ में संपादक दिविक रमेश ने लिखा था, ‘अकविता प्रमुखत: निषेधात्मक अभिव्यक्तियों की कविता है। सब कुछ को नकार देने और खुद को सनम समझने की हिटलरी मुद्रा इस कविता और इसके कवियों की प्रमुख पहचान है।’ इस सबके बाद भी ‘दिशाबोध’ के प्रवेशांक के लिए जगदीश चतुर्वेदी ने अपनी कविताएं सहर्ष दी थीं तो लेखक के अनुसार ‘यह एक बड़े और अपने प्रति अदम्य विश्वास रखने वाले कवि और व्यक्ति का ही आचरण था।’
त्रिलोचन के कवि-व्यक्तित्व पर लेखक ने सर्वाधिक विस्तार से तीन निबंधों में लिखा है। इन निबंधों में दुहराव न के बराबर है। संस्मरणों की अच्छी शृंखला इनमें देखी जा सकती है। त्रिलोचन के कविता-वैभव के प्रति लेखक की शुरुआती अज्ञानता और फिर त्रिलोचन के मित्र कवि शमशेर के माध्यम से क्रमश: आत्मीयता और प्रशंसा भाव इनमें खुल कर व्यक्त हुए हैं। त्रिलोचन की देशज आधुनिकता पर लेखक ने बहुत डूब कर लिखा है। त्रिलोचन के साथ लेखक के कई व्यक्तिगत संस्मरणों ने इन निबंधों को बेहद पठनीय बना दिया है।
हिंदी की प्रगतिशील कविता पर सर्वाधिक आक्षेप शिल्प के नएपन के प्रति लापरवाही को लेकर लगाया जाता है। उचित ही लेखक ने त्रिलोचन की कविताओं की विशिष्टताओं के माध्यम से इस आक्षेप को कुंद किया है। लेकिन इससे भी महत्त्वपूर्ण ढंग से इस आक्षेप का उत्तर केदारनाथ अग्रवाल पर लिखे निबंध ‘कवि केदारनाथ अग्रवाल का काव्य विमर्श’ के माधयम से लेखक ने दिया है। इसमें केदारनाथ अग्रवाल की शिल्प-सजगता उभर कर आई है, जिससे एक व्यवस्थित काव्य-चिंतक के रूप में केदारजी की एक नई छवि अपेक्षाकृत युवा पाठकों के सामने आई है। इससे केदारनाथ अग्रवाल के चिंतक पक्ष के प्रति पुराने वरिष्ठ आलोचकों का उपेक्षापूर्ण रवैया भी सामने आता है।
साहित्य-चिंतन संबधी केदारजी की तीन पुस्तकें हैं- ‘विवेक विवेचन’, ‘समय समय पर’ और ‘विचार बोध’। इन पुस्तकों में बिखरे केदारजी के काव्य चिंतन के उपयुक्त उद्धरणों से लेखक ने उनके काव्य-चिंतक रूप को स्थापित करने का सफल प्रयास किया है। बिंब, प्रतीक, छंद, अलंकार, रचना-प्रक्रिया, काव्य-भाषा आदि पर उनके मत उद्धृत करते समय लेखक के इन मतों पर सहमति भी समझी जा सकती है।
‘अज्ञेय की शास्त्रीयता बनाम अज्ञेय का काव्य-भाषा विमर्श’ एक विस्तृत आलोचनात्मक निबंध है, जिसमें लेखक ने माना है कि ‘अज्ञेय के शास्त्रीय रूप की अवहेलना नहीं की जा सकती। और इस निष्कर्ष का यह आशय कदापि नहीं कि हम उनकी शास्त्रीयता के हर पक्ष से सहमत हों ही।’ लेखक ने अन्य निबंधों में भी बिना किसी पूर्वग्रह के असहमति का साहस और नापसंदगी का विवेक व्यक्त किया है। यहां तक कि अपने मित्र कवि-नाटककार प्रताप सहगल पर लिखे बेहद आत्मीयतापूर्ण निबंध में भी उनका यह पक्ष कुंठित नहीं हुआ है।
पुस्तक में समकालीन कविता, भारतीय कविता की भारतीयता, कविता में स्त्री छवि, कविता में ग्राम्यांचल, कन्नड़ का वचन साहित्य, कोरियाई मां आदि विषयों पर भी लेख संकलित हैं, जो पुस्तक की उपयोगिता बढ़ाते हैं। पूरी पुस्तक में विदेशी कवि-चिंतकों से आक्रांत होकर महिमामंडित करने के बजाय उन्हें हिंदी के श्रेष्ठ कवियों के अगल-बगल रख कर प्रस्तुत किया गया है। इससे लेखक की निजी पक्षधरता और प्रतिबद्धता स्पष्ट हो जाती है।
समझा परखा: दिविक रमेश; किताबवाले, 22/4735 प्रकाशदीप बिल्डिंग, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली; 335 रुपए। (रमेश बर्णवाल)
………………………………………
मोक्षधरा
सुधीर रंजन सिंह के पहले संग्रह और ‘मोक्षधरा’ के बीच लंबा अंतराल है। कारण संभवत: ऐतिहासिक है। 1990 के बाद की घटनाओं ने कुछ समय के लिए उन कवियों के कवि कर्म को बाधित किया जो कविता में भविष्य को फलित करने की चेष्टा कर रहे थे। पुरानी काव्य-भंगिमाएं बेअसर हो गई थीं। सुधीर रंजन सिंह कवि के साथ-साथ आलोचक भी हैं। संतुलन बनाने में उनका आलोचनात्मक विवेक सहयोग करता है। उनकी आलोचनात्मक भंगिमा और कुछ नहीं, विकल्प की चेतना है। यह ‘निद्रा अनुभव’ से बाहर निकालती है। मनुष्य और समाज को समझने की दृष्टि देती है।
सुधीर रंजन सिंह संकट के अनुभवों से बिना अलग हुए उल्लास और मुक्ति के उस संसार को रचने की चेष्टा करते हैं, जिसमें जीवन का अर्थ स्पंदित होता है। उस अर्थ की लालसा, जो किसी अन्य पीड़ाहारक दिलासा से अधिक जरूरी है, उनकी कविता को गढ़ने का काम करती है। इस काम में ‘स्मृति की क्रीड़ा’ भूमिका निभाती है। ‘मोक्षधरा’ ऐतिहासिक अनुभवों को आत्मचेतना के स्तर पर रचने और ‘उत्कर्ष लोक’ तैयार करने का सफल प्रयास है।
मोक्षधरा: सुधीर रंजन सिंह; राजकमल प्रकाशन, 1-बी, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली; 300 रुपए।
…………………………
तीस बरस बाद मैं
हसन जमाल के पास कहानी कहने का अपना एक अलग निजी मुहगावरा है। चीजों को नए ढंग से देखने का तरीका और अपने आसपास घटने वाली घटनाओं और चरित्रों को वे जिस किस्सागोई अंदाज में अभिव्यक्त करते हैं, वह उनकी अपनी मौलिक दृष्टि का परिचायक है। इसी तरह इनकी भाषा जो हिंदी-उर्दू मिश्रति होती है, शिल्प की एक अलग जमीन तैयार करती है।
हसनजी हमारे आसपास की कहानियां लिखते हैं। न कोई बड़े दावे, न फतवे, न लादे गए निर्णय और न किसी आंदोलन से सीधा जुड़ाव। असल में हसन जमाल कहानियों के माध्यम से धीरे से जीवन में इस तरह प्रवेश करते हैं कि पाठक चकित रह जाता है कि अरे, यह तो मेरी ही या मेरे अगल-बगल की कहानी है। कोई कहानीकार इतने हौले से भी इस तरह समय के सच को अभिव्यक्त कर सकता है कि जिसे हम रोज देखते, सोचते हैं, पर कभी उस तरफ हमारी नजर क्यों नहीं जा पाती। यही हसनजी की कहानियों की विशेषता है।
तीस बरस बाद मैं: हसन जमाल; वाणी प्रकाशन, 4695, 21-ए, दरियागंज, नई दिल्ली; 250 रुपए।
………………………………..
सृजन के सात दशक
अपने अनुभव से सीखे हर सबक को जावेद अख्तर ने न भुलाते हुए जिंदगी में उतारा है। ऐसे लोग कम हैं जो जिंदगी और दुनिया के तमाम विषयों पर सोचते हैं, अपने विचार लिखते हैं, बात करते हैं, पर जीने के अंदाज में भी वे इन फलसफों पर खरे उतरते हैं। इस मामले में जावेद अख्तर एक मिसाल हैं। अपनी हर बात को कह देना और उस पर कायम रहना जावेद अख्तर के व्यक्तित्व का एक अद्भुत पहलू है। उन्होंने अपने विचारों को, अपने अनुभवों से जिंदगी और हालात की आंखों में आंखें डाल कर बनाए हैं।
इस किताब में जावेद अख्तर की कही और लिखी बातों को लिया गया है। हिंदी कैलीग्राफी में तैयार यह मकबूल फिदा हुसेन की आत्मकथा के बाद शायद दूसरी सुंदर किताब है। पुस्तक की कैलीग्राफी अशोक दुबे और रेखांकन मुकेश बिजौले ने तैयार की है। किताब निस्संदेह बहुत सुंदर कलात्मक प्रस्तुति का नमूना है।
सृजन के सात दशक: अरविंद मंडलोई, रूपांकन, 31 शंकरगंज, किला रोड, इंदौर; कोई मूल्य नहीं।