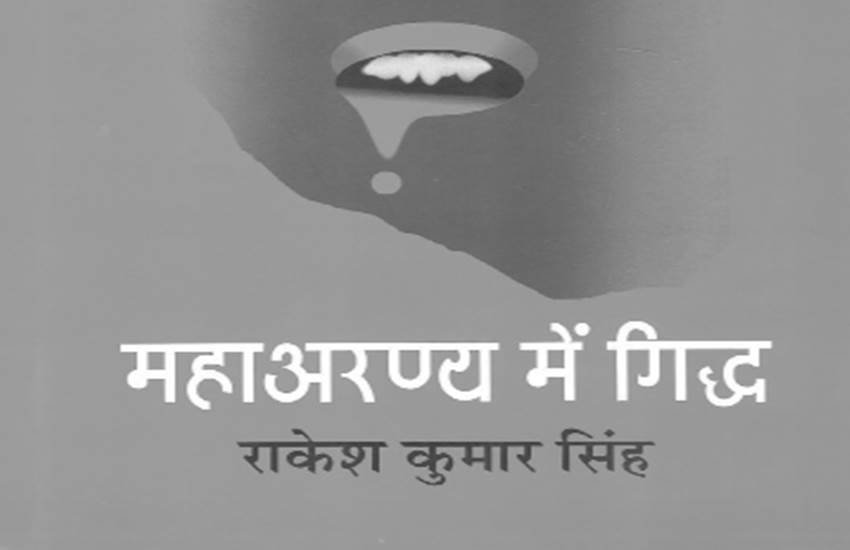तथाकथित विकास के झूठे सच ने हर वास्तविक सच को नजरअंदाज करके अधिकतम आबादी को हाशिये पर धकेल दिया है, जहां लोग जीने मात्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह हाशिया लगातार बढ़ रहा है। यों विकास परियोजनाओं का शिकार हर कमजोर आदमी हो रहा है, पर इसका सर्वाधिक विध्वंसक असर आदिवासियों पर पड़ रहा है। विकास उनके लिए विनाश का पर्याय बन चुका है। राकेश कुमार सिंह का उपन्यास महाअरण्य में गिद्ध आदिवासियों के बहुस्तरीय विनाश का बहुआयामी आख्यान है।
उपन्यास का भूगोल वर्तमान झारखंड के पलामू जिले का महुआटांड़ प्रखंड है। इसका नायक बुचानी मुरमू नामक आदिवासी है, जो घोर अत्याचारी स्थानीय जमींदार प्रभुदयाल शाहदेव का अतिविश्वस्त नौकर था। पूरे इलाके में जमींदार का आतंक था। जंगल के बीच काठगोदाम नाम से कुख्यात उसका एक यातनागृह था, जिसमें उसने अजगर, चीते और मगरमच्छ पाल रखे थे। वहां वह आदमियों को जिंदा फेंक देता था। इस तरह, लालसाहब या राजा गोमके के नाम से ख्यात प्रभुदयाल शाहदेव महुआटांड़ के रैयत- आदिवासियों ही नहीं, उस क्षेत्र में कार्यरत थाना प्रखंड आदि के सभी कारिंदों के लिए सरकार से कम नहीं था। राजा गोमके के इकलौते बेटे नान्ह बाबू द्वारा अपनी प्रेमिका देकुली को हवस का शिकार बना कर उसकी हत्या कर देने से बौखलाया बुचानी मुरमू एक दिन नान्ह बाबू की हत्या कर देता है और काठगोदाम में आग लगा कर भाग जाता है। आगे वह अलग झारखंड के लिए आंदोलनरत भूमिगत संगठन झारखंड मुक्ति दल (झामुद) का एरिया कमांडर बनता है और उसका नया नामकरण ददुआ मानकी होता है। झारखंड राज्य बनने के बाद दल के मुखिया कालीपद दत्त ‘गुरुजी’ द्वारा आंदोलनकालीन मूल्यों और आदर्शों को तिलांजलि देकर घोर अवसरवादी चरित्र अपनाए जाने के कारण ददुआ मानकी का इस संगठन से मोहभंग हो जाता है।
उपन्यास की मुख्य कथा इतनी ही है, पर लेखक ने अद्भुत किस्सागोई का परिचय देते हुए अनेक घटनाओं और प्रकरणों को परस्पर गुंफित कर मुख्य कथा को जोड़ दिया है। उपन्यास समाज, राजनीति और संस्कृति तीनों को एक साथ संबोधित करता है, पर सब कुछ साहित्य के स्वधर्म की रक्षा करते हुए। उपन्यास के कथानक में कहीं बिखराव नहीं है। दूसरे उपन्यासों की तुलना में यह इसलिए अलहदा है कि इसमें गैर-आदिवासियों (दीकू) और आदिवासियों के संपर्क और संघर्ष के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिणामों का सूक्ष्म और विस्तृत विवेचन तो है, पर कहीं भी तरह-तरह के राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों या इंटरनेट से प्राप्त सूचनाओं और आकड़ों को उपन्यास पर आरोपित नहीं किया गया है। यह उपन्यास अनुभव से ज्ञान की ओर यात्रा है, ज्ञान से अनुभव की ओर नहीं। यही कारण है कि लेखक ने दिल्ली, पटना या रांची की जगह महुआटांड़ प्रखंड को उपन्यास की मुख्य कथाभूमि बनाया है। इसमें एक बड़ी लेखकीय दृष्टि निहित है कि ऊपर (केंद्र) से नीचे (स्थानीय) परिभाषित नहीं होगा, बल्कि नीचे से ऊपर को परिभाषित होना होगा।
उपन्यास में पात्रों और घटनाओं के माध्यम से यह बार-बार रेखांकित किया गया है कि दीकू लोग (गैर-आदिवासी) अपने अंतिम निष्कर्षों में आखिरकार दिकू ही साबित होते हैं। आदिवासियों के लिए सहानुभूति और उनके कार्यों के पीछे की असली मंशा कुछ और होती है। आदिवासियों को प्रत्यक्षत: लूटने वाला गोमके प्रभुदयाल शाहदेव हो या सरकारी फेलोशिप लेकर आदिवासियों पर शोध करने वाला कामरेड योगराज जोशी, महुआटांड़ प्रखंड का बीडीओ सुबीर झा या भूमिगत संगठन झामुद का मुखिया कालीपद दत्त, सभी आदिवासियों को छलने वाले ही साबित होते हैं।
योगराज जोशी जैसे चरित्र के माध्यम से लेखक ने ऐसे तथाकथित कामरेड शोधार्थियों और बुद्धिजीवियों के चरित्र का परदाफाश किया है, जो सरकारी या गैरसरकारी संस्थाओं से प्रोजेक्ट लेकर आदिवासी इलाकों में जाते हैं और वहां स्त्री देह का आखेट करते हैं। ये तथाकथित प्रतिबद्ध कामरेड ऊपर से तो महानता ओढ़े रहते हैं, पर आदिवासी स्त्रियों को वे भी सिर्फ यौन-वस्तु ही मानते हैं, जैसा कि योगराज जोशी सोचता है और इसी कारण वह मारा भी जाता है। अलग झारखंड राज्य के लिए संघर्षरत तमाम भूमिगत संगठनों में से सर्वाधिक प्रभावशाली और लोकप्रिय संगठन झामुद के मुखिया कालीपद दत्त के पतनशील आचरण के माध्यम से लेखक ने बताया है कि आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व जब तक गैर-आदिवासियों के हाथ में रहेगा तब तक उनका भला नहीं हो सकता और वे ददुआ मानकी की तरह बार-बार छले जाने को अभिशप्त होंगे।
आदिवासी और गैर-आदिवासी के द्विविभाजन में सोचने का एक नुकसान यह होता है कि आदिवासियों के खुद के अंतर्विरोध और समस्याओं को प्राय: नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह अच्छी बात है कि लेखक ने आदिवासियों को अपने सामने रखने में संकोच नहीं किया है। आदिवासियों में अंधविश्वास की समस्या भयानक है। कई तरह की प्रथाएं प्रचलित हैं, जो बहुत अमानवीय हैं। औरतों को डायन बता कर मारने का भी रिवाज प्रचलित है। लेखक ने इस बात को भी सामने रखा है कि आदिवासी इलाके में काम कर रहे भूमिगत संगठनों में बहुत भटकाव आया है। बहुतों का लक्ष्य सिर्फ पैसा उगाही रह गया है।
इसके लिए वे तथाकथित वर्ग शत्रुओं से हाथ मिला लेते और ईमानदार लोगों की हत्या कर देते हैं। शांतिप्रिय ढंग से काम कर रहे उमेश और ममता की हत्या का वर्णन उपन्यास में है। सबसे गौर करने लायक बात यह है कि लेखक ने आदिवासी लड़कियों को नौकरी के सपने दिखा कर शहरों और महानगरों में उन्हें बेचने का काम करने वाली स्टेला कुजूर को आदिवासी महिला बताया है। यानी खुद आदिवासी महिला होते हुए भी स्टेला कुजूर आदिवासी बेटियों को बेचने का धंधा कर रही है। स्पष्ट है, राकेश कुमार सिंह ने आदिवासियों को पूरी तरह निर्दोष न बता कर इस बात को रेखांकित करने का प्रयास किया है कि बहुत से ऐसे आदिवासी भी हैं, जो अपने समाज से छल करके दिकू लोगों के साथ मिल गए हैं। इस तरह की कमजोरियों को दूर करने के लिए एक दृष्टिसंपन्न आदिवासी नेतृत्व आवश्यक है, जिसकी संभावना ददुआ मानकी जैसे लोगों में है।
महाअरण्य में गिद्ध: राकेश कुमार सिंह; भारतीय ज्ञानपीठ, 18, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली; 520 रुपए। (दिनेश कुमार)
………………………….
साहित्य के आसपास
इस कथित स्मार्ट युग में समय न मिलने की लाचारी में कलमी हाथ से पत्र लिखना कष्टदायी हो जाता होगा, जब पल्ले पैसा न हो या अस्वस्थता हो या तनिक फुरसत न हो लिखने की। सच में तो मूड न हो। प्रतिदान में कुछ हासिल की गुंजाइश न दिखे, तब भी कैसे दावा किया जा सकता है कि हम सत्यम साहित्यकार हैं, उससे पहले शिवम इंसान हैं और सुंदरम नीयत वाले हैं। हम ऐसे जमाने में रह रहे हैं, जिसमें आंखों पर चर्बी चढ़ी होती है, गले लगने की तहजीब में छाती से पहले चर्बीदार पेट आ जाता है। जब मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, ऐसी लयात्मक पंक्ति गूंजने लगे तो भी आश्चर्य होता है मैत्री भाव पर।
कहीं ऐसा तो नहीं हो जाता कि धनराशीय अकादमिक पुरस्कार या राष्ट्रीय पद्म सम्मान साहित्यकारों की ऊर्जा को निस्तेज कर देते हों। पुराने जमाने का मिलान आज के जमाने से करें तो मित्रता जैसा रिश्ता किस हृदय में मिलेगा? श्याम विमल की इस पुस्तक में पुरानी पीढ़ी से लेकर नई पीढ़ी तक के रचनाकारों की सोहबत में बिताए दिनों की याद और उनकी मित्रता की ऊष्मा महसूस की जा सकती है। इससे साहित्यकारों के मन को समझने में मदद मिलती है।
साहित्य के आसपास: श्याम विमल; संजना प्रकाशन, डी-70/4, अंकुर एन्क्लेव, करावल नगर, दिल्ली; 395 रुपए।
……………….
चाय, चाय
विश्वनाथ घोष कानपुर से मद्रास की लंबी रेल यात्रा के बीच मध्यप्रदेश के इटारसी स्टेशन पर थोड़ा हाथ-पैर सीधा करने और चाय की तलब मिटाने की कोशिश में रेल से नीचे उतरे। चाय की चुस्कियों के बीच स्टेशन पर हो रहे ट्रेन टाइम-टेबल की घोषणा को सुनते हुए उन्हें अहसास हुआ कि इटारसी रेलवे जंक्शन इंडियन रेल मैप का महत्त्वपूर्ण स्टेशन है, लेकिन असल में इटारसी शहर के बारे में शायद ही कोई जानता हो।
इसी से घोष देश के बड़े जंक्शन के पीछे छिपे गुमनाम कस्बों की तलाश में निकल पड़े: इटारसी, मुगलसराय, झांसी, शोरानूर, अरक्कोणम और जोलारपेट्टई- ऐसे कस्बे जो पड़ाव तो होते हैं, लेकिन मंजिल नहीं। भारत के प्रतीक इन छोटे-छोटे कस्बों का दिलचस्प सफरनामा, चाय चाय है। इस किताब की कहानी में लेखक ने चीजों और जगहों को एक नए ही नजरिए से पेश किया है।
चाय, चाय: विश्वनाथ घोष; ट्रैंकेबार प्रेस, यात्रा बुक्स, 93 प्रथम तल, शामलाल रोड, दरियागंज, नई दिल्ली; 250 रुपए।
………………………
जो पब्लिक चाहती है
जरा-जरा सी बात पर झंडा उलट देने को तैयार रहती है यह पब्लिक। जनतंत्र को महत्त्व दिया गया, मगर किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि यह तो भेड़ियाधसान है। नहीं तो तालियां बजा कर सरकार गिराने की प्रथा हमारे देश में नहीं थी। यही वह देश है, जिसका दिमाग तालियों में बसता है।
आज तक रहस्य बना हुआ है कि आखिर भारत की पब्लिक क्या चाहती है। भगदड़ और भूकंप में होड़ मची है। दूर खड़ा विनाश सारी लीलाएं देख रहा है। लोग संदेह, असहिष्णुता और ईर्ष्या की आग में जल रहे हैं। जो कस्तूरी उनके पास है वह उन्हें दिखाई नहीं पड़ती।
परशुरामपुर की धरती पर इतने पात्र अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आदर्श निरंतर यथार्थ बनने के लिए छटपटा रहा है। तब भी इच्छित परिणाम नहीं मिलता। परशुरामपुर ‘लघुभारत’ बनने का सपना देख रहा है। उस सपने को साकार करने वाले बहुत लोग हैं, किंतु जड़ से दीमक नहीं हटती और ढांचा कमजोर होता जा रहा है। उस दीमक की दवा लेखक ने अपनी कलम से खोजने का एक विनम्र प्रयास किया है। उसी का परिणाम है यह उपन्यास ‘जो पब्लिक चाहती है’।
जो पब्लिक चाहती है: रमाशंकर श्रीवास्तव; एजुकेशनल बुक सर्विस, एन-3/25 ए, डीके रोड, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, नई दिल्ली; 400 रुपए।