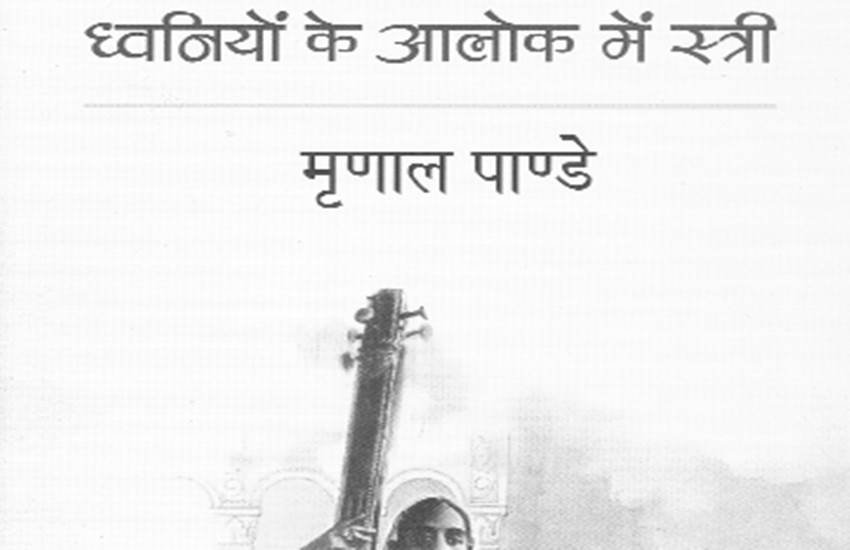मृणाल पांडे की नई किताब है- ध्वनियों के आलोक में स्त्री। इस किताब के साथ हमारे अनुभव और सुने हुए किस्सों के काफिले भी चलते हैं- गानेवालियों के रहन-सहन से लेकर मिजाज तक। इतिहास बताता है कि गानेवालियां राजघरानों से जुड़ी रही हैं और उन्होंने मोहर-अशर्फियां, गहने-जेवरात ही नहीं, हवेलियां और जायदाद बख्शिश में पाई हैं। ये गानेवालियां कौन हैं? सवाल इसलिए मन में उठता है कि गाने और नाचनेवालियों की एक जमात मध्यवर्ग के मनोरंजन के लिए भी रही है, जिनको बख्शिश नहीं, मेहनताना दिया जाता है और उनके हुनर को पेशा माना गया है।
असल गायकी जिसे माना जाता है, भले वह जमाने के साथ विलुप्त होती जा रही है और तिलवाड़ा, झूमरा और विलंबित तीन ताल के खयाल सुनने को न मिलते हों, लेकिन असल गायकी तो यही है, जिसके लिए बेगम अख्तर, जानकी बाई, जद्दन बाई और गौहर खान वगैरह को खूब सराहा गया। तभी न गिरजा देवी को आज भी अपने गायन की शुरुआत खयाल से करनी होती है, जबकि बराबर उनके श्रोता रसीली ठुमरी सुनने का इंतजार करते रहते हैं।
मृणाल संगीत के उस इतिहास की परत-दर परत खोलती हैं, जब संगीत के उस्ताद और गुरु राजनीति से हमेशा दूर रहे। असल में कलाकारों को वैसी कुटिल उठापटक फितरतन नापसंद थी। यहां तक कि जब बंटवारा हुआ तो एकाध को छोड़ कर अधिकतर मुसलमान गायक-गायिकाएं हिंदुस्तान छोड़ने को राजी नहीं हुए। ‘अपनों के बीच गाने-बजाने का मजा कुछ और ही है’ चले जाने वाले यह स्वीकार करते। हिंदू मुसलमान का भेद भी कुछ इस तरह था- ‘यह न पंडत का गाना है और न उस्ताद का, यह है असल हड्डी का गाना।’
इस किताब के जरिए स्त्री की बात करें तो सामने वह समय भी आता है जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। स्वदेशी आंदोलन में भाग लेती स्त्रियां तो रहीं, मगर उनके अनुभवों का कोई संकलन कहीं नजर नहीं आता। कहने का मतलब यह कि साहित्य, संगीत और स्वतंत्रता संग्राम, तीनों क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान पर परदा पड़ा रहा। वे अमुक की पत्नी, शिष्या वगैरह की तरह जानी गर्इं। जो कुछ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पार्इं, तो इसलिए कि उनकी अनगढ़ प्रतिभा को किसी जानकार पुरुष ने तराशा। यह अकारण नहीं कि बेगम अख्तर से लेकर सिद्धेश्वरी देवी सरीखी प्रतिभाओं ने सामाजिक दायरों में अन्यायपूर्ण द्वैत झेला और फिर बाहर आने का संकल्प लिया। मगर यह भी रहा कि गाने-नाचनेवालियों का जलसा मर्दाना बैठकखाने में ही सजता। घर की स्त्रियां परदे के पीछे रहतीं। पुरुषों की मांग पर बाई हाव-भाव सहित अदायगी करती। दोयम दर्जे पर रखी गर्इं ये कलावंतियां बड़े घरों के पुरुषों की रक्षिता बनीं या न बनीं, लेकिन मान ली गर्इं। और यहीं पर छिपा है वह दर्द, जो स्त्रियों की कलाओं के पीछे ऐसा मार्मिक आलोड़न है, जिसे हम देख कर भी नहीं देखते। बेशक पुरुष समाज सुधारकों ने भी महिलाओं की दुर्दशा पर उतना ध्यान नहीं दिया, जितना नैतिकता की स्थापना को जरूरी माना।
परिवारों ने संगीत को भी नैतिकता की रस्सी से बांध दिया, जिसमें घर की नानी-दादियां ही आगे रहीं, क्योंकि मर्दपरस्ती से आजाद नहीं थीं। मृणाल मिसाल पेश करती हैं- ‘हरमुनियां चालू होता, पिया की नज्जरिया जादू भरी… ई… ई।’ ‘पिया’ या ‘छतिया’ कुमारिकाओं के लिए वर्जित शब्द माने गए, सो राग-रागनियों के बीच गाया जाने लगा- ‘बिस्नू की नज्जरिया जादू भरी’ या ‘सखि मोरि रूमझूम कैसे गाऊं हरि पास बदरवा गरजे…’
बस इस तरह अपने आप ही औरतें दो किस्मों में बंट जाती हैं- भली (सद्गृहस्थ) और बुरी (गवनियां-नचनियां)। भली औरतें बच्चे पैदा करती हैं भले घरों में और बुरी औरतें (कोठेवालियां) मर्दों को रिझा कर, पैसा लूट कर उन्हें भिखारी बना देती हैं। दोनों वर्गों की औरतों का यह भयंकर विभाजन आज तक चला आ रहा है, मगर विडंबना यह है कि अपने-अपने पाले में न पारिवारिक विरासत की स्वामिनी परावलंबन में खुश है और न आर्थिक रूप से स्वावलंबी, मगर समाज से बहिष्कृत नाचने-गानेवाली को अपनी दशा रास आती है। मृणाल उदाहरण पेश करके यह सिद्ध करती हैं कि स्त्री अपने अपूर्व गुणों की स्वामिनी होने के साथ ही पुरुष वर्ग द्वारा दोयम दर्जे पर रखी गई है। कला, साहित्य, संगीत को खंगाला जाए तो उसमें से महिला का बराबरी का दावा नजर आएगा, जिसको अन्याय के दलदल में फंसा कर रख गया है। यह ऐसी किताब है जो शब्द-दर-शब्द, पंक्ति-दर-पंक्ति और पैरा-दर-पैरा पाठक के लिए अनदेखे, अनबुने किस्से कहती जाती है और गायन तथा नाचघरों के ऐसे गवाक्ष खोलती है, जहां वे कलावंतियां नजर आती हैं, जिनके बोलों, स्वरों और लयों पर हम झूमते रहे हैं। फिर उनकी जिंदगी इज्जत से बेगानी क्यों है? उनकी चर्चा हराम क्यों है? उनके साथ वादाखिलाफी क्यों है?
नई विचारधारा आई। इसमें कुछ संगीत शास्त्रज्ञों का अविस्मरणीय योगदान रहा। बदलते समय में संगीत शिक्षा में भी बदलाव जरूरी लगने लगा। संतोष और आश्वस्ति की सांस आती है संगीत की दुनिया में जब केसरबाई अपनी कला का प्रमाण खुद के तेजस्वी व्यक्तित्व से देती हैं। यह एक मिसाल है, लेखिका ने ऐसे कई आश्वस्तकारी दृष्टांत इस पुस्तक में रखे हैं। मृणाल पांडे के इस लेखकीय परिश्रम पर मैं चकित हूं और अनुभवों को सहेजने पर बधाई देती हूं। अब वह संवाद:
‘बाई मांगिए जो मांगना हो’ मुख्यमंत्री यशवंत चव्हाण ने कहा हाथ जोड़ कर।
‘सच!’
‘चलिए, एक दिन को अपना राजकीय दफ्तर मेरे हवाले कर दीजिए।’
राजनेता निरुत्तर हो रहे।
‘आगे कभी ऐसा वादा किसी से न करें साहिब, जो निभाया न जा सकता हो।’ केसर फिर ठठा कर हंस दी। उस हंसी की वेदना कौन भांप सकता है?
मैत्रेयी पुष्पा
ध्वनियों के आलोक में स्त्री: मृणाल पांडे; राधाकृष्ण प्रकाशन, 7/31, अंसारी मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली; 300 रुपए।
………………………………
चोर दरवाजा
जितेन ठाकुर की कहानियां यह स्थापित करती हैं कि कहानी एक निरंतर बदलने वाली विधा है, जो किसी परंपरा की मोहताज नहीं होती, क्योंकि कहानी अपने समय को यदि रूपायित नहीं करती और अपने काल की त्रासदी को नहीं पहचानती, तो उस समय और उस दौर का पाठक भी कहानी को पहचानने से इनकार कर देता है।
जितेन ठाकुर ने परंपरापूरक यथार्थवाद को नकार कर अपने अंदर और बाहर के यथार्थ को समेटा है। वे पाठक को उसी तरह परेशान करते हैं जैसे उसका समय उसे त्रस्त करता है और उसी तरह निष्कर्षवाद को नकारते हुए जितेन की कहानियां अन्विति पर पहुंचती हैं, जिन्हें पाठक महसूस तो करता है, पर शब्द नहीं दे पाता। शायद इसीलिए ये कहानियां एक लेखक की कहानियां न होकर अपने समय के जीवंत और अपने समय को विश्लेषित करने वाले समय के मित्र रचनाकार की कहानियां है।
ये आज के भयावह यथार्थ को केवल उजागर नहीं करतीं, बल्कि पाठकविहीन एकरसतावादी कहानियों की जड़ता को तोड़ते हुए यह साबित करती हैं कि कहानी अपने समय के मनुष्य की तमाम बेचैनियों और भयावहता को वहन करते हुए उसी मनुष्य को अपने समय को समझने और उसके संत्रस्त अस्तित्व को एक नई दृष्टि देने की भूमिका अदा करती है।
चोर दरवाजा: जितेन ठाकुर; परमेश्वरी प्रकाशन, बी-109, प्रीत विहार, दिल्ली; 250 रुपए।
……………
मन सर्जन
अज्ञान का, गरीबी का, बीमारियों का, अंधश्रद्धा का, सामाजिक विषमता का, एक-दूसरे पर अविश्वास का अंधकार हमारे समाज से दूर कर ज्ञान का, समृद्धि का, सत्श्रद्धा का, एक-दूसरे पर विश्वास का प्रकरण अगर चाहिए तो ऐसे सत्चरित्र व्यक्ति का निर्माण कैसे हुआ, इसका चित्रण सबके सामने आना चाहिए। बुद्धिमानी, निरंतर मेहनत करने की तैयारी, दूसरों की जरूरतों का अहसास, त्याग करने की मनोवृत्ति, सादे जीवन का महत्त्व जानना, सतत सीखने की प्रवृत्ति होना- अनेक ऐसे पहलू, जिनके व्यक्तित्व पर नजर डालने पर दृष्टिगोचर होते हैं, उनमें अनिल गांधी ‘कनिष्ठिकाधिष्ठित’ हैं। उन्हें जिन कठिनाइयों से रास्ता निकालना पड़ा, उनका इस पुस्तक में उन्होंने ईमानदारी से वर्णन किया है। अपने पिता और सगे भाई के गुण-दोष का वर्णन करते समय भी उन्होंने सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा। अपने गुरुजनों के बारे में आदर भाव में कमी न आने देते हुए, उनका योग्य मूल्यमापन किया है।
मन सर्जन: अनिल गांधी; राधाकृष्ण प्रकाशन, 7/31, अंसारी मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली; 400 रुपए।
……………………………….
उद्भ्रांत की श्रेष्ठ कहानियां
उद्भ्रांत मूलत: कवि हैं। कविताओं में रमे रहने के कारण उनकी कहानियों की तरफ लोगों का ध्यान कम ही गया। इनके कथा-संसार ने एक लंबी रचना-यात्रा तय की है। वे अपनी कहानियों में एक बड़ा परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं, जिसमें वे अपनी कहानियों में रचे गए प्रतीकों के निहितार्थ को स्वयं ही अपनी प्रखर पक्षधरता में विखंडित कर देते हैं और संघर्षशील सर्वहारा के साथ खड़े होकर उस दुनिया की ओर निकल जाते हैं, जो अपने जनवादी सपनों की निराकार स्थिति को मंजूर नहीं करती और अभी तक अपना न्याय मांग रही है।
उद्भ्रांत की कहानियों में निजत्व है, रूमानियत है, जीवन जीने का संघर्ष है, दर्द और शहर का दायरा है, कल-कारखाने हैं, मजदूरों के जीवन की समस्याएं हैं, तो साथ ही उनके समाधान हैं, श्रम और पूंजी का अंतर्विरोध भी मौजूद है, यानी इन कहानियों में पाठक को कथानक और पात्रों से संबंधित विविधता देखने को मिलती है। कहानियों की भाषा, शैली, प्रसंग और उद्देश्य के अनुरूप है।
उद्भ्रांत की श्रेष्ठ कहानियां: उद्भ्रांत; राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नेहरू भवन, 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज-2, वसंत कुंज, नई दिल्ली; 160 रुपए।