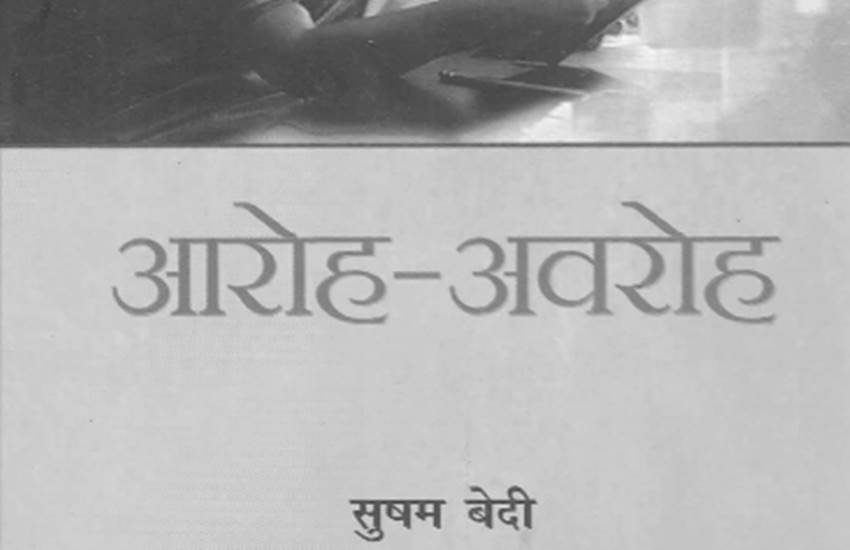हिंदी में आत्मकथाएं लिखने का चलन इधर बढ़ा है। वरिष्ठ लेखिका सुषम बेदी की आत्मकथा आरोह-अवरोह उसी की एक कड़ी है। वे कहती हैं कि वे और लेखिका एक होकर भी एक नही हैं। यानी आत्मकथा लिखते-लिखते कभी उनका अपना व्यक्तित्व उजागर होता है, तो कभी लेखिका का। वे आत्मकथा को अपनी अन्य कृतियों की तरह ही देखती हैं। एक ऐसी कृति, जिसके केंद्र में वे खुद हैं और लेखिका बनने के अब तक के सफर में आत्मपरीक्षण करती हुई वे किन-किन पड़ावों से होकर गुजरी हैं वही आरोह-अवरोह है। दरअसल, यह कथा एक डायस्पोरा लेखिका की भी है, जो एक साथ भारतीय और पाश्चात्य मूल्यों में तालमेल बिठाती हुई अपनी बात कहती है।
अपनी आत्मकथा को उन्होंने ग्यारह पाठों में विभाजित कर के प्रस्तुत किया है। घर की खोज में भिन्न-भिन्न शहरों के परिवेश को छूता लेखिका का जीवन सर्वप्रथम दिल्ली शहर में अपनी पहचान तलाशने की कोशिश करता है। वे मानती हैं कि उनका लक्ष्य केवल लेखन में नहीं, जीवन में नई जगह तलाशना भी रहा है। इसलिए ब्रसेल्स और इंग्लैंड के बाद न्यूयार्क उनका स्थायी घर बना। लेखिका के अनुसार भारत का वर्तमान उपनिवेशवाद से निकला है और आज भी उसी को जिया जा रहा है। वे सलमान रुश्दी और एडवर्ड सईद का उदाहरण देते हुए कहती हैं कि हम अपने जीवन की असंगति और विसंगतियों से जूझ रहे हैं और खोज रहे हैं एक समंजन। वे विदेश में जाकर बसने के पीछे कई कारणों को सामने रखती हैं- आधुनिकता-उत्तर औपनिवेशिकता और वैश्वीकरण के माहौल में बदलता हुआ भारतीय मेहनत से पढ़ाई के बावजूद जब नौकरी नहीं पाता तो वह अनाथ-सा महसूस करता है…। लेखिका भारत और विदेश में रहने के कई अच्छे और बुरे पक्षों को सामने रखती हैं।
एक आप्रवासी होने के नाते वे अमेरिका, इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों और भारत में रहते हुए घर की संकल्पना क्या रूप लेती है, इसकी विस्तृत चर्चा करती हैं। हो सकता है एक आप्रवासी दुनिया के अलग-अलग देशों में रहने से थोड़ा-थोड़ा हर देश का हो जाता है, इसीलिए देशों की भौगोलिक सीमाएं उसे बेमानी लगती हैं, लेकिन दूसरी दृष्टि से यह एक आदर्श विचार भी है। नन्ही स्मृतियों में वे अपने बचपन के हर गली-कूचे में विचरती हैं। विभाजन के बाद डेरा इस्माइलखान से भारत आया लंबा-चौड़ा कुनबा, कुनबे के विभाजन की त्रासदी के अनुभव, बचपन की शिक्षा और पिता के तबादले के कारण भिन्न-भिन्न शहरों के अनुभव को वे सिलसिलेवार बयान करती हैं। स्कूल, कॉलेज के खट्टे-मीठे अनुभव, रेडियो, टेलीविजन पर नाटक और संगीत की क्रियाशीलता और साहित्य में रचनात्मकता की ओर बढ़ते कदमों का विवरण वे विस्तार से देती हैं। आज के नामचीन अभिनेताओं के साथ अभिनय और धीरे-धीरे साहित्य लेखन की मंजिल के रास्ते को वे किस प्रकार तय करती गर्इं, इसका वर्णन करते हुए अपनी कविताओं, कहानियों और उपन्यासों के पात्रों के भीतर से कहलवाने लगती हैं।
आर्यसमाजी परिवार की पृष्ठभूमि में पलने-बढ़ने के कारण वे मानती हैं कि भले उनका परिवार मध्यवर्गीय था, लेकिन आम भारतीय परिवारों की अपेक्षा उन्हें हर प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अमेरिकी और भारतीय दोनों परिवेशों में आधुनिकता के कारण हुए परिवर्तनों का वर्णन करती हैं। भारतीय आवासी होते हुए भी वहां वे अपने संस्कारों के प्रति बहुत सजग रहते हैं। इसके वे कई उदाहरण देती हैं। मार्क्सवाद के क्षरण और पूंजीवाद के बढ़ते प्रभाव को वे एक विस्तृत कैनवस में देखती हैं। आजादी से पहले और आजादी के बाद नेहरू, इंदिरा गांधी से अब तक के भारत को चीन्हने का प्रयास करती हैं। वे बताती हैं कि एक डायस्पोरा का लेखन भारतीय परंपरागत जीवन और प्रवासी माहौल की टकराहटों का साहित्य है। हिंदी और दूसरी भाषाओं के साहित्य में भी यही घर्षण सुनाई देता है। चाय के बगीचों के अंतर्गत वे अपने वैवाहिक, गृहस्थ जीवन की विस्तार से चर्चा करती हैं। लेकिन यहां भी वे मात्र एक गृहिणी की भाषा से नहीं, बल्कि एक रचनाकार की हैसियत से पाठकों को सरोकारों से रूबरू कराती हैं- जैसे एक ओर अफसरों का ऐशभरा जीवन और दूसरी ओर उनके शोषण का शिकार हुए गरीब कैसे नक्सलवादी बनने को तैयार हो रहे थे।
पति की नौकरी के कारण यूरोपीय देशों में घटित वे अपने विभिन्न अनुभवों को बताती हैं और यहीं से वे खुद को एक डायस्पोरा लेखक के तौर पर प्रस्तुत करती हैं। अब अमेरिका में न्यूयार्क के मैनहैटन को वे अपना स्थायी घर मानती हैं। भारत और न्यूयार्क की तुलना में वे कहती हैं कि भारत अपनी संस्कृति, इतिहास और लोगों के कारण समृद्ध है, तो अमेरिका के पास वैसा इतिहास भले नहीं है, लेकिन लोगों का वैविध्य अवश्य है। क्योंकि यहां अलग-अलग देशों के निवासी बसे हैं। यहीं वे अपनी कहानियों और उपन्यासों में अमेरिकी भूगोल, संस्कृति और रहन-सहन की चर्चा करती हैं। साथ ही वे बताती हैं कि अमेरिका में उन्होंने हर छोटे-बड़े काम करने का प्रयास किया। अंतत कोलंबिया यूनिवर्सिटी में चौबीस साल पढ़ाने के अवसर ने उन्हें एक ओर जहां लेखन में सक्रिय किया, वहीं दूसरी ओर दिल्ली विश्वविद्यालय में छूट चुके शिक्षण कार्य से भी पुन: जोड़ा। लेखिका बनने की यात्रा को वे बड़े मनोयोग से बताती चलती हैं। वे कहती हैं- लेखन अब मेरा पर्याय बन चुका है।
प्रकृति के आदिम रिश्ते में फिर वे अपनी अतीत की स्मृतियों से होकर गुजरती हैं। अपने लेखन की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए वे अपनी बात को विशेष दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती हैं। वे मानती हैं कि धर्म के परे इंसान को इंसान की तरह जीने की आजादी मिलनी चाहिए। यहीं से आगे वे अपने लेखन के बारे में विस्तृत चर्चा करती हैं। वे अपने लेखन में भारतीय और पश्चिमी मिले-जुले प्रभावों को मानती हैं। वे मानव मुक्ति को केंद्रीय बिंदु मान कर चलती हैं। कुल मिला कर सुषम बेदी की यह आत्मकथा उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को समझाने का अवसर देती है।
आरोह-अवरोह: सुषम बेदी; सामयिक प्रकाशन, 3320-21, जटवाड़ा, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली; 495 रुपए। (वीणा शर्मा)
…………………….
सरसों से अमलतास
रिश्तों का जटिल संसार और प्रकृति का सरल, सहज अकुंठ विस्तार; इन कविताओं की जड़ें इन्हीं दो जमीनों पर फैली हैं। रिश्ते रंग बदलते हैं तो उनको एक सम पर टिकाए रखना, ताकि जिंदगी ही अपनी धुरी से न हिल जाए, अपने आप में बाकायदा एक काम है, जबकि अपने होने भर से, हमारे इर्द-गिर्द अपनी मौजूदगी भर से ढांढस बंधाती प्रकृति हमारी व्यथित-व्याकुल रूह के लिए एक सुकूनदेह विश्राम-भूमि।
और यही नहीं, ये कविताएं बताती हैं कि उनके रंगों में हमारी पीड़ा, हर उल्लास, हर उम्मीद, हर अवसाद के लिए कहीं-न-कहीं कोई रंग उपलब्ध है, जो हमारी अर्जित-अनर्जित संबंधों के शहरों, जंगलों, पहाड़ों और पठारों के अलग-अलग मोड़ों पर मन को अपना-सा लगता है, और सब तरफ से निराश होकर हम उसकी अंगुली थाम अपने अंतस की ओर चल पड़ते हैं- नए होकर लौटने के लिए।
शायद इसीलिए कि ये कविताएं प्रकृति का अवलंब कभी नहीं छोड़तीं। प्रकृति के स्वरों में ये रिश्तों के राग को भी गाती हैं और विराग को भी। टूटते-भागते संबंधों को पकड़ने की कोशिश में अगर इनकी हथेलियां रिस रही हैं और नानी के कहने से आसमान में दूर बैठे चांद को मामा मान लेने पर पश्चात्ताप कर रही हैं तो यह भरोसा भी उनमें विन्यस्त है कि ‘भीतर जमे रिश्ते ही/ बाहरी मौसम से बचाते हैं।’
सरसों से अमलतास: चित्रा देसाई; राजकमल प्रकाशन, 1-बी, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली; 250 रुपए।
……….
अनर्थ
सांप्रदायिकता जैसी जटिल समस्या को कमल चोपड़ा ने इस संग्रह की लघुकथाओं में स्याह हाशियों के बाहर और अंदर गिरे खून के छीटों को बेहद सूक्ष्मता और गहनता से जांच-परख कर कुछ मार्मिक और हृदयस्पर्शी चित्रों को संवेदना के साथ उकेरा है। दंगों से पहले की कुत्सित चालें और नापाक साजिशें हों या दंगे के दौरान मारकाट, आगजनी और लूटपाट में मरती-कटती, लुटती-झुलसती मानवता हो या दंगों के बाद लुटी-पिटी बरबाद लहूलुहान इंसानियत, सांप्रदायिक उन्माद के हर जटिल मसले के एक-एक रेशे को बहुत सतर्कता से जांचा गया है।
कमल चोपड़ा समाज के उन लोगों, राजनेताओं, अवसरवादी धर्मियों-विधर्मियों आदि सबको अच्छी तरह जानते हैं और विलुप्त होती मानवता के इस माहौल में आस्था, विश्वास, प्रेम, पारस्परिकता को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। कहीं किस्सागोई प्रधान नहीं है, सर्वत्र प्रधान है वक्त की नब्ज और तज्जन्य भावी स्थिति का अनुमान, पर उनका आस्थावादी स्वर कहीं क्षीण नहीं होता है।
अनर्थ: कमल चोपड़ा; अयन प्रकाशन, 1/20, महरौली, नई दिल्ली; 350 रुपए।
…………………………………………
हिंदी उपन्यास और भारतीय राजनीति
यह मानते हुए कि राजनीतिक प्रश्नों से परोक्ष-अपरोक्ष मुठभेड़ करके ही उपन्यास मनुष्य की मुकम्मल मुक्ति का आख्यान बनता है, इस पुस्तक में स्वातंत्र्योत्तर हिंदी उपन्यासों में स्वतंत्र भारत की राजनीति के विविध आयामों, संदर्भों और प्रश्नों की उपस्थिति का व्यवस्थित और गंभीर विवेचन-विश्लेषण कर हिंदी उपन्यास की मूल्यवत्ता और पहचान का विश्वसनीय रेखांकन किया गया है।
इस व्यापक अध्ययन में उपन्यासों की गवाही पर स्वतंत्र भारत की राजनीति का पूरा व्यक्तित्व दिख जाता है, जो क्रमश: विद्रूप होता गया है। उसकी जटिल बनावट के कारक तत्त्वों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संरचना में खोजबीन करने वाले उपन्यासों को चिह्नित किया गया है। न केवल उसकी सूरत, बल्कि सीरत की भी परख के चलते कुछ उपन्यास विमर्श के केंद्र में हैं।
उपन्यासों में जनविरोधी व्यवस्था के विरुद्ध किसानों, दलितों, मजदूरों, महिलाओं और छात्रों की प्रतिरोधी चेतना और उनके आंदोलनों के अंकन का आलोचनात्मक अध्ययन यहां उपलब्ध है।
स्वातंत्र्योत्तर हिंदी उपन्यास और भारतीय राजनीति: उन्मेष कुमार सिन्हा; नमन प्रकाशन, 4231/1, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली; 400 रुपए।