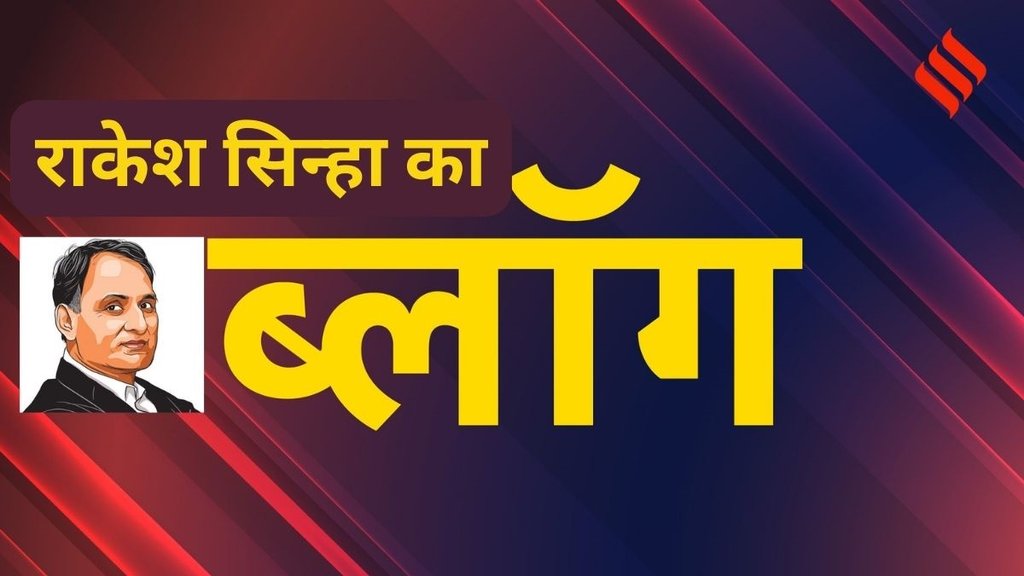प्रधानमंत्री ने ‘मन की बात’ रेडियो कार्यक्रम में एक महत्त्वपूर्ण, लेकिन उपेक्षित विषय को देशवासियों के सामने रखा है। वह है मौखिक इतिहास परंपरा, जो अंग्रेजी शब्दावली ‘ओरल हिस्ट्री ट्रेडिशन’ के नाम से प्रसिद्ध है। इतिहास, परंपराओं, घटनाओं आदि को दो स्वरूपों में जाना और समझा जा सकता है। एक लिखित रूप में, जिसका समकालीन संसार में वर्चस्व है और दूसरा मौखिक रूप में होता है, जिसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान का प्रवाह चलता रहता है। लिखते समय व्यक्ति अपने और समाज के प्रति जो पूर्वाग्रह रखता है, वह लेखन को औपचारिक बना देता है। फिर विषय का अनुशासन प्रवाह को नहर का रूप देता है।
मगर जब हम व्यक्ति से उसके जीवन के अनुभवों को, उसके द्वारा पूर्वजों से प्राप्त जानकारियों को और उसके सामाजिक-राजनीतिक परिवेश में उपलब्ध यथार्थ को टटोलते हैं तो अनेक मौलिक बातें सामने आती हैं जो उनकी दृष्टि में महत्त्व का नहीं होता है, लेकिन सामाजिक-राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पक्षों को समझने के लिए उसकी उपयोगिता होती है। मौखिक इतिहास परंपरा विषय के कठोर अनुशासन और औपचारिकता, दोनों से बिल्कुल मुक्त रहता है।
मौखिक इतिहास परंपरा की एक और खासियत है। यह जानकारी के फलक को बड़ा बना देता है। लिखित इतिहास पर चाहे-अनचाहे कुलीनों और विशेषज्ञों का एकाधिकार होता है। उसका परिणाम पूरी दुनिया देख रही है। जो लिखा हुआ परोसा जाता है और जो लोग अपनी बुद्धि-विवेक से जानते और समझते हैं, उसके बीच बड़ी खाई है। द्वितीय विश्वयुद्ध पर जो लिखा गया और जो हकीकत था, उसमें अंतर महसूस हुआ। अमेरिकी इतिहासकार स्टड तारकेल ने द्वितीय विश्वयुद्ध होने और उसके परिणामों से जुड़े दुनिया भर के लोगों का साक्षात्कार किया जो ‘द गुड वार’ के नाम से प्रकाशित हुआ।
हम सब इस विडंबना से सुपरिचित हैं कि पाश्चात्य जगत की कही गई बातें और किया गया काम पूरी दुनिया की कही और की गई बात के रूप में मान लिया जाता है। यह ज्ञान और समझ का उपनिवेशवाद अब भी जारी है। भूगोल और राजनीति पर साम्राज्यवाद का अंत हो गया, पर विचारों का स्वराज अभी भी सूर्योदय से दूर है। भारतीय दार्शनिक प्रो कृष्ण चंद्र भट्टाचार्य ने 1931 में आशुतोष मेमोरियल व्याख्यान (कोलकाता) में इस बात को बखूबी रखा था कि कैसे पाश्चात्य जगत उपनिवेश के लोगों के मन मस्तिष्क को धीरे-धीरे अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लेता है और वे दासत्व को अपनी प्रगति और आधुनिकता मान बैठते हैं। पर उनका भाषण जो भारतीय पाठ्यक्रम का अनिवार्यत: हिस्सा होना चाहिए, वह भी आंखों से ओझल है। सांकेतिकता ने हमारे विमर्श, समझ, अभिव्यक्ति और ज्ञान-बोध को इतना जकड़ लिया है कि हम किसी विषय की गहराई में जाने से परहेज करते रहते हैं।
इसी विडंबना का परिणाम है कि मौखिक इतिहास परंपरा का जनक अमेरिकी इतिहासकार डॉ. अल्लान नेविंस को माना जाता है। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में (1963) मौखिक इतिहास का कार्य शुरू किया था। आठ हजार साक्षात्कारों को दर्ज किया गया, जो दस लाख पृष्ठों में लिखित रूप से हुआ। मौखिक इतिहास परंपरा पर जो लेख लिखे जाते हैं या भाषण दिए जाते हैं, उसमें इसी को मौखिक इतिहास परंपरा की शुरुआत मान लिया जाता है। इसका एक निहितार्थ होता है कि नेविंस से पहले दुनिया इस विधा से वंचित थी। ऐसा मानना पूरे संसार की ज्ञान परंपरा और शैली को पश्चिम के ज्ञान के साम्राज्यवाद के हवाले कर देना है।
सच्चाई यह है भारत मौखिक इतिहास परंपरा का जन्मस्थल है। प्राचीन समय से हम अपने व्यक्तिगत और सामुदायिक परंपराओं और संस्कृति को लोक-कथा, लोक नृत्य, लोक गीतों द्वारा अभिव्यक्त करते रहे हैं। जितना हमारे पास लिखित सामग्री है, उससे कई गुना अधिक अलिखित सामग्री इतिहास के प्रवाह में विद्यमान है। लिखित सामग्री श्रुति और स्मृति के रूप में विद्यमान है।
हमने मस्तिष्क के स्वावलंबन को ज्ञान-प्रवाह में अनिवार्य माना है। इसे ‘स्मृति’ कहते हैं। जातक कथाएं, पंचतंत्र (पांचवी सदी), कथा सरितसागर (ग्यारहवीं सदी) श्रुति-स्मृति के पुस्तकाकार रूप में उदाहरण हैं। रामलीला और रासलीला के अतिरिक्त स्थानीय स्तरों पर अनेक और अनंत स्वरूप ने श्रुति-स्मृति की परंपरा सभ्यता और संस्कृति की धरोहरों को मृत नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री द्वारा ‘मन की बात’ में उठाए जाने के तीन आयाम हैं।
पहला, देश के विश्वविद्यालय या पुस्तकालय इस विधा को पुनर्जीवित कर विस्मृत हो रही घटनाओं, जानकारियों को एकत्रित करें। देश के बंटवारे को ही लें। लाखों लोग प्रभावित हुए और उसके कारण, प्रक्रिया और परिणाम के साक्षी थे। उनके प्रत्यक्ष अनुभवों को हम बटोर नहीं पाए। यह भारत के इतिहासकारों की सबसे बड़ी त्रासदी है। न ही आपातकाल से जुड़े लोगों का दास्तान एकत्रित कर पाए। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी ने इस काम को बखूबी आगे बढ़ाया था। पर एक ही प्रकार के वैचारिक पक्ष के लोगों का मौखिक इतिहास एकत्रित किया गया। देश के बड़े विश्वविद्यालयों/ पुस्तकालयों ने इसे भी जरूरी नहीं समझा। प्रधानमंत्री की मौखिक इतिहास दृष्टि भारतीय सभ्यता के बिखरे हुए असीमित आयामों को जोड़ने के लिए महत्त्वपूर्ण संदेश है। इस संबंध में शिक्षा से जुड़े हुए सभी सगठनों, खासकर शिक्षा मंत्रालय का योगदान अपेक्षित है।
दूसरा, श्रुति-स्मृति का कठोर सत्य सामने आता है। जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम, आचार्य जेबी कृपलानी जैसे लोगों द्वारा दिया गया साक्षात्कार मौखिक इतिहास के रूप में उपलब्ध है। उन पर या उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों से कई गुणा अधिक उनके सामाजिक-राजनीतिक जीवन, समकालीन राजनीतिक परिवेश की समझ बनती है। तीसरा, इससे बड़े प्रामाणिक ज्ञान और छोटे अप्रामाणिक ज्ञान का कृत्रिम अंतर समाप्त हो पाएगा। ज्ञान का लोक से जीवंत जुड़ाव हो पाएगा। लेकिन मौखिक इतिहास को श्रुति-स्मृति में ढालना आसान नहीं है। यह गंभीर कार्य है। साक्षात्कार करने वाले की अपनी विद्वता, समझ और जैसे मकड़ा जाल बुनता है, वैसी क्षमता आवश्यक है। यह तभी संभव है, जब विश्वविद्यालय इसे चुनौती के रूप में लें। हजारों साल की सभ्यता में हम अपनी परंपराओं और जानकारियों को विस्मृत होते देख रहे हैं। प्रधानमंत्री इसी बेसुधपने को संबोधित कर रहे थे।