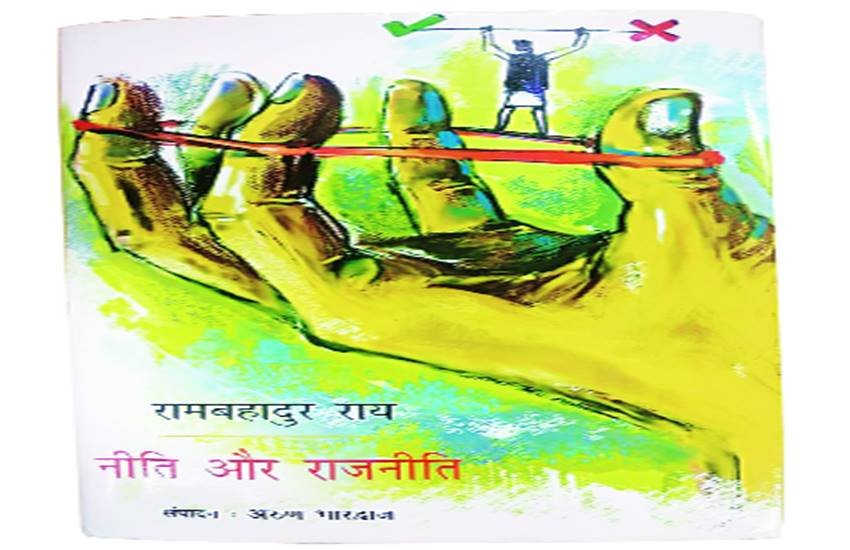दैनिक ‘जनसत्ता’ में 1998 से 2004 तक प्रकाशित होने वाला स्तंभ ‘पड़ताल’ अपनी अलग छाप छोड़ चुका था। यह वह दौर था जब राजग गठबंधन पहली बार सत्ता में आया था। अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी भाजपा के पर्याय बन चुके थे। उदारीकरण अपना असर दिखाने लगा था और भारतीय संसद के वाल स्ट्रीट से संबंध पर सवाल उठने लगे थे। राजनीतिक स्वार्थ के लिए जुड़ती और खुलती गठबंधनों की गांठ देखकर लग रहा था कि भारतीय राजनीति में जो मर्यादा चटखी है क्या वह कभी जुड़ पाएगी। इसे चाहे कितना भी जोड़ने की कोशिश करेंगे पर जनतंत्र के प्रेम पर गांठ तो पड़ ही जाएगी। यह लेखों का संग्रह जब किताबी रूप में आया है तो 1998 से लेकर 2004 का राजनीतिक इतिहास बन गया है।
‘जनसत्ता’ में छपे रामबहादुर राय के लेखों का संग्रह अरुण भारद्वाज के संपादन में ‘नीति और राजनीति’ के रूप में आकर बताता है कि एक अखबारी स्तंभ कितना अहम हो सकता है। इस किताब के 85 लेखों से समझा जा सकता है कि राजनीतिक टिप्पणी किस तरह कालजयी हो सकती है। यह किताब इस बात की भी तस्दीक करती है कि भारतीय राजनीति की नब्ज वही पकड़ सकता है जो यहां की जुबान और मिट्टी की पत्रकारिता करे।
‘नीति और राजनीति’ में माजी आज को मांज रहा है। जिक्र है कि 1999 में किस तरह शरद पवार ने विदेशी मूल के मुद्दे पर सोनिया गांधी से अलग होकर नई पार्टी का गठन किया था। आज शरद पवार उन्हीं सोनिया गांधी के साथ देश और संविधान बचाने के लिए गठबंधन कर रहे हैं। इस किताब में दर्ज लेखों में मंदिर निर्माण के मुद्दे पर संघ का भाजपा से मोहभंग हो रहा था और आज मंदिर वहीं बन रहा है और उसकी तारीख भी बता दी गई है। यह वह दौर था जब विजुअल मीडिया पर उदारीकरण का कब्जा हो गया था और भारतीय जनतंत्र पर पेड न्यूज का धब्बा लग चुका था। संसद की कार्यवाही घर-घर में जीवंत हो चुकी थी और जनसभाओं में बोलने वाले अटल बिहारी वाजपेयी का सुर संसद में किस तरह बदल जाता है वह जनता सीधे देख रही थी। सत्ता और धनबल के खेल की कवरेज में पत्रकारिता को नाकाम बताते हुए स्टिंग ऑपरेशन और जासूसी का ‘तहलका’ खड़ा हो गया था।
ये लेख अलग-अलग तारीखों पर लिखे गए हैं, और तारीखी इस बात में हैं कि टिप्पणीकार के सुर कहीं नहीं बदले हैं। शुरू से आखिर तक सत्ता को लेकर बागी तेवर अपनाए हुए हैं। इस तरह ‘यथावत’ को संभालना मुश्किल होता है। 1998 से 2004 तक की पड़ताल निर्मोही है। फकीर और कबीर परंपरा को आगे बढ़ाया जाए तो वह रामबहादुर राय के लेखन में दिखता है। कालजयी राजनीतिक टिप्पणी लिखने के लिए फकीर या कबीर सरीखा होना पड़ता है।
इस किताब के लेखों की खासियत है कि सत्ता के साधकों पर सवाल खड़े करते हुए अगर पाठकों की श्रद्धा उमड़ती है तो राजनीति के फकीरों पर। कौन हैं वे राजनीति के फकीर-गोविंदाचार्य, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, चंद्रशेखर और जॉर्ज फर्नांडीज। ये वो नेता हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति और राजनीति को एक समझते हुए फक्कड़पने की राजनीति की। किताब के लेखों को पढ़ने के बाद जिस जीवित व्यक्ति के बारे में सबसे ज्यादा श्रद्धा उमड़ेगी और पाठक अपनी पड़ताल करना चाहेगा वे हैं गोविंदाचार्य। मुरली मनोहर जोशी मानव संसाधन को देश की माटी से जोड़ने की कोशिश करते हैं तो लेखक की नजर उन पर भी है।
एक सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से चेतन देश में ऐसे लेख कब लिखे जा सकते हैं इसका जवाब इसी किताब की भूमिका में है कि अज्ञेय मानते थे कि जिस रचना में लेखक की सांस्कृतिक अस्मिता मुखर न हो, जहां पहचान उभरकर प्रभावी न हो सके, वह रचना नहीं है। लेखक-पत्रकार अपनी सांस्कृतिक पहचान को लगातार धारण किए रहते हैं। रामबहादुर राय महाभारत के संजय की तरह हैं। राजनीति की युद्धभूमि से कटी जनता के लिए संसद का सीधा प्रसार करते हैं तो इनकी भाषा लोकपक्ष की होती है। इनका प्रतिरोध सत्ता से होता है संस्कृति के लिए। भारत की राजनीति कैसी हो, भारत की सांस्कृतिक चेतना को तज कर बनने वाली संसद का स्वरूप क्या होगा।
इस पुस्तक के पुरोवचन में जिस शब्द पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया, वह है आगत का अन्वेषण। इसमें अटल-आडवाणी के उत्कर्ष काल को उनके अवसान काल के रूप में वर्णित किया गया है। जो भारत को बदलने के लिए इतिहास में उसका हक देने के लिए आए थे वो कैसे बदल गए। सत्ता में आते ही भाजपा की उम्मीद वाले चेहरे कांग्रेस की भाषा कैसे बोलने लगे। कांग्रेस और भाजपा के दो ध्रुव में सतरंगी तीसरी शक्ति की पड़ताल भी की गई है। रामबहादुर राय भारतीय राजनीति और संसद को खरी-खरी सुनाते हैं, ‘जय-जयकार के जमावड़े से निंदकों को दूर रखो’। ‘हमारे यहां राजनीतिक दल कैसे चलें इस सवाल का हल होना बाकी है। दलीय प्रणाली विकसित ही नहीं हुई है’।
इस किताब का अहम पक्ष है इसकी भाषा। कहते हैं कि बसंत आता नहीं लाया जाता है। इनकी पूरी भाषा में वही बसंत लाने की कोशिश दिखती है। जब राजनीतिक टिप्पणीकार कहते हैं ‘भाजपा अपने गांव पहुंची’ और गांव का मतलब ‘नागपुर’ निकलता है तो इस शब्द-साधक की शक्ति को समझा जा सकता है। संघ के मुख्यालय नागपुर को गांव बता संघ और स्वदेशी के गर्भनाल संबंध को सामने रख देते हैं। वे संसद को देश की सबसे ऊंची पंचायत कहते हैं। पंचायत के लिए देश की सबसे छोटी संसद का इस्तेमाल तो होता रहा है लेकिन संसद के लिए सबसे ऊंची पंचायत का प्रयोग एकबारगी रोक कर कुछ सोचने के लिए मजबूर करता है।
भारत की राजनीति में जिस स्वदेशी को सिर के बल खड़ा कर दिया गया है यह शब्द उसे पांव के बल खड़ा कर देता है। रामबहादुर राय ‘पुरोहित’ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। गरीबी हटाओ और लोकतंत्र बचाओ जैसे नारे जब घिसे-पिटे तरीके से लगाए जाते हैं तो वे आगाह करते हैं कि जनता पुरोहितगीरी और नेतागीरी में फर्क करना जानती है। वे लिखते हैं, ‘राजनीतिक दल इस मुगालते में न रहें कि उनका कहा लोग उसी तरह मान लेंगे जैसे पुरोहित का मंत्र मान लिया जाता है’। आज के संदर्भ में इस किताब में चौंकाने वाला शब्द है ‘चौकीदार’ और ‘पहरेदार’ जो संसद और राजनेताओं के संदर्भ में है। लेखक जब लिखते हैं कि ‘बहस बासी है’ तो बासी जैसे देशज शब्द की खुशबू फैल जाती है। राजनेताओं के बनावटीपन पर एक जगह लिखते हैं, ‘जो साधना पड़े वह स्वभाव नहीं होता है’।
इस काल के लिए लेखक राजनीति का रसायनशास्त्र इस्तेमाल करते हैं जो बहुत सटीक है। इस किताब में सबसे अहम खंड है भाजपा पर लिखे लेख। क्योंकि यह वह समय था जब भाजपा पहली बार केंद्र में आई, एक वोट के जुगाड़ में नाकामी के कारण गिरी और आज इनकी ‘पड़ताल’ का वह वक्त है जब भाजपा प्रचंड बहुमत से केंद्र में है। इस किताब के नायक मुरली मनोहर जोशी वर्तमान सरकार में मार्गदर्शक हैं। भाजपा राजनीतिक शक्ति है तो संघ सांस्कृतिक और अब राजनीतिक शक्ति दोनों है। राजनीति और संस्कृति का टकराव इन लेखों में साफ-साफ दिखता है।