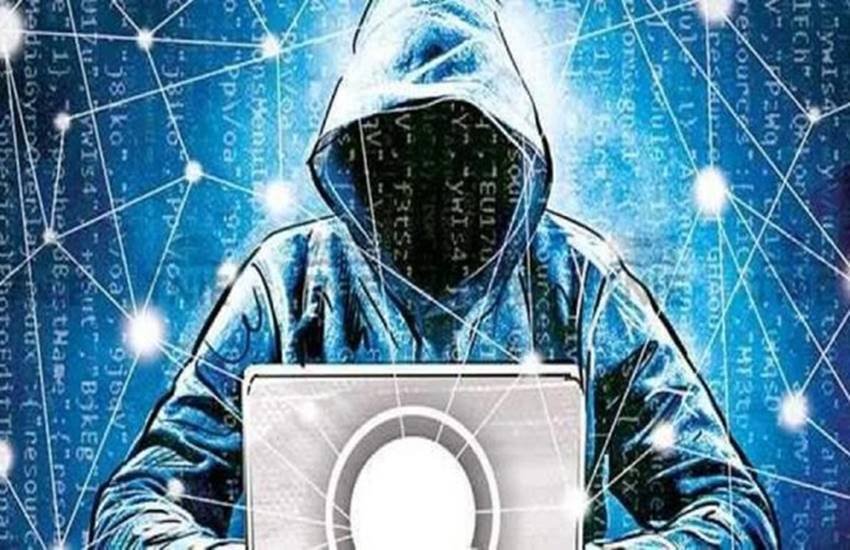विनोद के. शाह
भारतीय रिर्जव बैंक डिजिटलीकरण की नीति पर जोर तो देता है, लेकिन बैंक ग्राहकों को साइबर अपराध से बचाने के लिए उसने अब तक कोई प्रभावी व्यापक नीति नहीं बनाई है। ग्राहकों के व्यतिगत ब्योरे और उनके खाता संबंधी सर्वाधिक जानकारियां बैंकों और बीमा कंपनियों द्वारा ही दूसरों तक पहुंच रही हैं। मगर उन्हें सुरक्षित रखने में आरबीआइ, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने विशेष रुचि नहीं दिखाई है।
भारत सरकार देश में वित्तीय लेनदेन को अधिकाधिक डिजिटल बनाने की कोशिश में जुटी है। इसके लिए शहरी ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र के बैंकों, पोस्ट आफिसों के वित्तीय लेनदेन को भी डिजिटल किए जाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अंर्तगत ग्रामीण क्षेत्र के बैंक अब अपने अशिक्षित और कम पढ़े-लिखे ग्राहकों को भी डिजिटल लेनदेन करने का निर्देश दे रहे हैं।
स्थानीय बैंकों ने अब अपने नगद जमा निकासी के काउंटर कम कर दिए हैं। दस हजार तक की लेनदेन को नगद के बजाय एटीएम और मशीन से करने का दबाव डाला जा रहा है। मगर कम पढ़े-लिखे और अशिक्षित ग्राहकों को डिजिटल बैंक व्यवस्था से परिचित कराने का बैंकों और सरकार ने औपचारिकता के अलावा कोई प्रभावी इंतजाम नहीं किया है।
2018 में भारत सरकार द्वारा दिए डिजिटल इंडिया के नारे का जनून कुछ ऐसा है कि देश में डिजिटल बैंकिंग लेनदेन को प्रतिवर्ष तैंतीस फीसद की दर से बढ़ाया जा रहा है। वित्तवर्ष 2021-22 के फरवरी माह तक देश में 8.26 लाख करोड़ रुपए का डिजिटल वित्तीय लेनदेन हुआ, जो कि बीते वित्तवर्ष की तुलना में चार गुना अधिक है। भारतीय रिर्जव बैंक की ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की सिफारिश के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्किंग सुधार लाने, जीपीआरएस, पीएसटीएन नेटवर्क की प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच बनाने के लिए संचार और वित्त मंत्रालय ने एड़ी-चोटी का दम लगा रखा है। केंद्र और राज्य सरकारें हितग्राहियों को सीधे लाभांवित करने के लिए बैंकिंग प्रणाली की मदद ले रही हैं।
मगर वित्तीय समावेशन पर हुए एक निजी संस्थान के सर्वेक्षण में यह बात भी सामने आई है कि देश के इकहत्तर फीसद हितग्राही, जिनमें ग्रामीण और कामगार मजदूर शामिल हैं, को बैंकिंग प्रणाली की साक्षरता बिल्कुल नहीं है। ये लोग दूसरों की मदद से बैंकिंग गतिविधियों का संचालन कर पा रहे हैं। इससे साइबर ठगी की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। भारत सरकार के वित्तीय समावेशन योजना के अंर्तगत देश भर में खोले गए जीरो बैलेंस बैंक खाते, जिसमें सत्तर फीसद खाताधारी अशिक्षित ग्रामीण हैं, बैंक इन खाताधारियों को निशुल्क एटीएम प्रदान कर नगद काउंटर निकासी के बजाय क्योसेक सेंटरों से लेनदेन करने का दबाब बनाने लगे हैं। इसके ठीक विपरीत डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने वाले ग्राहकों से बढ़ती वित्तीय ठगी के आंकड़े अधिक चौकाने वाले हंै।
बीते चार बरसों में देश के ढाई लाख लोगों से सात सौ नब्बे करोड़ की ठगी के मामले दर्ज किए गए हैं। ये वे मामले हैं, जिनकी पुलिस को सूचना दी गई। जबकि प्रतिवर्ष पच्चीस फीसद ऐसे मामले भी आ रहे हैं, जिनकी शिकायत ही दर्ज नहीं हो पा रही है। वित्तवर्ष 2018-19 से 2021-22 के बीच चार वर्षों के दौरान लोकसभा में प्रस्तुत राज्यवार आंकड़ों में देश के सर्वाधिक शिकार दस राज्यों- महाराष्ट में 99,339 लोगों से 252.3 करोड़ रुपए, हरियाणा में 26,394 लोगों से 82.24 करोड रुपए, एनसीआर में 25,555 लोगों से 80.75 करोड़ रुपए, उप्र में 15,518 लोगों से 42.88 करोड़ रुपए, कर्नाटक में 12,628 से 56.45 करोड़, गुजरात में 10,881 से 28.08 करोड़, तेलांगाना में 7,303 से 22.4 करोड़, पश्चिम बंगाल में 4,276 से 35.38 करोड़ और राजस्थान में 3,739 लोगों से 19.14 करोड़ रुपए की साइबर ठगी हुई है।
साइबर अपराधियों के शिकार सभी श्रेणी के खाताधारी हैं। इसमें बुर्जग, महिलाओं के अलावा युवा, सरकारी कर्मचारी सहित देश के आइएएस अधिकारी तक शामिल हैं। ओटीपी, हैंकिंग, लाटरी, जाब स्कैम, सरकारी योजनाओं, निजी कंपनियों, बैंक और बीमा कंपनियों की फर्जी वेबसाइट, फेक कस्टमर केयर द्वारा केवाईसी, बीमा स्कैम और फर्जी एप्स के माध्यम से अधिकांश लोगों को शिकार बनाया गया है।
गर इसके बावजूद साइबर अपराध रोकने में केंद्र-राज्य सरकारों सहित बैंकों और बीमा कंपनियों की भूमिका ग्राहक के हित में प्रभावी नहीं हो पाई है। थानों में साइबर अपराध की प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया बोझिल है, जो कि पुलिस हवालदार के व्यवहार पर निर्भर रहती है। यही वजह भी है कि ठगी के शिकार कुछ लोग शिकायत दर्ज कराने भी नहीं जाते हैं। राष्टीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की स्थिति यह है कि उपलब्ध टोल फ्री नंबर 1930 से हजार कोशिशों के बाद भी संपर्क होता नहीं है।
आनलाइन लिखित शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया इतनी लंबी है कि शिक्षित जानकर भी परेशान हो जाता है। जैसे-तैसे शिकायत दर्ज हो भी जाए तो इसकी विवेचना के लिए साइबर सेल के पास पर्याप्त तकनीकी प्रशिक्षित पुलिसकर्मी ही नही हैं। अंतत: आवेदक की शिकायत को उसी स्थानीय पुलिस स्टेशन को विवेचना के लिए प्रेषित कर दिया जाता है, जिसने घटना के समय पीड़ित की शिकायत को गंभीरता से सुना तक नहीं था।
केंद्र से प्राप्त आंकड़ों में सबसे ज्यादा साइबर घोटाले पश्चिम बंगाल, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और नई दिल्ली से संचालित हो रहे हंै। मगर इन राज्यों की पुलिस दूसरे राज्यों की पुलिस को विवेचना करने, अपराधियों की धर-पकड़ करने में सहयोग नहीं करती है। मध्यप्रदेश पुलिस 1534 वर्चुअल वांटेड को तलाश रही है, जिनके मोबाइल नंबर और आइपी एड्रेस अठारह राज्यों से जुड़े हुए हैं।
ये अपराधी इन राज्यों से आपराधिक नेटवर्क संचालित कर रहे हैं। मगर इनमें से कई राज्यों की पुलिस अपराधियों की धर-पकड़ और विवेचना में सहयोग नहीं करती है। देश के नौ राज्यों ने केंद्र सरकार से आपसी विवाद के चलते सीबीआइ को राज्यों में मिली जनरल कंसेट (आम सहमति) को समाप्त कर दिया है। इसके चलते इन राज्यों में 173 आर्थिक अपराध के मामले, जो लगभग 21,074.43 करोड़ रुपए के हैं, हल नहीं हो पाए हैं।
भारतीय रिर्जव बैंक डिजिटलीकरण की नीति पर जोर तो देता है, लेकिन बैंक ग्राहकों को साइबर अपराध से बचाने के लिए उसने अब तक कोई प्रभावी व्यापक नीति नहीं बनाई है। ग्राहकों के व्यक्तिगत ब्योरे और उनके खाता संबंधी सर्वाधिक जानकारियां बैंकों और बीमा कंपनियों द्वारा ही दूसरों तक पहुंच रही हैं। मगर उन्हें सुरक्षित रखने में आरबीआइ और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने विशेष रुचि नहीं दिखाई है। ग्राहकों के आर्थिक हित संरक्षण में इनकी भूमिका मात्र औपचारिक बनी हुई है।
देश के कई बड़े बैंकों के नियम विरुद्ध अपने वीजा कार्डों की छपाई विदेशों में कराने के मामले उजागर हुए हैं। पर इन बैंकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने में आरबीआइ नाकाम रही है। साइबर सिक्योरिटी कंपनी साइबर एक्स 9 ने नबंवर, 2021 में अपने एक खुलासे में दावा किया था कि पंजाब नेशनल बैंक से सात माह तक अठारह करोड़ ग्राहकों का डाटा लीक होता रहा था। मगर बैंक ने इसे तकनीकी गड़बड़ी का मामला बता कर बड़े ही हल्के में मामले को शांत कर दिया था।
अक्सर साइबर अपराध के शिकार ग्राहक को यह भी नहीं मालूम होता कि उसे ठगी की सूचना कहां देनी है। आरबीआइ की नियमावली के अनुसार ठगी के शिकार बैंक ग्राहक को घटना के बहत्तर घंटे के भीतर अपने साथ हुई धोखाधड़ी की सूचना अपने बैंक को देने पर नुकसान की भरपाई संबंधित बैंक को बीमा कंपनी के माध्यम से करने का प्रावधान है। मगर बैंक सहित आरबीआइ इन सूचनाओं के सार्वजनिक प्रकाशन से अपने को दूर ही रखे हुए हैं। जबकि इस सूचना का प्रकाशन बैंक पटल पर किया जाना चाहिए। भारत सरकार के संकल्प में डिजिटल लेनदेन देश के विकास का पैमाना हो सकता है, लेकिन वास्तविक विकास के लिए देश के नागरिकों के आर्थिक हितों की सुरक्षा देना भी अब सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।