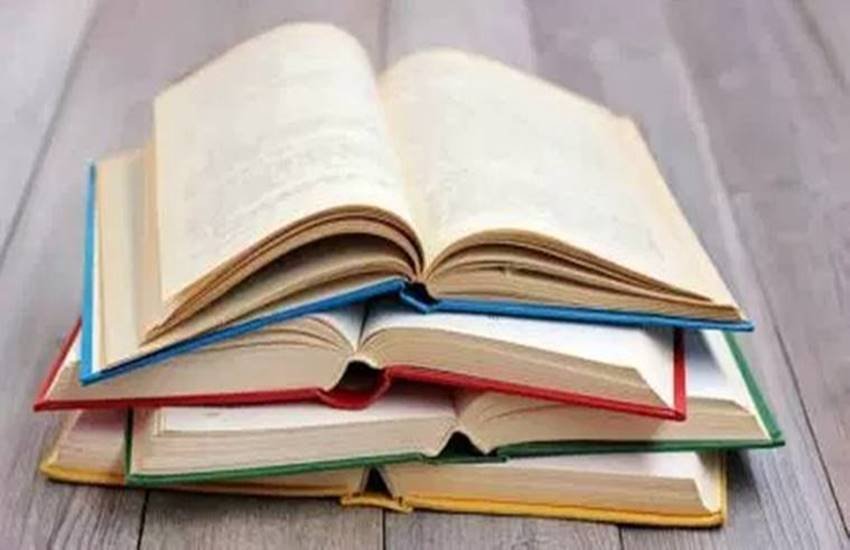राजकुमार भारद्वाज
दीर्घ समयांतराल में भारतीय उप महाद्वीप के सोचने-समझने के दृष्टिकोण में व्यापक स्तर पर बदलाव देखने को मिला है। यवन और पाश्चात्य संस्कृति के आक्रमण से भारतीय संस्कार और परिभाषाओं का तेजी से क्षरण हुआ। इसका प्रभाव यह हुआ कि आज पाश्चात्य संस्कृति के भौतिक अनुभवों पर आधारित संस्कृति से शिक्षित-प्रशिक्षित भारतीयों की भरमार हो गई है। इनमें आध्यात्म आधारित संस्कार का नितांत अभाव दिखता है। मोटे तौर पर अकादमिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण का मिश्रण लाभकारी प्रतीत होता है। इससे जीवन-यापन की सुगमता आसानी से संभव है। किंतु इस प्रसंग की कठिनाई यह प्रतीत होती है कि शिक्षण-प्रशिक्षण से नियोजन व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य बनता जा रहा है। भय यह है कि अर्थ प्रधान संकल्पना कहीं शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों को तिरोहित तो नहीं कर रही है!
पंडित दीन दयाल उपाध्याय ने मानव एकात्मवाद दर्शन में सुस्पष्ट मत रखा है कि ‘अनुभव प्रसारण की क्रिया को ही शिक्षा कहते हैं। यदि शिक्षा न हो तो समाज का जन्म ही न हो।’ यदि हम प्रस्तर युग का पृष्ठ अवलोकन करें तो पता चलता है कि मानव के विकास क्रम में मानव ने प्रारंभ में विभिन्न प्रकार की क्षतियों की कीमत पर अनुभव प्राप्त किया। उस कालखंड में सर्वाधिक संघर्ष आहार के लिए था।
आहार जुटाने और उसके लिए आवश्यक अस्त्र-शस्त्रों का विकास हुआ। इसके शोध और अन्वेषण में मानव का पूर्ववर्ती अनुभव काम आया। यह अनुभव पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हुआ। उसके बाद के अनुभवों का जीवन की अन्य आवश्यकताओं और चुनौतियों के संदर्भ में परिमार्जन किया गया और परिशोधित अनुभव भावी पीढ़ियों को हस्तांतरित किए गए। अनुभव का यह हस्तांतरण उत्तरवर्ती काल में संस्कार और शिक्षा का स्वरूप गढ़ता गया। इससे समाज की रचना हुई।
पंडित दीन दयाल जी की पीड़ा आज के संदर्भ में स्पष्ट जान पड़ती है। अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए बच्चे ‘इकतालीस और उनहत्तर कितना होता है’ पूछते हुए नजर आते हैं। उन्हें वैदिक काल गणना के चैत्र, पौष, माघ, फाल्गुन नहीं पता। वे आइटी के सफल पेशेवर हो सकते हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि उनकी माता का शव तब तक फ्रिज में रखा जाए या तेरहवीं को स्थगित कर दिया जाए कि जब तक वे स्वदेश वापस न आ जाएं, अथवा उनकी अनुपस्थिति में ही यह काम भी निबटा दिए जाएं।
ऐसे कई उदाहरण हैं। देश के एक नामी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के एक सेवानिवृत्त प्राध्यापक की पत्नी की असामयिक मृत्यु इसलिए हो गई कि उन्हें समय पर सही उपचार नहीं मिला, कारण कि अमेरिका में रहने वाला उनका बेटा बार-बार संदेश भेजने पर भी छह माह तक नहीं आया। ऐसी ही एक अन्य घटना में, गुरुग्राम की एक संभ्रांत बस्ती में रहने वाले एक शिक्षक का शव पंद्रह दिन तक शवगृह में रखा रहा। अमेरिका में रहने वाला उनका बेटा हवाई अड्डे से सीधा श्मशान घाट गया, संस्कार कर वहीं से अमेरिका चला गया। मां उसे रुकने का आग्रह करती रही, लेकिन वह नहीं रुका और दु:ख में यह मां भी असामयिक मृत्यु को प्राप्त हो गई। रोजगारोन्मुखी शिक्षा क्या वाकई इतनी निष्ठुर होती है कि आपसी संबंधों में स्नेह और प्रेम का परम तत्व शुष्क हो जाए। या फिर शिक्षा की अवसंरचना और ब्रांड पर इतना बल दिया गया है कि व्यक्ति से समष्टि के बीच संबंधों का प्रमुख अवयव विलोप हो गया है।
आज का युग वैमानन यांत्रिकी, सूचना तकनीक, चिकित्सा और सूक्ष्म जैविक तकनीक आदि विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार का युग है। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में इन्हीं आवश्यक और रोजगारोन्मुख विषयों के पठन-पाठन पर विशेष जोर है। फिर युवा कभी नहीं जान पाएगा कि महाराणा प्रताप ने मुगलों से संघर्ष करते हुए कभी जंगलों में घास की रोटियां खाई थीं या फिर चेरापूंजी में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। भारतवर्ष की अवधारणा ‘या विद्या सा विमुक्तये’ है, अर्थात विद्या यानि शिक्षा वह है, जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती हो। शिक्षा का अर्थ नियोजन मात्र में निहित नहीं हो सकता।
रोजगार और उससे जुड़ी शिक्षा से किसी को आपत्ति नहीं है। किंतु नियोजन शिक्षा की अंतिम सीमा नहीं हो सकती। जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन जीने के लिए होता है। उसके लिए लोक-व्यवहार में धन की आवश्यकता होती है। किंतु जीवन का वास्तविक ध्येय तो शिक्षा के माध्यम से मानव के पुरखों के अनुभवों को और अधिक समृद्ध करना और प्रकृति के गूढ़तम सिद्धांतों का विश्लेषण करना है, ताकि मानव पुनश्च अपनी प्रकृति में केंद्रित हो प्रकृति से प्रकृतिसम व्यवहार कर सके। क्या हमें विश्व ऐसा ही मिला था कि बेजिंग में चौबीस घंटे व्यतीत करने वाला व्यक्ति अनचाहे ही चालीस सिगरेट जितना धूम्रपान करने को विवश है। इसीलिए बार-बार यह प्रश्न हमें भीतर से विचलित करता है कि विकास की अंधी दौड़ ने कहां लाकर खड़ा कर दिया है?
रोजगारोन्मुखी शिक्षा के साथ अनिवार्य रूप से मानव को जब तक इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र आदि विषयों का गहन अध्ययन नहीं करवाया जाता, तब तक रोजगारोन्मुखी शिक्षा नगर-महानगर तो बसा देगी, लेकिन वे भुतहा शहर होंगे। वहां बसने वाला कोई नहीं होगा।
मात्र अध्यापन और शालेय शिक्षा के अतिरिक्त समाज में संस्कार और स्वाध्याय के बिना व्यक्ति की शिक्षा अधूरी कही जाएगी। शालेय शिक्षा अकेले ही मनुष्य का निर्माण नहीं करती। संस्कार और अध्यापन का बहुत-सा क्षेत्र ऐसा है, जो शालेय शिक्षा से बाहर है। इसका सीधा अर्थ है कि शालेय शिक्षा यानि विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों आदि में प्रदान और ग्रहण की जाने वाली शिक्षा के अतिरिक्त संस्कार और स्वाध्याय भी महत्त्वपूर्ण आधार हैं। इसे साधारण शब्दों में कहें तो यह अंतर पढ़े होने और कढ़े होने के बीच का अंतर है।
शालेय शिक्षा के साथ-साथ और उसके पश्चात भी व्यक्ति समाज के संपर्क में आता है। समाज के प्रत्येक अंग और लोक व्यवहार से उसके संस्कार निर्मित होते हैं। विद्यार्थी ग्रहण की गई शिक्षा को समाज के अनुकरण से तौलता है। यदि उसे प्राप्त शिक्षा और लोक व्यवहार में साम्य प्रतीत होता है, तो उसकी वह शैक्षणिक अनुभूति स्थायी भाव में परिवर्तित हो जाती है। वह उस भाव और ज्ञान पर और अधिक चिंतन और शोध करते हुए उस बिंदु और विषय को समृद्ध करता है।
विद्यार्थी गणित और विज्ञान के साथ विद्यालय में यह भी सीखता है कि अपने से बड़ों का आदर किया जाए। किंतु वह उस पर तब ही कार्यान्वयन कर पाता है, जब वह समाज में अन्यान्यों को ऐसा करते हुए देखता है। इस तरह समाज और लोक व्यवहार से उसे शिक्षा के अतिरिक्त श्रेष्ठ संस्कार मिलते हैं, जिसका वह अनुशीलन कर ग्रहीत शिक्षा को नए आयाम प्रदान करता है। विद्यार्थी अपने प्रयोगों और अनुभव से शिक्षा को प्रायोगिक तौर पर रूपांतरित करता है। संस्कार उसमें इस भाव का उद्दीपन करते हैं कि वे प्रयोग कितने लोकोपयोगी हैं। क्या उनका प्रतिफलन वर्तमान परिवेश और मानव के उत्तरोत्तर विकास के लिए सहायक है या कहीं चमक-धमक तक सीमित तो नहीं।
शिक्षा अनवरत प्रक्रिया है। शिक्षा में विरति, संरोध और स्थगन से बचने के लिए सतत स्वाध्याय चाहिए। यह विद्यार्थी को नूतन विचारों के प्रस्फुटन और तत्पश्चात उन्हें मूर्तरूप देने की प्रकिया से जोड़ता है। शिक्षा वह ऋण है, जो पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी पर चढ़ता है। विद्यार्थी इस ऋण से तब उऋण होता है, जब वह सिखावन और विषय का जीवन पर्यंत संवर्द्धन करता रहता है। इस भांति संस्कारित शिक्षा स्वाध्याय के अवधान से निखरती है। विषयवस्तु और ज्ञान का ओज बढ़ता है और जो सर्वहितकारी और सर्वसुखकारी होता है।