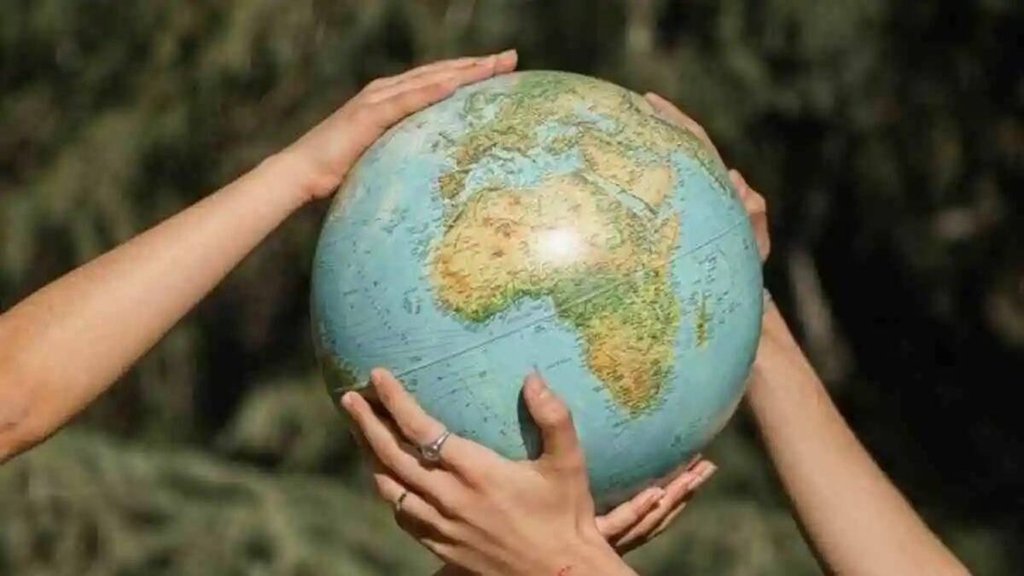वेंकटेश दत्ता
इस कोष के संचालन से जुड़े महत्त्वपूर्ण कई मुद्दे बेहद विवादास्पद हैं। इनमें कोष में भुगतान कौन करेगा, कौन इसका लाभ उठा पाएगा और इसे कैसे प्रबंधित किया जाएगा, जैसे प्रश्न शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हानि और क्षति के संबंध में विकासशील देशों की आवाज इस साल मिस्र में अधिक प्रमुखता से उठाई गई। पिछले वर्ष वार्ता के अंतिम दिनों में धनी देशों ने इस तरह के प्रस्तावों को खारिज कर दिया था। चीन, यूरोपीय संघ और कुछ अन्य विकसित देश पहली बार जलवायु हानि और क्षति कोष के समर्थन में सामने आए।
इस तरह अमेरिका ने अपनी लंबे समय से चली आ रही विरोध-नीति को पलट दिया। हानि और क्षति पर सीओपी-27 समझौता महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन बैठक में कई अन्य जरूरी मुद्दों पर बात नहीं हुई। इस बैठक में कमजोर और विकासशील देशों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश तो की गई, मगर स्वच्छ ऊर्जा की ओर आवश्यक सहयोग या धन जुटाने के लिए कोई प्रारूप प्रदान नहीं किया गया।
नया नुकसान और क्षति कोष पेरिस समझौते (2015) के तहत, जिम्मेदारी के न्यायसंगत बंटवारे की दिशा में पहला सैद्धांतिक कदम है। भविष्य में यह कैसे विकसित होगा, कहना मुश्किल है। इतना तो तय है कि जलवायु नुकसान और क्षति का मुद्दा विवादास्पद रहने वाला है, जाहिर है, आने वाले समय में कुछ देश इस संकल्प से पीछे हट जाएंगे।
पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं में 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को तैंतीस से पैंतीस फीसद तक कम करना शामिल था। विवाद इस बात को लेकर था कि जलवायु परिवर्तन से जुड़े ‘नुकसान और क्षति’ के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार, यानी वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाले देश कौन हैं, और इन्हें विकासशील देशों को कैसे भुगतान करना चाहिए, जिससे क्षतिपूर्ति की जा सके। यह तो सबको पता है कि इस वक्त संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और अन्य बड़े धनी देश जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार गैसों का सबसे ज्यादा उत्सर्जन करते हैं।
सीओपी-27 में चीन की घोषित स्थिति यह है कि वह नुकसान और क्षति कोष का समर्थन तो करता है, लेकिन एक विकासशील देश के रूप में वह कोष में किसी भी योगदान के लिए तैयार नहीं है। सीओपी-27 में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी बहुत सारी बहसें और घटनाक्रम हमारे सामूहिक और सतत विकास के मायने तय करेंगे, लेकिन जो बाइडेन और शी जिनपिंग का एक साथ मिलना और नुकसान और क्षति कोष की स्थापना इस बैठक की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।
दुनिया की कुल आबादी का सत्रह फीसद होने के बावजूद, भारत वैश्विक उत्सर्जन का लगभग सात फीसद उत्सर्जन करता है। 2019 के आंकड़ों के अनुसार चीन ग्रीन हाउस गैसों का सत्ताईस फीसद उत्सर्जन करता है, उसके बाद अमेरिका ग्यारह फीसद और फिर भारत 6.6 फीसद करता है। भारत हर साल लगभग तीन गीगाटन कार्बन डाइआक्साइड का उत्सर्जन करता है, इसमें प्रति व्यक्ति योगदान लगभग ढाई टन के बराबर है। यह दुनिया के प्रति व्यक्ति औसत का आधा है। यूएनईपी का अनुमान है कि 2030 तक यह तीन और चार टन के बीच होगा। भारत में कार्बन उत्सर्जन चीन की तुलना में बहुत कम है, लेकिन बहुत तेजी से बढ़ रहा है।
जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है। 1901 और 2018 के बीच भारत में औसत तापमान करीब 0.7 सेंटीग्रेड तक बढ़ गया है। देखने में यह बहुत कम लगता है, लेकिन प्रकृति के लिए यह बहुत ज्यादा है। ऐसा बदलाव प्रकृति की मुश्किल बढ़ा सकता है। कुछ अनुमानों के अनुसार, वर्तमान सदी के अंत तक भारत में सूखे की गंभीरता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। 2022 में उत्तर भारत में जो गर्मी की लहर आई थी, उसकी तीव्रता जलवायु परिवर्तन के कारण तीस गुना अधिक थी।
सितंबर-2021 तक भारत अपनी बिजली का 39.8 फीसद अक्षय ऊर्जा स्रोतों से और 60.2 फीसद बिजली जीवाश्म र्इंधन से उत्पन्न करता रहा है, जिसमें से इक्यावन फीसद कोयले से उत्पन्न होता है। भारत में कोयले के खनन के साथ-साथ, कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों में जलाने के लिए कोयले का आयात भी होता है। नए संयंत्रों के बनने की संभावना नहीं है, पुराने संयंत्रों को बंद किया जा सकता है और बाकी बचे संयंत्रों में अधिक से अधिक कोयला जलाया जा सकता है। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती से भारत में वायु प्रदूषण तो कम होगा ही, कटौती लागत से चार से पांच गुना ज्यादा स्वास्थ्य लाभ होगा, जो दुनिया में सबसे अधिक सस्ता होगा।
पिछले साल के सीओपी में कोयले को धीरे-धीरे कम करने का संकल्प लिया गया था और इस साल भारत ने सभी देशों को चुनौती दी है कि वे सभी जीवाश्म र्इंधनों को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए प्रतिबद्ध हों। हालांकि, सीओपी का अंतिम बयान केवल एक विविध ऊर्जा-मिश्रण की मांग करता है।
समझौते में ऐसा कुछ भी नहीं था, जिससे उत्सर्जन में कटौती पर अधिक कार्रवाई की जा सके या जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अधिक वित्तीय या तकनीकी संसाधन जुटाए जा सकें। उत्सर्जन में कटौती पर कुछ मजबूत प्रावधानों को लागू करने के प्रयासों को सभी पक्षों की सहमति नहीं मिली। सभी जीवाश्म र्इंधनों को चरणबद्ध रूप से बंद करने का प्रस्ताव, मूल रूप से भारत द्वारा आगे रखा गया था। इसे बड़ी संख्या में देशों का समर्थन भी हासिल हुआ, पर इसे अंतिम समझौते में शामिल नहीं किया गया।
जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए वित्तीय प्रवाह बढ़ाने पर प्रतिबद्धता की कमी सबसे बड़ी चुनौती रही है। शुद्ध-शून्य या नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के रूप में हर साल लगभग चार खरब डालर की आवश्यकता होगी। निम्न-कार्बन विकास पथ में वैश्विक परिवर्तन के लिए हर साल कम से कम चार से छह खरब डालर की आवश्यकता पड़ेगी। विकासशील देशों को ही जलवायु कार्य योजनाओं को पूरा करने के लिए 2030 से पहले लगभग 5.6 खरब डालर की आवश्यकता है। विकसित देशों ने अभी तक प्रति वर्ष सौ अरब डालर की अपेक्षाकृत छोटी राशि देने का अपना वादा भी पूरा नहीं किया है।
यह समझौता अक्षय ऊर्जा और हरित परियोजनाओं में अधिक से अधिक निवेश जुटाने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजार को बदलने की बात करता है। यह सुनिश्चित करता कि जलवायु कोष सभी के लिए, विशेष रूप से छोटे और कमजोर देशों को आसानी से सुलभ हो। हालांकि अभी इस पर और भी काम करने की जरूरत है।
जलवायु आपदाओं से प्रभावित विकासशील देश अब भी अपने पुनर्निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं। इस कोष के संचालन से जुड़े महत्त्वपूर्ण कई मुद्दे बेहद विवादास्पद हैं। इनमें कोष में भुगतान कौन करेगा, कौन इसका लाभ उठा पाएगा और इसे कैसे प्रबंधित किया जाएगा, जैसे प्रश्न शामिल हैं। इन सभी मुद्दों पर गौर करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें धन के स्रोतों की पहचान और विस्तार की संभावना भी शामिल है। कोष का निर्माण वास्तव में महत्त्वपूर्ण है, लेकिन यह केवल पहला कदम है, अभी बहुत सारे काम किए जाने बाकी हैं। फिर भी यह एक बड़ी सफलता है।
इस कोष के निर्माण ने विकसित देशों के बड़े प्रदूषकों को एक चेतावनी दी है कि वे अब अपने जलवायु विनाश से बच नहीं सकते। कई देश विनाशकारी तूफान, लू, बाढ़ और बढ़ते समुद्र स्तर का सामना कर रहे हैं। विकसित देशों को मिल कर काम करना और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नया कोष पूरी तरह से चालू हो सके और जलवायु परिवर्तन से जूझते सबसे कमजोर देशों और समुदायों को जवाब दे सके।