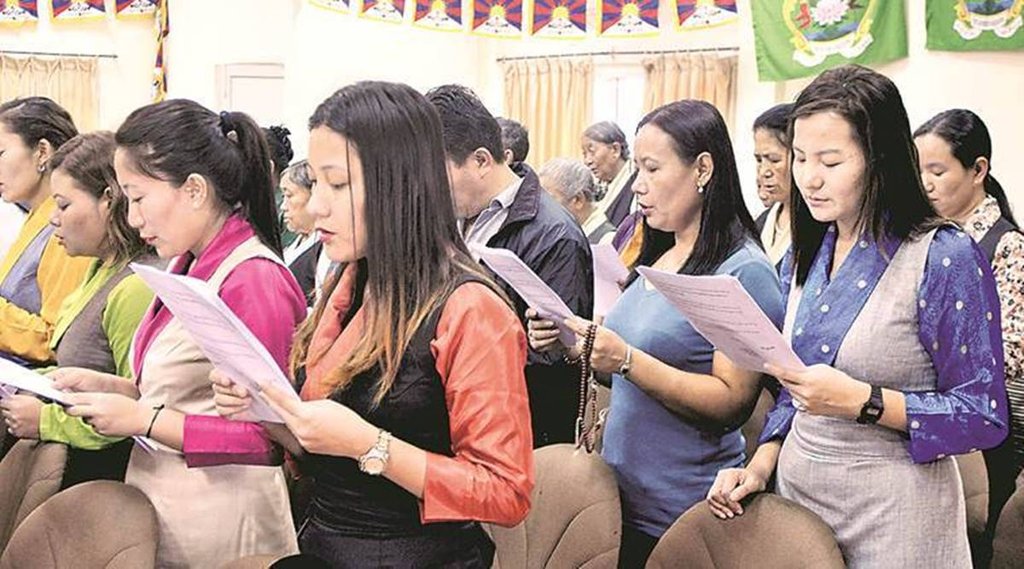सतीश कुमार
चीन के नजरिये से देखें तो तिब्बत उसकी सुरक्षा के लिए सबसे अहम है। वर्ष 2008 में चीन की केंद्रीय सैन्य कमान कहा था कि चीन की बुनियादी सुरक्षा तिब्बत पर टिकी है, ताइवान और हांगकांग बाद में आते है। 2018 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी यही बात दुहरायी थी। जब चीन को लगने लगा कि तिब्बत के इर्द-गिर्द बहुत कुछ बदल रहा है तो उन्होंने भारत के साथ सीमा संघर्ष की शुरू कर दिया। तिब्बत की अहमियत केवल तिब्बत तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका दायरा पूरे दक्षिण और पूर्व एशिया के लिए भी अहमियत रखता है। ब्रह्मपुत्र, यांगक्सी और इंडस जैसे नदियां तिब्बत के मुहाने से निकलती हैं और लगभग आधे से अधिक एशियाई देशों से गुजरती हैं। इसलिए अमेरिका द्वारा बनाया गया तिब्बत कानून का महत्त्व भारत और एशियाई देशों के लिए भी उतना ही अहम है, जितना कि तिब्बत के लिए।
सन 1949 में माओत्से तुंग ने कहा था कि जो भी देश तिब्बत के पठार को अपने कब्जे में कर लेता है हिमालय के तटवर्ती देश उसी के प्रभाव में होंगे और वही एशिया का मसीहा होगा। शी जिनपिंग की सोच भी यही है। चीन पहले से ही तिब्बत, लद्दाख, सिक्किम, नेपाल और भूटान को हाथ की पांच अंगुलियां मानता है।
भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में दलाई लामा की सरकार को भारत में मान्यता दी थी। लेकिन 2003 में भारत ने जब यह मान लिया था कि तिब्बत चीन का अभिन्न अंग है, उसके बाद से ही चीन तिब्बती संग्रहालय के हवाले यह बात साबित करने में जुट गया कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है। जबकि दुनिया जानती है कि 1911 में मांचू साम्राज्य के पतन के बाद तिब्बत 1912 से लेकर 1949 तक एक स्वतंत्र देश था। भारत की सीमा कभी भी चीन से नहीं मिलती थी, वह तिब्बत से मिलती थी। मैकमोहन रेखा समझौते में भी तिब्बत एक आजाद देश के रूप में था।
तिब्बत के मुद्दे पर अमेरिका फिर से चीन को घेरने में लग गया है। ऐसी ही कोशिश 2018 में भी की गई थी। प्रश्न यह उठता है कि क्या सच में अमेरिका दलाई लामा की खंडित प्रतिष्ठा को स्थापित करना चाहता है या यह महज एक नौटंकी है जो अंतराष्ट्रीय दंगल में एक दूसरे को परेशान के लिए की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि साठ के दशक से लेकर आज तक तिब्बत को लेकर अमेरिका की कोई स्थायी नीति नहीं रही है। समय और परिस्थिति के साथ नियम बदलते रहे हैं।
एक वक्त था जब दलाई लामा को अमेरिका सहित पूरे यूरोप में सबसे पसंदीदा शख्सियत के रूप में देखा जाता था। उस समय अमेरिका ने चीन के साथ अपने संबंधों की शुरुआत कर दलाई लामा की योजना को खटाई में डाल दिया था। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ अपने रिश्तों को लेकर काफी विवादास्पद रहे।
पिछले दिनों अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विदाई से पहले तिब्बत को लेकर विवादित विधेयक ‘रेसीप्रोकल एक्सेस टू तिब्बत एक्ट- 2018’ पर दस्तखत कर इसे कानून बना दिया था। इसके पारित होने से चीनी आधिपत्य वाले इस इलाके में अमेरिकी अधिकारियों व नागरिकों के प्रवेश का रास्ता खुल गया है। चीन ने इसका कड़ा विरोध किया है। चीन शुरू से इसका विरोध करता रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र पर वह अपना अधिकार मान कर अपनी मर्जी से किसी भी देश के राजनयिकों को प्रवेश देता है।
चीन इसलिए परेशान है क्योंकि इस कानून से उन चीनी अधिकारियों पर वीजा पाबंदी लगाने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा जो अमेरिकी नागरिकों, सरकारी अधिकारियों और पत्रकारों को तिब्बत के निर्वासित आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा के गृह क्षेत्र (तिब्बत) में जाने की अनुमति नहीं देते हैं। यह कानून अमेरिका के राजनयिकों, अधिकारियों, पत्रकारों और अन्य को तिब्बत में जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। ट्रंप ने यह कदम ऐसे वक्त में उठाया जबकि चीन इस संबंध में कानून पारित करने को लेकर अमेरिका से सख्त कूटनीतिक प्रतिरोध जता चुका था। उसने अमेरिका से इस सिलसिले में कानून नहीं बनाने का अनुरोध किया था। चीन का कहना है कि तिब्बत सदियों से उसका हिस्सा रहा है। चीनी शासन के खिलाफ विफल विद्रोह के बाद दलाई लामा 1959 में भारत पलायन कर गए थे।
तिब्बत का मुद्दा अमेरिका और चीन के बीच समुद्री लहरों की तरह कभी ऊपर उठता है, तो कभी अचानक गुम हो जाता है। दूसरा महत्त्वपूर्ण आयाम भारत की भूमिका और तिब्बत के सामरिक महत्त्व को लेकर है। जब अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों की गति में तेजी आती है, तो चीन को पसीना आने लगता है। इसका मूल कारण तिब्बत है। चीन के क्रांतिकारी नेता माओत्से तुंग ने एक पंक्ति में तिब्बत की सामरिक अहमियत बता दी थी। उन्होंने कहा था कि ‘तिब्बत दंत शृंखला है और चीन जिह्वा। जब तक दांत मजबूत हैं और बंद हैं तब तक चीन के लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन जैसे ही दंत शृंखला में सेंधमारी होगी, चीन की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी।’ चीन की सामरिक सोच यह रही है कि तिब्बत पर अमेरिका अपने बूते उसे कोई भी बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अमेरिका चीन से बहुत दूर है।
पचास के दशक में अमेरिका ने खंपा विद्रोहियों को हवा देकर तिब्बत को स्वतंत्र करने का असफल प्रयास किया था। पंडिच जवाहर लाल नेहरू के चीन प्रेम या कहें गुटनिरपेक्षता ने अमेरिकी पहल को भारत का समर्थन मिलने की राह बंद कर दी थी, इसलिए यह प्रयास असफल हो गया था। चीन मानता है कि भारत के पास इतना भी दम-खम नहीं है कि वह तिब्बत को आजाद करा सके। लेकिन चीन की बेचैनी उस वक्त बढ़ जाती है जब भारत और अमेरिका एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। तब उसे लगने लगता है कि तिब्बत खतरे में है और उसकी सुरक्षा को भेदा जा सकता है।
लेकिन यहां अहम प्रश्न यह है कि अमेरिका चीन के विरुद्ध इस मोर्चे पर सचमुच गंभीर है या यह महज दिखावटी क्रोध है। अभी तक अमेरिका चीन के खिलाफ एक कार्ड के रूप में तिब्बत का उपयोग करता रहा है। 1950 से 1972 तक शीत युद्ध के दौरान अमेरिका की मंशा साम्यवादी खेमे की घेरेबंदी करने की थी, क्योंकि उसे डर था कि चीन तिब्बत को अपने कब्जे में लेकर साम्यवाद का प्रसार पूरे दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में करेगा। 1973 में निक्सन और किसिंजर की जोड़ी ने चीन के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित कर वैश्विक राजनीति की धारा ही मोड़ दी। चीन को पूर्व सोवियत संघ के विरुद्ध इस्तेमाल करने की जोर अजमाइश की जाने लगी। इस तरह तिब्बत का मसला खटाई में पड़ गया। लेकिन वियतनाम की घटना के बाद तिब्बत का मुद्दा अमेरिका में फिर उछला। इस बार सामरिक सोच कम, मानवाधिकार हनन का दंश ज्यादा हावी रहा।
दूसरा बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि तिब्बत का मुद्दा अमेरिका की सरकारी फाइलों से निकल कर सार्वजनिक रूप ले चुका था। कई बड़े हॉलीवुड अभिनेता, लेखक और सांसद तिब्बत और दलाई लामा के मुरीद बन गए। इस बीच शीत युद्ध खत्म गया। अंतरराष्ट्रीय समीकरण तेजी से बदलने लगे। चीन आर्थिक रूप से मजबूत होता गया। उसे नाराज करना किसी भी देश के लिए कठिन हो गया। अमेरिका ने भी चुप्पी साध ली।
भारत और अमेरिका की मिलीभगत तिब्बत के मुद्दे पर बन सकती है। इसमें दोनों देशों का हित है। लेकिन अहम प्रश्न यह है कि अमेरिका तिब्बत को एक कार्ड के रूप में आखिरकार कब तक इस्तेमाल करता रहेगा। अगर यह कानून भी उसी मानसिकता के साथ बना है तो दलाई लामा के संदर्भ कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि उनकी समस्या और बढ़ेगी।