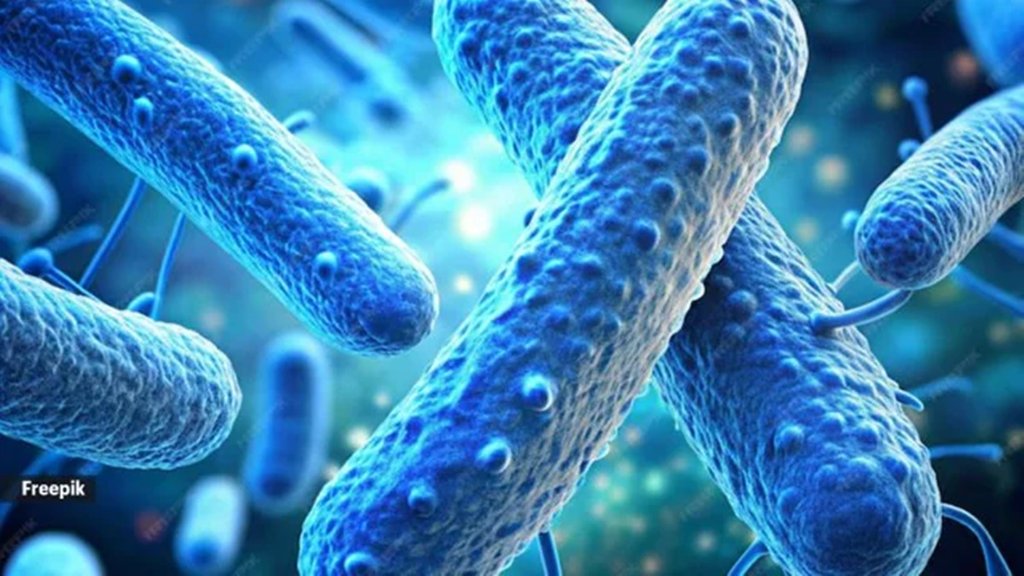एक समय आएगा जब बिना किसी उपकरण के किसी इंसान के बारे में शरीर में मौजूद कुछ सूक्ष्म जीवों से पता लगाया जा सकेगा। कौन कब और कहां था या अब कहां है, पता लग जाए, तो यह कैसा होगा! आम बोलचाल की भाषा में कहें तो कोई मनुष्य वास्तविक रूप से किस समय कहां है, इसका पता लगाना आसान हो जाए, तो दुनिया एक नए दौर में होगी। विज्ञान हमारे जीवन को बदल चुका है। रोज नए बदलाव सामने आ रहे हैं। तकनीक विज्ञान का हिस्सा है, लेकिन विज्ञान की दुनिया में इसके विकास और विस्तार ने नया संसार खोल दिया है। नई-नई तकनीक हर दिन लोगों को अचरज में डाल देती है। एक तकनीक आई नहीं कि उससे भी एक कदम आगे दूसरी तकनीक उसको बहुत जल्द पुराना कर देती है।
तकनीक की क्रांति ने मानव जीवन को सबसे अधिक प्रभावित किया है। ऐसी ही एक तकनीक है जीपीएस यानी ‘ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम’ जो एक उपग्रह आधारित प्रणाली है। जीपीएस तकनीक अब दुनिया भर में किए जाने वाले तमाम कार्यों का अभिन्न अंग भी बन गई है। यह हमारे मोबाइल, वाहन, घड़ी और अब तो बच्चों के स्कूल बैग में भी उपयोग होने लगी है। एक तरह से यह वह दौर है, जहां जीपीएस के बिना काफी कुछ असंभव-सा लगता है। इसीलिए इसके नाम और काम से आज हर कोई परिचित है।
तकनीक में गुम होता ज्ञान, मोबाइल के बिना जीवन बन रहा अप्रासंगिक
इस बीच अब वैज्ञानिकों के सामने एक चुनौती यह है कि क्या इंसान की कहीं भी मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है? इसको लेकर अब तक अलग-अलग विचार और प्रयोग सामने आए, लेकिन ये अव्यावहारिक ही रहे। पहनने योग्य जीपीएस उपकरण और ‘रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन’ यानी ‘आरएफआइडी’ प्रत्यारोपण जैसे विकल्प मौजूद हैं। ऐसे चिप को शरीर में लगाया जा सकता है। मगर वह व्यक्ति कहां है, इसकी जानकारी यह नहीं देती। सिर्फ पहचान बताती है। जीपीएस चिप को काम करने के लिए बाहरी उपग्रहों से संकेत की जरूरत होती है, लेकिन ऐसे संकेत त्वचा के नीचे नहीं पहुंचते हैं। वहीं ऐसी चिप को ऊर्जा के लिए बैटरी की भी जरूरत होगी जो स्वाभाविक रूप से छोटी होगी और सीमित समय तक ही चलेगी। इसे बार-बार बदलना भी कठिन होगा।
अब वैज्ञानिक एक नई खोज की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। यदि सब कुछ ठीक रहा, तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे शरीर में पाए जाने वाले जीवाणु, जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, वे तकनीक का हिस्सा बन जाएंगे। शरीर में लाखों की संख्या में अलग-अलग प्रकार के बैक्टीरिया यानी जीवाणु होते हैं। इनमें से कई शरीर में अंदर और बाहर पाए जाते हैं। ये अपनी प्रकृति अनुसार फायदेमंद और नुकसानदेह, दोनों ही होते हैं। मगर यही बैक्टीरिया जीपीएस का काम करने लगें, तो क्या होगा! स्वीडन के शोध दल ने एक कृत्रिम मेधा उपकरण विकसित कर ‘माइक्रोबायोम जियोग्राफिक पापुलेशन स्ट्रक्चर’ यानी ‘एमजीपीएस’ से यह पता लगाने में सफलता पाई है कि व्यक्ति किन स्थानों पर गया है।
तकनीक और समाज; जब विज्ञान से आगे बढ़ती है नीतियों की जरूरत
इसमें जीवाणुओं का विश्लेषण कर उन स्थानों के बारे में मालूम किया सकता है। यह कृत्रिम मेधा उपकरण जीवाणुओं को भौगोलिक फिंगरप्रिंट के रूप में उपयोग करते हुए यह पहचान कर सकता है कि कोई व्यक्ति कहां-कहां गया। शोधकर्ताओं ने पाया कि कई स्थानों पर जीवाणुओं की विशिष्ट आबादी होती है, इसलिए जब कोई, किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी सतह को छूता है, तो उस सतह पर मौजूद जीवाणु के संपर्क में आ जाता है। जिनका उपयोग उसे, उस सटीक स्थान तक वापस जोड़ने के लिए किया जा सकता है। मानव डीएनए के विपरीत जीवाणुओं का समूह विभिन्न वातावरण के संपर्क में आने पर लगातार बदलता रहता है।
यह जिज्ञासा भी स्वाभाविक है कि जीवाणुओं के उपयोग से कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति कहां-कहां गया था। अपने अध्ययन में, शोधकर्ताओं ने उन बैक्टीरिया पर ध्यान केंद्रित किया जो सूक्ष्म रूप से अंगुलियों पर निशान की तरह काम करते हैं। शहरी परिवेश, मिट्टी और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों से ‘माइक्रोबायोम’ के नमूनों के व्यापक डेटासेट का विश्लेषण किया और अंगुली के निशान की पहचान करने और उन्हें भौगोलिक निर्देशों से जोड़ने के लिए जब एक एआइ माडल को प्रशिक्षित किया, तो सकारात्मक नतीजे आए।
विज्ञान के प्रति रुचि जगाने की जरूरत
स्रोत स्थल की सटीकता भी सही निकली। निश्चित रूप से ‘माइक्रोबायोम डेटा’ ही इसके पीछे था। इस नए शोध की सफलता का पता इससे चलता है कि जब विभिन्न वातावरणों से मिले ‘माइक्रोबायोम डेटा’ का परीक्षण किया गया तो वे कसौटी पर खरे उतरे। शोध दल ने बानबे फीसद शहरी नमूनों में सही शहर की पहचान करने में सफलता पाई।
यकीनन, यह एक बहुत बड़ी तकनीक बन कर सामने आई है जो स्रोत का सटीक पता लगाने में सफल रही है। इससे चिकित्सा, महामारी विज्ञान और फारेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। इतना ही नहीं इस कृत्रिम मेधा उपकरण को चुनौती देते हुए हांगकांग में शोध दल ने 82 फीसद सटीकता के साथ उस भूमिगत स्टेशन का पता भी लगा लिया जहां से नमूने आए थे। जबकि न्यूयार्क में तो एक मीटर से कम दूरी पर भी परीक्षण किया गया, तो भी विश्वसनीयता की कसौटी पर विभिन्न स्थानों के अंतर को इसने बखूबी पहचान लिया।
इसे इस तरह भी समझा जा सकता है। सूक्ष्मजीव स्वयं को जब-तब बदलते रहते हैं। विशेषकर तब, जब हम अलग-अलग स्थानों पर जाते हैं तो उसी वातावरण में ढल जाते हैं। इससे तकनीक यह बताने में मददगार होती है कि सूक्ष्मजीव कुछ समय पहले कहां थे। इससे कई तरह की मदद मिलेगी। पहला किसी बीमारी के फैलाव और संक्रमण के स्रोत का पता चल जाएगा। दूसरा, आपराधिक जांच में भी सहयोग मिल सकेगा और अपराधी की पहचान करना आसान होगा। कोरोना के समय यह तकनीक होती, तो इतनी बड़ी त्रासदी से बचा जा सकता था। संक्रमण के स्रोत का पता लगाना नामुमकिन नहीं होता। ‘एमजीपीएस’ एआइ उपकरण हाल के स्थानों का पता लगाता है तथा जीवाणुओं को विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति से जोड़ कर फारेंसिक और महामारी विज्ञान में सहायता करता है।
अब वैज्ञानिक अपने इस शोध की सफलता के बाद इस एआइ का उपयोग करने के लिए उपकरणों को सक्षम या उन्नत बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। स्मार्ट फोन की स्क्रीन को अब और आधुनिक बनाया जाएगा, जिससे वह उपयोक्ता की अंगुलियों पर मौजूद बैक्टीरिया की पहचान कर ले और पता लगा सके कि वह किस जगह पर है। वैज्ञानिक आश्वस्त हैं कि भविष्य में जब यह तकनीक स्मार्टफोन में होगी, तो इससे हर किसी को फायदा मिल सकेगा।
स्मार्टफोन की स्क्रीन में नई सुविधाएं जोड़ी जाएंगी, जैसे जीवाणुओं का पता लगाने के लिए विशेष सेंसर लगेंगे, जिससे स्क्रीन, उपयोक्ता की अंगुलियों पर मौजूद सूक्ष्म जीवों की पहचान कर सकेगा और यह बता पाएगा कि वह कहां है। इस तकनीक से न केवल बीमारी फैलने पर रोक लग सकेगी, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारियां मिलेंगी। विज्ञान और तकनीक की यह उपलब्धि जीवन के विभिन्न पहलुओं को बदलने की क्षमता रखेगी। नई खोज मनुष्यों के जीवन में नया गुल खिलाने वाली है।