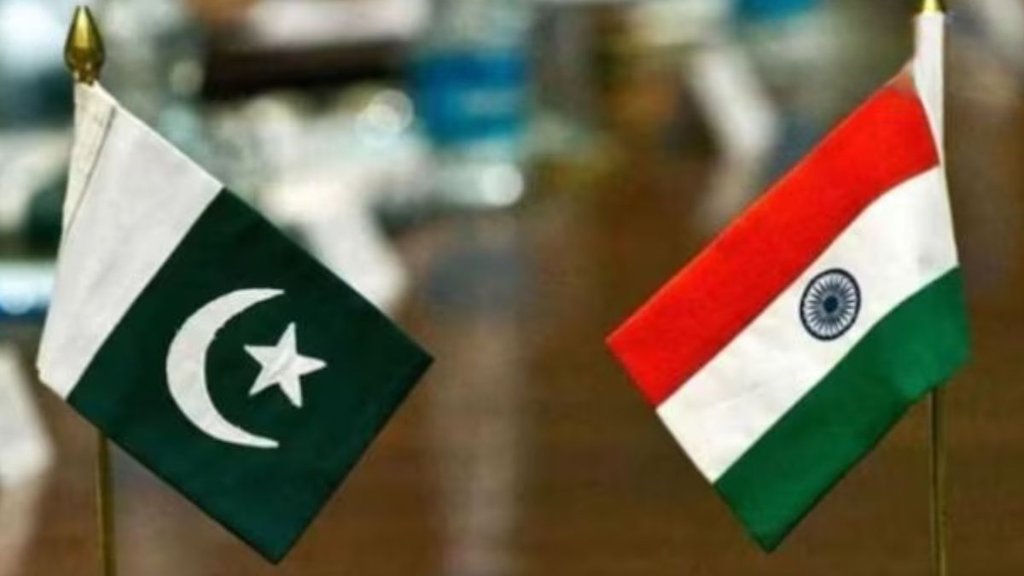Simla Agreement: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने कड़े कदम उठाए। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद गुरुवार को पाकिस्तान ने 1972 के शिमला समझौते को निलंबित कर दिया। यह 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित एक महत्वपूर्ण शांति संधि थी।
शिमला समझौता क्या है?
1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद 2 जुलाई 1972 को हस्ताक्षरित शिमला समझौते का उद्देश्य भारत और पाकिस्तान के बीच शांति बहाल करना और संबंधों को सामान्य बनाना था। युद्ध के परिणामस्वरूप भारत के हस्तक्षेप के बाद पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गया और स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ। हिमाचल प्रदेश के शिमला में हस्ताक्षरित इस संधि पर तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे।
समझौते में क्या कहा गया?
आधिकारिक बयान में कहा गया है कि भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार ने यह तय किया है कि दोनों देश अपने संबंधों को खराब करने वाले संघर्ष और टकराव को खत्म करें और मैत्रीपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने तथा उपमहाद्वीप में स्थायी शांति की स्थापना के लिए काम करें, ताकि दोनों देश अपने संसाधनों और ऊर्जा को अपने लोगों के कल्याण को आगे बढ़ाने के महत्वपूर्ण कार्य में लगा सकें।
प्रमुख समझौते-
संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांत और उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को नियंत्रित करेंगे।
दोनों देश द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से अथवा उनके बीच पारस्परिक रूप से सहमत किसी अन्य शांतिपूर्ण तरीके से अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए दृढ़संकल्पित हैं।
दोनों देशों के बीच किसी भी समस्या का अंतिम समाधान होने तक, कोई भी पक्ष एकतरफा रूप से स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगा तथा दोनों पक्ष शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण संबंधों के रखरखाव के लिए हानिकारक किसी भी कार्य के संगठन, सहायता या प्रोत्साहन को रोकेंगे।
सिंधु जल संधि क्या है? इसके रद्द होने से पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा; आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी
दोनों देशों के बीच मेल-मिलाप, अच्छे पड़ोसीपन और स्थायी शांति के लिए पूर्वापेक्षा यह है कि दोनों देश समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के प्रति सम्मान और एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की प्रतिबद्धता दिखाएं।
पिछले 25 वर्षों से दोनों देशों के बीच संबंधों में व्याप्त मूल मुद्दों और संघर्ष के कारणों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान किया जाएगा।
वे सदैव एक-दूसरे की राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता और संप्रभुता समानता का सम्मान करेंगे।
संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार वे एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल प्रयोग या धमकी से परहेज करेंगे।
शिमला समझौते के प्रमुख प्रावधान
शांतिपूर्ण द्विपक्षीय समाधान: दोनों देश तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के बिना द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से विवादों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध थे – एक ऐसा खंड जिसे भारत ने अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप का विरोध करने में लगातार उजागर किया है, खासकर कश्मीर मुद्दे में ।
नियंत्रण रेखा (एलओसी): समझौते ने 1971 की युद्धविराम रेखा को नियंत्रण रेखा (एलओसी) में बदल दिया, जिससे जम्मू और कश्मीर में प्रभावी रूप से एक वास्तविक सीमा स्थापित हो गई। इसने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी पक्ष इस रेखा को एकतरफा रूप से बदलने की कोशिश नहीं करेगा, जिससे यथास्थिति मजबूत हो।
क्षेत्र की वापसी:
भारत ने युद्ध के दौरान कब्जा की गई 13,000 वर्ग किमी से अधिक जमीन वापस कर दी, जिससे सद्भावना और शांति के लिए प्रतिबद्धता का प्रदर्शन हुआ। हालांकि, इसने चोरबत घाटी में तुरतुक और चालुंका जैसे रणनीतिक क्षेत्रों को बरकरार रखा।
अगस्त 2019 में भारत द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था, जिसने जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द कर दिया था। जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच कूटनीतिक ठहराव आ गया। इस्लामाबाद ने तब से संबंधों को कम कर दिया है और बार-बार कश्मीर मुद्दे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाया है। जिसमें शिमला समझौते का जिक्र किया गया है।
अब शिमला समझौते के निलंबन पाकिस्तान के दृष्टिकोण में रणनीतिक बदलाव का संकेत दे सकता है। यह अब कश्मीर संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए तीसरे पक्ष की भागीदारी – संभवतः संयुक्त राष्ट्र या चीन या इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) जैसे सहयोगियों से भी मांग कर सकता है। साथ ही कह सकता है कि यह शिमला ढांचे का सीधा उल्लंघन होगा।
नियंत्रण रेखा पर संभावित प्रभाव नियंत्रण
रेखा लंबे समय से दोनों देशों के बीच टकराव का केंद्र रही है, जहां अक्सर संघर्ष विराम उल्लंघन, सीमा पार से गोलाबारी और घुसपैठ की कोशिशें होती रहती हैं।
आगे क्या ?
शिमला समझौते के निलंबन से तत्काल सामरिक परिणाम नहीं हो सकते हैं, लेकिन इससे कूटनीतिक और सैन्य अस्थिरता के लिए रास्ता खुल सकता है। इससे क्षेत्रीय स्थिरता कमज़ोर हो सकती है और बातचीत की बची हुई संभावनाएं भी पटरी से उतर सकती हैं।
यह भी पढ़ें-
पाकिस्तान ने भारत के लिए बंद किया अपना एयर स्पेस, पानी रोकने को ही बता दिया युद्ध का ऐलान