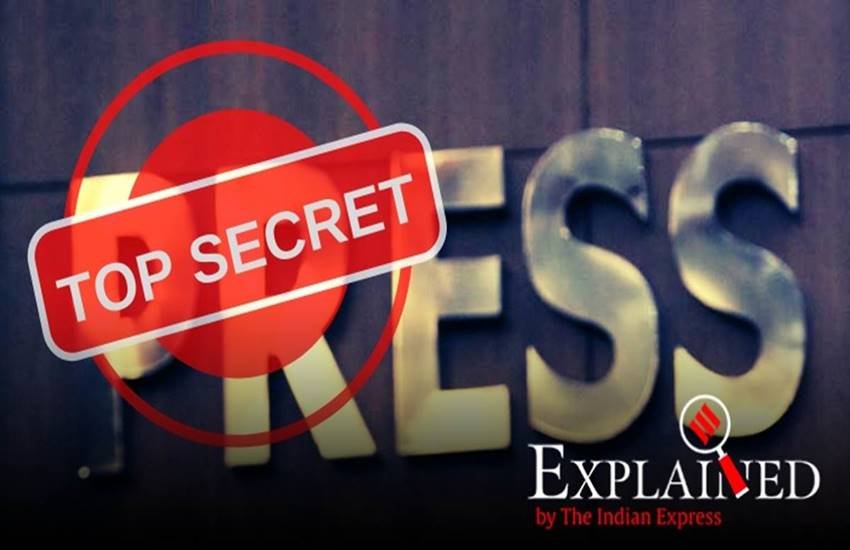मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने उन दो मीडिया संस्थाओं के खिलाफ ऑफसल सीक्रेट एक्ट (OSA) लागू करने की धमकी दी जिन्होंने राफेल डील से संबंधित दस्तावेज को उजागर किया। सरकार का कहना है कि डील से संबंधित दस्तावेज चोरी किए गए हैं। इस घटना के बाद से OSA को लेकर चर्चाएं काफी हैं। मीडिया इस एक्ट को लेकर खासा सतर्क दिखाई दे रही है। उसका मानना है कि यह एक्ट लोकतंत्र और उसके प्रोफेशन के लिए बाधक है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस एक्ट को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। आइए हम आपको विस्तार से इस एक्ट के बारे में बताते हैं।
क्या है ऑफिशल सीक्रेट एक्ट?
ऑफिशल सीक्रेट एक्ट को संक्षेप में OSA कहा जाता है। दरअसल, OSA का मूल अंग्रेजों के शासनकाल से जुड़ा है। अंग्रेजों ने 1889 में इंडियन ऑफिशल सीक्रेट एक्ट (Act XIV) नाम से कानून लाया। इसका मुख्य उद्देश्य उस दौरान देश में छपने वाले अख़बारों की आवाज को दबाना था। क्योंकि, अख़बार लगातार लोगों के भीतर राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा दे रहे थे और यह अंग्रेजी राज के लिए ख़तरा बन रहा था। उस दौर में ब्रिटिश हुकूमत ने इस कानून की मदद से विभिन्न भाषा में छपने वाले कई अखबारों का गला घोंट दिया। कई संपादकों को जेल में बंद किया गया।
इस कानून में आगे और बदलाव किए गए और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल दौरान इसे ‘इंडियन ऑफिशल सीक्रेट एक्ट 1904’ नाम दिया गया। 1923 में इस कानून का एक नया वर्जन सामने आया, जिसे ‘द इंडियन ऑफिशल सीक्रेट एक्ट (Act No XIX 1923) नाम दिया गया। इस कानून के मुताबिक सरकार की किसी भी गोपनीयता को जनता के बीच उजागर नहीं किया जा सकता था।
इस कानून की क्या शर्तें हैं?
यह कानून मुख्य रूप से दो मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार रखता है। इसके सेक्शन 3 के प्रावधन के तहत जासूसी करने और सेक्शन 5 के तहत गोपनीय जानकारी, पासवर्ड, स्केच, योजनाओं आदि को सार्वजनिक करने पर सजा दी जा सकती है। गौर करने वाली बात यह है कि दस्तावेजों के संबंध में कार्रवाई को लेकर संबंधित मंत्रालय OSA नहीं बल्कि अपने 1994 के दिशा निर्देशों का पालन करता है। हालांकि, यह कानून अक्सर सूचना के अधिकार (RTI) वाले कानून के आड़े आ जाता है। किसी भी विभाग से जानकारी हासिल करने के संबंध में सूचना के अधिकार कानून के साथ OSA का टकराव हो जाता है।
RTI और OSA में किसको दी जाती है वरीयता?
सूचना के अधिकार (RTI) के सेक्शन-22 OSA समेत तमाम प्रतिबंध लगाने वाले कानून पर वरीयता रखता है। ऐसे में अगर कोई जानकारी OSA का हवाला देकर नहीं साझा की जाती है, तब ऐसे में RTI उस कानून के प्रभाव को खत्म कर देता है। हालांकि, RTI के सेक्शन 8 और 9 के मुताबिक सरकार के पास अधिकार है कि वह जानकारी देने से इनकार कर दे। हालांकि, यदि सरकार किसी दस्तावेज को गोपनीय मानती है और वह OSA के सेक्शन 6 के प्रभाव क्षेत्र में आता है तो उसे RTI के दायरे से बाहर रखा जाता है। कानून के जानकार इसी को बहुत बड़ी खामी मानते हैं।
क्या OSA के प्रावधानों में बदलाव किए जा सकते हैं?
OSA के संदर्भ में पहली बार 1971 में लॉ कमिशन को ऑफिशल बॉडी बनाया गया। इसका उद्देश्य OSA की बारिकियों की समीक्षा करना था। राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के आरोप पर अपनी रिपोर्ट में लॉ कमिशन ने बताया कि अगर पब्लिकेशन कोई गोपनीय दस्तावेज लोगों के हित में छापता है और इससे राष्ट्रीय आपातकाल जैसी स्थिति नहीं उत्पन्न हो रही हो तब तक OSA को लागू नहीं किया जा सकता। हालांकि, उस दौरान लॉ कमिशन ने इस कानून में कोई भी बदलाव करने के सुझाव नहीं दिए।
2006 में दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिशन (ARC) ने OSA को खत्म करने की वकालत की। कमिशन ने इस कानून को पारदर्शी लोकतंत्र के लिए सेहतमंद नहीं माना था। इसके बाद वर्तमान सरकार ने 2015 में OSA और आरटीआई के प्रावधानों को लेकर एक कमेटी का गठन किया है। 16 जून, 2017 को अपनी रिपोर्ट में कमेटी ने सुझाव दिया कि OSA को और पारदर्शी बनाने की जरूरत है।
कब-कब OSA को लागू किया गया?
आजाद हिंदुस्तान में 1985 में इस कानून का इस्तेमाल कूमर नरायण जासूसी केस में किया गया। 2002 में उन 12 सदस्यों को 10 साल की सजा सुनाई गई जो प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति भवन में कार्यरत थे। इन लोगों को दूसरे देशों को गोपनीय दस्तावेज साझा करने का दोषी पाया गया। इसके अलावा एक और हाईप्रोफाइल केस सामने आया, जिसमें इसरो में जासूसी की बात सामने आई। इसरो वैज्ञानिक एस नंबी नारायण को भी OSA के तहत ट्रायल से गुजरना पड़ा। ताजा घटनाक्रम 2018 का है जब इस्लामाबाद में कार्यरत माधुरी गुप्ता को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को गोपनीय दस्तावेज देने के आरोप में तीन साल की सजा सुनाई गई। इसके अलावा कश्मीर टाइम्स के पत्रकार इफ्तकार गिलानी को भी OSA के तहत 2002 में गिरफ्तार किया गया था।