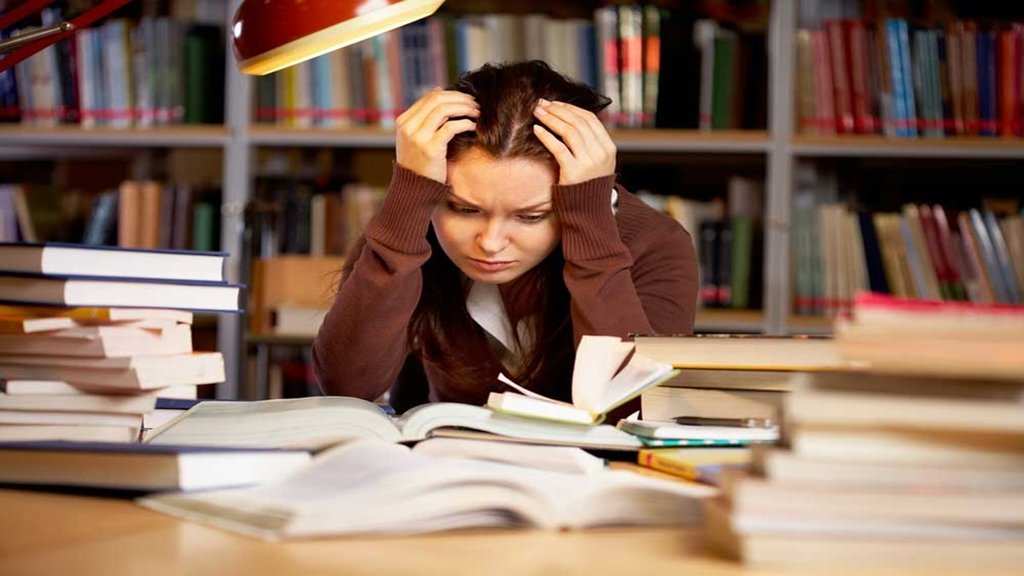शिक्षा का उद्देश्य तनाव देना नहीं, बल्कि तनाव को दूर भगाना होता है। जब शिक्षा तनाव देने का माध्यम बन जाए, तो वह उद्देश्यहीन हो जाती है। पिछले कुछ सालों से ऐसा लगने लगा है कि शिक्षा विद्यार्थियों में दबाव, कुंठा और पलायन की प्रवृत्ति विकसित कर रही है। शायद यही कारण है कि किशोरों और युवाओं में आत्महत्या की दर बढ़ रही है।
पिछले वर्ष केवल कोटा में उनतीस विद्यार्थियों ने आत्महत्या कर ली और इस साल के पहले महीने में ही वहां दो विद्यार्थियों ने खुद को फंदे पर लटका दिया, जोकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। समाज वैज्ञानिकों का मानना है कि शिक्षा विद्यार्थियों को चुनैतियों का सामना करना, जीवन में संघर्ष करना सिखाती है, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना और संवैधानिक मूल्यों को आत्मसात कर समाज का एक सभ्य नागरिक बनना सिखाती है। पर आत्महत्याओं की संख्या में होती वृद्धि तो कुछ और ही कहानी कहती है।
दरअसल, शिक्षा के बाजारीकरण ने शिक्षा को लाभ केंद्रित व्यवसाय बना दिया है। जहां लाभ कमाना प्रमुख लक्ष्य होता है, वहां सार्वजनिक हित या कल्याण की बात सोचना उचित प्रतीत नहीं होता। एक रपट के अनुसार देश में इस वक्त कोचिंग उद्योग करीब 58,088 करोड़ रुपए का है और वर्ष 2028 तक इसके 1,33,995 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो जाने का अनुमान है। विचार का विषय यह है कि आखिर क्यों इन कोचिंग संस्थानों का बाजार इतना फल-फूल रहा है। क्या विद्यालय और महाविद्यालय शिक्षा देने में असमर्थ हो गए हैं या वे बाजार की मांग के अनुरूप शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं और बच्चों को बाध्य होकर कोचिंग में जाना पड़ता है।
इसमें संदेह नहीं कि जबसे शिक्षण संस्थान उद्योग के रूप में उभर कर आए हैं और उद्योगपतियों ने शिक्षा को एक उत्पाद के रूप में क्रय-विक्रय की वस्तु बना दिया, तब से शिक्षा बाजार की जरूरतों के हिसाब से दी जाने लगी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाजार के अनुरूप शिक्षा समाज के विरुद्ध शिक्षा बनती जा रही है, क्योंकि वर्तमान शिक्षा बच्चों में पलायनवाद की प्रवृत्ति को विकसित कर रही है।
वे अपने पहले प्रयास में ही सफलता के उच्चतम शिखर को छूने की आकांक्षा रखते हैं और ऐसा न होने पर स्वयं को समाप्त करने से भी नहीं चूकते। इस बाजारवाद के दौर में शिक्षा महंगी और जान सस्ती हो गई है। पहले के समाजों में जब परिवारों का आकार बड़ा होता था और व्यक्ति को जीवन जीने के लिए अनेक संघर्ष करने पड़ते थे, तब भी वे आत्महत्या के बारे में नहीं सोचते थे। हर समस्या का सामना सूझ-बूझ और सामूहिक प्रयास से करने की कोशिश करते थे। मगर आज की किशोर और युवा पीढ़ी मानो जीवन जीना ही नहीं जानती।
इसका एक महत्त्वपूर्ण कारण हमारी शिक्षण प्रणाली भी है। स्कूल में बच्चे केवल प्रतिस्पर्धा करना नहीं सीखते, बल्कि समूह में कार्य करना, अपनी टीम का नेतृत्व करना, निर्णय लेना, मस्ती करना, लीक से हट कर सोचना, खेलना-कूदना, मित्रों के साथ त्योहार और उत्सव मनाना, सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों में सहभागिता करना और समाज में व्याप्त विविधता को भी सीखते हैं।
मगर अब छोटी-छोटी उम्र में कोचिंग का हिस्सा बनना और गलाकाट प्रतिस्पर्धा में शामिल होने से बच्चे इन सब गतिविधियों से वंचित होते जा रहे हैं। उन्हें अपने सहपाठियों में मित्र नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धी नजर आते हैं। नतीजतन, वे अपने मन की बातों को भी आपस में साझा नहीं कर पाते और तनाव में आकर ऐसे कदम उठा लेते हैं, जिनके परिणाम से संभवत: वे अवगत भी नहीं होते।
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जैसे शिक्षा और ज्ञान व्यक्तित्व विकास के लिए जरूरी होते हैं, वैसे ही सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेलकूद संबंधी गतिविधियां भी व्यक्तित्व विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्कूल में बच्चों को इन सब गतिविधियों का हिस्सा बनने का मौका मिलता है, लेकिन कोचिंग में नहीं। यही कारण है कि कोचिंग में पढ़ रहे बच्चे स्कूल से कहीं ज्यादा तनाव में होते हैं।
स्कूल में बच्चों के दोस्त होते हैं, जिनके साथ वे अपनी समस्याओं को साझा करके पढ़ाई का तनाव कम कर लेते हैं, लेकिन कोचिंग में बच्चे दोस्त नहीं बना पाते, क्योंकि उन्हें हर किसी में प्रतिस्पर्धी नजर आता है। उन्हें केवल पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए निर्देशित किया जाता है, बाकी सभी गतिविधियों को उपेक्षित करने की सलाह दी जाती है।
शायद पढ़ाई या प्रतियोगी परीक्षा में सफलता को ही वे जीवन और विफलता को मृत्यु समझने लगते हैं। ऐसी शिक्षा किस काम की, जो बच्चों पर इतना दबाव डाले कि वे दबाव को न झेल पाने के कारण आत्महत्या तक कर लें। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनसुार अब कोई कोचिंग संस्थान सोलह साल से कम उम्र के छात्र का नामांकन नहीं कर सकता।
सिर्फ माध्यमिक की परीक्षा के बाद ही नामांकन करना होगा। साथ ही अब कोचिंग संस्थान अच्छी रैंक और गुमराह करने वाले वादे भी नहीं कर सकते। अगर कोई संस्थान ऐसा करता है तो पहली बार पच्चीस हजार रुपए, फिर एक लाख रुपए के दंड का भागी होगा और जरूरत पड़ने पर उस संस्थान का पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है। इसे एक सकारात्मक और महत्त्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है।
हालांकि ऐसे दिशा-निर्देश पहले से मौजूद हैं, लेकिन उनकी पालना आज तक नहीं हो पाई। इसलिए कि दिशा-निर्देशों की पालना अनिवार्य नहीं मानी जाती। अगर निर्देशों को कठोरता से लिया जाता, तो अब तक इस दिशा में कुछ तो सुधार हो गया होता। इसलिए कठोर नियम बनाने की जरूरत है, ताकि शिक्षा को बाजार में लाभ की वस्तु बनने से रोका जा सके।
नेल्सन मंडेला का मानना था कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। मिशेल फूको मानते हैं कि ज्ञान शक्ति है। अगर ऐसा है तो फिर अधिकतर शिक्षित व्यक्ति ही आत्महत्या जैसे कदम क्यों उठाते हैं। आज के समय में ज्ञान और शिक्षा का जितना अधिक विस्तार हुआ है, ऐसा लगता है कि युवाओं में चुनौतियों का सामना करने या संघर्ष करने की क्षमता भी कम हुई है।
वे बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, इसलिए जरूरत है कि सरकार, प्रशासन, शिक्षक, बुद्धिजीवी सभी पाठ्यक्रमों और शिक्षा नीति का निर्माण करते समय इन सभी पक्षों पर गंभीर चिंतन करें और बाजार की मांग या जरूरत के अनुरूप नहीं, बल्कि विद्यार्थी और समाज की आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करें। बच्चों को रोजगार केंद्रित या केवल तथ्यों/ सूचनाओं को एकत्र करने वाली शिक्षा के लिए प्रेरित न करें, बल्कि मानवता और सामाजिकता सीखने और जीवन में संघर्ष करने का जज्बा विकसित करने का पाठ सीखने के लिए प्रेरित करें।