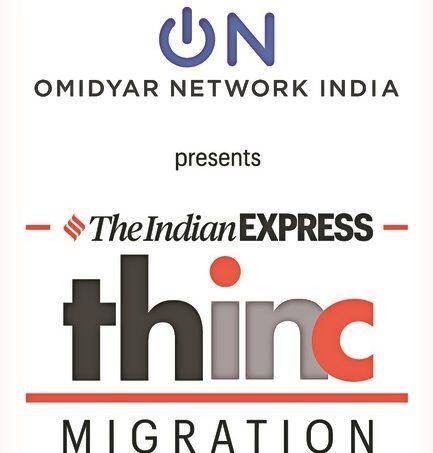दूसरी लहर में प्रवासी संकट
विनोद कापरी : मैं आज भी कई प्रवासी मजदूरों के संपर्क में हूं। मैं कहूंगा कि इस बार, जैसे-जैसे मौतें हुईं और आॅक्सीजन की कमी हुई, प्रवासी मजदूर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने घर का रुख कर लिया, केवल इस बार बसें और ट्रेनें चल रही थीं और वे घर पहुं च गए। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उन में से कई घर वापस चले गए क्योंकि वे आश्वस्त थे कि लॉकडाउन के बाद, उन्हें सबसे पहले नजरअंदाज किया जाएगा। उन्हें सबसे पहले घर छोड़ने के लिए कहा जाएगा। और अगर बाद में ट्रेनों को रोक दिया जाएगा, तो उन्हें साइकिल से और सबसे अधिक बुरी स्थिति में पैदल ही घर वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एक साल बाद भी, वे इस व्यवस्था पर भरोसा नहीं करसकते, वे ह म पर भरोसा नहीं कर सकते।
भारत में विशाल प्रवासी संकट के कारण
अर्चना गरोडिया गुप्ता : भारत में प्रवासियों की संख्या करीब 40 करोड़ है, जो प्रतिशत के लिहाज से संभवत: दुनिया में सबसे ज्यादा लगभग 30-35 प्रतिशत है। भारत में प्रवासी श्रमिकों का प्रतिशत सबसे अधिक है। यह एकतरफा विकास, कुछ निश्चित स्थानों पर ही नौकरियों की उ पलब्धता के कार ण हुआ है, और ये नौकरियां स्थायी नहीं हैं और इनसे पर्याप्त पारिश्रमिक नहीं प्राप्त होता है। कुछ लोग आकर बस जाते हैं लेकिन उन्हें शहर में अपने परिवार का भरण- पोषण करने के लिए एक स्थायी नौकरी और पर्याप्त आय की जरूरत होती है। अगर नौकरियां घर के करीब होतीं, तो इतना अधिक प्रवासी संकट नहीं होता। या यदि आप नौकरी के लिए दूसरे शहर में चले गए हैं, तो प्रवासी को वहां बसना भी पड़जाता है। किसी व्यक्ति के लिए पूरे साल अ पने परिवार से दूर रहना उचित नहीं है। हमें ऐसे ढांचे बनाने के बारे में सोचना होगा जिससे लोगों को अपने परिवारों के साथ रहने में सहायता मिल सकें। इसलिए नौकरियों की उपलब्धता पर ध्यान देना होगा और सरकार को एमएसएमई तथा श्रम प्रधान उद्योग को बढ़ावा देने पर ध्यान देना होगा।
क्या भारत में नागरिक समाज पर्याप्त सहयोग देता है?
अतुल सतीजा : जाहिर तौर पर यह दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी आपदा थी। लेकिन ह मने हर साल छोटे, नियमित भूकम्प, चक्रवात, बाढ़ और अन्य आपदाओं में नागरिक समाज की प्रतिक्रिया को एक जैसा देखा है। बचाव, राहत, कुछ रिकवरी और सहायता, और उसके बाद पुनर्वसन का कार्य किया जाता है। जब तक मीडिया में, बोर्डरूम में, ड्राइंग रूम में गर्मजोशी से चर्चा जारी रहती है, नागरिक समाज द्वारा सहायता का कार्य तेजी से चलता रहता है। आपदा के समय लोगों के लिए आगे आना और सहायता करना आसान होता है क्योंकि हम मनुष्य के रूप में जुड़े हुए हैं और सहानुभूति की मात्रा अधिक होती है। जब परिचर्चा बंद हो जाती है, तो हम सब अपने नियमित व्यस्त जीवन में वापस आ जाते हैं। इंडिया कोविड रिस्पांस फंड अर्थात आईसीआरएफ, जिसे हमने पिछले साल शुरू किया था और दुबारा इस साल भी, इस में हमारे पास 10 लाख डोनर हैं जिन्होंने आगे बढ़कर हमारे प्लेटफॉर्म पर दान दिया। हमारे पार्टनर प्लेटफॉर्म पर भी 25 लाख लोगों ने दान दिया।
यह केवल भारत में देने वालों का एक छोटा अंश है। जब हम लोगों पर भरोसा करते हैं तो हम देते हैं। इसलिए जब अपने ड्राइवर या नौकरानी, अपने समुदाय में किसी परिचित के कष्ट में होने की जानकारी मिलती है, तो हम मदद करते हैं। इसलिए, आपदा के समय सहायता वास्तव में कोई स मस्या नहीं है। होता क्या है कि स्थायी समस्याएं जैसा कि अर्चना ने कहा, जैसे आजीविका, रोजगार सृजन, लैंगिक संकट के लिए पुनर्वसन में निवेश करने की आवश्यकता की समझ का अभाव है। नागरिक स माज की भूमिका परि च र्चा करने, हितधारकों को जवाबदेह बनाने की है, सरकार की भूमिका नीतियों और बुनियादी ढांचे तैयार करने की है, लेकिन निजी क्षेत्र की भी भूमिका है कि वह आगे आए और प्रवासी कार्यबल में भाग्य को व्यवसाय के रूप में देखें।
संरचनात्मक हस्तक्षेप की आवश्यकता
रंजना कुमारी : देश में राज्य तंत्र की पूर्णत: संवेदनहीनता थी। वे समस्या का सामना नहीं करना चाहते थे। ये लोग कौन हैं? ये गांव के सबसे गरीब हैं, जो शहरों की ओर पलायन करते हैं। वे मौसमी प्रवासी नहीं हैं, बल्कि उन में बस जानेवाले भी हैं। यद्यपि उनके पास किसी तरह की नौकरी की गारंटी थी लेकिन वे लोग भी वापस चले गए क्योंकि उनकी नौकरियां चली गयीं या कंपनियां बंद हो गईं। नियोक्ताओं ने उनसे इतनी आसानी से कैसे छुटकारा पा लिया? किसी ने यह पूछने की जहमत नहीं उठाई कि नियोक्ताओं ने जिम्मेदारी क्यों नहीं ली। सरकार ने उनके बारे में कोई नीति नहीं बनाई। पुरुषों और महिलाओं के बीच टीकाकरण दरों में भी बड़ी असमानता है। वे स्वस्थ नहीं हैं और उनके पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है और अब उनका टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। हमें संरचनात्मक नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है। कोई भी अपने घर और गांव को छोड़ कर शहरी क्षेत्रों में न जाना चाहता, न संघर्ष करना चाहता है और न जीवन-या पन करना चाहता है। सेंट्रल विस्टा के बजाय ग्रा मी ण क्षेत्र में बहुतसारे बुनियादी ढां चे हमें चाहिए और इससे रोजगार पैदा होगा। ह में हर हाथ को का म देने की जरूरत है ताकि हर मुंहको निवाला िमल सके। मुझे लगता है कि इस स मय प्राथमिकताएं खो गई हैं।
घरों में रोजगार पैदा करना
गुप्ता : भारत में, हमारे पास शिल्पकारों का खजाना है, जो समाप्त हो रहे हैं। ये ऐसे कौशल हैं जिनकी मांग है। दुनिया में हस्तशिल्प की मांग करीब 400 अरब रुपए हैं और भारत सिर्फ एक अरब रुपए का निर्यात करता है जबकि हमारे पास् ादुनिया के करीब 30 फीसदी शिल्पकार हैं। महिलाओं को ई-कॉ मर्स प्लेटफॉ र्म पर लाने के लिए नेटवर्क बना कर हम गांवों में आजीविका और आय बढ़ा सकते हैं। आपके पास दुनिया भर में ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने इसे सफलता पूर्वक किया है। उदाहरण के लिए, चीन में टॉम्बो नामक एक मंच है जो ग्रामीण ई-कॉमर्स पर काम कर रहा है। यह अलीबाबा के स्वामित्व में है। सरकार के साथ काम करते हुए उन्होंने एक लाख गांवों को टॉम्बो गांव के रूप में नामित किया है। जिन गांवों में यह सफल रहा है, वहां रिवर्स माइग्रेशन (शहरों से गांव की ओर वापसी) होता है।