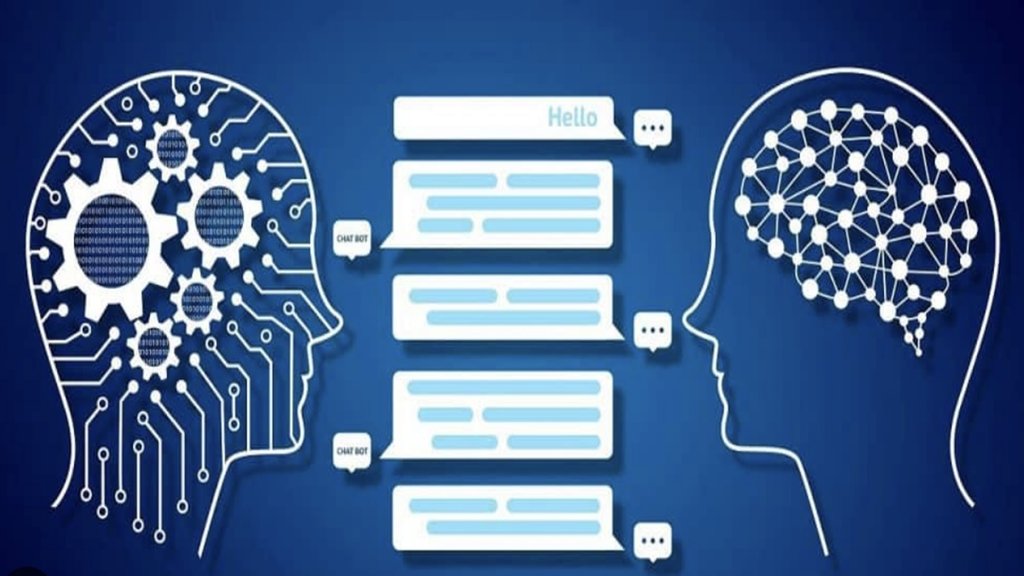भाषा व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है, वैसे ही जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। व्यक्ति की पहली भाषा ही उसकी जातीय पहचान और उसकी आंतरिक क्षमता के विस्तार का सशक्त माध्यम होती है। इसलिए व्यक्ति की क्षमता का महत्तम उद्घोष उसकी मातृभाषा में होता है। जाहिर है कि भारत जैसे बहुभाषिक देश में अल्पसंख्यक भाषाओं के संकुचन को स्वीकार करना दरअसल लोगों की मौलिक क्षमता के विस्तार में व्यवधान उत्पन्न करने के समान और राष्ट्र की व्यापक क्षमता के विकास को रोकने जैसा है।
हालांकि, भारत में भाषाई अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बहस पुरानी है, लेकिन धरातल पर जो नीति बनी, वह सब अंग्रेजी और उसके इर्द-गिर्द घूमती रही। इसलिए नीति-निर्माण, अनुपालन की मानसिकता, शिक्षण, शोध और रोजगार जैसे क्षेत्रों में अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ता गया। भारतीय भाषाओं को द्वितीयक होना पड़ा है। इसका जो नुकसान सामान्य संदर्भों में हुआ, उनका मूल्यांकन होना बाकी ही था कि आज इन्हीं कारणों से डिजिटल संदर्भों में भारतीय भाषाओं और प्रकारांतर से उनके मूल भाषा-भाषियों को जो नुकसान हो रहा है, वह पहले से अधिक भयावह है।
अगर राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया में देश की भाषाओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाई गई होती, तो भारतीय भाषाएं अंग्रेजी के संघर्ष में एक बेहतर स्थिति में होतीं और आज कृत्रिम मेधा वाले दौर में उन पर आसन्न नए खतरे अपेक्षाकृत कम होते। ध्यान रहे कि हमारे संविधान-निर्माता इसको लेकर सजग थे और भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 29 (1) के माध्यम से भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों की अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार, अनुच्छेद 29 (2) द्वारा राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश पाने का अधिकार और अनुच्छेद 30 (1) के माध्यम से भाषा सहित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित करने के अधिकार की व्यवस्था की गई थी। संयुक्त राष्ट्र घोषणा-पत्र के अनुच्छेद 1 (3) के माध्यम से भी आश्वासन दिया गया था कि वैश्विक मामलों में बिना किसी भाषाई भेदभाव के मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता और सम्मान को बढ़ावा दिया जाएगा।
आज भारत की विशाल आबादी, उसमें स्मार्टफोन के प्रयोक्ताओं की वृहद संख्या, उनमें इंटरनेट की खपत और नागरिकों की सोशल मीडिया में सामग्री निर्माणकर्ता के रूप में उपस्थिति अभूतपूर्व और संख्या की दृष्टि से वैश्विक स्तर पर निर्णायक है, लेकिन इन सबके बावजूद भारतीय भाषाओं की डिजिटल क्षमता द्वितीयक है। इसलिए भी हमने भाषाओं को द्वितीयक बनाए रखने को अपनी प्राथमिकता में शामिल कर लिया है।
इसीलिए वैश्विक आबादी में सर्वोच्च स्थान होने के बावजूद हमारी भाषाएं डिजिटल उत्पादों में उस मात्रा में नहीं दिखतीं। इंटरनेट सोसायटी फाउंडेशन के मई 2023 के एक आंकड़े के अनुसार वेब-पृष्ठों के माध्यम के रूप अंग्रेजी पचपन फीसद वेबसाइटों की भाषा है, दूसरे स्थान पर स्पेनिश है, जो महज पांच फीसद है। इस सूची के शीर्ष दस भाषाओं में किसी भारतीय भाषा का कोई नामलेवा भी नहीं है।
बात यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि इसी बुनियाद पर कृत्रिम मेधा में भाषाई सामर्थ्य विकसित होता है। यहां कृत्रिम मेधा की स्वीकृति की गति को समझना आवश्यक है। कृत्रिम मेधा टूल ‘चैटजीपीटी’ को अपने दस करोड़ ग्राहकों तक पहुंचने में केवल दो महीनों का समय लगा, जबकि इस संख्या तक पहुंच बनाने में दूसरे इंटरनेट उत्पाद, जैसे ट्विटर, को पांच साल और पांच महीने, फेसबुक को चार साल और छह महीने, वाट्सएप को तीन साल और छह महीने, इंस्टाग्राम को दो साल और छह महीने, गूगल को एक साल दो महीने लगा और टिकटाक को नौ महीने लगे थे। गौरतलब है कि इस गति में भारतीय भाषाएं तो द्वितीयक हैं, लेकिन संख्या बल में सर्वाधिक होने के कारण भारतीय उपभोक्ता प्राथमिक हैं, जिनको अपनी भाषाओं से परे अंग्रेजी की प्राथमिकता को स्वीकार करना पड़ रहा है। ऐसे में, हमारी स्थिति बिना किसी मेहनताना के मजदूर जैसी है।
इस वैश्विक प्रतिस्पर्धा में जब हमारे संविधान की आठवीं अनुसूची की भाषाएं नहीं हैं, तो अल्पसंख्यक भाषाओं की स्थिति क्या होगी, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। ऐसे में, इनसे उभरने वाले बाजार में भी उनके प्राथमिक होने के उम्मीद प्राय: नहीं करनी चाहिए, जब तक कि सरकार द्वारा व्यक्तिगत डिजिटल डाटा के मुक्त दोहन प्रक्रिया पर प्रभावी हस्तक्षेप न करे। दिलचस्प है कि भारतीय उपभोक्ताओं की डिजिटल गतिविधियों से ही कृत्रिम मेधा की कंपनियों ने अपनी क्षमता बढ़ाई है और अब जब उत्पाद बन गए, तो उनके ग्राहक भी यही भारतीय बन रहे हैं। कई कंपनियां तो कृत्रिम मेधा के आधार पर बने अपने उत्पाद बेचना शुरू भी कर चुकी हैं।
इसका दूसरा पक्ष यह है कि उपलब्ध डिजिटल सुविधाओं की स्वाभाविक भाषा अंग्रेजी होने के कारण देश में आम आदमी, जो सिर्फ अपनी भाषा जानता है, उनके शोषण की संभावना और बढ़ रही है। जैसे, देश में ‘यूपीआइ’ के माध्यम से पैसे का लेन-देन एक क्रांति की तरह है और इसका सुदूर ग्रामीण बाजारों में भी चलन हो गया है। दूसरी तरफ, जन-धन योजना के तहत एक बहुत बड़े ऐसे तबके को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया है, जो इससे पहले शायद ही कभी बैंक गए हों।
इन लोगों के लिए ‘यूपीआइ’ और स्मार्टफोन दोनों का उपयोग नई बात है। ऐसे में मोबाइल प्रचालन प्रणाली में अंग्रेजी के वर्चस्व और अल्पसंख्यक भाषाओं की अनुपस्थिति भी साइबर अपराध के विस्तार में एक कारक बन रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2022 में साइबर अपराध के 65,893 मामले दर्ज किए गए, जो 2021 की तुलना में 24.4 फीसद अधिक है। इनमें से अधिकांश मामले अनलाइन खरीदारी, एटीएम और ओटीपी आधारित बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले हैं। इस तरह भारतीय भाषाओं की डिजिटल अनुपस्थिति ने शातिर अपराधियों के हौसले और बढ़ाए हैं।
अब भाषा का उपयोग सिर्फ घर-परिवार और समाज से संवाद के लिए नहीं, बल्कि मशीनों को निर्देश देने के लिए भी किया जा रहा है। इन सबमें निस्संदेह अंग्रेजी का वर्चस्व है, लेकिन अब बाजार अपने दूसरे चरण के विस्तार के रूप में अनेक भारतीय भाषाओं को जोड़ना शुरू कर चुकी है। दूसरी तरफ, भारत सरकार कृत्रिम मेधा आधारित भाषा-संसाधन टूल ‘भाषिनी’ के माध्यम से भारतीय भाषाओं की डिजिटल क्षमता के विकास की योजना पर काम शुरू कर चुकी है।
मगर आवश्यकता इस बात की है कि इसकी गति और मात्रा दोनों बढ़ाई जाए, ताकि समय रहते अधिकतम भारतीय भाषाओं को कृत्रिम मेधा से जोड़ा जा सके। साथ ही लोगों को जागरूक किया जा सके, अन्यथा देश की हजारों भाषाओं का असमय अवसान हो जाएगा। साथ ही, उनकी सांस्कृतिक थाती, देश की विविधता के अनेक रंग और सबसे महत्त्वपूर्ण, किसी व्यक्ति का अपनी भाषा में डिजिटल जीवन का अधिकार भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा।