IE Thinc सीरीज के चौथे संस्करण में द इंडियन एक्सप्रेस ने ओमिडयार नेटवर्क इंडिया के साथ जलवायु संबंधी समस्याओं पर एक चर्चा की। इसमें क्लाइमेट चेंज के कई एक्सपर्ट्स शामिल हुए। इंडियन एक्सप्रेस के क्लाइमेट और साइंस के एडिटर अमिताभ सिन्हा ने पैनल को मॉडरेट किया।
चर्चा के दौरान अर्बन प्रैक्टिस हेड अभय कंटक ने कहा, “संविधान के अनुसार शहरी विकास राज्य का विषय है और प्रत्येक राज्य सरकार के पास पालन करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। देश के सभी नगर निगम एक जैसे नहीं हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में नगर निगम सभी प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं जैसे पानी, वेस्ट वाटर और सॉलिड वेस्ट प्रबंधन, अस्पताल और शिक्षा। उनके पास सार्वजनिक परिवहन की एक सेवा भी है। इसलिए कुछ शहर सिटी बस सेवा भी प्रदान करते हैं। लेकिन यह सभी निगमों के लिए सच नहीं है। बेंगलुरु महानगर पालिका केवल सॉलिड वेस्ट प्रबंधन, बिजली और सड़कें प्रदान करती है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आप अपने कचरे का प्रबंधन और निपटान कैसे करते हैं? मुंबई जैसे शहर बस सेवा प्रदान करते हैं, इसलिए उन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करना एक चुनौती है। ग्रीनहाउस गैसों के सबसे बड़े एमिशन में से एक इमारतें हैं। आप विकास नियंत्रण विनियम कोड कैसे बनाते हैं जो ग्रीन बिल्डिंग्स को बढ़ावा देगा, निर्माण के प्रभाव को कम करेगा और ऊर्जा खपत की निगरानी करेगा?”
अभय कंटक ने आगे कहा, “आदर्श रूप से नगर निगम का राजस्व देश की जीडीपी का 3-4 प्रतिशत होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में यह 0.9-1 प्रतिशत है। 2 प्रतिशत तक बढ़ना संभव है। प्रॉपर्टी टैक्स जो वर्तमान में जीडीपी का 0.15 प्रतिशत है, लगभग 1 प्रतिशत होना चाहिए। प्रॉपर्टी टैक्स शहर के प्रशासन की जीवंतता को भी दर्शाता है। 14वें वित्त आयोग के सुझाव के अनुसार 1980 के दशक से 2,400 रुपये तक सीमित व्यवसाय टैक्स को बढ़ाया जाना चाहिए। शहरों को चुंगी जैसे उपभोग से जुड़े टैक्स की भी आवश्यकता है, जिसकी जगह अपर्याप्त मुआवज़ा ने ले लिया है, जिससे नगरपालिका की आय को नुकसान पहुँच रहा है।”
शिलांग की वादियों में सजेगा इंडियन एक्सप्रेस का Adventure Tourism Meet, यहां जानिए हर डिटेल
सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अश्वनी भाटिया ने कहा, “क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के अनुसार, भारत जलवायु परिवर्तन के प्रति सातवां सबसे संवेदनशील देश था। दुनिया भर के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से कुल 21 भारत में हैं। पिछले कुछ वर्षों में अचानक बाढ़, जंगल की आग और प्रदूषण और गर्मी की लहरों के प्रभाव के कई मामले सामने आए हैं। नगर पालिकाए, स्थानीय शासन और सेवा वितरण में सबसे आगे, इन जलवायु मुद्दों को संबोधित करने के लिए विशिष्ट रूप से तैनात हैं। वे बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक सेवाओं और सामुदायिक कल्याण के प्रबंधन में रुचि रखते हैं, जिससे जलवायु समाधानों को लागू करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।”
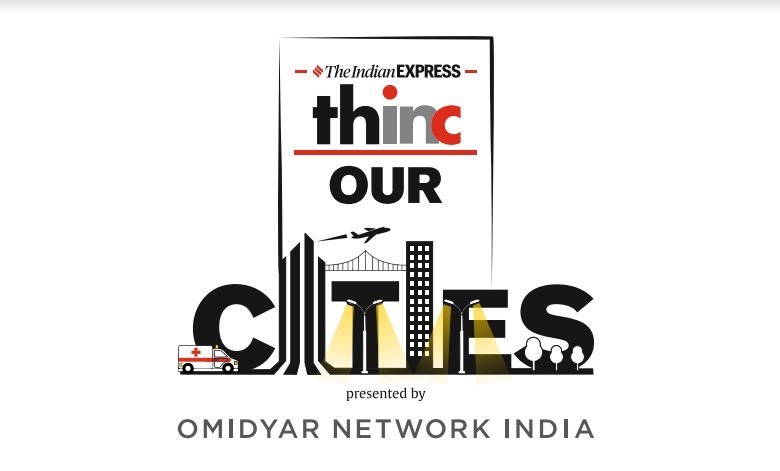
वहीं जलवायु परियोजनाओं पर शेखर सिंह ने कहा, “बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए दो दृष्टिकोण हैं। एक मौजूदा बुनियादी ढांचे को आपदा-लचीला बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि सीवेज उपचार संयंत्र (STP) और जल उपचार संयंत्र, जो अत्यधिक वर्षा जैसे जलवायु परिवर्तन प्रभावों के प्रति संवेदनशील हैं। दूसरे में नई परियोजनाएं विकसित करना शामिल है जो जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करती हैं, जैसे कि रिवरफ्रंट विकास, जिसमें नदियों की सफाई और एसटीपी को अपग्रेड करना शामिल है। उदाहरण के लिए पिंपरी-चिंचवड़ में अकेले पावना रिवरफ्रंट विकास की लागत लगभग 1,400 करोड़ रुपये है। शहर भी स्थायी गतिशीलता पर काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसों में बदलाव कर रहे हैं, लेकिन उच्च लागत के कारण उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पिंपरी-चिंचवड़ और पुणे एक बस फ्लीट साझा करते हैं, जहां 35 प्रतिशत फ्लीट इलेक्ट्रिक बसें हैं, हालांकि लक्ष्य बहुत अधिक है। ग्लोबल मानकों को पूरा करने के लिए इसका विस्तार करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।”
क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर अर्नब चौधरी ने कहा, “हम मार्जिन बैंकर के रूप में काम करते हैं। नगर पालिकाओं को पूंजी बाजार में प्रवेश करने के लिए तैयार करने में मदद करते हैं। सेबी अपने दृष्टिकोण में प्रगतिशील रहा है, इसे बढ़ावा देने के लिए रूपरेखा तैयार कर रहा है, लेकिन नगर पालिकाओं को अक्सर मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। उनकी अपनी चुनौतियां हैं और वित्त उनकी ज़िम्मेदारियों का केवल एक पहलू है। हमें पिछले साल तीन नगर पालिकाओं के साथ काम करने और दूसरों के साथ जुड़े रहने पर गर्व है। पूंजी बाज़ार नगर पालिकाओं को उनके संचालन को ऑर्गनाइज करने में भी मदद करते हैं। कई लोगों ने इन बाजारों में प्रवेश करने की तैयारी करके ही अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार किया है। उदाहरण के लिए गुवाहाटी नगर निगम कैश बेस्ड एकाउंटिंग का उपयोग करने के बावजूद बाजार की तैयारी के लिए अपनी तैयारी के हिस्से के रूप में डबल-एंट्री बहीखाता पद्धति को अपनाने के लिए काम कर रहा है। यह प्रक्रिया अकेले ही बेहतर वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करती है, भले ही उन्हें तुरंत आवश्यक रेटिंग प्राप्त न हो। अंत में गुवाहाटी जैसी नगर पालिकाओं को भूजल की कमी और अचानक बाढ़ जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन बाधाओं के बावजूद बाजार के अवसरों का पता लगाने और इन बाधाओं को दूर करने का दृढ़ संकल्प बढ़ रहा है।”
नागरिक सुविधाओं पर संतोष तिवारी ने कहा, “जन्म से लेकर मृत्यु तक यूएलबी (शहरी स्थानीय निकाय) महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जन्म, मृत्यु और यहां तक कि विवाह प्रमाण पत्र भी यूएलबी द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इनके अलावा यूएलबी स्वच्छ पेयजल तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं, सीवेज का प्रबंधन करते हैं और परिवहन प्रणालियों को बनाए रखते हैं। आज यूएलबी को पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना चाहिए, जिसके लिए कई स्तरों पर उपचार की आवश्यकता होती है। इनके अलावा, बढ़ती शहरी जरूरतों को पूरा करने के लिए यूएलबी को अब पुल, फ्लाईओवर, आरओबी (रोड ओवरब्रिज) और एफओबी (फुट ओवरब्रिज) जैसे बुनियादी ढांचे में निवेश करना चाहिए। वडोदरा के लिए इन परियोजनाओं का वित्तपोषण महत्वपूर्ण है। कुछ परियोजनाओं में देरी हो सकती है लेकिन कई में नहीं। उदाहरण के लिए, वडोदरा पहले 400 एमएलडी सीवेज उत्पन्न करता था लेकिन केवल 200 एमएलडी का ही उपचार कर पाता था। बाजार से 100 करोड़ रुपये जुटाकर, शहर अब 440 एमएलडी सीवेज का उपचार करता है। मौसम के बदलते मिजाज के कारण इस तरह की फंडिंग पर जोर दिया जाता है। जलवायु परिवर्तन के कारण अधिक गर्मी का प्रकोप भी हुआ है, जिससे यूएलबी पर मांग और बढ़ गई है। यही कारण है कि वडोदरा ने बॉन्ड फाइनेंसिंग मॉडल को अपनाया है, जिसके दोनों बॉन्ड बेहद सफल रहे हैं।”
शिल्पा कुमार ने कहा, “भारतीय शहर देश के विकास में प्रमुख योगदानकर्ता रहे हैं, जो आजीविका की तलाश में लोगों को आकर्षित करते हैं। शहर न केवल आर्थिक केंद्र हैं बल्कि वे स्थान भी हैं जहां लोग अपना जीवन बनाना चाहते हैं। शहर आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। हवा की गुणवत्ता से लेकर पार्कों और साफ पानी तक पहुंच तक, शहरी सरकारें शहरी जीवन के पैमाने को प्रबंधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि भारतीय शहरों को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खासकर उनकी आबादी के विशाल पैमाने और सीमित संसाधनों के कारण।

