सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के अंदर आरक्षण देने की इजाजत दी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ सहित सात जजों की पीठ ने छह-एक के बहुमत से फैसला दिया कि राज्यों को संवैधानिक रूप से SC-ST कैटेगरी के अंदर सब-क्लासिफिकेशन करने का अधिकार है, ताकि आरक्षण के जरिए उस जाति-समूह के ज्यादा जरूरतमंद लोगों की स्थिति ऊपर उठाई जा सके। साथ ही, जस्टिस बी.आर. गवई ने अपना मत देते हुए लिखा कि सरकारों को एससी-एसटी के अंदर क्रीमी लेयर की पहचान करने का भी तरीका निकालना चाहिए। हालाँकि, उन्होंने इस निर्धारण के लिए कोई स्पष्ट मानदंड नहीं दिया।
अभी ओबीसी के आरक्षण में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू है। क्या इसी तर्ज पर एससी-एसटी के आरक्षण में भी यह लागू हो सकता है?
‘क्रीमी लेयर’ का क्या मतलब है?
क्रीमी लेयर की अवधारणा 1992 के महत्वपूर्ण इंद्रा साहनी फैसले से उत्पन्न हुई थी। मंडल आयोग की सिफारिश पर आधारित, वीपी सिंह सरकार ने 13 अगस्त, 1990 को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए सिविल पदों और सेवाओं में 27% आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी। इसे इंद्रा साहनी और अन्य लोगों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
27% ओबीसी आरक्षण
16 नवंबर, 1992 को जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता वाली नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने क्रीमी लेयर को छोड़कर 27% ओबीसी आरक्षण को बरकरार रखा। क्रीमी लेयर में वे लोग थे जो ओबीसी के बीच सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से अधिक उन्नत थे। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि आरक्षण के लाभ उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।
क्रीमी लेयर सब-क्लासिफिकेशन या सब-कैटेगराइजेशन के समान नहीं है। क्रीमी लेयर एक निश्चित जाति/समुदाय के भीतर एक ऐसे समूह को प्रदर्शित करता है जो कुछ मानदंडों के आधार पर बाकी से बेहतर है।

ओबीसी के बीच क्रीमी लेयर की पहचान कैसे की जाती है?
क्रीमी लेयर का निर्धारण करने का आधार सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राम नंदन प्रसाद की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किया गया था। यह समिति इंद्रा साहनी मामले में कोर्ट के फैसले के बाद गठित की गई थी। समिति ने 10 मार्च, 1993 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके आधार पर 8 सितंबर को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने उन छह श्रेणियों के लोगों की सूची जारी की जिनके बच्चों को क्रीमी लेयर में माना जाएगा। ये हैं:
- संवैधानिक/कानूनी पद।
- केंद्रीय और राज्य सरकारों के ग्रुप ‘A’ और ग्रुप ‘B’ अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), सांविधिक निकायों व विश्वविद्यालयों के कर्मचारी।
- सशस्त्र बलों में कर्नल व इनसे ऊपर रैंक के अधिकारी और अर्धसैनिक बलों में इनके समकक्ष अधिकारी।
- डॉक्टर, वकील, प्रबंधन सलाहकार, इंजीनियर जैसे पेशेवर।
- कृषि भूमि या परती जमीन और या भवन के मालिक और
- आय कर या संपत्ति कर भरने वाले लोग।
क्रीमी लेयर और अंतर
संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के बच्चों के अलावा क्रीमी लेयर के मुख्य दो आधार बने। एक सरकारी नौकरी में रहे या कर रहे लोगों के बच्चे और दूसरा, निजी क्षेत्र में काम करने वालों के बच्चे। इन दो कैटेगरी में बड़ा अंतर यह है कि एक को क्रीमी लेयर में रखने का आधार आय है, जबकि दूसरे को रैंक के आधार पर रखा गया।
शुरू में आय सीमा प्रति वर्ष 1 लाख रुपये निर्धारित की गई और हर तीन साल पर इसमें संशोधन की व्यवस्था की गई। हालाँकि, 2017 के बाद से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 2017 में आय की सीमा 8 लाख रुपये रखी गई। 2015 में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) ने आय सीमा को 15 लाख रुपये तक बढ़ाने की सिफारिश की थी, हालाँकि इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई।
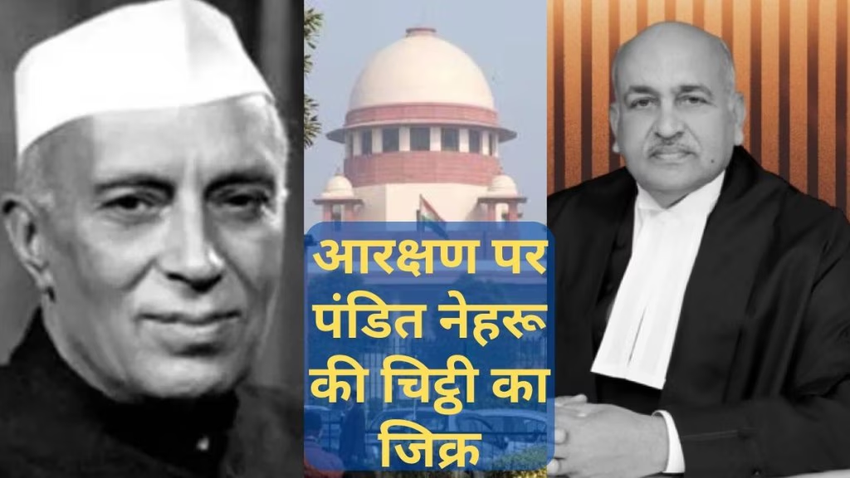
इन बच्चों के लिए जिनके माता-पिता में से कोई एक या तो ग्रुप-ए अधिकारी के रूप में भर्ती हुए हैं या 40 वर्ष की आयु से पहले ग्रुप-ए अधिकारी के रूप में प्रमोट हुए हैं उन्हें ओबीसी आरक्षण के लिए अयोग्य बना देता है। दोनों माता-पिता का ग्रुप-बी अधिकारी होना भी बच्चों को क्रीमी लेयर में रखता है। इसी तरह, सेना में कर्नल या उससे उच्च रैंक के अधिकारियों के बच्चे, और नौसेना और वायु सेना में समकक्ष रैंक वाले अधिकारियों के बच्चे भी क्रीमी लेयर में आते हैं।
केंद्र सरकार ने इस मानदंड की समीक्षा के लिए मार्च 2019 में पूर्व DoPT सचिव बी. पी. शर्मा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था लेकिन इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है।
किस राज्य में किस दलित जाति का है दबदबा?
महाराष्ट्र में तीन दर्जन से अधिक अनुसूचित जातियां हैं, जिनमें महार और मतंग सबसे प्रमुख हैं। महार समुदाय उच्च शिक्षित होने के साथ-साथ सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय है। ये ज्यादातर वे लोग हैं जिन्होंने 1956 में बाबा साहब भीम राव आंबेडकर के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया था। मतंग दूसरा सबसे बड़ा एससी समुदाय है, जो ज्यादातर हिंदू हैं।
महाराष्ट्र की जनजातियों की बात की जाये तो दो प्रमुख जनजातियों में से एक गोंड है जो जो विदर्भ में रहते हैं, विशेष रूप से गढ़चिरौली और चंद्रपुर जिलों में। दूसरी जनजाति भील है जो उत्तरी महाराष्ट्र के नंदुरबार, नासिक और धुले जिलों में रहती हैं।
राजस्थान की बात की जाये तो यहां एससी की लिस्ट में 59 जातियां हैं। इनमें मेघवाल सबसे बड़ा है, जो पूरे राज्य में फैले हैं। ये मुख्य रूप से बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के सीमावर्ती जिलों में फैले हैं। पूर्वी राजस्थान में बैरवा और जाटव का बाहुल्य है।
मीणा राजस्थान की सबसे प्रभावशाली जनजाति है जिन्होंने दर्जनों विधानसभा सीटों पर चुनावी नतीजों को प्रभावित किया है। देशभर में पुलिस और नौकरशाही में समुदाय की महत्वपूर्ण उपस्थिति है। भील जनजाति भी यहां प्रभावी है जिनमें से कुछ खुद को हिंदू नहीं मानते हैं। ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में प्रभावी हैं।
ओडिशा में आदिवासी राज्य की जनसंख्या का 22.85% और भारत की आदिवासी आबादी का 9.17% हैं (2011 की जनगणना के मुताबिक)। राज्य में 62 जनजातियां और 13 अन्य जनजातियाँ हैं। जिनमें खोंड की संख्या सबसे ज्यादा है जो ज्यादातर दक्षिणी ओडिशा के रायगढ़ा, कंधमाल, कालाहांडी, कोरापुट जिलों में रहते हैं। संथाल दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी समूह है, उसके बाद गोंड आते हैं।
राज्य में 93 एससी जातियां हैं। ये कुल जनसंख्या का 17.13% (2011 की जनगणना के मुताबिक) हैं। पैन प्रमुख एससी समुदाय है उसके बाद डोम आते हैं। अन्य एससी समुदायों में धोबा, गांडा, कांड्रा, बाउरी शामिल हैं।
छत्तीसगढ़ की 2.55 करोड़ आबादी (2011 की जनगणना के मुताबिक) में 30% से अधिक एसटी हैं। 43 आदिवासी समुदायों में गोंड सबसे प्रभावशाली हैं जो जनजातीय आबादी का लगभग 55% हिस्सा है। इसके बाद कावर/कंवर (11% से अधिक) और ओरांव (लगभग 10%) हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, 44 एससी समूह राज्य की आबादी का 12.7% हिस्सा हैं।
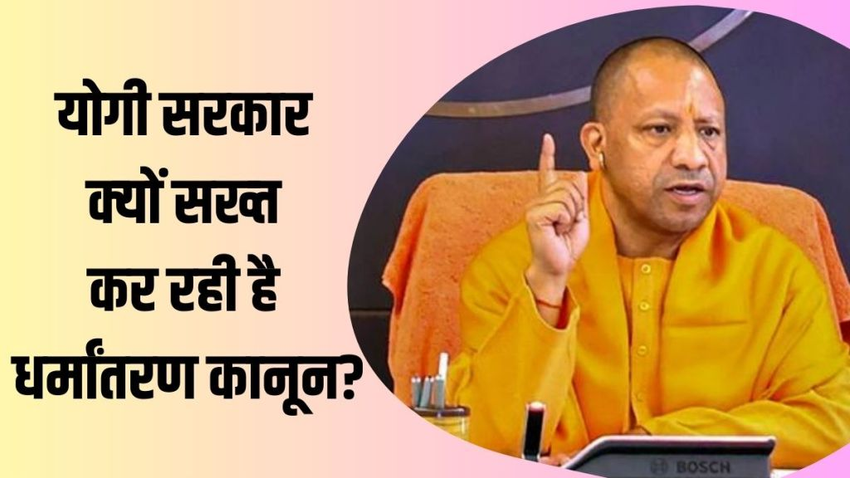
मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति राज्य की आबादी का लगभग 15.6% है। एससी समुदाय का 47% से अधिक हिस्सा पारंपरिक रूप से चमड़े का काम करने वाले श्रमिक हैं और राज्य भर में रहते हैं। बलाई जो मालवा क्षेत्र में रहते हैं, राज्य की अनुसूचित जाति आबादी का लगभग 12% हैं।
राज्य में एसटी आबादी 21% हैं। भील सबसे बड़ा समुदाय है, जो जनजातीय आबादी का 39% से अधिक है। गोंड दूसरा बड़ा समुदाय है जो राज्य की एसटी आबादी का लगभग एक तिहाई है।
पश्चिम बंगाल में राजबंशी सबसे बड़ा एससी समूह है। मटुआ अब दूसरा सबसे बड़ा एससी समूह है। वे ज्यादातर उत्तर और दक्षिण 24-परगना और नादिया, हावड़ा, कूच बिहार, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर और मालदा जैसे सीमावर्ती जिलों में रहते हैं। तीसरा सबसे बड़ा एससी समुदाय बागड़ी है जो मुख्य रूप से बांकुरा और बीरभूम में रहते हैं।
गुजरात में 27 दलित जातियाँ हैं। जिनमें से वानकर जिनका पारंपरिक व्यवसाय बुनाई है, राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी का लगभग 35-40% हिस्सा हैं। रोहित जो एससी आबादी का लगभग 25-30% हैं दूसरा सबसे प्रभावशाली एससी समुदाय हैं।
भील आदिवासी आबादी का लगभग 43% हिस्सा हैं और मुख्य रूप से डांग, पंचमहल, भरूच, बनासकांठा और साबरकांठा जिलों में रहते हैं। हलपति जो मुख्य रूप से सूरत, नवसारी, भरूच और वलसाड के दक्षिणी जिलों में रहते हैं, राज्य की 6% से अधिक आदिवासी आबादी हैं।
असम में जनजातीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का 12.4% है (2011 की जनगणना के अनुसार)। कार्बी आंगलोंग और उत्तरी कछार पहाड़ियों के स्वायत्त जिलों में पंद्रह मान्यता प्राप्त जनजातियाँ रहती हैं जबकि राज्य के बाकी हिस्सों में 14 जनजातियां हैं। राज्य में बोडो सबसे बड़ी जनजाति (आदिवासी आबादी का 35.1%) है। कार्बी सबसे बड़ी पहाड़ी जनजाति और राज्य की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है।
त्रिपुरा में 19 मान्यता प्राप्त आदिवासी समुदाय राज्य की आबादी का 30% से अधिक हिस्सा हैं। प्राचीन त्रिपुरी कबीले में देबबर्मा समुदाय शामिल है, जो त्रिपुरा का पूर्व शासक राजवंश था। राज्य में 34 एससी हैं, जो जनसंख्या का लगभग 18% हैं । अनुसूचित जाति में दास, बाद्यकर, शब्दकार, सरकार आदि समुदाय शामिल हैं।
उत्तराखंड में ठाकुर और ब्राह्मण आबादी का लगभग 55% हैं। यहां ओबीसी लगभग 18% हैं और एससी और एसटी कुल मिलाकर लगभग 22% हैं। हरिजन और बाल्मीकि सबसे बड़े एससी समूह हैं। जौनसारी और थारू राज्य के दो सबसे बड़े एसटी समूह हैं।

