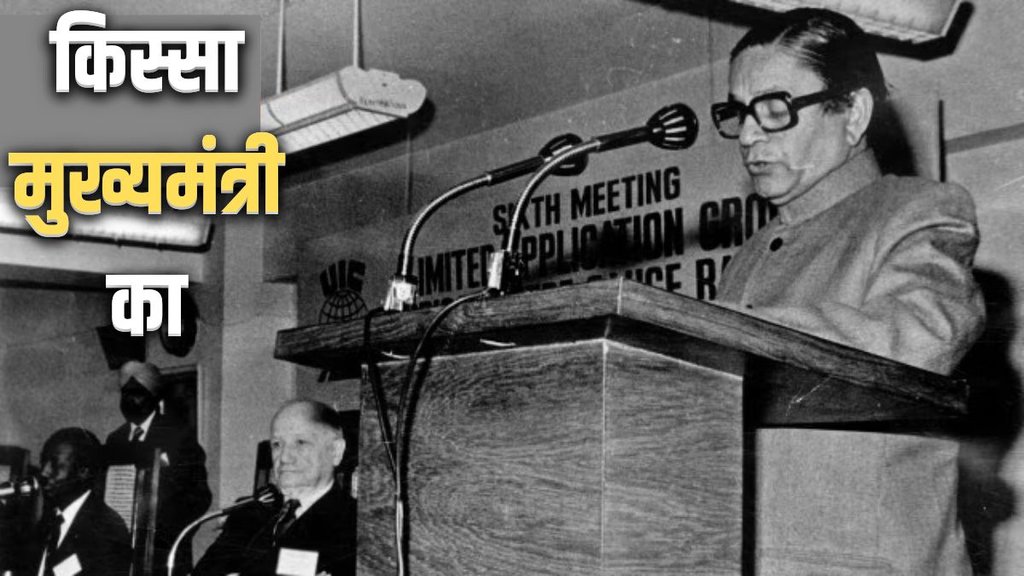बिहार की राजनीति हमेशा से उतनी ही दिलचस्प रही है, जितनी अस्थिर। यहां सत्ता की हर करवट के साथ न सिर्फ़ समीकरण बदलते हैं, बल्कि इतिहास की नई इबारतें भी लिखी जाती हैं। इन्हीं इबारतों में एक नाम दर्ज है केदार पांडेय का – बिहार के बारहवें मुख्यमंत्री, जिनसे मतदाताओं ने स्थिरता की उम्मीद की थी, लेकिन जिनका कार्यकाल भी गुटबाजी की आंधियों में बह गया। एक ऐसे दौर में, जब कांग्रेस को जनता ने निर्णायक बहुमत दिया था, पांडेय उस स्थिर सरकार के प्रतीक बनकर उभरे – पर कुछ ही महीनों में वही सरकार असहमति, महत्वाकांक्षा और अंदरूनी राजनीति की भेंट चढ़ गई। यह कहानी है उस मुख्यमंत्री की, जिसने सर्वसम्मति के साथ शुरुआत तो की, पर अंत में वही सर्वसम्मति उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन गई।
बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री ने तीन कार्यकालों तक राज्य का नेतृत्व किया, लेकिन कभी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। उनका अंतिम कार्यकाल लगभग 200 दिनों का रहा और उन्होंने 10 जनवरी 1972 को इस्तीफा दे दिया, जिससे कांग्रेस (आर) के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार समाप्त हो गई। बिहार में मार्च 1972 में चुनाव हुए – पांच अशांत वर्षों के बाद, जिनमें दो विधानसभाएं, नौ सरकारें, विभिन्न गठबंधन सरकारें और तीन बार राष्ट्रपति शासन रहा।
कांग्रेस (आर), इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाले गुट ने 318 सीटों में से 167 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (कांग्रेस के साथ गठबंधन में) ने 35, सोशलिस्ट पार्टी ने 33, कांग्रेस (ओ) ने 30 और भारतीय जनसंघ ने 25 सीटें जीतीं।
1962 के बाद यह पहली बार था जब कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। राजनीतिक अस्थिरता और लगातार सत्ता हथियाने की कोशिशों के प्रति मतदाताओं की प्रतिक्रिया नतीजों में साफ दिखाई दी, जहाँ 200 से ज़्यादा नए विधायक जीते और कई मौजूदा विधायक हार गए। ये चुनाव 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश के निर्माण के कुछ ही महीनों बाद हुए थे, जिससे राष्ट्रीय भावना सत्तारूढ़ कांग्रेस के पक्ष में काफ़ी बढ़ गई।
निर्णायक बहुमत के साथ कांग्रेस अपने उच्च-जातीय नेतृत्व की जड़ों की ओर लौट आई और केदार पांडे सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेता चुने गए। उन्होंने 19 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे पांडे ने विधानसभा में नौतन (पश्चिम चंपारण) निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पहले वे 1957 और 1967 में बगहा से चुने गए थे।
मुख्यमंत्री के रूप में पांडे के शुरुआती दिन सुचारू रूप से बीते। उन्होंने जल्दी ही अपने मंत्रियों की सूची को अंतिम रूप दिया और कुशलतापूर्वक विभागों का वितरण किया। हालांकि पांडे को केंद्रीय मंत्री ललित नारायण मिश्रा की पसंद माना जाता था, उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि उनके कई मंत्री मिश्रा के प्रति ज़्यादा वफ़ादार हैं – जो इंदिरा गांधी के भरोसेमंद सहयोगी भी थे। मिश्रा ने बिहार के कांग्रेस संगठन और राजनीति पर अपना खासा प्रभाव जमा लिया था, जिससे दिल्ली में कई नेताओं में बेचैनी पैदा हो गई थी।
फिर भी, पांडे ने केंद्रीय मंत्रियों उमाशंकर दीक्षित और जगजीवन राम सहित केंद्रीय नेताओं के साथ नियमित संपर्क बनाए रखा ताकि उन्हें बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम से अवगत कराया जा सके। इन प्रयासों के बावजूद, आंतरिक तनाव गहराता गया। मई 1973 में, पांडे ने अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करने और एल.एन. मिश्रा के करीबी माने जाने वाले सात मंत्रियों को हटाने का फैसला किया। उन्होंने उनसे इस्तीफा देने को कहा, लेकिन उनमें से चार ने यह कहते हुए इस्तीफा देने से इनकार कर दिया कि मुख्यमंत्री को कांग्रेस विधायक दल का विश्वास नहीं है।
एक शर्मनाक स्थिति और संभावित विद्रोह का सामना करते हुए, पांडे ने 27 मई 1973 को इस्तीफा दे दिया, जिससे चारों मंत्री अपने पद खो बैठे। राज्यपाल ने उन्हें फिर से सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और उन्होंने अगले ही दिन एक बार फिर शपथ ली। हालांकि, उनके प्रशासन को फिर से स्थापित करने का प्रयास बुरी तरह विफल रहा। उनके 37 सदस्यीय नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में 14 मंत्री असहमति जताते हुए नहीं आए, हालांकि अगले दिन पार्टी आलाकमान के दबाव में उन सभी ने शपथ ले ली।
इस बीच, एल.एन. मिश्रा के वफादार पांडे को हटाने के लिए विधायकों के बीच पैरवी करते रहे। कांग्रेस आलाकमान ने हस्तक्षेप किया और पांडे, मिश्रा और अन्य नेताओं के साथ कई दौर की बातचीत की। अंततः, जिन चार मंत्रियों ने पहले इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था, उन्हें पांडे के मंत्रिमंडल में बहाल कर दिया गया, जिससे फेरबदल का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो गया।
इस प्रकार, जहां 1972 के मतदाताओं ने कांग्रेस (आर) को एक स्थिर सरकार प्रदान करने का स्पष्ट जनादेश दिया था, वहीं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और जातिगत समीकरणों से प्रेरित गुटीय प्रतिद्वंद्विता ने पार्टी को भीतर से कमजोर कर दिया। शीर्ष नेतृत्व द्वारा खुले मुकाबले (जैसा कि पिछली विधानसभाओं में होता था) के बजाय सर्वसम्मति से नेतृत्व चयन पर ज़ोर देने से कांग्रेस विधायक दल का नेतृत्व करने के इच्छुक कुछ नेता भी नाराज हो गए और गुटबाजी और बढ़ गई।
1973 के मध्य तक, पांडे को पद से हटाने के नए प्रयासों की अफवाहें तेज़ हो गईं। 22 जून 1973 को, उनकी सरकार के 24 मंत्रियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफ़ा दे दिया, जिससे सरकार टूटने के कगार पर पहुंच गई। कांग्रेस नेतृत्व ने तय किया कि जुलाई 1973 में कांग्रेस विधायक दल के भीतर शक्ति परीक्षण होगा। इसके बाद पांडे बहुमत खो बैठे और उन्हें इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे बिहार में एक और अल्पकालिक कांग्रेस सरकार का अंत हो गया।
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एल.एन. मिश्रा, राम लखन सिंह यादव और जगजीवन राम जैसे नेताओं से परामर्श के बाद पांडे को चुना था। उनके चयन का उद्देश्य बिहार में गैर-विवादास्पद और सर्वसम्मति पर आधारित नेतृत्व लाना था। वास्तव में, पांडे ने अपने कार्यकाल की शुरुआत ऐसी ही प्रतिष्ठा के साथ की थी। फिर भी, प्रतिस्पर्धी गुटों से घिरे और सत्ता के आकांक्षी दिल्ली स्थित नेताओं के बढ़ते प्रभाव से कमजोर होकर उन्होंने खुद को लगातार अलग-थलग पाया।
अंततः, उनका कार्यकाल गठबंधन युग के उनके नौ पूर्ववर्तियों के कार्यकाल जैसा ही रहा — संक्षिप्त, संघर्षपूर्ण और अस्थिर। पांडे की सरकार इस बात का एक उदाहरण है कि कैसे पार्टी के भीतर गुटबाजी एक स्पष्ट चुनावी जनादेश को भी पराजित कर सकती है। उन्होंने स्थिरता, दक्षता और शासन के एक नए युग की शुरुआत की आशा की थी, लेकिन उनके पतन ने — गुप्त चालों और बदलती वफ़ादारियों के बीच — यह दिखा दिया कि गुटबाजी की सड़ांध बिहार कांग्रेस में कितनी गहराई तक समा गई थी। यह एक नया दौर था, जहां कांग्रेस पार्टी का संगठन कमजोर होने लगा और पूरी तरह से सरकार व शीर्षस्थ नेता पर निर्भर हो गया। इस प्रकार, बिहार के अशांत राजनीतिक इतिहास का एक और छोटा अध्याय समाप्त हो गया।