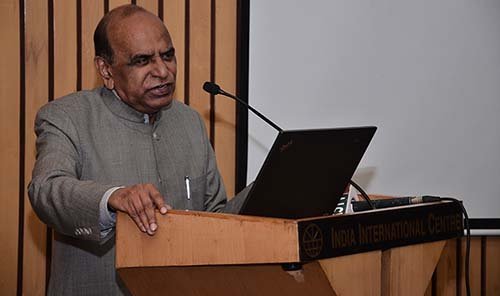‘मेरे यारों, यह हादसा हमारे ही समयों में होना था, कि मार्क्स का सिंह जैसा सिर सत्ता के गलियारों में मिनमिनाता फिरना था’। पंजाबी कवि पाश ने भारतीय राजनीति में सिर्फ सत्ता पाने के लिए कुर्सी गिराने और बनाने वाले नेताओं से आहत होकर ये पंक्तियां लिखी थीं। इन पंक्तियों के लिखने के लंबे समय बाद आज सत्ता के गलियारों में मिनमिनाते सिरों का कोलाहल इतना बढ़ गया है कि दहाड़ता सिंह जैसा सिर लुप्तप्राय बन चुका है। ‘पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है’? इस सवाल पर संसद से सड़क तक मिनमिनाते चेहरों के बीच सिंह जैसा एक लुप्तप्राय चेहरा है देवी प्रसाद त्रिपाठी का।
यह चेहरा अपनी राजनीति से सिर नहीं छुपाता बल्कि सत्ता और समाज के द्वंद्व की राजनीति के गलियारों में घुसपैठ कराकर विमर्श के नए रास्ते खोलता है। प्रेमचंद मानते थे कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। त्रिपाठी का भी मानना रहा है कि साहित्य और राजनीति के बीच दूरी पैदा करने वाले अधिनायकवाद की राह पकड़ते हैं। वह साहित्य ही है जिसके जरिए सत्ता और जनता के बीच लोकतांत्रिक संवाद हो सकता है।
दोस्तों के बीच (वैसे ये किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते) डीपीटी के नाम से पुकारे जाने वाले त्रिपाठी उन गिने-चुने सियासतदानों में से हैं जिन्होंने सत्ता के शीर्ष पर पहुंच कर भी समाज के संघर्ष से मुंह नहीं मोड़ा। दादरी से लेकर बाबरी तक उठी असहिष्णुता की सुनामी को जब केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली कागजी क्रांति कह कर खारिज कर रहे थे तो उस समय डीपी त्रिपाठी संसद को कलमकारों की शक्ति का अहसास कराकर मोदी सरकार को आगाह कर रहे थे कि सिर्फ ‘भक्ति’ खोज कर अपने जनसमर्थन की कब्र न खोदें। छात्र आंदोलन से निकले त्रिपाठी को युवा शक्ति का अहसास है। रोहित वेमुला की मौत के बाद त्रिपाठी ने संसद में बेबाक कहा, ‘मेरी नजर में रोहित की मौत संस्थागत हत्या है’। एक समय में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे त्रिपाठी ने सांप्रदायिक और फासीवादी विचारधारा पर हमेशा हल्ला बोला है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि सरकार देश की युवा शक्ति से न उलझे और सरकारी अत्याचारों से आजादी की मांग की।
अपनी लेखनी की वैचारिक प्रतिबद्धता के कारण ही वे राज्यसभा तक पहुंचे। राजनीतिक प्रशिक्षण उनके कलम की धार को तेज बनाने में और मददगार हुआ। सक्रिय राजनीति के बाद भी उन्होंने लिखने-पढ़ने से कभी अपना नाता नहीं तोड़ा। यह उनके निष्पक्ष व्यक्तित्व का प्रभाव ही है कि वे वैचारिक या सैद्धांतिक विरोधियों के साथ एक जैसा प्रेमभाव रखते हैं। विरोधी का व्यक्तित्व उनकी पहचान पर हावी नहीं हो पाता है। यही वजह है कि उनके चरम विरोधी आमने-सामने बैठ कर एक-दूसरे को समझने-समझाने की कोशिश में जुटे रहते हैं।
महात्मा गांधी और नेहरू, हिंदुस्तान की सियासत में ये दो ऐसे नाम हैं जिन्होंने राजनीतिक पहचान के साथ अपने लेखन को जोड़ा था। इनके लिए लेखन राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता का एक साधन था। डीपीटी ने भी कलम के जरिए अपनी राजनीतिक और सामाजिक प्रतिबद्धता को मजबूती से जाहिर किया। और, अपना सियासी रुतबा साहित्यलेखन को समर्पित किया। यही वजह है कि नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे और एमएम कलबुर्गी के मामलों में साहित्यकारों की पैरवी वे हर मोर्चे पर आगे रह कर करते रहे हैं। और, औपचारिक या अनौपचारिक मौके को चूके बिना अपनी बात कहते हैं।
एक स्वर में रघुवीर सहाय, कालिदास और मिर्जा गालिब का उद्धरण देने वाले त्रिपाठी सहज ही अपने गहन अध्ययन की छाप छोड़ जाते हैं। उनके कहकहे उनकी हस्ताक्षरनुमा पहचान हैं और असहिष्णुता जैसी कठिन घड़ी में भी उनके सहिष्णु बोल कहकहों से ही छन कर बाहर निकलते हैं। अपनी बात कहते हुए सामने वाले की सहमति जैसे वे जबरन खींच लेते हैं। खास बात यह है कि शब्दों के इस शिल्पी ने अगर राजनीति को भी समांतर रूप से चुना तो उसमें भी एक मजबूत पहचान बनाई।
त्रिपाठी साहित्य और राजनीति का ऐसा संगम हैं जो आज के समय में दुर्लभ है। आज जो जेएनयू सत्ता के निशाने पर है, वहीं से उन्होंने सत्ता और समाज को समझने की शुरुआत की। जेएनयू से बजरिए छात्र संगठन राजनीति का प्रशिक्षण लेने के बाद उन्होंने कुछ अरसा शिक्षण भी किया। लेकिन उनका मुकाम उन्हें राजनीति में ही मिला। वाम विचारधारा से प्रशिक्षण की शुरुआत कर कांग्रेस और फिर राष्टÑवादी कांग्रेस पार्टी में गए। राजनीति की पथरीली सड़क का संघर्ष उन्हें कलम से अलग नहीं कर पाया। ज्ञान अर्जित करने में वे किसी सीमा में नहीं बंधे। विदेशी भाषाओं को सीखने और दुनिया को समझने के जुनून ने उनके लेखन को समृद्ध किया।
त्रिपाठी राज्यसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं। उनकी खासियत है, सदन में हाजिरी और भागीदारी। जनपक्षधरता से जुड़े हर मसले पर उन्होंने संसद में आवाज उठाई। इस वक्त तो संसद में साहित्यकारों और तर्कवादियों की बात कहने वाले वे एकमात्र सदस्य हैं। ललित कला अकादमी पर जब सरकारी नियंत्रण की बात हुई तो त्रिपाठी ने इसके खिलाफ अपनी बुलंद आवाज उठाई। उन पर लिखी एक पुस्तक उनके जीवन में आई कठिनाइयों के बारे में बताती है कि कैसे उन्होंने जीवन की चुनौतियों से लड़ कर अपना रास्ता बनाया। यह उनका हौसला ही था कि छात्र जीवन में उन्होंने फैसला कर लिया था कि मेनका गांधी का रास्ता रोकें। बेखौफ। आपातकाल के हौलनाक समय में जेएनयू में आजाद लब और दिमाग की अगुआई की।
इनके व्यक्तित्व का जो पहलू सहज ही छू जाता है, वह है राजनीति की तमाम बंदिशों के बाद भी जनपक्षधरीय लेखन से करीबी रिश्ता बनाए रखना। इनका धैर्य अद्भुत है। इतना अप्रतिम कि अगर असहिष्णुता पर भी उन्हें संवाद की संभावना खोजनी है तो वे पूरी सहिष्णुता से वक्त का इंतजार करते हैं और फिर उस पर अमल की कोशिश। ‘पुरस्कार वापसी’ जैसे समय में सरकार ने लेखकों के विरोध को कागजी क्रांति कह कर खारिज कर दिया। सरकार और साहित्यकारों की तकरार के बीच त्रिपाठी धैर्य से अपने काम में लगे रहे। और जब पहला मौका मिला सत्ता और साहित्यकार को आमने-सामने बिठा उनका संवाद करा दिया। दोनों पक्ष अपने गिले-शिकवे कहते रहे और त्रिपाठी किनारे बैठ लुत्फ लेते रहे। वक्त से आगे न बढ़ कर वक्त का इंतजार करना किसी भी कोशिश की कामयाबी की दिशा में महत्त्वपूर्ण है। और ये उन सियासतदानों में से हैं जो अपने लिखे को कहते हैं, कहे को जीते हैं। कलमबद्ध प्रतिबद्धताओं से मुकरने वाले इतिहास से बेदखल होते हैं। अपनी कलम के साथ डटे रह कर वे इतिहास तो लिख ही रहे हैं।