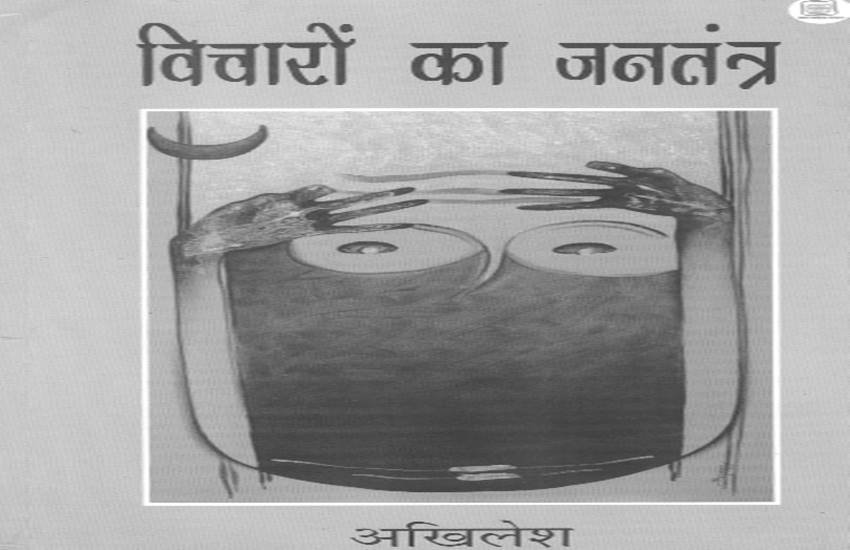साम्ययोग के आयाम
आधुनिक औद्योगिक सभ्यता के इस दौर में संकट और चुनौतियों के कई आयाम मानव-जाति के सामने हैं और वर्तमान काल की प्रमुख विचारधाराएं- उदारवाद और मार्क्सवाद एवं उनके विभिन्न संस्करण इस संकट का सामना करने में अक्षम और अपर्याप्त साबित हो रहे हैं। विनोबा की कीर्ति एक सिद्ध संत के रूप में ज्यादा मान्य होने के कारण उनके आध्यात्मिक चिंतन पर ही ध्यान ज्यादा केंद्रित रहा है। उनके सामाजिक चिंतन में भूदान से संबंधित लेखन पर ही लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ है। इसलिए उनके सामाजिक-राजनीतिक-आर्थिक चिंतन पर समग्रता में कम विचार हुआ है। इसीलिए गांधीजी के ‘हिंद-स्वराज’ की श्रेणी में रखने लायक उनकी कृति ‘स्वराज्य-शास्त्र’ विद्वानों की नजर से वंचित ही रही। इस संदर्भ में कवि, लेखक, विचारक एवं अनेक विद्याओं और विधाओं में पारंगत नंदकिशोर आचार्य की नई कृति ‘साम्ययोग के आयाम’ में विनोबा-चिंतन का पुनर्पाठ अपनी अलग और विशिष्ट महत्ता रखता है। इसमें लेखक की कोशिश रही है कि विनोबा-चिंतन के आध्यात्मिक, सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक पक्षों पर सम्यक रूप से विचार कर उसका सारगर्भित सार-सर्वस्व प्रस्तुत किया जाए। आचार्य इस बौद्धिक प्रयास में पूर्णतया सफल दिखते हैं।
साम्ययोग के आयाम: नंदकिशोर आचार्य; प्राकृत भारती अकादमी, 13-ए, गुरुनानक पथ, मेन मालवीय नगर, जयपुर; 180 रुपए।
कोयले की चिनगारी
कोयले की चिनगारी’ नामक कविता-संग्रह में रमणिका गुप्ता के सामाजिक सरोकारों से जुड़ी ज्यादातर कविताएं हैं। इन कविताओं को पढ़ने के पेश्तर यह जानना जरूरी है कि वे लगभग तीस वर्षों तक हजारीबाग जिले की कोयला खदानों के मजदूरों के बीच काम करती रही हैं, यूनियन चलाती रही हैं। राजनीति में भी उनकी सक्रियता के पीछे यही मजदूर आंदोलन रहा है। इसीलिए उन्होंने इस संग्रह में जिस तरह की कविताओं को संकलित किया है, वैसी कविताएं हिंदी के किसी दूसरे कवि ने नहीं लिखीं। संग्रह की पहली कविता ‘कोयला’ सत्रह खंडों में विभाजित हिंदी की एक अनुपम कविता है, जिसमें कोयला अपनी अत्मकथा स्वयं सुना रहा है। इस कविता में कोयले के निर्माण की प्राक-ऐतिहासिक काल की प्रक्रिया के बहाने पूरी पृथ्वी की संरचना को समझाते हुए रमणिका गुप्ता ने वर्तमान पूंजीवादी तंत्र में कोयले के महत्त्व को रेखांकित किया है, साथ ही साथ कोयला खदानों के मजदूरों की व्यथा-कथा को कलात्मक संयम के साथ अभिव्यक्त किया है।
कोयले की चिनगारी: रमणिका गुप्ता; समीक्षा पब्लिकेशन्स, एक्स/ 3284 ए, स्ट्रीट नं. 4, रघुबरपुरा नं. 2, गांधीनगर, दिल्ली; 350 रुपए।
विचारों का गणतंत्र
विचारों का जनतंत्र’ नामक यह निबंध संकलन सुप्रसिद्ध लेखक-पत्रकार अखिलेश ने ‘तद्भव’ पत्रिका के विभिन्न अंकों से चुनिंदा लेख लेकर तैयार किया है। विचारों का यह लोकतंत्र वस्तुत: कई तरह की बहुवचनात्मकता से निर्मित जनतंत्र है। हमारे समय की उलझनों, समस्याओं बहसों-मुबाहिसों, प्रश्नाकुलताओं से जूझते इन वैचारिक लेखों का विषय, विचार और प्रस्तुतिपरक विविधता ही इस जनतंत्र की बहुलता की सूचक है। समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षा, साहित्य से जुड़े विद्वानों और सामाजिक चिंतकों की नई-पुरानी पीढ़ी का विचार-विमर्श यहां एकत्र है। उत्तर आधुनिकता और भूमंडलीकरण के दौर में दुनिया की सभ्यता-संस्कृति का स्वरूप तो बदला ही है, उसे जानने-समझने की दृष्टि भी प्रभावित हुई है; अतीत और वर्तमान को देखने-विचारने और व्याख्यायित करने के नजरिए में भी बदलाव और बहुलता का समावेश हुआ है। जब किसी चीज पर हमले होते हैं, वह संकटग्रस्त होती है, तो उसका धीरे-धीरे क्षरण होता है। लेकिन इस तरह भी होता है कि उसका जितना ही दमन किया जाए, वह उतना ही सिर उठाएगी। उसमें अधिक तेजस्विता, निखार और गहराई का विस्तार होने लगेगा। विचार के संसार में आमतौर पर ऐसी ही रासायनिक क्रिया देखने को मिलती है। ‘विचारों का जनतंत्र’ के निबंध इन बदलावों को रेखांकित करने के साथ-साथ उनके निहितार्थ को खोलते हैं; नए विमर्शों को उद्घाटित करते हैं।
विचारों का जनतंत्र: संपादक- अखिलेश; सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन, एन- 77, पहली मंजिल, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली; 450 रुपए।