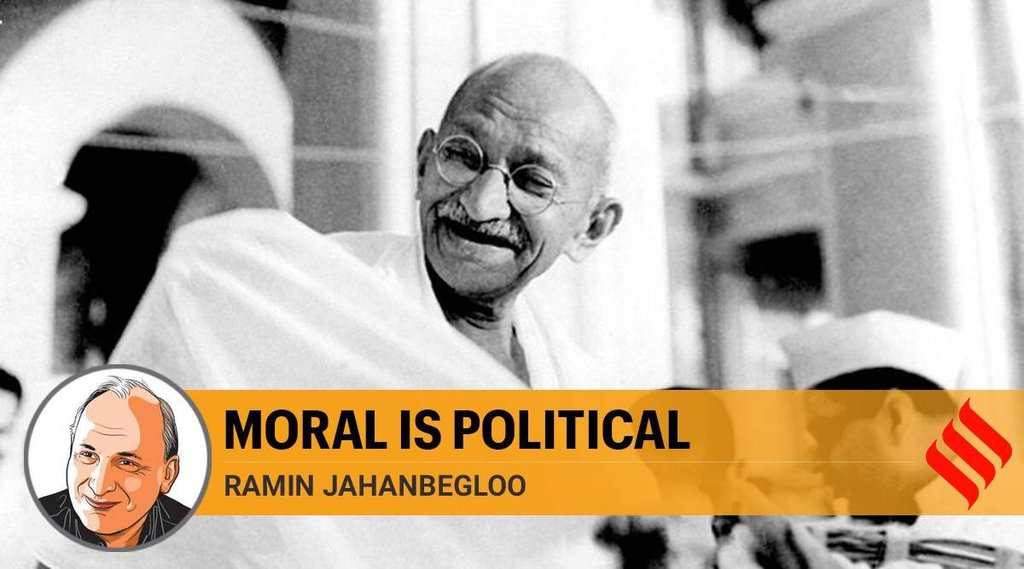जब से राजनीतिक दलों ने किसी भी तरह सत्ता पाने के समीकरण साधने शुरू किए हैं, तबसे राजनीति में सिद्धांतों की जगह बाकी सारी चीजें प्रभावी होती चली गई हैं। उसमें बाहुबल, धनबल, जाति, धर्म, क्षेत्रीयता आदि को तो जगह मिली ही है, ऐसे प्रत्याशियों का मोल बढ़ गया है, जो किसी भी तरह अपनी सीट जीत सकते हैं। यही वजह है कि दल-बदल विरोधी कानून होने के बावजूद पिछले कुछ सालों में सांसदों, विधायकों के पाला बदलने की प्रवृत्ति फिर से तेज हो उठी है। इस तरह कई राज्यों में ऐसे दल सत्ता पर काबिज हो गए, जिनके पास बहुमत नहीं था, पर दूसरे दल के नेताओं को तोड़ कर अपने पाले में ला सके। अभी पांच राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों में तो जैसे सारे रिकार्ड टूटते नजर आ रहे हैं।
ऐसे कई विधायक हैं, जो अपनी पार्टी की स्थिति डांवाडोल देख दूसरी पार्टी में जगह बनाने की कोश्शि करते देखे गए या देखे जा रहे हैं। पंजाब में तो एक विधायक ने पिछले डेढ़ महीने में तीन बार पार्टी बदली। ऐसे ही कई विधायक गोवा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी देखे गए। उत्तर प्रदेश में तो सत्ताधारी दल से टूट कर जीत की संभावना वाले दल में शामिल हाने वाले विधायकों का तांता-सा लग गया था। इस तरह नेताओं के पाला बदलने से लोकतंत्र जैसे मजाक बन गया है। धन्य हैं वे राजनीतक दल भी, जो ऐसे विधायकों से गलबहियां कर लेते हैं।
दरअसल, पिछले कुछ सालों में राजनीति का भी कारपोरेटीकरण हो गया है। जहां वेतन अधिक मिला, वहीं नौकरी पकड़ ली! राजनेताओं को भी पार्टी के सिद्धांत और उसके या फिर समाज और देश के प्रति निष्ठा से ज्यादा सत्ता में जगह पाने का सिद्धांत महत्त्वपूर्ण लगता है। वे अब सत्ता से कतई बाहर रहना नहीं चाहते। राजनीतिक दलों को भी अगर कोई नेता ऐसा मिलता है, जिसके चुनाव जीतने की गारंटी लगती हो, वे उसे गले लगा लेते हैं, नेता का चरित्र देखने की जहमत नहीं उठाते।
यही वजह है कि राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों की तादाद लगातार बढ़ती गई है। बेशक इसे लेकर अदालतें तल्ख टिप्पणियां करती रही हों, पर राजनीतिक दलों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनमें इस मामले में एक मूक सहमति-सी भी जान पड़ती है। पश्चिम बंगाल चुनाव के समय कई नेता इधर से उधर गए, उनमें से कुछ चुनाव जीत भी गए, मगर किसी भी दल ने उन पर दल-बदल कानून के जरिए कार्रवाई की जरूरत नहीं समझी। इसलिए कि ऐसा करने से एक का राज्यसभा में अपना समीकरण गड़बड़ हो रहा था, तो दूसरे का विधानसभा में।
हर नेता किसी पार्टी में इसीलिए जाता है कि उसे टिकट मिलेगा और वह चुनाव जीत कर सत्ता में पहुंचेगा। मगर पिछले कुछ साल पहले तक हर पार्टी की पहचान उसके कुछ सिद्धांत हुआ करते थे, लोग हारते या जीतते, सत्ता से बाहर रहा करते थे, पर उनकी निष्ठा अपने दल के साथ जुड़ी होती थी। वह अब खत्म हो गया है। यही वजह है कि हर चुनाव के वक्त दल-बदल की प्रक्रिया तेज हो जाती है। कुछ राजनीतिक दल खुद भी दूसरे दलों के नेताओं को तोड़ने का प्रयास करते हैं। यह स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान नहीं कही जा सकती। राजनेता तो शायद ही अपनी इस आदत से बाज आएं, पर इसमेंं मतदाता की जिम्मेदारी और उसका विवेक भी प्रश्नांकित होने लगा है।