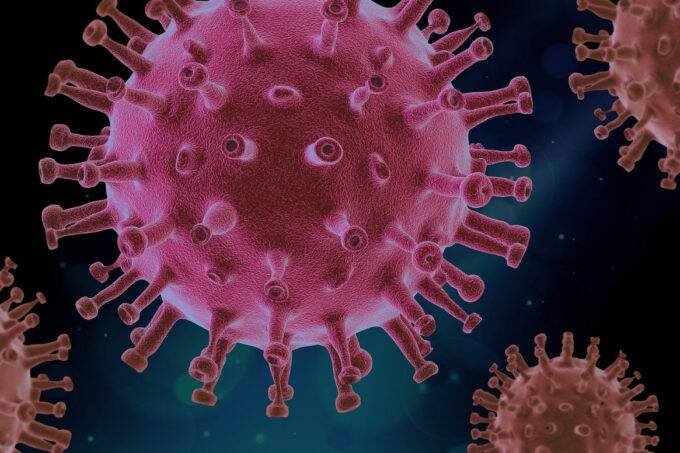सुरेश सेठ
एक लंबी अवधि के बाद जब महामारी से थोड़ा छुटकारा मिला, तो रूप बदल कर दूसरे रोग मारक मुद्रा में सामने आ गए। उखड़ती सांस और बेतरह खांसी, जो कभी परदादा होने का सूचक थी, वह एक ऐसा सच हो गई, जिसे आज कोई भी समेटना नहीं चाहता। अरे-अरे क्या कह दिया आपने? जानते तो हो कि आजकल खांसी की बात करना गुनाह है। खांसी की बात करोगे, तो फिर जुकाम और छींक की बात करोगे, फिर हल्के बुखार और दम घुटने की बात करोगे, फिर फ्लू तशरीफ लाएगा, फिर उससे दस गुना ताकतवर कोरोना फ्लू तशरीफ लाएगा। लोग दहशतजदा होकर आंकड़े पढ़ेंगे। विश्व के कितने देश इस महामारी से प्रभावित हो गए? आज महामारी से संक्रमित होने का आंकड़ा कितना बढ़ा है? बचपन से सुनते आए हैं, राम से बड़ा राम का नाम। अब कलयुग आ गया, इसलिए सुनने लगे, महामारी से बड़ा महामारी का नाम।
सुनो तो ही महसूस होने लगता है। बदन का तापमान बढ़ गया, बुखार तेज होने लगा। सांस घुट रही है। फेफड़े रुक गए, भरे-भरे से, कफ और बलगम की तासीर है, जिस पर जान जाने का भय उस पर पालथी मार कर बैठा है। बुद्धिमान कहते हैं कि नए विषाणु हैं। इनका टेंटुआ पकड़ने का हमारे पास कोई इलाज नहीं। अमीर देशों के दरवाजे पर इन्होंने पहले दस्तक दे दी, इसलिए भारी भरकम धन राशियां उनकी सटीक चिकित्सा और औषधि की तलाश करने में आबंटित हो गर्इं।
गरीब देश का आदमी औषधि के आविष्कार की प्रतीक्षा कर रहा है। इसके बारे में आशाप्रद खबरें आने लगीं, साल-डेढ़ साल तक दवाओं की खेप भी उनकी मंडियों तक पहुंच जाएगी। जहां खरीदने वाले डेढ़ बरस और जीने की गुजारिश कर रहे हैं, वहां बेचने वाला खुश है। अभी बचाव के उपकरण बेच रहा है, फिर उपचार की दवा बेच कर दुगने-चौगने दाम पर जीवनदान देगा। कितनी बड़ी सेवा है, मानव जाति उपकृत हो गई। सरकार कहती है, भाई जरूरी वस्तुए हैं, दाम घोषित हो गए। अब इसी दाम पर बेचो।
बेचने वाले ने कहा, इस दाम पर यह बचें न बचें, हमारी मर्जी। खरीदना है तो हमारे दाम पर खरीदो। खुले दिन में नहीं रात के अंधेरे में खरीदो। नहीं खरीदने का हक है तो विषाणुओं की पीठ पर लद कर दूसरे धाम की यात्र का टिकट कटाओ। सबसे अधिक भय उसे ही लगता है, दूसरे धाम के महा प्रयाण का, जिसके पेट में रोटी नहीं, हाथ में काम नहीं, बदन पर कपड़ा नहीं। बड़े बंगलों और प्रासाद मालिकों का क्या है? वे तो बड़ी-बड़ी पार्टियों से जमाना बदल जाने का नृत्य नाचते हैं। मदमत्त मादकता उनकी नसों में फिरकी की तरह घूमती है। ये वे लोग हैं जो संक्रमित होते नहीं, बाहर खड़ी जिंदगी की भीख मांगती वंचितों की भीड़ को संक्रमित करते हैं।
तुम्हें तो कहा था न इस महामारी का संदेश है, अब भीड़तंत्र निर्वासित हो गया, अकेले-दुकेले हो जाने का मौसम है। बदलते मौसम को स्वीकार करो और इस बीहड़ अकेलेपन में और भी अकेले हो जाओ। न निकलो अपने घरों से बाहर, तुम्हारा चेहरा भी किसी को नजर न आए। चेहरा नजर आ जाएगा तो अब कहीं महामारी की कतार में लगा डेंगू इसे झपट न ले। तो फिलहाल यों ही सोचो कि हमें अब ऐसे दिन काटने की आदत हो गई है। उपकृत होकर बदलते विषाणुओं का आभार प्रकट करो। इसने कम से कम हमें तालियां बजा कर विषाणु भगाने का रास्ता तो सुझा दिया।
हर नए दिन मौत के आंकड़े बढ़ जाते हैं, और कोई संवेदनशील कवि नहीं कहता, कि ‘मौत तू भी एक कविता है। कविता का वायदा था कि वह मिलेगी हमसे एक नई जिंदगी बन कर।’ जिंदगी तो वही रही, कि जैसे किसी खंडहर होती अंधेरी रात में चमगादड़ अपने डैने ड़फड़ाते हैं। डैनों के फड़फड़ाने की आवाज बरसों से हो रही है, क्या बरसों होती रहेगी? इस आवाज को बंद करने का कोई रास्ता नहीं?
डरे हुए लोग हुजूम बन कर जाने वाली रेलगाड़ियों पर लद रहे हैं। ये रेलगाड़ियां उन्हें वापस उन्हीं ठिकानों पर ले जा रही हैं, जहां से उन्होंने कभी सपनों की एक नई दुनिया इन शहरों में अपने लिए रचने की सौगंध खाई थी। लेकिन लौटते हुए लोगों के उतरे हुए चेहरे बताते हैं कि शायद उनकी नियति ही है ऐसी कसमें खाने की। कभी साहस करने की गुस्ताखी कर लें तो इस पर शार्मिंदा होते हुए भयाक्रांत वापस लौटना। मगर कब तक लौटते रहेंगे ये डरे हुए लोग? क्या वे अपनी जिंदगी को अजाब बना देने वाले इन विषाणुओं की पहचान कर पाएंगे? क्या वे कभी समझ सकेंगे कि ये विषाणु केवल महामारी पैदा नहीं करते, रूप बदल-बदल कर पैदा होने का कारण भी बन जाते हैं। वे इन सब रूपों की पहचान करना चाहते हैं, लेकिन अजनबी शहरों में अपने डैने फटफटाते हुए चमगादड़ उन्हें ऐसा नहीं करने देते। क्यों?