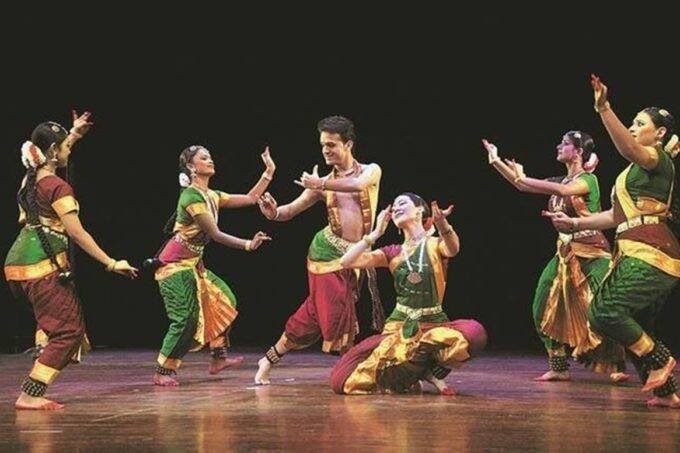हमारे शास्त्रीय संगीत में दिन के हर प्रहर के लिए अलग-अलग स्वर संयोजन का विधान है। विविध संयोजन से उपजे विशिष्ट राग विभिन्न मनोस्थितियों को प्रतिध्वनित करते हैं और आंदोलित भी। भोर की शांत वेला में भैरव का गंभीर, सौम्य निनाद आध्यात्मिकता का दर्शन कराता है तो वेदना में डूबी हुई शिवरंजनी आधी रात को उदासी की चादर में लपेट लेती है। विविध स्वरों के ताने और ऋतु चक्र द्वारा जगाए गए भावों के बाने की बुनाई से उपजा संगीत जब आभिजात्य दायरे को तोड़ कर खेत-खलिहानों, गली-चौबारों में बिखरा हुआ मिलता है तो लोक संगीत कहलाता है। धान के खेत में घुटने भर पानी में कमर झुका कर रोपनी करती हुई महिलाओं के समवेत स्वर में गाए गीत जिस तरह उनके हाड़तोड़ परिश्रम से लथपथ स्वरों की मिठास से भरे होते हैं, उसी तरह शास्त्रीय संगीत जीवन के हर पहलू को उजागर करने लगता है तो लोक संगीत बन जाता है। शास्त्रीय नियमों और व्याकरण के बंधन तोड़ कर वह उस उन्मुक्त निर्झर की तरह बहता है, जिसमें डुबकी लगाने वाला अपनी मनोभावना के अनुकूल दिशा में बहने के लिए स्वतंत्र होता है।
मसलन पूर्वी अंग के चैता को ही लें। आमतौर पर चैत-वैशाख की तपन में सुलगती विरहिन की उदासी ही जिस चैता के शब्दों मे प्रतिध्वनित होती है, वही चैता अयोध्या नगरी में राम के जन्म पर सोल्लास खुशियां भी मनाता है। परस्पर विरोधी मनोस्थितियों का निरूपण करने की स्वतंत्रता उसे लोकसंगीत की श्रेणी में आने से मिलती है। लोकसंगीत जीवन के हर पहलू से प्राणतत्त्व पाता है, हर मनोस्थिति का चित्र खींचता है। ऐसे ही वैविध्य की छटा दिखाई पड़ती है वर्षा की फुहारों में भीगे हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के उस लोक संगीत में जिससे अर्धशास्त्रीय पूर्वी अंग की गायकी के तार जुड़े हुए हैं। ठुमरी, दादरा, चैता आदि से समृद्ध पूर्वी या बनारसी अंग की गायकी सावन की रिमझिम फुहारें पड़ते ही सावन, झूला और कजरी के रंगों में रंग जाती है। इन रंगों को भरने वालों में प्रमुख थे महादेव प्रसाद मिश्र, गिरिजा देवी, सिद्धेश्वरी देवी, सविता देवी आदि। उन्होंने जिस परंपरा को समृद्ध बनाया, वह बनारस को बड़ी मोती बाई, छोटी मोती बाई और विद्याधरी से मिली थी। छन्नूलाल मिश्र , गणेश प्रसाद मिश्र और भोलानाथ मिश्र के बनारसी सुरों में गणपतिराव ग्वालियर वाले ने भी सुर मिलाया था।
किसी कृषि प्रधान अंचल में वर्षा का आगमन एक वरदान से कम नहीं होता। शायद इसीलिए महीनों से तपती धरती के कलेजे में ठंडक पहुंचाने वाले बादलों के स्वागत से पहले कजरी, सावन और झूला के गीतों में देवी-देवताओं की वंदना होती है। गहन आध्यात्मिक अंदाज को दरकिनार करके लोक संगीत की ये विधाएं खुद देवताओं को वर्षा की रिमझिम के बीच झूला झूलते हुए शृंगार रस में सराबोर देखती हैं। वह सावन ही क्या जिसपर मुग्ध होकर खुद भोलानाथ अपने आराधकों का सामीप्य पाने के लिए धरती पर न उतर आएं! फिर नीम की डाली पर पड़े झूले पर पेंग भरते लोग हों या सावन के स्पर्श से कायाकल्प पा जाने वाली पुरोधाएं- सभी गा उठती हैं- ‘ए सखि, उमा संग हरि गिरी से देखें सावन की बहार!’ इन गीतों में किसी को ‘सिया संग राम’ झूला झूलते दिखाई देते हैं तो कोई ‘राधा झूलें, किशन झुलाएं’ गाते हुए नटखट कृष्ण को इतने वेग से राधा को झुलाते देखता है कि गोरी राधा श्यामवर्ण बादलों में छुप जाएं। कजरी गायन के लिए मशहूर मिर्जापुर में कजरी गायन शुरू होता है विंध्याचल पर्वत पर विराजने वाली विंध्यवासिनी देवी की आराधना से। ‘निबिया तले, बागीचा तले, मैया रुनझुन आ जा निम्बिया तले’ से मां के आवाहन के बाद ‘निबिया की डाली पड़े रे हिंडोलवा, मैया झूला झूलीं ना’ गाकर देवी के भी सावन के सम्मोहन से पुलकित होने की कल्पना की जाती है।
सावन, झूला और कजरी- तीनों विधाएं देवी देवताओं को वर्षा ऋतु के उल्लास में सराबोर देखती हैं, लेकिन कजरी ठेठ भौतिक धरातल पर उतर कर मानवीय नायक नायिका के संयोग-वियोग के चित्र भी रचती है। कजरी के गीतों में झूले में पेंग लगाने वाली प्रसन्नमना युवती या परदेसी प्रीतम की याद में तड़पती विरहिन के साथ उनकी सास-ननद भी होती हैं। जब भाभी ताना देकर पूछती है- ‘कैसे खेलन जइबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आइल ननदी’, तो ननद भी पलट कर कहती है- ‘भौजी बोलत बाटू बोली, लागे हमरा दिल में गोली, काहे पड़ली बाटू हमरी डगरिया, बदरिया घेर आइल ननदी।’
जमीनी स्तर पर रची कजरी समाज की मौजूदा स्थितियों से रूबरू रह कर बदरिया का तुक कचहरिया आदि से भी मिला लेती है। कजरी व्यंग्य भी करती है और मुस्कान भी बिखेरती है। बस दुख इसका है कि आम आदमी की भावनात्मक जड़ों को बरखा के संगीत से सींचने वाली कजरी अब डिस्को डांस वाले वीडियो में भी घुसाई जाने लगी है, भले ही इस फूहड़ कोशिश में उसका सहज पारंपरिक सौंदर्य समकालीनता की वेदी पर बलि चढ़ जाए।