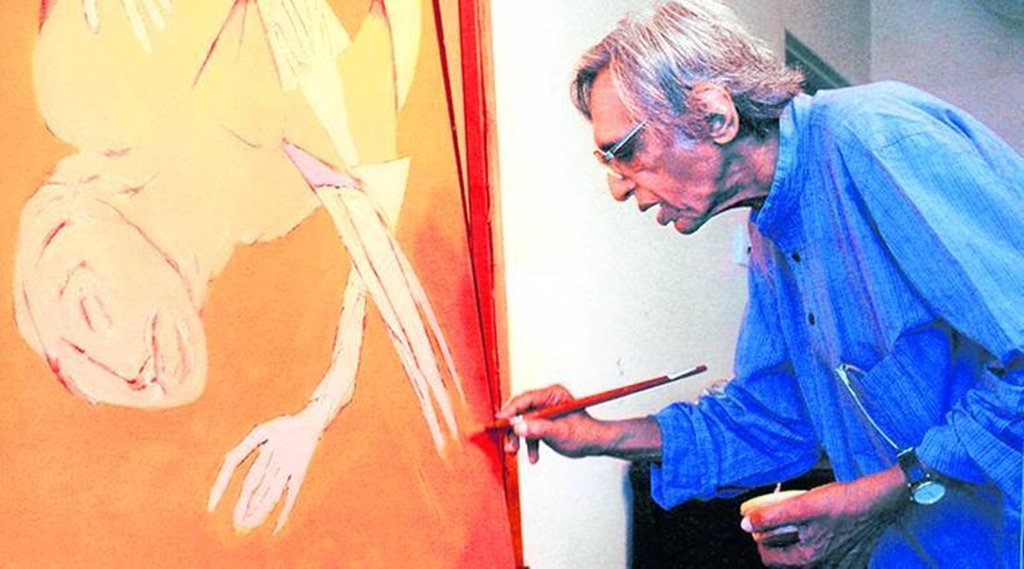स्टेशन के बाहर एक फक्कड़ आदमी दीवारों पर चित्र उकेर रहा था। वह एक हंसती तस्वीर बनाता, फिर उसके बगल में कोई रोती तस्वीर उकेरता, फिर एक खिलखिलाती तस्वीर पर कूची चलाता और ठीक उसके बगल में कोई गुस्सैल, कोई दुखी चित्र रंग देता। कुछ लोग रुकते, देखते और आगे बढ़ जाते। कुछ हैरान होते। कई ऐसे भी थे, जिन्हें कोई मतलब नहीं था। कोई पागल कह कर, हंस कर चला जा रहा था, तो किसी को वह दार्शनिक नजर आ रहा था। तभी एक लड़की वहां से गुजरी, फोन निकाला और सेल्फी ले ली।
मगर तुरंत फोटो मिटा भी दी। वह उस आदमी के पास जाकर बोली कि आप बेहतरीन ब्रश चलाते हैं, तो कुछ सुंदर रंगिए। ये मुस्कराती तस्वीरों की बगल में उदास और दुखी चित्र जम नहीं रहे। वह आदमी हंस पड़ा और बोला- हंसती तस्वीर बनाना बेहद सरल है और रोती, दुखी तस्वीरें बनाने, उनमें गुस्से के भाव भरने में मुझे भी दोगुना समय लगता है। मगर हमें सरल चीजें रास कहां आती हैं? कह कर वह हंस पड़ा। लड़की भी आंखों में सवाल लिए आगे बढ़ गई। हंसना आसान है, लेकिन हम पूरे दिन तनाव चेहरे पर तान कर रखते हैं। जो भाव हमें तस्वीर में नहीं जमते, उन्हें हम जीवन में लाद कर घूमते हैं।
किस्से-कहानियां एक बेहतर जरिया हैं उन आसान चीजों और बातों को समझने का, जिन्हें हम बेवजह मुश्किल बना देते हैं। पर क्या कहानियां कोरी कल्पना होती हैं? शायद हमेशा नहीं, क्योंकि कल्पना को भी उड़ान भरने के लिए कहीं न कहीं सच का कोई सहारा जरूर चाहिए। बाल पत्रिकाओं की मजेदार और सीख भरी कहानियां, चाचा चौधरी के किस्से, ढेरों कॉमिक्स आज के युवा और अधेड़ अभिभावकों के बचपन का हिस्सा जरूर रही होंगी। दादी, नानी की हंसगुल्लों से भरी कहानियों के जिक्र के बिना तो कहानियों की कहानी भी पूरी नहीं हो सकती।
उनकी कहानियां वह झरोखा हैं, जिसे खोल कर हम बचपन में झांक लेते हैं। बचपन ही शायद इनके बिना अधूरा रहता। पसीने से तर-बतर गरमी में भी खाट पर उनसे चिपक कर कहानियां सुनने का अलग ही रस था। सर्दियों में तसले में सुलगती आग, मंूगफली-गजक चबाते-चबाते बिना पलक झपकाए दादी-नानी को ऐसे घूरते रहते थे कि मानो सामने टीवी ही चल रहा हो और पलक झपकी, तो जैसे दृश्य खो जाएगा। पानी का गिलास लेने के लिए भी शर्त होती थी- मेरे आए बिना कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। जन्मदिन या कक्षा में अव्वल आने पर कहानियों की किताबों का इनाम ही नाचने के लिए काफी होता था।
उम्र बढ़ने के साथ ही हमारा कहानियों से रिश्ता भी परिपक्व होता जाता है। हल्की-फुल्की, हंसाती, गुदगुदाती कहानियां जीवन की सच्चाई और गंभीरता से रूबरू होने लगती हैं। मनोरंजन करती इन कहानियों ने ही साहित्य और समाज से निकलती और उन्हीं में समाती कहानी, उपन्यासों की राह बनाई होगी। कहानियां जीवन ही तो होती हैं। किसी घटना का किस्सा ही कहानी की शक्ल लेता है। कहानियां कभी नहीं मिटतीं, ये कल भी थीं, आज भी हैं और कल भी रहेगीं। पर अब न तो बच्चे कहानी सुनने में दिलचस्पी रखते हैं और न ही दादी-नानी को कहानियां सुनाने की बेचैनी होती है। कोरोना काल ने पढ़ाई ही नहीं, जिंदगी के भी ‘वर्चुअल’ बन जाने की ऐसी वजह हमें दे दी है कि हमने खुद ही कहानियां ही नहीं, रिश्तों से भी दूरियां बनानी शुरू कर दी है। दादी-नानी भी ‘स्मार्ट’ हो गई हैं।
वीडियो चला कर कहानी दिखाने-सुनाने में उन्हें मजा आने लगा है। खैर, समय तो है ही बदलने के लिए, यह इसकी चाल है और बदलाव इसका काम। मगर कहानियों का नाता किताबों से है, बतकही का अंदाज इसे जिंदा करता है। वर्चुअल औैर पीडीएफ फॉरमेट, किताब का सुख नहीं दे सकता। किताब हाथ में लेकर पढ़ने का जोे एहसास अंगुलियों में रमा रह जाता है, वह कहानी और लेखक से एक अलग ही नाता जोड़ देता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आंधी में प्रिंट मीडिया के पैर उखड़ने की बातें भी ज्यादा पुरानी नहीं हैं। पूर्णबंदी में किताबों, अखबारों को छूकर पढ़ने की कमी सबसे ज्यादा खली। जिन चीजों को हम छू सकते हैं उनसे रिश्ता भी उतना ही गहरा और नजदीकी होता है।
मगर जब कहानियों, उपन्यासों से ही रवानगी हो रही है, सरकारें तय करें कि वोट डालने की समझदारी रखने वाले युवा क्या पढ़ेगें और क्या नहीं। हांलाकि अश्लील साहित्य फिर चाहे वह पन्नों में छिपा हो या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नाच रहा हो, वहां हमारा ध्यान और विवेक नहीं जाता। हंसी आती है कि ये किताबें पढ़ने में दिलचस्पी रखने वाला तबका, विचारशील है या फिर कोई उन्मादी भीड़, जो पढ़ कर, सोचने के बजाय विद्रोह की मशाल उठा लेगा। कहानियों के बहाव को समाज में बहने से रोकना शायद सवालों से भागना और सच को पीठ दिखाने से ज्यादा कुछ नहीं।