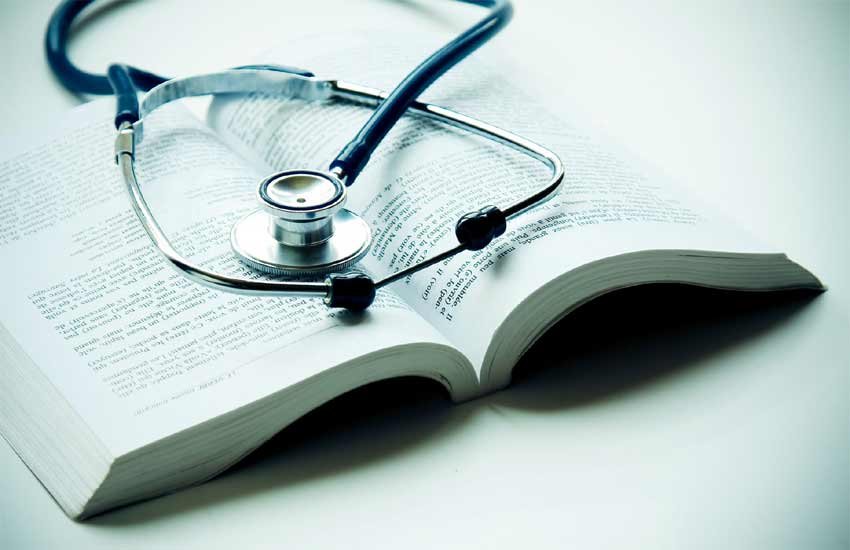हाल ही में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने पहले अपने परिवार वालों पर तलवार से जानलेवा हमला किया और फिर बाहरी लोगों के साथ-साथ बीच-बचाव करने आए पुलिसकर्मी पर भी वार किया। आखिरकार पुलिस को उस युवक को गोली मारनी पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। देश के एक युवक का यों चला जाना दुखद है, लेकिन उससे भी दुखद वे कारण हैं, जिन्होंने उसे इस हद तक अवसादग्रस्त कर दिया था। वह युवक आइएएस की प्रारंभिक परीक्षा में असफल हो गया था, इस ‘सदमे’ को बर्दाश्त नहीं कर सका और मानसिक संतुलन खो बैठा। जबकि उसे रोजगार की चिंता नहीं थी और वह किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत था, जहां शायद अच्छा-खासा वेतन मिलता होगा। यह कोई अकेली घटना नहीं है, लेकिन इसके विश्लेषण में जाने पर कई परतें खुलती हैं। आखिर यह सिविल सेवा का तिलिस्म क्या है, जिसमें असफलता एक अच्छे-भले नवयुवक को इस कदर मौत के मुंह तक ले जाती है। दूसरे, बेरोजगारी का सवाल है, जो इस घटना से प्रत्यक्षत: नहीं जुड़ी हुई है।
दरअसल, आइएएस होने या न होने के बीच एक बड़ी सामाजिक प्रतिष्ठा की खाई है। इसमें इस और उस पार के बीच वही अंतर हो जाता है जो एक मालिक और अधीनस्थ में होता है। सुनने में ये शब्द कठोर जरूर लगते हों, लेकिन यह एक सच है जो परंपरागत भारतीय समाजों में और भी गहरे रूप से स्थापित है। बचपन से ही समाज हमें यह बताता रहता है कि एक बार आइएएस बन कर ‘लालबत्ती’ ले लो फिर तो पूरा संसार ही तुम्हारा है।
मैंने अपने गांव में देखा है कि डीएम का नाम सुनते ही आदमी अनायास थोड़ा मुग्ध हो जाता है। अब अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें कोई आइएएस क्या करे! किसी ने इसके लिए मजबूर तो नहीं किया है! लेकिन सच यह है कि इसके लिए एक तरह से बाध्य ही किया जाता है एक ऐसी संस्कृति का निर्माण कर। अधिकारीगण अपने आपको आम जनता से काट कर रखते हैं और एक अलग-सी छवि बनाते हैं। उसे हवा मिलती है ऐसी सामाजिक मानसिकता में जीने वाले लोगों से जो खुद को असहाय मान कर उन्हें ‘माई-बाप’ का दर्जा दे देते हैं। इसके तमाम उदाहरण मौजूद हैं।
इस पद की ‘उच्चता’ का आलम यह है कि लोग बेचैन रहते हैं किसी भी प्रकार से ‘साहब’ से अपना संबंध जोड़ लेने ले लिए, चाहे वह जाति के आधार पर हो, क्षेत्र, भाषा या किसी अन्य माध्यम के आधार पर। फिर यह अंतर सिर्फ आइएएस अधिकारी और आम जनता के बीच नहीं, बल्कि आइएएस और गैर-आइएएस अधिकारी के बीच भी है। इन्हें न केवल पदोन्नति में अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है, बल्कि ये हरेक विभाग के प्रमुख हो जाते हैं, भले ही किसी ने उस विभाग में इनसे कई गुना अधिक अनुभव क्यों न अर्जित किया हो! अनेक सुधार आयोग भी ऐसे सुझाव दे चुके हैं और सातवें वेतन आयोग के प्रशासनिक सुधार संबंधी सुझाव भी इस ओर इशारा करते हैं। जरूरत है इस व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव करने की, ताकि इस तरह के विभाजन पर रोक लगे। इसका बोझ इतना न बढ़ जाए कि इसमें असफल होने वाला व्यक्ति जिंदगी को ही अलविदा कह दे। यह खतरनाक है और हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।
दूसरा मुद्दा बेरोजगारी का है और वह ज्यादा खतरनाक है। यह कल्पना भी डरावनी है कि एक व्यक्ति ने जीवन के पच्चीस-तीस वर्ष पढ़ने में लगा दिए, लेकिन वह एक अदद नौकरी नहीं प्राप्त कर सका। बाजारवाद के इस युग में उसकी मनोदशा कैसी होगी? क्या हम उसे जीने लायक छोड़ रहे हैं? क्या बेरोजगारी ‘गरिमापूर्ण जीवन’ जीने के हमारे मौलिक अधिकार का हनन नहीं करती है? जिसके पास जीने लायक संसाधन न हो, वह तनाव और फिर अवसाद से ग्रस्त क्यों नहीं हो जाएगा? एक ऐसे देश में, जिसके पास विशाल जनसंख्या हो, लेकिन देने के लिए जरूरत भर रोजगार न हो, वहां तो स्थिति और भी विकट हो जाती है।
सवाल यह है कि हम इसके समाधान के लिए क्या कर रहे हैं! आर्थिक पक्ष तो है ही कि इसके लिए रोजगार उत्पन्न करने होंगे, लेकिन हमें सामाजिक स्तर पर भी जिम्मेदारी निभानी होगी। अवसाद और फिर आत्महत्या की एक बड़ी वजह यह होती है कि व्यक्ति के मन में बहुत द्वंद्व चलता रहता है और वह किसी भी अपने के पास उसे व्यक्त नहीं कर पाता है। जरूरत है संवाद के दायरे को बढ़ाने की। ऐसे मामलों में समस्या का हल बातचीत और उचित संवेदना प्रकट कर देने से भी निकल आता है। जीवन काफी महत्त्वपूर्ण है और एक ही है। इसमें उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन आत्महत्या इसका समाधान नहीं है। इससे जूझने में ही कर्म की सार्थकता है। बहुत मामूली मौकों पर भी खुशी खोजनी चाहिए। इस जीवन से बढ़ कर कुछ भी नहीं।