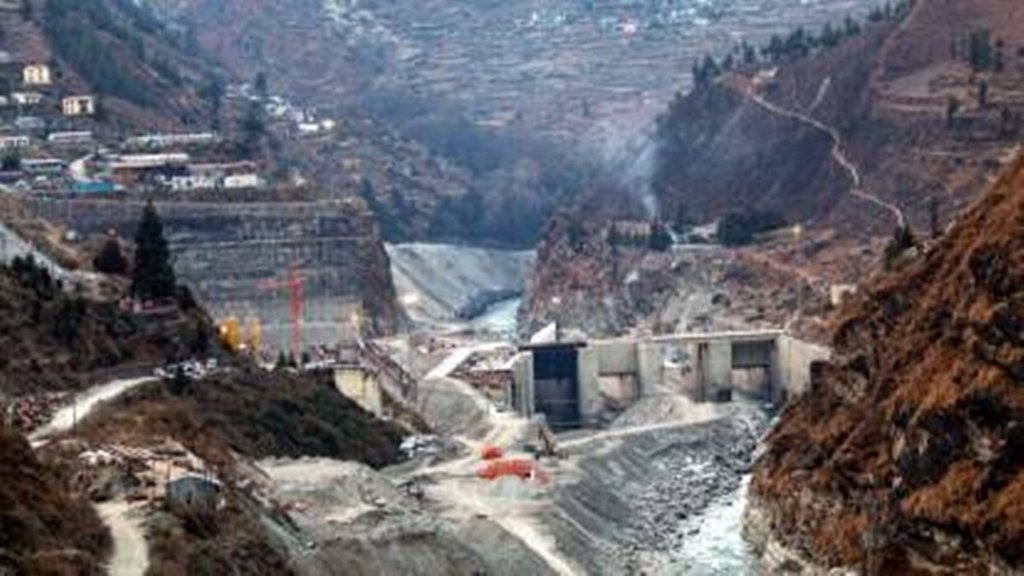विकास का पूरा दावा ही प्रकृति के विनाश पर खड़ा है। एक समय था जब जल के बिना कोई संकल्प नहीं हुआ करता था। अब तो गंगा हमसे नाराज है। नदियों के पूजक देश के साहित्य में नदियों को पुराण पुरुष की नाड़ी कहा गया है, क्योंकि उनसे ही देश की भौगोलिक, सांस्कृतिक और मिथकीय एकता का आधार मिलता है।
लेकिन नदियां अब राजनीति के मुद्दों से अधिक कुछ नहीं। यह सरकारी अनुदान पाने का एक जरिया है। पुलों का टूटना, सड़कों का नष्ट हो जाना महज एक आपदा है, जिसका बाकायदा मुआवजा मिलता है। यह एक रहस्यमय व्यक्तिनिष्ठ रोमांटिक दुनिया है जो व्यक्ति केंद्रित है और हमारी धार्मिकता एकांगी। दरअसल, शिक्षा-संस्कृति का क्षेत्र न तो धर्म क्षेत्र है, न ही कुरुक्षेत्र।
इसे ज्ञान का क्षेत्र ही बने रहने की कोई स्थायी मनोभूमि हमारे पास नहीं। नदियां, तीर्थों, पर्वों, उत्सवों, मेलों का रंग अब बाजारू हो गया है। उनको सहजेने के पीछे की मुहिम सांस्कृतिक नहीं व्यावसायिक है। उन्हीं को भेदकर आधुनिक बाजार खड़ा करने की साजिश विस्तार ले रही। अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में कहीं कोई अंतर्संबंध नहीं दिखता।
दो कमरों में सिमटी शहरी जिंदगी जितनी कुरूप उतनी अंधेरी। कहने को आलीशान और शानदार तरीके से बनाई गई गगनचुंबी इमारतें, लेकिन उनकी बनावट ऐसी कि इसमें बने घरों के भीतर सूरज झांक नहीं सकता। वीडियो बनाकर थकी वे स्त्रियां सो जाती हैं कि सुबह दफ्तर जाना है। शहरीकरण के कुहासे में बसी स्त्रियां आधुनिक हो गई हैं और आत्मनिर्भर भी।
हालांकि आधुनिकता और आत्मनिर्भरता के वास्तविक मूल्य कितने जीवंत हैं, यह नहीं कहा जा सकता। कभी प्रकृति से जीवन पाने वाली पहले की पीढ़ियों के बीच ही आज गिलहरी, फूलदान, चिड़िया, फूल-पत्ती से दूर हो चुके बच्चे अब सिर्फ यंत्र की भाषा समझते हैं। पड़ोसीजन्य आत्मीयता अब सूख चुकी। यों भी यंत्रों की दुनिया में गुम इंसानों के बीच अपनी संवेदना बचेगी भी कहां। वहां भी तो यंत्रों और उसके प्रभाव से संचालित दुनिया बनेगी! आधुनिकता की लपटों में वैयक्तिकता का धुआं विस्तार पा रहा और हम भूमंडलीय मीडिया से भूमंडलीय नागरिक हो गए।
अपनी जड़ों और जमीन से कटे-कटे हम शोरगुल ही नहीं, शोर-शराबे में खोए भ्रम, प्रपंचों, सोशल मीडिया के छायाभासों और छलनाओं के युग में रच बस रहे हैं। चकाचौंध और ग्लैमर के शिखरों से उतारी गई शख्सियतें बड़े-बड़े व्यावसायिक परिसरों या मालों ऐसे इठला रही हैं, जैसे पूरी व्यवस्था और तंत्र उनकी गिरफ्त में हो। और क्या भरोसा कि ऐसा सचमुच ही हो। उनके जीवन और एक साधारण इंसान के जीवन में जितना फांक और फर्क होता है, उसमें तो कुछ भी संभव दिखता है। इसे तो ऐसे भी देख सकते हैं कि व्यवस्था या तंत्र किसके लिए किस तरह और कितनी सक्रियता से काम करता है, किससे कितना सरोकार रखता है।
इसी यंत्रवत जीवन के विकास के बीच सोच और संवेदना भी यंत्रीकृत होती जा रही है और यह हमारे अपने दायरे में भी सिर चढ़ कर बोलने लगा है। मसलन, भ्रूणहत्या करते-करते हमने कन्या भाव का ही अंत कर दिया है। कन्याएं आज के आधुनिक कहे जाने वाले दौर में भी बराबरी के लिए राह ताक रही हैं। केवल सफलताओं की ही नहीं, संकट की भी कई दृष्टियां होती हैं।
नेहरू के युग की विकास योजनाएं जिस तरह अपनी ठसक खो रही हैं, एक नए किस्म का अर्थतंत्र रचा जा रहा, जिसका लक्ष्य उपभोक्ता को संतुष्ट करना नहीं, बाजार आश्रित बना देना है। दुखद आश्चर्य यह है कि इन तमाम संकटों के केंद्र में धर्म है। राममनोहर लोहिया कहते थे- ‘धर्म एक दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति एक अल्पकालीन धर्म’।
हम एक ऐसी दुनिया का हिस्सा हो चुके हैं, जिसमें भूमाफियाओं, अकादमियों के क्षेत्र उन लोगों की बन आई है, जिन्होंने इस समाज और दुनिया में किसी न किसी रूप में वर्चस्व कायम किया है। अब डीजे के शोर में कहीं कोई लोकगीत नहीं गाता। क्या पता, गाने ही न दिया जाए! सुनने वाला भी कौन मिलेगा! पश्चिम की आधुनिकता ने सांस्कृतिक आचार-व्यवहार की पद्धतियों और आपस में एक दूसरे को बरतने का न सिर्फ भाव बदल दिया, बल्कि बाजार भी बदल दिया। टीवी चैनलों का चर्चा-चक्र देशीपन को खदेड़ रहा। हल-बैल और कुलदेवता की पूजा जैसी बातें अपढ़ या निरक्षर और रूढ़िवादी लगने लगी हैं। लेकिन क्या इस बीच जीवन के वास्तविक तत्त्व भी ऐसे ही हाशिए पर नहीं चले जा रहे हैं!
गावों को विस्थापित कर महानगरों में रूपांतरित कर हम एक अजनबी शहर का निर्माण कर रहे हैं। संस्कृति के नाम पर युद्ध का आंगन नहीं बनना है। हमें भारतीयता के समग्र में झांकना होगा, जहां आत्मनिर्भता तो हो, लेकिन शीलता और करुणा का उत्सर्ग भी हो। ‘ग्लोबल राइटिंग’ या वैश्विक लेखन के मायावी सपनों में उतरने से पहले हमें अपनी तासीर आबोहवा जरूर एक बार टटोलना चाहिए।