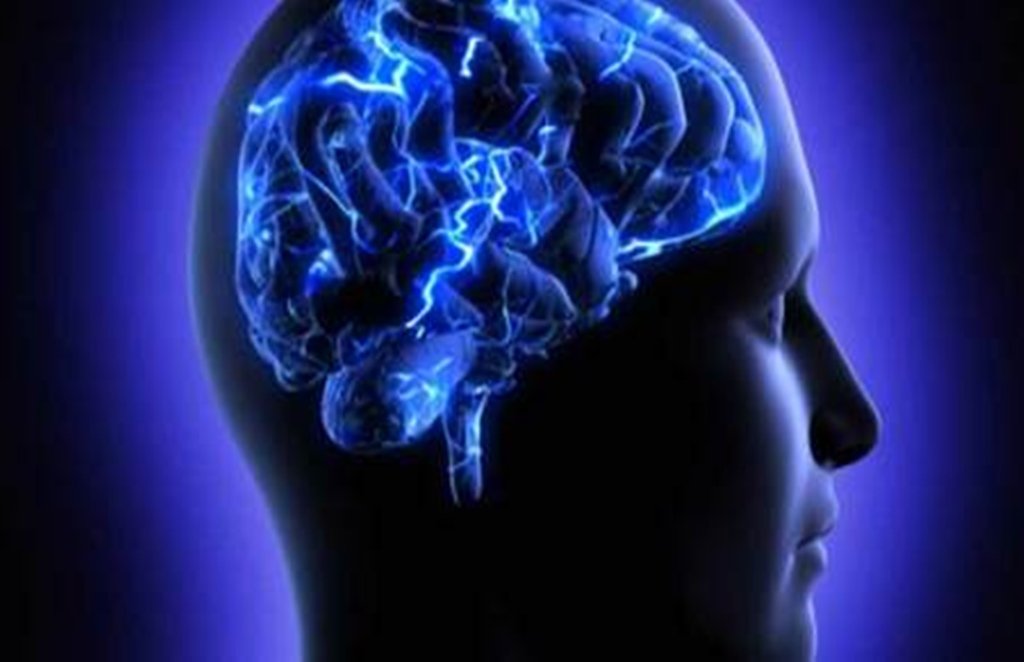मोनिका भाम्भू कलाना
मनुष्य आमतौर पर पूर्वाग्रह से भरा हुआ जीव है। किसी नई जगह जाने या किसी नए व्यक्ति से मिलने से पहले हम कई बार सिर्फ कुछ बातें सुन कर या फिर कल्पना करके उसके बारे में एक धारणा बना चुके होते हैं। इस क्रम में सोचने-समझने का कोई अवसर मिले, उससे पहले ही इतनी गलतफहमियां बीच में पनप जाती हैं कि एक लंबी प्रक्रिया और बहुत लंबे समय के बावजूद हम उनसे पार नहीं निकल पाते।
दरअसल, यह व्यक्ति के मनोविज्ञान की परतों में छिपी ग्रंथियां होती हैं, जो कई बार उस पर हावी हो जाती हैं और उसे निरपेक्ष नहीं रहने देतीं। ऐसी स्थिति में संवेदना के स्तर पर जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होनी चाहिए, वह नहीं हो पाती और इसका सीधा असर सामने वाले से तारतम्य बिठा पाने पर पड़ता है, जिसकी दिशा आमतौर पर नकारात्मक रुख अख्तियार कर लेती है।
दरअसल, ऐसी धारणाएं मानवीय चेतना का हिस्सा इस तरह बन जाती हैं कि इससे अलग हम सोच ही नहीं पाते। अब चूंकि व्यक्तिवाद पर आधारित सोच और बर्ताव हर जगह हावी दिखता है, दूसरे की जिंदगी में व्यक्ति का दखल केवल अनचाहा है, तब पूर्वाग्रह भी एक तरह से अपनी सोच को दूसरे पर थोपने जैसा है। यह अमूमन व्यक्ति के रूप में एक वर्ग का दूसरे के प्रति भाव होता है, जिसकी शुरुआत राय बनने से होती है।
इसी वजह से दो भिन्न स्तर पर जी रहे लोगों के बीच ही अधिकतर विवाद उभरने की संभावना रहती है। इससे हम सामने वाले व्यक्ति के पूरे मनोविज्ञान और सभी तरह की पृष्ठभूमियों को नजरअंदाज करके अपने और केवल अपनी भावना की संतुष्टि के लिए उसके बारे में निर्णय दे देते हैं। जबकि हो सकता है कि जिस धारणा की बुनियाद पर खड़े होकर ऐसा किया गया होता है, उसकी जमीन बहुत कमजोर होती है। हमारी धारणा के विपरीत वह व्यक्ति बहुत अच्छा हो सकता है या फिर बहुत बुरा भी हो सकता है।
सच यह है कि अधिकतर पूर्वाग्रह समय के साथ गलत साबित होते हैं और उन्हीं के साथ व्यक्ति और उसकी धारणाएं भी कहीं न कहीं उसी अनुपात में गलत साबित होती जाती है। इससे साबित यही होता है कि अपने आग्रहों के निर्माण के क्रम में हमें अपना आकलन करना चाहिए, ताकि अपनी ही धारणा के बरक्स सोचने की नौबत नहीं आए।
लेकिन बार-बार ऐसा होने के बावजूद व्यक्ति समांतर इस पूरी प्रक्रिया को जारी रखता है। व्यक्तियों के एक समूह में अनायास किसी अनिवार्यता की वजह से नए व्यक्ति का जुड़ना अक्सर एक दुर्घटना की तरह प्रतीत होता है। हमें जिन लोगों से जुड़े हुए चार दिन हुए होते हैं, हम उनके साथ सहज महसूस करने लगते हैं, लेकिन पांचवे दिन किसी का आना बर्दाश्त से बाहर होता जाता है। यह दिखाता है कि कैसे मनुष्य दो विरोधाभासों को एक साथ जीता रहता है। कई बार इस तरह के विरोधाभासों के निर्माण और उसकी प्रक्रिया के बारे में सोचती हूं कि यह किन हालात में संभव हो पाता है।
मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि लगभग हर जगह ऐसी स्थिति में हमें कभी न कभी बाहरी जैसा महसूस कराया जाता है। और यह भी मजेदार बात है कि ऐसा केवल विशिष्टता के आग्रही लोगों के बीच ही होता है, सामान्य कहे-माने जाने वाले लोगों के बीच कतई और किसी प्रकार नहीं। अधिकतर समस्याएं स्तरीयता के साथ ही होती हैं, वरना नहीं। हम किसी छोटी क्लास यानी जिसमें सदस्य बहुत कम हों, जाकर जितना असहज महसूस करते हैं, उतना सैकड़ों की संख्या वाली एक कक्षा में जाकर नहीं।
बाजार में जाकर तो शायद ही हमें कुछ खास लगे। अपरिचय बोध अवश्य लग सकता है, लेकिन असहजता तो बिल्कुल नहीं। इसकी वजह यह होती है कि हम बाजार में जाने के बाद सब कुछ वैसा पाते हैं, जिसके प्रति बचपन से सहज रहते आए हैं। घर के आसपास से लेकर बाहर निकलने तक ऐसे माहौल से रूबरू होना पड़ता रहा जिससे ठीक से परिचित रहे। लेकिन जैसे-जैसे कुछ बातों को लेकर आग्रह पनपते हैं, वैसे-वैसे हमारी अनुभूतियों में भी बदलाव आने लगता है। फिर असहजता पूर्वाग्रह के साथ चली ही आती है।
जहां हम किसी को नहीं जानते, कोई हमें नहीं जानता, वहां कोई दुविधा, कोई असहजता, कोई विशिष्टता और कोई आग्रह नहीं होता। यह भी है कि पूर्वाग्रह जैसी चीजों का फर्क सामने वाले व्यक्ति पर तब तक कतई नहीं पड़ता, जब तक वह खुद हीन ग्रंथि से ग्रस्त न हो। आत्मविश्वासी और समर्थ व्यक्ति जीवन संग्राम में जैसे अन्य तमाम दुविधाओं से संघर्ष करता है, उसी तरह इससे भी पार पा लेता है।
लेकिन आखिर हमें सोचना चाहिए कि हमारा पूर्वाग्रह क्यों किसी के द्वंद्व की वजह बने और अगर काफी कोशिशों के बावजूद हम इससे नहीं बच सकते, तब इतना अभ्यास तो हमें करना चाहिए कि कम से कम हम इसे जाहिर तो न ही होने दें। बहुत बार यह होता है कि यह मजाक से शुरू होकर घातक रूप लेता जाता है। इतना भी कि नए व्यक्ति को पलायन के लिए विवश कर दे। इसमें किसकी जीत और किसकी हार देखी जाएगी?