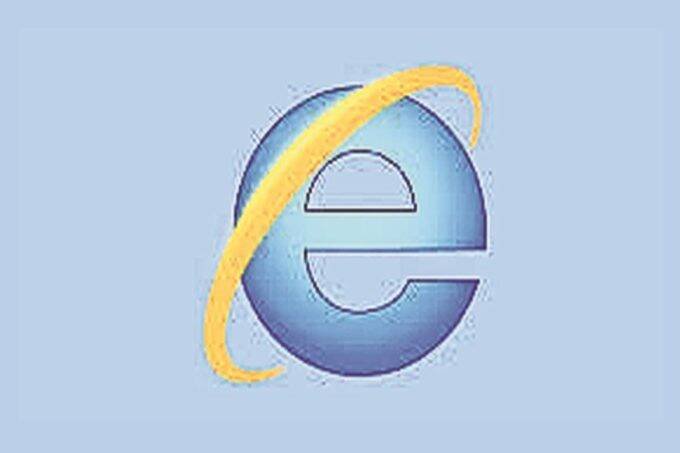एस्टोनिया एक ऐसा देश है जो सन् 2001 से ही अपने यहां सभी नागरिकों को इंटरनेट की उपलब्धता के लिए प्रयासरत है और इंटरनेट को अधिकारों की सूची में सम्मिलित किया गया है। लेकिन वहां भी महामारी के संकट में स्कूल बंद होने के बाद ही ऑनलाइन शिक्षा का अस्थायी विकल्प अपनाया गया है। इटली में महामारी का कहर अधिक रहा है। पिछले साल स्कूल बंद होने के साथ ही वहां के शिक्षा मंत्री ने गूगल के अधिकारियों को बुला कर अपने स्कूलों को ऑनलाइन करने के लिए डिजिटल तकनीक का सहयोग मांगा था। ब्रिटेन में भी गरीब बच्चों को लैपटॉप दिया गया था, लेकिन वहां भी स्कूल खोलने के विकल्पों पर लगातार बात होती रही। यही नहीं, वहां ऑनलाइन शिक्षा को लेकर कई अध्ययन किए गए। एक अध्ययन में यह निकल कर आया कि ऑनलाइन माध्यम में पढ़ाई के घंटे कम हो गए हैं। वहां के शिक्षक और अधिकारी कुछ महीनों की स्कूल बंदी से विद्यार्थियों का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था कर रहे हैं।
हमारे देश में कुछ दिनों को छोड़ दें तो बीते करीब डेढ़ साल से स्कूल कमोबेश बंद ही रहे हैं। लेकिन इस बीच ऑनलाइन शिक्षा को लेकर प्रचार-प्रसार तेजी से बढ़ा है। स्कूल बंद होने के कारण, शिक्षा तकनीक का व्यापार करने वाली कंपनियों के अपने बाजार का जबर्दस्त विस्तार हुआ है। आज जूम, गूगल क्लासरूम, टीम्स जैसे ऐप आम हो गए हैं। पिछले साल एक दिन में तीन लाख अठारह हजार लोगों ने जूम ऐप डाउनलोड किया था। उसके बाद से अब तक का अंदाजा लगाया जा सकता है। जब दुनिया के ज्यादातर देश अपनी अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार से जूझ रहे हैं, तो शिक्षा तकनीक की कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं। जोर-शोर से प्रचारित शिक्षा तकनीक आपदा में एक वैकल्पिक अवसर तो देती है, लेकिन यह माध्यम नियमित स्कूलों का विकल्प नहीं बन सकता है।
हाल ही में मैंने जम्मू, पूंछ, साम्बा के कुछ ग्रामीण स्कूली छात्र-छात्राओं से मुलाकात की। जो ग्यारहवीं-बारहवीं में हैं, उन्होंने बताया कि उनकी एक-दो घंटे ऑनलाइन कक्षा चलती है, जिसमें उनको कोई गृह कार्य दे दिया जाता है। कार्य करने के बाद वे शिक्षकों को मूल्यांकन के लिए भेज देते हैं। लेकिन निचली कक्षाओं के बच्चों के पास न तो ऐसे संसाधन हैं और न ही उनके लिए कोई प्रबंधन। स्कूल बंदी के दौरान देश के कई हिस्सों में सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने ऑनलाइन के विकल्प के तौर पर वाट्सऐप, यूट्यूब, लाउडस्पीकर आदि का उपयोग करके अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने का प्रयास किया है।
कुछ शिक्षकों ने गांव-मोहल्ले में पढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन उनकी खबर, स्थानीय स्तर तक सीमित रही। बड़ी कंपनियों ने विज्ञापन देकर, ब्रांड अंबेसडर उतार कर, स्वयंसेवी संस्थाओं को आर्थिक सहयोग देकर अपने लिए जगह बनाने की रणनीति अपनाई है। शिक्षा तकनीक की बड़ी कंपनियां कुछ शिक्षकों को मुफ्त प्रशिक्षण भी दे रही हैं, ताकि वे शिक्षक दूसरे शिक्षकों को इन कंपनियों के शैक्षिक उत्पादों के बारे में बताएं।
इन सभी प्रयासों के बीच क्या यह सच नहीं है कि शिक्षा तकनीक हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक असमानता पैदा कर रही है? अपने देश में लगभग बत्तीस करोड़ स्कूली विद्यार्थियों में से चार करोड़ से कम विद्यार्थी ही ऑनलाइन माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख पा रहे हैं। तो जो अट्ठाईस करोड़ बच्चे तकनीकी संसाधनों से वंचित हैं, उनके लिए शिक्षा की चुनौतियां क्या और नहीं बढ़ गई हैं? यों भी महामारी और आर्थिक चुनौती के चलते विद्यार्थियों की एक बड़ी संख्या स्कूल छोड़ सकती है तो शिक्षा में तकनीक कैसे हमारे लिए सहायक हो रही है?
ऑनलाइन शिक्षा के लिए सिर्फ एक स्मार्टफोन की जरूरत नहीं रहती है। उसके लिए हर महीने कम से कम ढाई सौ, तीन सौ या इससे ज्यादा का इंटरनेट डाटा खरीदना पड़ता है। पाठ के प्रिंट निकलवाना होता है और इंटरनेट की अनवरत कनेक्टिविटी की जरूरत होती है। जिन विद्यार्थियों का पोषण स्कूल के मध्याह्न भोजन पर निर्भर हो, क्या वह ऑनलाइन शिक्षा के प्रवाह में शामिल हो पाएंगे? ऐसी घटनाएं भी सामने आईं, जिनमें स्मार्टफोन या कंप्यूटर के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाने पर किसी बच्ची ने खुदकुशी कर ली। कितने बच्चे अभी ही ऑनलाइन पढ़ाई के दायरे से बाहर हो चुके हैं। स्कूली शिक्षा में ऑनलाइन मॉडल सामाजिक-आर्थिक रूप से सक्षम विद्यार्थियों के लिए कुछ-कुछ सीखने के लिए तो ठीक है, लेकिन देश के ज्यादातर बच्चों लिए समावेशी नहीं है। इस तकनीक से स्कूली विद्यार्थियों के बीच एक नई चुनौती और नया विभाजन पैदा हो सकता है।
स्कूलों की भूमिका व्यापक है। वह सामाजिक-राजनीतिक मूल्यों के साथ वयस्क समाज के लिए जिम्मेदार नागरिक तैयार करने की एक संस्था भी है। वहां विद्यार्थी सिर्फ विषय ही नहीं पढ़ते हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ समन्वय, हर्ष-उल्लास, हार-जीत, सह जीवन, जाति-धर्म से ऊपर मनुष्यता के आधारभूत दर्शन को भी सीखते हैं। स्कूल में शिक्षकों के साथ अनुभव और सूचना के समन्वय से ज्ञान का सृजन होता है। शिक्षा में तकनीक की सहायक भूमिका तो हो सकती है, लेकिन वह स्कूलों का विकल्प नहीं बन सकती है।