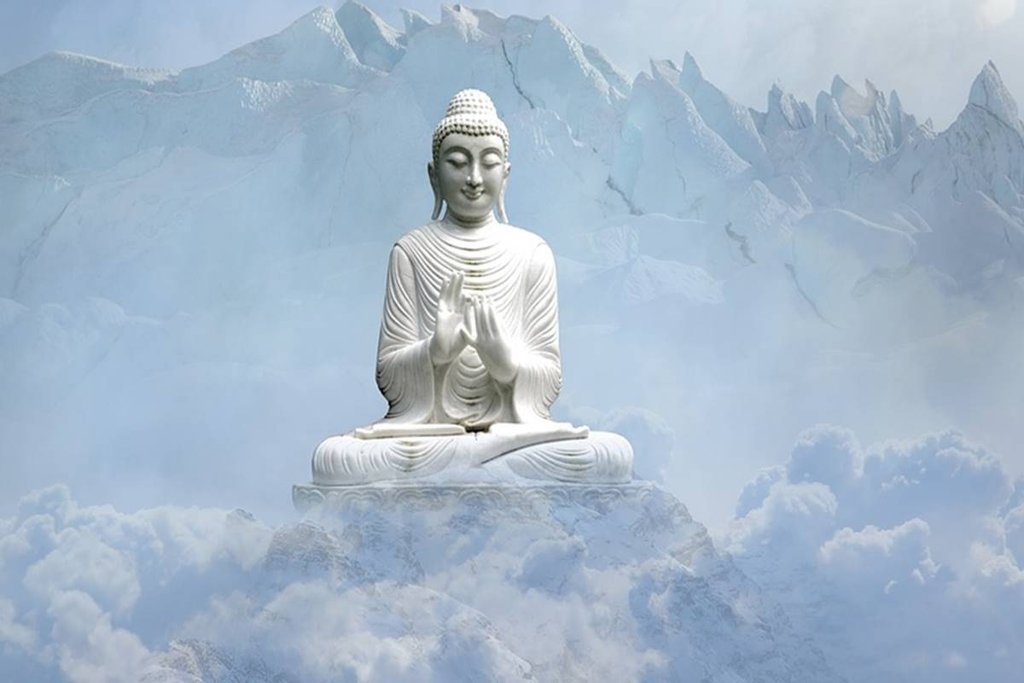मोनिका भाम्भू कलाना
बुद्ध ने कहा था कि परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी सत्ता है। मनुष्य का जीवन प्रति पल बदलता रहता है और इस प्रक्रिया में वातावरण और उससे जुड़े व्यक्तियों की अनुकूलता और प्रतिकूलता भी परिवर्तित होती रहती है। बदलाव से भागना असंभव है। सामाजिक प्राणी के तौर पर मनुष्य द्वारा बनाए गए रिश्ते-नाते भी इसी प्रक्रिया में आते हैं। यह सच है कि रिश्ते जितनी सहजता से बनते हैं, उतनी सहजता उनके टूटने में नहीं होती। वे मानवीय भरोसे के धरातल को बिल्कुल हिला कर ही विदा होते हैं। मनुष्य खुद को समर्पित करके ही यकीन पाता है। उस यकीन का टूटना बेहद पीड़ादायक होता है।
अब तक समाज में रिश्ते बनने की प्रक्रिया प्रत्यक्ष थी। लोग आपस में मिलते-जुलते थे। एक दूसरे को समझते थे और रिश्तों को एक मजबूत जमीन देते थे। एक बार आपस में तालमेल बन जाने, मन में एक दूसरे के लिए जगह बन जाने के बाद उन्हें हिला पाना इतना आसान नहीं होता था। कभी किसी मौके पर किसी बात पर अगर मनमुटाव होता भी था, तो अपने भीतर के अहं को किनारे रख कर उस रिश्ते को आमतौर पर संभाल लिया जाता था।
यह कहा जा सकता है कि वे रिश्ते चूंकि आभासी नहीं होते थे, यथार्थ की जमीन पर बनते और पलते थे, इसलिए उनमें उतार-चढ़ाव की खूबसूरती बनी रहती थी। लेकिन आज रिश्तों के बनने-बिगड़ने में सोशल मीडिया जिस तरह की भूमिका निभा रहा है, वह शोचनीय है। कुछ भी अव्यवस्थित होने पर लोग उसे समझने और संभालने के बजाय कई स्तर पर बेलगाम सार्वजनिक मंच पर यह जाहिर करना अधिक जरूरी समझते हैं कि वे धोखा खा रहे हैं और उनकी जिंदगी उस मोड़ पर है, जहां से कुछ भी नहीं किया जा सकता।
यह एक नया चलन है, जिसके माध्यम से लोग रिश्तों की बुनियाद की परख तो नहीं ही कर पाते हैं, वे न केवल अपने साथी की भावनाओं का अपमान करना सीख गए हैं, बल्कि यह अहसास दिलाना भी कि गलती सदैव एक ही पक्ष की होती है। सोशल मीडिया पर ‘लाइक’ और टिप्पणियां अर्जित करने और आभासी सहानुभूति पाने के लिए लोग बार-बार यह दिखाने को उतावले रहते हैं कि वे बहुत कमजोर पड़ रहे हैं। इस तरह से सोचने का मूल्य कुछ भी नहीं हो सकता।
भारतीय सामाजिक व्यवस्था शुरू से ही व्यक्ति को इस तरह संस्कारित करती आई है कि वह अपनी पीड़ा का बखान एक सीमा से अधिक न करे। यह दुख को अपने भीतर समेटने की प्रक्रिया का प्रतीक है। लेकिन इस क्रम में कई बार व्यक्ति अपने भावनात्मक दबाव के चक्रव्यूह में घिर जाता है और दूसरों की गलती के लिए खुद को ही सजा देने के रास्ते पर बढ़ जाता है।
इससे कभी यह भी हो सकता है कि गलती या अन्याय करने वाला निर्दोष के रूप में स्थापित रह जाए और पीड़ित को ही सारे दुख और अन्याय झेलना पड़े। इसलिए यह हमेशा सही नहीं होता है। लेकिन आज की हड़बड़ी से भरती जा रही दुनिया में ऐसा कई बार ऐसा जरूरी हो जाता है। हर बात हर किसी को नहीं बताई जा सकती।
रिश्तों की कई बातें बेहद संवेदनशील होती हैं और उनकी अपनी गरिमा होती है। इसलिए इन बातों पर चर्चा करने के लिए जिस व्यक्ति को चुना जाए, उसके भीतर संवेदना की गरिमा की समझ होनी चाहिए। हर संबंध की अपनी गरिमा और निजता होती है। और जो लोग दोनों पक्षों के बारे में कुछ भी नहीं जानते, उनके लिए आपकी भावनाओं का कोई मूल्य नहीं है।
अति भावुकता या गुस्से में की गई हमारी कोई भी टिप्पणी अन्य लोगों के लिए महज एक खबर होती है। ठीक उसी तरह, जैसे समाचार माध्यमों की खबरें होती हैं। व्यक्ति को अपनी समस्याओं से आखिरकार अकेले और केवल अकेले ही लड़ना होता है। फिर सहानुभूति पाने की लालसा से होना क्या है?
रही बात लोकप्रियता की, तो लोग केवल दूसरों की जिंदगी में तभी तक रुचि रखते हैं, जब तक कोई आलोचना का विषय हो। सच यह है कि बेचारा बनने पर अपने कहे जाने वाले लोग भी भागने लगते हैं। इस आभासी दुनिया में कवि बनने की महत्त्वाकांक्षा में उन रिश्तों के बारे में, जिनको सींचने में दो पक्ष अपना व्यक्तित्व और जीवन लगाते हैं, कुछ भी लिख कर उन लोगों से टिप्पणियां पाकर जो हमें एक फीसदी नहीं जानते, आखिर हम क्या हासिल कर लेंगे?
सभी चीजें अपनी जगह महत्त्व रखती हैं। सोशल मीडिया रिश्तों का विकल्प नहीं हो सकता। व्यक्ति को चाहिए कि समस्या आने पर समाधान वहीं से तलाशे, जहां समाधान संभव है। दूसरी जगह न आंसू बहाने से कुछ मिलने वाला है, न किसी की आलोचना से व्यक्ति की अपनी जिंदगी में सुधार संभव है। जहां से मुश्किलें पैदा होती हैं, हल भी आखिर वहीं से मिलेंगे। न फालतू के भटकाव में कुछ रखा है, न बात का बतंगड़ बना कर हंसी का पात्र बनने में।
सोशल मीडिया विचार साझा करने का अच्छा मंच हो सकता है, लेकिन बिगड़े रिश्ते बनाने का नहीं। समझदारी इसी में है कि जहां जो उपचार काम आए, वहां वही किया जाए, ताकि बाद में पछताने के लिए भी आभासी सावर्जनिक मंचों का इस्तेमाल न करना पड़े!