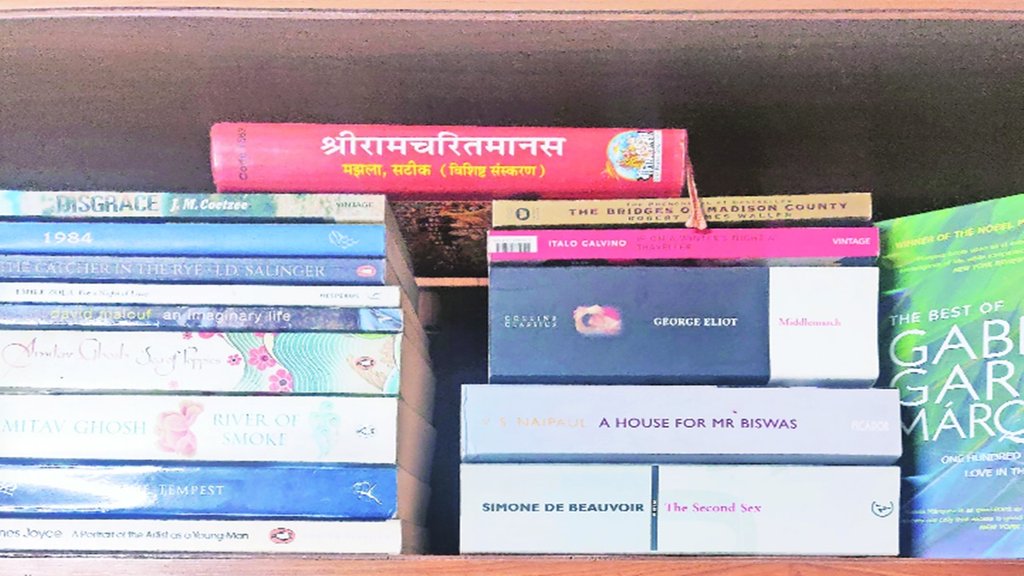नारी की झांई पड़त
अंधा होत भुजंग
कबिरा तिन की कौन गति
जो नित नारी को संग
ये पंक्तियां कबीरदास के नाम पर दर्ज हैं। तुलसीदास के बरक्स कबीरदास को छोड़ कर आपको ले चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर जहां कुश्ती की खिलाड़ी प्रदर्शन करते हुए रो रही हैं। वे कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर यौन शोषण के आरोप लगा रही हैं। यौन शोषण के आरोप पर सिर्फ इस्तीफा क्यों? यौन शोषण एक अपराध है और साबित होने पर इसकी सजा सिर्फ इस्तीफा नहीं है। लेकिन, इतने अहम मसले पर राजनीतिक दल के नेता जंतर-मंतर नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि उन्हें अभी अतीत में जाकर तुलसीदास को जातिवादी और स्त्री विरोधी घोषित करना है।
बिहार के शिक्षामंत्री ‘प्रोफेसर’ चंद्रशेखर ने ‘श्रीरामचरितमानस’ को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया। ऐसे बयान के बाद सिर्फ गुस्सा आ सकता है और लोकतंत्र से सहानुभूति जताई जा सकती है कि साधारण नौकरी के लिए भी शैक्षणिक योग्यता की दरकार होती है। लेकिन, अपने नाम के आगे ‘प्रोफेसर’ लगाने वाले नेता ऐसी साहित्यिक कृति को नफरत फैलाने वाला बताते हैं जिसने अपने समय और उससे आगे के पूरे लोक में करुणा का संचार किया है। ऐसे नेताओं का मकसद सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाना है।
चंद्रशेखर के बयान को मजबूती देने के लिए एक वर्ग बाबा नागार्जुन की पंक्तियों को इंटरनेट पर विस्तार दे रहा है जिसमें रामचरितमानस को ‘दकियानूसी दस्तावेज’ कहा गया है। एक बार फिर से तुलसीदास जाति और स्त्री-विमर्श की अदालत के कठघरे में खड़े कर दिए गए हैं।
कुछ समय पहले बाबा नागार्जुन पर बाल-यौन शोषण के आरोप लगते ही तुलसीदास को घेरने वालों ने गांधी के तीन बंदरों की तरह अपने नाक, आंख, कान बंद कर लिए थे। साहित्यकारों द्वारा वह नारीवादी बहिष्कृत की जा रही थी जो हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम से नागार्जुन का बहिष्कार करने की मांग कर रही थी। तर्क दिया जा रहा था कि जब आज नागार्जुन अपने आरोपों को साबित करने के लिए नहीं हैं तो इस पर चर्चा क्या करना? ये भी तर्क आ गए थे कि उस समय के साहित्यकार बाल और स्त्री अधिकारों को लेकर सजग नहीं थे।
बाल-यौन शोषण के आरोपी की पंक्तियों से तुलसीदास को घेरने वाले इतिहास और साहित्य के मूल्यांकन के बुनियादी सिद्धांत को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। कई सौ साल पहले लिखी रचना को आप आज के आधुनिक विमर्श पर तौलना चाहते हैं। तुलसीदास का भी एक रचनाकार के तौर पर धीरे-धीरे विकास हुआ होगा आपका कथित वैज्ञानिक सिद्धांत मानने को तैयार क्यों नहीं होता है।
एक तरफ तो आप उसे धर्मग्रंथ नहीं एक साहित्यिक स्रोत मानते हैं तो दूसरी तरफ तुलसी की एक दैवीय छवि रचते हैं कि वे ‘श्रीरामचरितमानस’ के आगे और पीछे कुछ हैं ही नहीं। बस वे स्त्री और जाति के खिलाफ खास पंक्तियां लिखने के लिए ही अवतरित हुए थे।
मंटो की रचनाओं में स्त्री के लिए वही भाषा है जो तब प्रचलित था
आधुनिक भारत के रचनाकारों में स्तब्ध करने वाले लेखक हैं सआदत हसन मंटो। मंटो का समाज को देखने का अपना नजरिया है। मंटो अपने बारे में लिखते हैं कि मेरी नायिका चकले की एक … हो सकती है। यहां पर तीन बिंदु इसलिए कि मंटो ने यौनकर्मी के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया है, समाज वही इस्तेमाल करता है। लेकिन, आज हम एक अखबार के स्तंभ में उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। मंटो के बाद स्त्री-विमर्श बहुत आगे बढ़ चुका है। मंटो की रचनाओं में स्त्री के लिए वही भाषा है जो उस समय का समाज बोलता है। मंटो अपने अफसाने के लिए जैसे किरदार, जिस तरह की स्थितियां चुनते हैं नब्बे के दशक के स्त्री-जागरण के बाद उन शब्दों, उन हालात को लिखने-देखने के तरीके बदल चुके हैं। लेकिन, आपको बीसवीं सदी में स्त्री-पुरुष के संबंधों के बीच पितृसत्ता को समझने के लिए उन शब्दों, उन शाब्दिक चित्रों से गुजरना होगा जो आपको व्यथित कर सकते हैं।
‘सीजर की पत्नी को हर शंका से ऊपर रहना चाहिए’। आज के समय में स्त्री-विमर्श के नजरिए से विलियम शेक्सपियर का यह कालजयी संवाद त्याज्य है। सिर्फ सीजर की पत्नी को क्यों, सीजर को क्यों नहीं? तात्कालिक युग के समाज को दर्शाने के लिए शेक्सपियर अपनी रचना के संवादों में उन सभी स्त्री-विरोधी बातों को लिखते हैं जो उस समय की नैतिकता के तहत मान्य थे।
साहित्यिक कृति की तरह ‘श्रीरामचरितमानस’ में नायक-खलनायक दोनों हैं
आज दुनिया भर के मंचों पर शेक्सपियर के नाटकों का मंचन होता है। अब यह आपके नजरिए पर है कि ‘मैकबेथ’ के स्त्री-पात्रों में पितृसत्ता के खिलाफ प्रतिरोध देखें या शेक्सपियर को हर पाठ्यक्रम, हर मंच, हर शोध-लेख से बाहर कर दें। ‘मैकबेथ’ पर बनी हर फिल्म को दर्शकों से दूर कर दें। तुलसीदास उस समय की जनभाषा अवधी में प्रबंध काव्य लिख रहे थे। ‘श्रीरामचरितमानस’ में वे पूरा एक लोक रचते हैं। उस समय का समाज क्या था, और क्या होना चाहिए था। जाहिर सी बात है कि वे अपने ही समय की उपज होंगे और उन्होंने ‘श्रीरामचरितमानस’ लिखने से पहले सिमोन द बोउआर की स्त्री-मुक्ति पर लिखी किताब नहीं पढ़ी होगी। एक साहित्यिक कृति की तरह ‘श्रीरामचरितमानस’ में नायक और खलनायक दोनों हैं। एक पूरे बनते-बिगड़ते राज-समाज की कथा है।
रावण और समुद्र जैसे खल-पात्रों के कहे संवाद को भी तुलसीदास के खाते में रख दिया जा रहा। हाशिए पर की एक जाति की स्त्री अगर आराध्य से मिलेगी तो वह सामयिक चेतना के अनुसार ही अपने भाव प्रकट करेगी। वह समाज श्रम-विभाजन पर आधारित था, जहां तुलसी समता लाने की वकालत करते दिखते हैं। पूरा भक्ति-काल ही भक्त और भगवान का ऐसा रिश्ता तैयार करता है जिसमें भक्त खुद को भगवान के आगे तुच्छ समझता है। लेकिन, यह समझिए कि यह अपने समय से आगे की साहित्यिक यात्रा है। रामायण की स्त्री-पात्र भी भगवान के सामने उसी तरह विह्वल होती हैं, जैसे मीराबाई। वैसे, आज के उग्र अस्मितावादी समय में तो संत कवि मीराबाई को हर तरह से खारिज हो जाना पड़ेगा। मीराबाई को लेकर जितने स्त्रीवादी विमर्श हुए हैं विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों को अपनी आलमारियों से वे किताबें खाली करनी पड़ेंगी।
भक्त और संत कवियों की रचना भावना प्रधान है
भक्त और संत कवियों की रचना भावना प्रधान है। वे आस-पास के समाज से लेकर पेड़-पौधों, पशु-पक्षियों को भावना के स्तर पर देखते हैं। तुलसीदास प्रकृति और मनुष्य का सहचर दिखाते हैं। वे उस कपास के फूल का महिमामंडन करते हैं जो सभी मनुष्यों की नग्नता ढकता है। तुलसीदास सीता के वनवास से परहेज करते हैं, उसे समय और स्त्री-न्याय के खिलाफ मानते हैं। तुलसीदास एक प्रबंधकाव्य लिख रहे हैं। प्रबंधकाव्य में आपको पूरी सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक व्यवस्था से टकराना होता है। साथ ही उसके बाद विकल्प भी देना होता है।
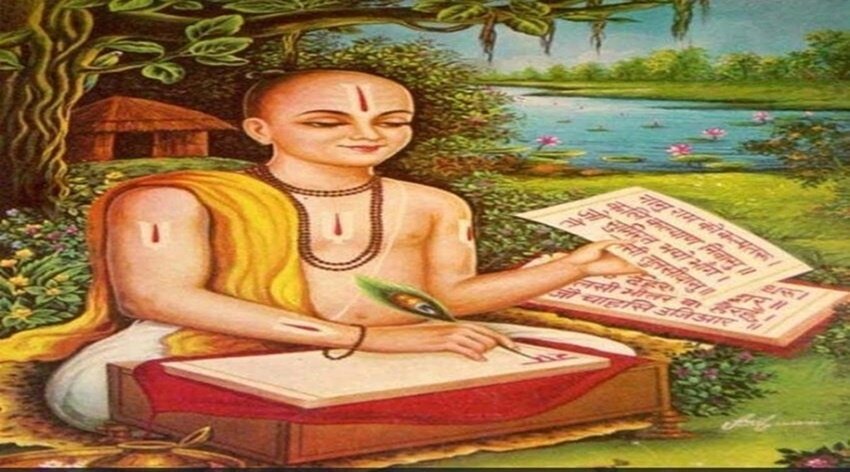
तुलसीदास पूरी संवेदनशीलता से उस यथार्थ से टकराते हैं और रामराज्य का विकल्प देते हैं। उनके समाज से टकराते क्षेपकों को उठा-उठा कर आधुनिक साहित्य के क्षत्रप बार-बार उन्हें खारिज करने पर तुल जाते हैं, जबकि किसी भी प्रबंधकाव्य को पूरी समग्रता में देखने की जरूरत है। तुलसी भी समय-काल के हिसाब से खुद को लेकर एक तकलीफदेह लड़ाई से गुजरे थे।
जब भारतीय इतिहास का भव्य-काल चल रहा था कारीगरों, विलासिता और बाजार का समय था तो चौपाई लिखने वाले की क्या पूछ होती। अपने लिए उस मुश्किल समय में भी तुलसी ने वही किया जो हर समय का साहित्य करता है। वह अपने समय से आधुनिक होकर यथास्थिति के खिलाफ विकल्प रचते हैं। तुलसीदास विवेक पर विश्वास की शुरुआत कर रहे हैं। उनका विकल्प है रामराज्य का समतामूलक समाज। आज का समाज तुलसीदास के समाज से आगे है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुलसी को उनके वक्त में जाकर पीछे धकेल दिया जाए।
तुलसी अपने साहित्य के लोकतत्त्व के कारण जन-जन के कंठ तक पहुंचे
तुलसी अपने साहित्य के लोकतत्त्व के कारण जन-जन के कंठ तक पहुंचे। उनके प्रबंधकाव्य की गेयता ने उन्हें शादी व तीज-त्योहारों के गीतों तक पहुंचाया। तुलसी सत्ता के साहित्यकार नहीं थे, यह दूसरी बात है कि उनके आगे के समय-काल की सत्ता उनके दिए ‘विकल्प’ रामराज्य को आदर्श मान लेती है और वे सत्ता के पक्ष में खड़े दिखाए जाने लगते हैं। तुलसीदास वह जनता हैं जिसको अपने साथ लाने के लिए सत्ता जतन करती है। जाति, स्त्री के आधुनिक विमर्श के लिए आपके पास आधुनिक नायक और पाठ हैं। तुलसी अपने समय में जनता के और जनता द्वारा बने रचनाकार हैं। विकासक्रम सिर्फ मानव का नहीं साहित्य का भी होता है और साहित्य से क्रम और काल को अलग करने का अवैज्ञानिक काम तो तुलसीदास ने भी नहीं किया था।