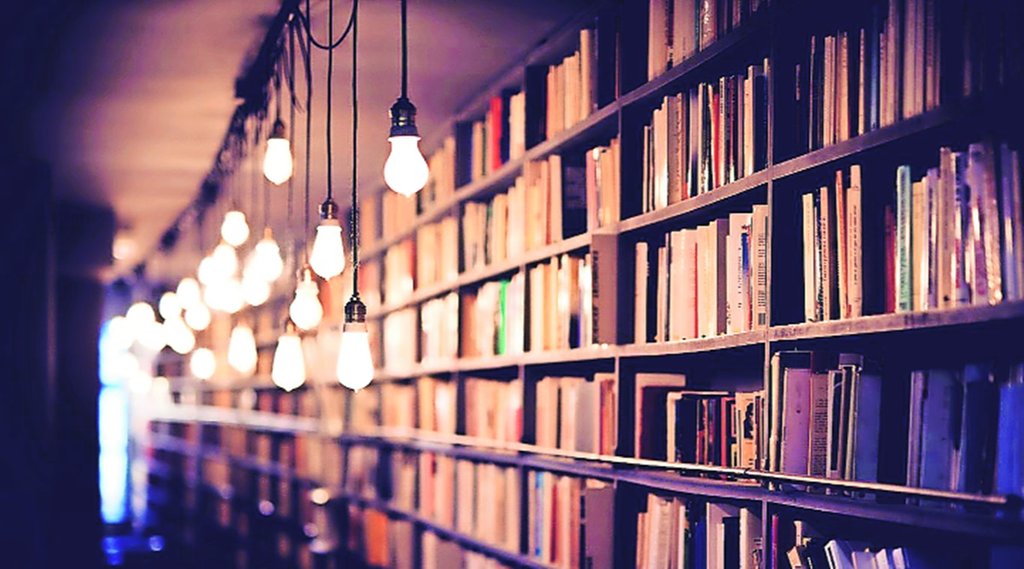अंबर्तो ईको खुले पाठ को एक अवधारणा की तरह विकसित करने में अग्रणी हैं। वे कृतियों के अर्थ संसार को क्वांटम शास्त्र की तरह ‘सर्व पाठ स्पर्शी’ मानते हैं। खुले पाठ की अवधारणा का विकास आरंभिक तौर पर पाठकवादी आलोचना पद्धति के द्वारा किया गया। इस संदर्भ में रोलां बार्थ के निबंध ‘द डेथ आॅफ द आॅथर’ की विशेष भूमिका है। उन्होंने साहित्यिक कृतियों को दो तरह का माना- लेखकीय पाठ और पाठकीय पाठ।
पाठकीय पाठ बहुत से हो सकते हैं। वे लेखकीय पाठ का पूरक भी हो सकते हैं और उसे अपदस्थ करने का आधार भी। इस तरह अपने अर्थ संसार के फैलाव की वजह से एक कृति ‘लेखक की मृत्यु’ की वजह तक हो सकती है। तथापि कृति का लेखकीय पाठ अनिवार्यत: कृति में मौजूद रहता है और विविध प्रकार से ‘बोलने’ का प्रयास भी करता है, इसलिर फ्रैंकफर्ट स्कूल के कुछ आलोचक लेखक के परिवेश और समय में जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि वे सब वहां किन जुबानों से बोलते हैं।
इस तरह पाठकीय पाठों की तरह लेखकीय पाठों के भी विविध-बहुल हो सकने की बात सामने आ गई। पर अंबर्तो ईको ने खुले पाठ को अपने निबंध ‘पाठक की भूमिका’ (द रोल आॅफ रीडर) में मुख्यत: पाठकवादी रूप में ही समझने की कोशिश की है। ईको ने कृतियों के बहुपाठीय स्वरूप को तीन कोटियों में विभाजित किया है- नैतिक, रूपकात्मक और रहस्यात्मक। ध्यान से देखा जाए तो तीनों कोटियां रचनाशीलता के परंपरागत पाठों की कोटियां ही हैं। मानव मस्तिष्क के भाषा के मार्फत रचनाशील होने की ये तीन बुनियादी पद्धतियां हैं। तथापि जिसे हम खुला पाठ कह सकते हैं, उसका रचनात्मक रूप भी तमाम कोटियों में बंधने से इनकार करने वाला होना चाहिए। पर उसके बजाये यहां खुले पाठ पर पाठकवादी नजरिए से ही विचार किया गया है। इसलिए जिसे रोलां बार्थ ‘लेखकीय पाठ’ कहते हैं, उसके खुलेपन की व्याख्या के लिए हमें अनेक भाषाओं की मौजूदगी वाले पहलू की ओर देखना पड़ेगा।
इस संदर्भ में स्त्री भाषा, जातीय भाषा, शिशु भाषा, प्राणी भाषा, अप्राणी भाषा आदि बहुत सी भाषाओं के तल पर रचनाशील होने वाला एक नया संसार खुल रहा है। इसे हम पाठकीय पाठों के तहत न रूपकात्मक कह सकते हैं, न रहस्यात्मक। नैतिक अर्थ वाली कोटि तो इसके लिए एकदम अनुपयुक्त ही है। तो हमें एक नई कोटि बनानी पड़ेगी। इसे हम ‘आत्मविस्तारक कोटि’ कह सकते हैं। ऐसी ही एक कोटि ‘आत्मन्वेषी कोटि’ भी हो सकती है। खुले पाठ की संभावनाओं का प्रकट होना अभी अपने शैशव काल में है। भविष्य के गर्भ में बहुत कुछ छिपा हो सकता है।
पाठकीय पाठों की अनेकता के पीछे पाठक की मनोदशाएं सामाजिक स्थिति, राजनीतिक विचारधारा, सांस्कृतिक चेतना आदि अनेकानेक कारण हो सकते हैं। इस आधार पर लेखकीय पाठ को भी अपनी रचनाशीलता की अभिव्यक्ति के लिए खुला छोड़ देने की आजादी की बात भी उठी है। ब्रेख्त के नाटक मंच से बाहर आकर दर्शकों से सीधा संवाद रचने के लिए खुले छोड़े गए। बेशक इससे नाटकों की परिणतियां तो नहीं बदलीं पर वहां तक पहुंचने के रास्ते अवश्य अनेकमुखी हो गए। कुछ धारावाहिक इस दिशा में आगे बढ़ते हैं और दर्शकों के साथ सहयोगी प्रयास की तरह लिखे जाने लगते हैं। वैसे बात उस हद तक न भी खुली हो तो भी यह तो होता ही है कि हर कृति का हर पाठ उसकी एक तरह की पुनर्रचना है। हमारे समय में पाठक की भूमिका का इस रूप में जो विस्तार हुआ है, उसने लेखन के स्वरूप को बदला है। उसके लिए परंपरागत विधाओं में बंधकर लिखने का जो राजमार्ग बनाया गया था, उस पर चलने से वह लेखन अब कहीं पहुंचता मालूम नहीं होता।