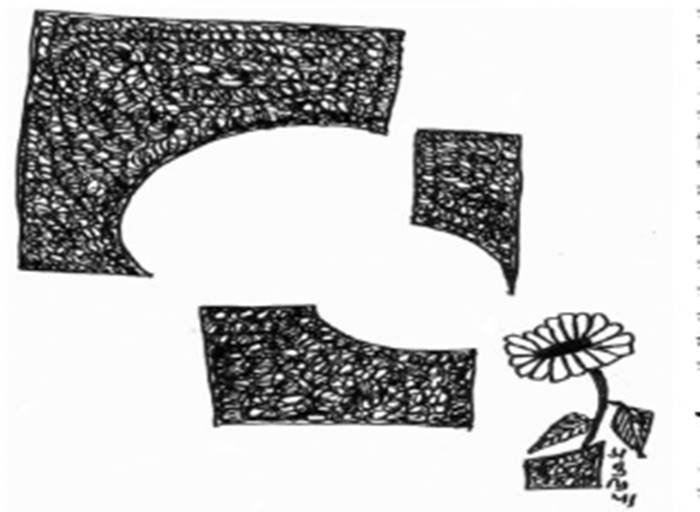दुनिया भर में चीजों की भौगोलिक पहचान आधारित पेटेंट के मसले बढ़ रहे हैं। इन्हें लेकर होने वाली मुकदमेबाजी किस स्तर तक पहुंच चुकी है, इसकी मिसाल यह है कि पेटेंट से जुड़े मुकदमों पर सिर्फ अमेरिका में 2011 में 29 अरब डॉलर खर्च हुए थे। इधर ऐसा ही एक मुकदमा पश्चिम बंगाल और ओडिशा के बीच चल रहा है। इसके केंद्र में एक बेहद मीठा रसदार व्यंजन रसगुल्ला है। यह रसगुल्ला है या रोसोगुल्ला, दोनों में से किसकी पहचान आखिरी और निर्णायक होगी- इसका फैसला अदालत को करना है। पिछली कई सदियों से देश के विभिन्न में प्रचलित और स्वीकृत मिठाई के रूप में रसगुल्ले की एक विशिष्ट पहचान है। अपने नाम से ही मुंह में स्वाद जगाने वाली मिठाई- रसगुल्ले की भौगोलिकता पर पहले तो कोई विशेष विवाद नहीं था, आम तौर पर लोग इसे बंगाल की एक मिठाई के तौर पर जानते-पहचानते रहे हैं। पर इधर कुछ वर्षों से ओडिशा ने इस पर अपना दावा ठोंक रखा है। असल में विवाद की एक शुरुआत 2010 में एक अंग्रेजी पत्रिका द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण से हुई, जिसमें रसगुल्ले को राष्ट्रीय मिठाई के रूप में पेश किया गया था।
इसे देखते हुए ओडिशा सरकार ने रसगुल्ले की भौगोलिक पहचान (जीआई- जियोग्राफिकल इंडिकेशेन टैग) खुद से जोड़ने का उपक्रम यह कहते हुए शुरू किया कि इस मिठाई का ताल्लुक उससे है। दरअसल, जीआई टैगिंग ही वह आधिकारिक तरीका है जो किसी वस्तु के उद्गम या खोज स्थल के बारे में बताती है। इसके तहत किसी वस्तु के नाम या चिह्न को उसके उत्पन्न होने की भौगोलिक स्थिति- जैसे शहर, क्षेत्र या गांव-कस्बे या देश के नाम से पहचानबद्ध किया जाता है। यह विभिन्न उत्पादों के प्रमाणीकरण में भी काम आता है और बताता है कि किसी उत्पाद का निर्माण किस पारंपरिक विधि से हुआ है और यह किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में ही उत्पन्न हुआ है। इस पहचान के आधार पर वस्तु के पेटेंट तय किए जाते हैं। तिरुपति के मंदिर में प्रसाद के रूप में दिए जाने वाले लड्डू को 2009 में ऐसी ही जीआई टैगिंग प्रदान की गई थी। दार्जिलिंग की चाय को भी यह भौगोलिक पहचान हासिल है जिससे दुनिया भर में उसे प्रतिष्ठा मिली हुई है।
फिलहाल मुद्दा यह है कि ओडिशा सरकार की ओर से किया जा रहा दावा है। इस दावे के मुताबिक ओडिशा सरकार का कहना है कि रसगुल्ले की उत्पत्ति इसी राज्य में हुई है। बताया जा रहा है कि जगन्नाथ मंदिर में आयोजित की जाने वाली वार्षिक रथयात्रा के दौरान भगवान के भोग के लिए रसगुल्ले को बनाया गया। ओडिशा के सांस्कृतिक इतिहासकार असित मोहंती का इस बारे में दावा है कि एक 300 साल पुरानी परंपरा के अनुसार रथयात्रा के समापन के समय भगवान जगन्नाथ मां लक्ष्मी को उपहारस्वरूप रसगुल्ला भेंट करते हैं। इन्हीं तथ्यों के मद्देनजर ओडिशा के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय ने ऐसे दस्तावेज जमा करने की पहल की है, जिनसे साबित हो सके कि पहला रसगुल्ला भुवनेश्वर और कटक के बीच (रथयात्रा के पथ में) अस्तित्व में आया था। ओडिशा ने रसगुल्ले को अपनी विशिष्ट पहचान और खोज साबित करने के उद्देश्य से पिछले साल यह मामला राज्य की विधानसभा में भी उठाया था। सत्तारूढ़ बीजू जनता दल(बीजद) के सदस्यों ने अगस्त, 2015 में यह मुद्दा उठाते हुए सरकार से राज्य की इस सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए कदम उठाने की मांग की थी।
ए क वरिष्ठ बीजद सदस्य और पूर्व मंत्री आरपी स्वैन ने कहा था कि पश्चिम बंगाल उनके राज्य की धरोहर झपटने का प्रयास कर रहा है, जबकि इसके दस्तावेजी सुबूत हैं कि रसगुल्ला भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा के दौरान चढ़ाया जाता रहा है। ऐसे में बंगाल सरकार कैसे यह दावा कर सकती है कि यह मिठाई उसकी खोज है। ओडिशा के दावे चाहे जो हों, पर बंगाल सरकार इन सभी दावों का तोड़ खोजती रही है। संदेह नहीं कि आज रथयात्रा के दौरान प्रसाद के रूप में रसगुल्ला दिया जाता है, लेकिन यह परंपरा अति प्राचीन है- इस दावे में ज्यादा दम नहीं लगता क्योंकि भगवान श्रीकृष्ण को लगाए जाने वाले छप्पन भोग में कहीं भी रसगुल्ले का उल्लेख नहीं मिलता है। एक अन्य इतिहासकार चित्रा बनर्जी के अनुसार, श्रीकृष्ण के संबंध में जितनी भी कथाएं प्रचलित हैं, उनमें दूध, दही, घी का उल्लेख तो है लेकिन छेने या छेने से बनने वाली मिठाई का नहीं। यहां तक कि मध्यकालीन भारत में भी छेने का कोई विवरण नहीं मिलता, जबकि चैतन्य महाप्रभु मिठाई के बहुत शौकीन थे। हालांकि मध्यकाल में बंगाल में खोए से बने संदेश का उल्लेख जरूर है।
बंगाल में कोलंबस आॅफ रोसोगुल्ला के रूप में विख्यात नोबिन चंद्रा के पड़पोते अनिमिख रॉय कहते हैं कि रसगुल्ला तो असल में उनके परदादा ने ही 1868 में बनाया था। चंद्रा ने इसे बनाने की विधि विदेशियों से सीखी थी। माना जाता है कि 18वीं सदी के दौरान बंगाल में मौजूद डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों ने छेने (छैने) से मिठाई बनाने की तरकीब ईजाद की और तभी से बंगाल में रोसोगुल्ला वजूद में आया और उसका प्रचलन बढ़ा। रसगुल्ले को अपना साबित करने के लिए बंगाल सरकार ने मिठाई की दुकानों की एक शृंखला केसी दास प्राइवेट लिमिटेड की मदद ली है। यह शृंखला नोबिन चंद्रा के वंशजों द्वारा संचालित की जा रही है। रसगुल्ले पर बंगाल का ही दावा सही है- इसे साबित करने के पक्ष में अनिमिख रॉय की दलील यह कि ओडिशा अपने रसगुल्ले को 300 से 700 साल पुराना साबित कर रहा है, जबकि असलियत यह है कि इस डिश की ईजाद आज से डेढ़ सौ साल पहले ही हुई थी। एक अन्य शोधकर्ता व लेखक हरिपद भौमिक ने अपनी किताब रसोगुल्ला के जरिए ऐसे कई दस्तावेज मुहैया कराए हैं जिनसे साबित होता है कि रसगुल्ला सबसे पहले बंगाल में ही बनाया गया था। इन्हीं तथ्यों के आधार बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक डॉजियर भी तैयार किया है जिसे केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के हवाले कर रसगुल्ले पर अपना हक जताया है।
सवाल यह है कि बंगाल का हो या ओडिशा का, रसगुल्ले पर हक की इस लड़ाई से आखिर क्या फर्क पड़ने वाला है? असल में यह मामला पेटेंट का है। दुनिया में अभी बौद्धिक और जैव विविधता संबंधी अधिकारों के बारे में पूरी तरह जागरूकता नहीं आई है, ऐसे में हमारा आम समाज और प्रमुख संगठन तक नहीं जानते कि भारतीय चीजों और बौद्धिक संपदाओं का विदेशों में खासकर यूरोपीय-अमेरिकी कंपनियों द्वारा पेटेंट करा लिए जाने पर भारतीय उत्पादों का यूरोपीय-अमेरिकी बाजारों में प्रवेश रुक सकता है। ऐसी स्थिति में इन वस्तुओं का व्यापार करने के लिए पेटेंटधारी कंपनी को हर साल रॉयल्टी देनी पड़ती है। इस अज्ञानता का लाभ चंद बहुराष्ट्रीय कंपनियां उठाने की कोशिश करती हैं। अतीत में नीम, हल्दी से लेकर कई चीजों का पेटेंट वापस पाने के लिए भारत सरकार को काफी मेहनत करनी पड़ी है। पिछले कुछ अरसे में यही स्थिति भारतीय खादी के संबंध में भी पैदा हुई थी। जर्मनी की एक कंपनी- खादी नेचरप्रोडक्टे यूरोपीय बाजारों में शैंपू, साबुन और तेलों आदि हर्बल उत्पादों को खादी प्रोडक्ट बताकर बेच रही थी, जबकि खादी आजादी के आंदोलन के समय से ही भारतीय ट्रेडमार्क है। जर्मनी की कंपनी खादी के उत्पाद बेचने में इसलिए सफल हुई क्योंकि भारतीय खादी को भौगोलिक संकेतक (जियोग्राफिकल इंडिकेशन- जीई) स्टेटस दिलाने का मामला फाइलों में ही उलझा हुआ था। अपनी चीजों पर समय रहते जीआई टैगिंग हासिल न करना कितना महंगा और नुकसानदेह हो सकता है, अतीत में यह नीम, हल्दी, बासमती चावल जैसी चीजों की भारतीयता के मामले में कई बार साबित हुआ है।
नब्बे के दशक में अमेरिका की एक कंपनी ने हल्दी पर अपना दावा ठोंक दिया था। इसे बचाने में भारत को पांच साल लग गए और अमेरिकी वकीलों को फीस के रूप में करीब 12 लाख डॉलर का भुगतान करना पड़ा था। इसी तरह 1995 में अमेरिका की ही एक अन्य फर्म ने भारत की नीम पर अपना दावा जता दिया था। भारत को इसके अमेरिकी पेटेंट को रद्द कराने में दस साल लग गए। इस पूरी मशक्कत पर दस लाख अमेरिकी डॉलर खर्च हो गए थे। इसी तरह का एक विवाद 1997 में भारतीय चावल की एक अहम किस्म- बासमती का उठा था। टेक्सास स्थित अमेरिकी कंपनी- राइसटेक सितंबर, 1997 में बासमती चावल के उत्पादन और विक्रय का बौद्धिक अधिकार प्रदान किया गया था। राइसटेक को बासमती चावल पर पेटेंट दिए जाने की घटना को बायोपाइरेसी का उत्कृष्ट उदाहरण बताया गया था। यह पेटेंट दिए जाने के बाद भारत ने अपनी आपत्ति जताई थी। भारत ने वे तथ्य मुहैया कराए, जिनसे पता चलता था कि भारत में तकरीबन दस लाख हेक्टेअर और पाकिस्तान में 7.5 लाख हेक्टेअर क्षेत्रफल में बासमती चावल की खेती होती है। यह भी साबित किया कि भारत और पाकिस्तान में विशाल भूभाग पर वहां के किसान सदियों से बासमती चावल की उम्दा किस्म की पैदावार करते रहे हैं, इसलिए अमेरिकी कंपनी को दिया गया पेटेंट रद्द किया जाए। इतिहास साक्षी है कि भारत ने पेटेंट की यह जंग जीती थी, लेकिन अभी भी कई अन्य भारतीय चीजों के मामले में यह संकट खड़ा हो सकता है।
खादी हो या रसगुल्ला, उनके भौगोलिक संकेतक स्पष्ट करने का महत्त्व इससे समझा जा सकता है कि जिस तरह स्कॉच ह्विस्की एक निश्चित भौगोलिक पहचान है, उसी तरह रसगुल्ले और खादी को भी उसकी निश्चित पहचान दिलानी जरूरी है। साफ है कि यह मामला रसगुल्ले पर दो राज्यों की भिड़ंत मात्र का नहीं, बल्कि एक भारतीय उत्पाद की वैश्विक पहचान और पेटेंट सुरक्षित रखने का है, जिसके बारे में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। १
सवाल यह है कि बंगाल का हो या ओडिशा का, रसगुल्ले पर हक की इस लड़ाई से आखिर क्या फर्क पड़ने वाला है? असल में यह मामला पेटेंट का है। दुनिया में अभी बौद्धिक और जैव विविधता संबंधी अधिकारों के बारे में पूरी तरह जागरूकता नहीं आई है, ऐसे में हमारा आम समाज और प्रमुख संगठन तक नहीं जानते कि भारतीय चीजों और बौद्धिक संपदाओं का विदेशों में खासकर यूरोपीय-अमेरिकी कंपनियों द्वारा पेटेंट करा लिए जाने पर भारतीय उत्पादों का यूरोपीय-अमेरिकी बाजारों में प्रवेश रुक सकता है।