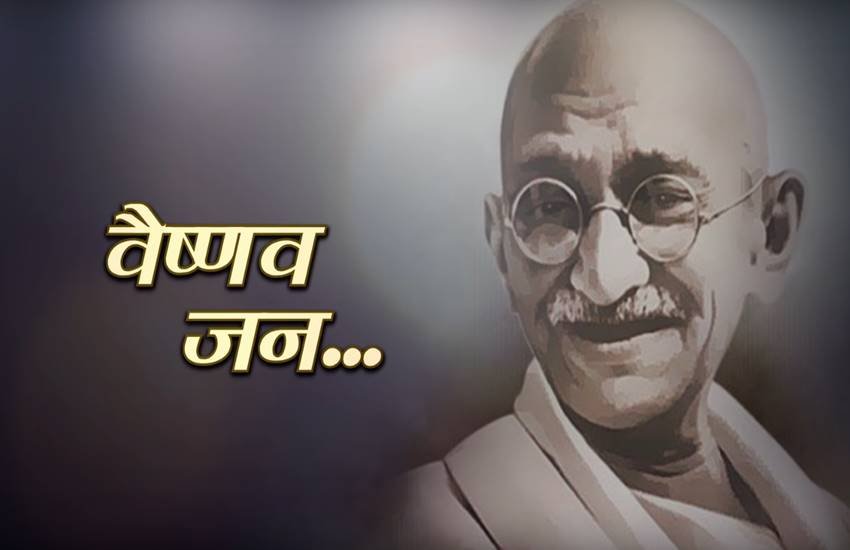विमर्श- राजीव रंजन गिरि
कहना न होगा कि नरसी मेहता ने वैष्णवता की पूरी नई परिभाषा दी है। इसके मुताबिक वैष्णव होने के लिए वैष्णव परिवार में जन्म होना न तो आवश्यक है और न ही काफी; इसके लिए जरूरी है, भजन में व्यक्त मान्यताओं को पूरा करना। गांधीजी इस भजन को अपना प्रिय मानकर और प्रार्थना सभा में इसका गायन कराकर, इसकी मान्यताओं को स्वीकृति प्रदान कर रहे थे।
गांधीजी के सबसे प्रिय भजनों में से है- वैष्णव जन तो तेने कहिए। इसके रचयिता हैं गुजराती के भक्त कवि नरसी मेहता। नरसी का नाम गुजराती की भक्तिकाव्यधारा के पुरोधा संत कवि के तौर पर लिया जाता है। इनकी भक्ति का केंद्रीय तत्व वैष्णव भाव है। इनकी मुख्य रचनाएं हैं- हार-माला, चातुरी षोडसी, चातुरी छत्तीसी, सामल दास नो विवाह, दान-लीला, गोविंद गमन, सुरत-संग्राम। इतिहास के जिस दौर में नरसी अपने शब्द-कर्म में सक्रिय थे, पूरे देश में अपनी-अपनी ‘भाखा’ में, संत-भक्तअपनी वाणी को अभिव्यक्तिदे रहे थे। यह संस्कृत के बरअक्स मातृभाषाओं के उत्थान का दौर था। भक्ति इसके केंद्र में थी। सभी संत-भक्त इस काल में अपने-अपने मुताबिक भक्ति को परिभाषित कर गति और नया आकार दे रहे थे।
महात्मा गांधी को नरसी मेहता का यह भजन क्यों इतना प्रिय था कि वे अपनी प्रार्थना में इसे नियमित शामिल करते थे। दरअसल, किसी भी पसंदगी-नापसंदगी की कुछ वजहें होती हैं। सांस्कृतिक अभिप्राय होते हैं। और गांधीजी के मामले में यह दिखता ही है कि उनके हर राजनीतिक-सांस्कृतिक कदम के पीछे व्यापक आशय निहित रहते थे। गांधीजी की पसंदगी का कारण इस भजन में ही अनुस्यूत है। यह भजन वैष्णव होने की परिभाषा गढ़ता है। वैष्णव किसे कहा जाएगा, बताता है। एक वैष्णव का आचरण कैसा होना चाहिए, स्पष्ट करता है।
नरसी मेहता के इस भजन के मुताबिक एक वैष्णव उसी व्यक्ति को कहा जा सकता है, जो दूसरों की पीड़ा को समझे।
दूसरों की पीड़ा को जानना-समझना पहली कसौटी है, वैष्णव होने के लिए। लेकिन उसे पीड़ा जानने तक ही सीमित नहीं रहना है। दूसरों की तकलीफ जानने के बाद उसे दूर करने की कोशिश करनी है। दूसरों का दुख समझ, उस पर उपकार करना है। उस पीड़ा को खत्म करने का प्रयास करना है। साथ ही, ध्यान रहे इस उपकार को करने से मन में किसी तरह का अभिमान न आए। किसी के प्रति उपकार कर मन में अभिमान न आए, वैष्णव होने के लिए यह भी उपकार करने जितना ही जरूरी है। ऐसा अमूमन दिखता है कि लोग किसी की सहायता करते हैं और इसका ढोल भी खूब बजाते हैं। ढोल बजाना तो आगे की बात है, इस भजन में तो यहां तक कहा गया है कि मन में भी लेश मात्र अभिमान न हो। ऐसा नहीं कि भले ही अन्य लोगों को उपकार के बारे में न बताया जा रहा हो, पर मन-ही-मन इस अभिमान से प्रमुदित रहा जाए।
मन में अभिमान का लेश मात्र नहीं होना, वैष्णवता की शर्त है। ख्यात साहित्यकार विष्णु प्रभाकर ने एक प्रसंग का जिक्र किया है। गांधीजी के एक साथी थे परचुरे शास्त्री। उन्हें कोढ़ था। एक दिन बिना सूचना दिए वे आश्रम में पहुंच गए। उस रात गांधीजी की चिंता का पार नहीं था। सोचने लगे- शास्त्री जी कोढ़ी हैं, और आश्रम में दूसरे लोग भी रहते हैं। उनके स्वास्थ्य का भार भी तो मुझ पर है; लेकिन यह जो व्यक्ति मेरे द्वार पर आया है, ऐसा लगता है, जैसे स्वयं प्रभु ही मेरे द्वार आए हों… नहीं-नहीं, वह यहीं रहेंगे। वह वापस नहीं जाएंगे।
और परचुरे शास्त्री फिर वापस नहीं गए। गांधीजी स्वयं प्रतिदिन उनके घावों को साफ करते और शरीर की मालिश करते। उनके लिए यह सत्य का एक और प्रयोग था। गंभीर-से-गंभीर क्षणों में भी वह उन्हें भूलते नहीं थे। एक बार वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण बैठक हो रही थी। वे बीच में उठे, बोले, ‘मुझे बहुत जरूरी काम से सेवाग्राम जाना है।’ पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले, ‘क्या वह काम स्वराज्य से भी बढ़कर है।’
गांधीजी बोले, ‘हां, मेरे लिए परचुरे शास्त्री की सेवा स्वराज्य से भी बढ़कर है।’ और वे चले गए।
स्वराज्य पाने के महाआख्यान में, बड़े स्वप्न में भी गांधी को याद रहता था, एक कुष्ठ रोगी की सेवा-सरीखा जरूरी काम।
नरसी मेहता भजन में कहते हैं कि वैष्णव वह है जो विनम्र हो, सबका आदर करता हो और दूसरों की निंदा नहीं करता हो। वैसा शख्स वैष्णव कहलाने का अधिकारी है, जो मन, वचन और कर्म से निश्छल हो।
गौरतलब है कि निंदा और आलोचना में फर्क होता है। आलोचना बेहतर की उम्मीद में की जाती है। जबकि निंदा मन की मलिनता का नतीजा होती है। निंदा में ईर्ष्या और वैमनस्यता का पुट होता है। शब्द के सच्चे मायने में वैष्णव होने के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति मन, वचन और कर्म – तीनों से निश्छल हो। कई दफे यह दिखता है कि निश्छलतापूर्वक कर्म करने वाले भी कठोर वचन बोलते हैं। संयमित वाणी का अभाव होता है। यह भी संभव है कि कर्म और वचन वाले का मन निश्छल नहीं हो, दुर्भावनायुक्त हो। गांधी के इस प्रिय भजन के मुताबिक मनसा-वाचा-कर्मणा निश्छल, प्रपंचरहित व्यक्ति ही वैष्णव होने की पात्रता रखता है। मनसा-वाचा-कर्मणा में कठिनाई के लिहाज से अनुक्रम बनाएं तो बनेगा-कर्मणा, वाचा और मनसा। ये तीनों स्तर कसौटी है, वैष्णव की परख के लिए।
वैष्णव वह है जो सबको एक नजर से देखता हो। इंसान-इंसान में फर्क नहीं करता हो। लिंग, जाति, वर्ण, रंग, क्षेत्र, भाषा किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति को हेय नहीं समझता हो। जिसके अंदर तृष्णा नहीं हो। जो पर-स्त्री को मां के समान समझता हो। जिसकी जुबान कभी झूठ न बोलती हो। जो दूसरों के धन को हाथ न लगाता हो। कष्ट सहकर भी जिसमें सच बोलने का साहस हो। दूसरे की संपत्ति को देखकर जिसके मन में लालच पैदा नहीं हो। जिसके मन में दृढ़ वैराग्य का भाव हो; जिसे मोह-माया अपने जाल में फांस न सके। जिसका मन राम में लग गया हो। ऐसे व्यक्ति को भटकना नहीं पड़ता; कारण कि सब उनके हृदय में ही होता है। ऐसा व्यक्ति जो लोभ, कपट, काम और क्रोध से रहित हो। बकौल नरसी मेहता, ऐसे व्यक्ति के दर्शन से कुल भी तर जाता है।
कहना न होगा कि नरसी मेहता ने वैष्णवता की पूरी नई परिभाषा दी है। इसके मुताबिक वैष्णव होने के लिए वैष्णव परिवार में जन्म होना न तो आवश्यक है और न ही काफी; इसके लिए जरूरी है, भजन में व्यक्त मान्यताओं को पूरा करना। गांधीजी इस भजन को अपना प्रिय मानकर और प्रार्थना सभा में इसका गायन कराकर, इसकी मान्यताओं को स्वीकृति प्रदान कर रहे थे। इससे गांधी के दौर की वैष्णवता को एक नया अर्थ मिल रहा था। यह वैष्णवता स्वाधीनता आंदोलन के दौर में गांधी के राजनीतिक-सांस्कृतिक निहितार्थ को स्पष्ट कर रहा था और पूर्ति भी।
इतिहास के विकास क्रम में वैष्णव समुदाय भी कट्टरता, छुआछूत, ऊंच-नीच सरीखी गलत मान्यताओं को मानने लगा था। नरसी मेहता का यह भजन इन सब कुरीतियों को इनकार कर वैष्णव होने के लिए मानवीय शर्त प्रस्तावित करता है। जिनके आचरण में ये सारी बातें हों, वही वैष्णव जन हैं। स्वाधीनता आंदोलनके दौर में नरसी मेहता द्वारा पेश वैष्णवता की परिभाषा को मान्यता देना काबिलेगौर है। इसमें चरित्रगत पवित्रता और अहिंसा को स्वीकार किया गया है।
महात्मा गांधी नरसी मेहता के भजन में मौजूद परिभाषा को जी रहे थे। वे शब्द के सच्चे मायने में ‘वैष्णव जन’ थे। जिक्र करने लायक बात यह भी है कि गांधीजी अपने चिंतन-दर्शन के जरिए मौजूद सभ्यता का जो विकल्प प्रस्तावित कर रहे थे, इस भजन में उसी की बुनियाद है। सच्चाई और अहिंसा गांधीजी के जीवन का केंद्रीय बिंदु हैं। आजादी की लड़ाई में वे इसे पूरे तौर पर लागू कराना चाहते थे। नरसी मेहता का भजन भी इसी की याद दिलाता था।
काबिलेगौर बात यह भी है कि गांधीजी अपनी राजनीतिक बातों को भी धार्मिक मुहावरे व शब्दावली में जाहिर करते थे। उनके लिए धर्म सही अर्थों में ‘दीर्घकालीन राजनीति’ था और राजनीति ‘अल्पकालीन धर्म’। असल में गांधीजी धर्म का प्रयोग जिन अर्थों में करते थे, उसका आशय न तो ‘रिलीजन’ है और न ही ‘मजहब’। गांधीजी से पहले भारतीय ज्ञान परंपरा में भी ‘धर्म’ शब्द का अभिप्राय मजहब या रिलीजन के अर्थ में नहीं था। यहां धर्म था-प्रकृति के अर्थ में। स्वभाव के अर्थ में। धर्म का मतलब था- कर्तव्य एवं दायित्व-बोध। गांधीजी के मुताबिक किसी के लिए भी वैष्णव होने का यही धर्म है। वे स्वाधीनता आंदोलन में भी अपने इसी धर्म का पालन कर रहे थे। नरसी मेहता का भजन प्रार्थना सभा में गायन कराकर लोगों की चेतना को इस दिशा में बदलने की कोशिश कर रहे थे।