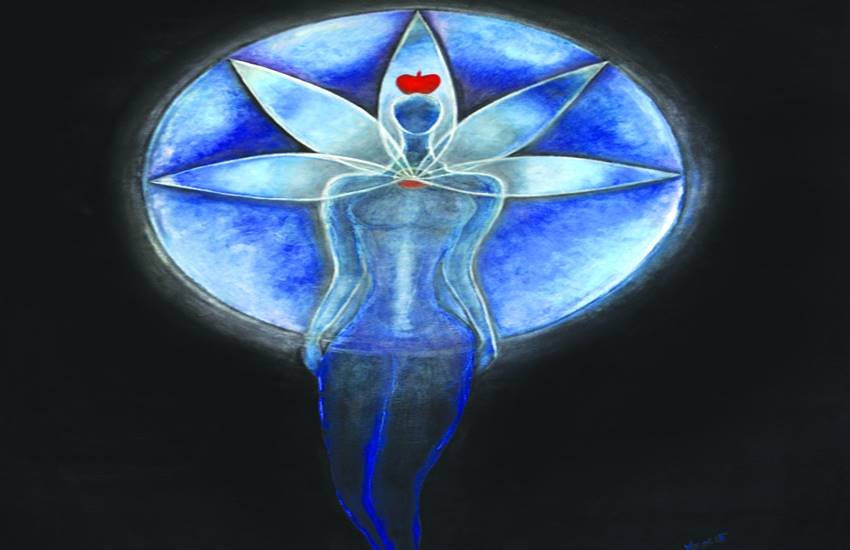दलित-विमर्श, स्त्री-विमर्श, आदिवासी विमर्श, थर्ड जेंडर या किन्नर विमर्श जैसे अस्मितावादी विमर्शों ने साहित्य-जगत में ऐसा परिदृश्य उपस्थित कर दिया है, जिसके पीछे स्वानुभूति या भोगे हुए यथार्थ, जीवनानुभवों का प्रबल तर्क है। इस तर्क के अनुसार साहित्य सामान्य मनुष्य का न होकर दलित द्वारा दलित के लिए, स्त्री द्वारा स्त्री के लिए, आदिवासी द्वारा आदिवासी के लिए होगा। चंूकि पुरुष या सामान्य मनुष्य या मनुष्येतर प्राणी को लेकर कोई विमर्श है ही नहीं, इसलिए साहित्य-संसार में इनके लिए कोई स्थान होगा ही नहीं। जाहिर है, इस धारणा को स्वीकार कर लेने से अब तक का लिखा साहित्य, जो लिंग, जाति, धर्म, वर्ग विशेष से परे समस्त मनुष्य-जाति की धरोहर रहता आया था, इतिहास के कूड़ेदान में चला जाएगा। यह स्थिति इन विमर्शवादियों को जितनी प्रीतिकर प्रतीत हो, पर मेरे जैसे व्यक्ति के लिए यह साहित्य के स्वधर्म के साथ-साथ मनुष्यता के अवसान का संकेत देती प्रतीत होती है।
देखा जाए, तो ये सभी अस्मितामूलक विमर्शवादी साहित्य की बात करते हुए भी साहित्य की मूल प्रवृत्ति या ‘साहित्य के स्वधर्म’ से अनभिज्ञ हैं। काव्य या साहित्य जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ‘कविता क्या है’ नामक निबंध में कहा है, ‘‘शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंधों की रक्षा और निर्वाह का साधन है। वह मनुष्य के अंदर मनुष्यता का निर्माण करता है।’’ यानी साहित्य न केवल मनुष्य जगत, बल्कि मनुष्येतर के साथ भी प्रेम, सौहार्द, संशक्ति और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का संबंध स्थापित करते हुए मनुष्य को अन्य के साथ समरसता-सूत्र से संबद्ध करता है। दूसरे शब्दों में, साहित्य सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों से आगे बढ़ कर मनुष्य के अंदर संवेदनात्मक सत्याग्रह को उद्बुद्ध करता है। साहित्य की यह भूमिका ही उसे इतिहास, राजनीति, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र जैसे ज्ञानानुशासनों से स्वतंत्र और स्वायत्त पहचान प्रदान करती है। समाजशास्त्र केवल सामाजिक संस्थाओं और मानवीय संबंधों के विकास, राज्य संबंधी गतिविधियों, अतीत की घटनाओं के पुनर्लेखन, अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के विवेचन से सम्बद्ध रहे हैं, जबकि साहित्य में समस्त संसार का समावेश होता रहा है- मानव समाज के साथ-साथ वह पशु-पक्षी, पेड़-पहाड़, जंगल-रेगिस्तान, धरती-आकाश, नदी-समुद्र आदि को भी वह अपने दामन में समेटे हुए है। तभी तो हमारे आदि कवि का आदि श्लोक व्याध के वाण से विद्ध क्रौंच पक्षी के क्रंदन से उपजे शोक की अभिव्यक्ति बन कर उमड़ पड़ा- ‘मा निशाद प्रतिष्ठाम्, त्वमगम शाश्वती समा:’ और हमारे ऋषि-मुनि यह कह गए- ‘समुद्रवसने देवि पर्वतस्तन मंडले, विष्णुपत्नी नमस्यतुभ्यम् पादस्पर्श क्षमस्व मे।’
दरअसल, साहित्य के विराट संसार में मनुष्य-मनुष्येतर, स्त्री-पुरुष, ऊंच-नीच, अमीर-गरीब, राजा-प्रजा, सवर्ण-अवर्ण, गोरा-काला, धर्म-संप्रदाय आदि के आधारों पर कभी कोई विभेद नहीं रहा, न ही इनके आधार पर कभी किसी का विशेष महत्त्व रहा। इन दिनों दलित चेतना और इतिहास की सबाल्टर्न अवधारणा के प्रभाव में तमाम क्लासिक कृतियों को अभिजात वर्ग- राजा-रानी की गाथा मान कर खारिज करने का चलन बढ़ता जा रहा है। रामायण, महाभारत जैसी प्राचीन काव्य कृतियां भी इस चपेट से अछूती नहीं रह गई हैं। पर इस सत्य को हमें ओझल नहीं होने देना चाहिए कि साहित्यिक कृतियों में कोई भी चरित्र इसलिए महत्त्वपूर्ण नहीं हो जाता कि वह राजा है या रानी, राजकुमार है या राजकुमारी या फिर वह बड़े पद वाला है या बहुत पैसे वाला।
काव्य जगत से लेकर लोकजीवन तक राम और कृष्ण की फैली हुई लोकप्रियता, जनप्रियता का कारण उनका राजा या ईश्वर होना नहीं, बल्कि उनके द्वारा सामान्य मनुष्यता के धरातल पर पुत्र, भाई, पति, मित्र आदि विविध रूपों में मानवीय व्यवहारों का निर्वाह किया जाना है। यही कारण है कि भारत के जन-जन की जुबान पर जितनी राम, कृष्ण और शिव की गाथाएं चढ़ी हुई हैं, उनकी तुलना में सम्राट अशोक से लेकर अकबर तक के ऐतिहासिक वृत्तांतों का दसवां हिस्सा भी नहीं है। कालिदास का ‘अभिज्ञान शांकुतलम्’ इसलिए महत्त्वपूर्ण नहीं है कि वह एक राजा की प्रेम-कहानी है, बल्कि इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि, जैसा जर्मन कवि गेटे ने कहा है, ‘अगर कोई तरुणाई का फूल और प्रौढ़ावस्था का फल, स्वर्ग और मर्त्य दोनों को एक साथ देखना चाहे तो उसे ‘शकुंतला’ में यह चीज मिलेगी।’ और रवींद्रनाथ ठाकुर के अनुसार तो ‘शकुंतला’ पौराडाइज लॉस्ट भी है और पैराडाइज रीगेंड’ भी है।
इतिहास की घटनाओं, तथ्यों का महत्त्व, जैसा कि अरस्तू ने भी कहा है- देश और काल विशेष तक सीमित होता है, पर वही साहित्य का सत्य बन कर सार्वकालिक और सार्वदेशिक हो जाता है। इतिहास बेशुमार राजाओं के वृतांतों से भरा पड़ा है, पर इतिहासविदों के सिवा उन्हें कौन जानता है। रोमन साम्राज्य के संस्थापक जुलियस सीजर की तुलना में अधिक जाना जाता है वह सीजर, जिसे शेक्सपियर अपने ‘जुलियस सीजर’ नामक ट्रैजेडी में गढ़ गए। यह रोमन योद्धा जिस तरह अपने मित्रों के विश्वासघात के कारण मारा जाता है, उससे वह पाठकों की सहानुभूति का पात्र बनता है और उसका यह कथन ‘यू टू ब्रूटस’ हरेक इंसान की जुबान पर विश्वासघाती दोस्त के लिए आप्तवाक्य बन जाता है। ‘ओथेलो’ में डेस्डीमोना यद्यपि रानी है, लेकिन बेवफाई के संदेह में उसका पति ओथेलो जिस तरह उसका गला दबा कर उसकी हत्या करता है, उसे पढ़ते हुए पाठक को लगता है कि उसका गला दबाया जा रहा है।
इन दृष्टांतों से स्वत: सिद्ध है कि साहित्य सदैव स्थान, समय और मनुष्य द्वारा स्थापित सीमाओं और विभेदों का अतिक्रमण करते हुए हमें सच्चा इंसान बनने, दबे-कुचले, पीड़ित जनों के साथ सहानुभूति और प्रेम का रिश्ता बनाने की प्रेरणा देता रहा है। इस लिहाज से दलित या स्त्री विमर्श वाले लेखन भी दलितों या स्त्रियों के प्रति हमारी संवेदना को जरूर जागृत करते हैं, लेकिन जब वे साहित्य की दलित या स्त्री संवेदना तक हदबंदी करने लगते हैं, तब वह हमारे लिए स्वीकार्य नहीं हो पाता। ऐसे विमर्श साहित्य को खंड-खंड में बांट कर उसकी समग्रता को छिन्न-भिन्न करने वाले हैं। स्त्री-विमर्श तो ज्यादा ही खतरनाक मोड़ लेता जा रहा है।
जहां तक दलित विमर्श का सवाल है, वह भले समग्रता, सामान्यता का परित्याग कर एक समुदाय विशेष तक केंद्रित हो गया हो, लेकिन उसका सकारात्मक मानवीय पक्ष यह है कि अपने दायरे में ही सही, वह कम-से-कम दबे, कुचले, उत्पीड़ित जनों के दुख-दर्द को तो सशक्त स्वर दे रहा है। इसके विपरीत अब स्त्री विमर्शवादियों को न स्त्री-जाति के दुख-दर्द से मतलब रह गया है, न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रताओं, समानताओं की चिंता रह गई। उनका सारा उत्साह यौन-स्वच्छंदता का परचम लहराने में प्रकट होने लगा है। इनके अनुसार अब तक का समस्त साहित्य पुरुषों द्वारा लिखे जाने के कारण पुरुषवादी, मर्दवादी है, जिसने पत्नीत्व और मातृत्व के तटबंधों के बीच स्त्री-जाति का शोषण-दोहन किया है। इसलिए ये पत्नीत्व और मातृत्व को स्त्री-शोषण का कारण मान कर ऐसा साहित्य रच रहे हैं, जो उनकी देह-मुक्ति की गौरव-गाथा बन सके। यौन-मुक्ति के इस महायज्ञ में तमाम पारिवारिक, सामाजिक रिश्तों का समिधा सदृश्य उत्सर्ग किया जाने लगा है। यह सब बढ़ती हुई बाजारवादी अपसंस्कृति का परिणाम है, जिससे साहित्य को बचा कर उसे मनुष्यता के उत्कर्ष की दिशा में लगाए रहना सभी रचनाकारों और संस्कृतिकर्मियों का दायित्व है, क्योंकि साहित्य वही टिकेगा, जो बाजार को नहीं मनुष्यता को बढ़ाने में सहायक होगा।
उल्लेखनीय है कि जायसीकृत ‘पद्मावत’ में सिंहलद्वीप के अंतरराष्ट्रीय बाजार में सबसे कम दाम पर बिकने वाला हीरामन तोता चित्तौड़गढ़ में आकर वहां के राजा रत्नसेन और सिंहलद्वीप की राजकुमारी पद््मावती के रूप में दो आत्माओं का मिलन-सेतु बन कर गुरु का पद प्राप्त करता और पाठक के दिलोदिमाग में चिरस्थायी पात्र के रूप में बस जाता है। लेकिन उसी बाजार में लाखों-करोड़ों के मोल में बिकनेवाले हीरे-जवाहरात को कोई याद नहीं रखता। ठीक इसी तरह आज भी बाजारवाद, उपभोक्तावाद तथा नाना अस्मितावादी विमर्शों की चकाचौंध के बावजूद वही साहित्य टिका रहेगा, जो दो आत्माओं के, मनुष्य-मनुष्येतर के बीच मिलन का सेतु बनेगा तथा विश्वव्यापी रागात्मकता का क्षरण करने वाली मुनाफा संकुल बाजारवादी अपसंस्कृति के विरुद्ध मनुष्यता का पथ-प्रदर्शन करता रहेगा। दरअसल, स्व के विवर से निकल कर अधिक से अधिक जड़-चेतन के साथ एकात्म होने, रागात्मकता सवंर्द्धित करने की चेतना और प्रेरणा पैदा करने में ही साहित्य की सार्थकता रही है और रहेगी। इससे स्खलित होकर वह जो कुछ बन जाए, साहित्य का दर्जा हरगिज नहीं हासिल कर सकता।