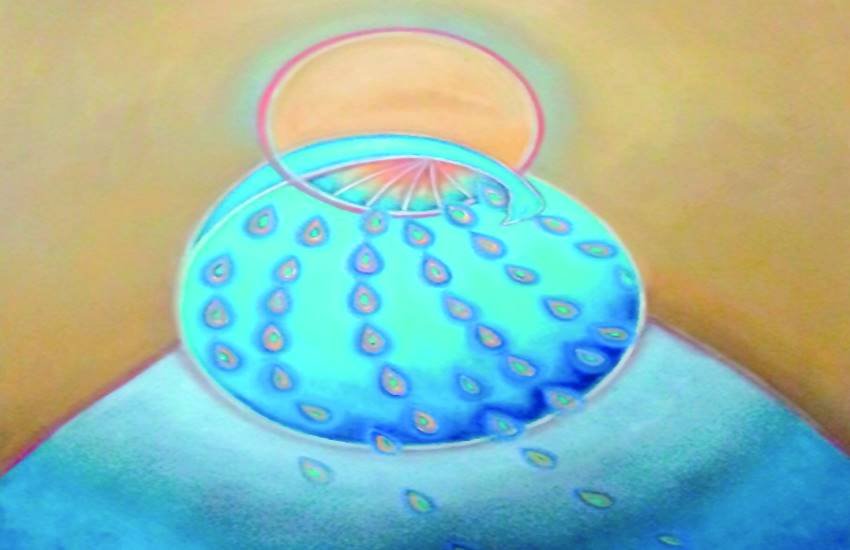अतुल कनक
हिंदी में एक देशज शब्द है- भिनसारा। इस शब्द का प्रयोग सुबह के संदर्भ में होता है। ढाई-तीन दशक पहले तक यह शब्द खूब प्रयोग में लिया जाता था। लेकिन नई पीढ़ी इस शब्द से अपरिचित सी हो गई है। भिनसारा ऐसा अकेला शब्द नहीं है, जो समय के साथ बदली हुई सामान्य प्राथमिकताओं के कारण आमजीवन से गुम होने लगा है। ऐसे अनेक देशज शब्द हैं जो देखते ही देखते बोलचाल की भाषा के राजपथ पर उपेक्षित से हो गये हैं। इसके विपरीत ऐसे अनेक देशज शब्द भी हैं जो देखते ही देखते हमारी रोजमर्रा की बातचीत में शामिल हो गये हैं। खासकर युवा पीढ़ी की भाषा तो कतिपय मुहावरों के स्तर पर पूरी तरह बदली हुई प्रतीत होती है।
आज से करीब दो दशक पहले तक भी कोई व्यक्ति यदि अपने संवाद में ‘जिंदगी झंड कर दी’ वाक्यांश का प्रयोग करता तो लोग उसकी तरफ अचरज भरी निगाहों से देखते। लेकिन अब ऐसे अनेक वाक्यांश परस्पर बातचीत में धड़ल्ले से काम लिए जा रहे हैं। परस्पर बातचीत में ‘फट्टू’ जैसा संबोधन पिछले दौर में किसी को भी अप्रिय हो सकता था, लेकिन नई पीढ़ी के लिए यह एक सहज संबोधन है। किसी वाक्य की प्रतिक्रिया में ‘घंटा’ कहना पिछली पीढ़ी के लिए अश्लील था, पर इस दौर के युवा ऐसा नहीं मानते। ‘तेरी तो फट रही है’ और ‘अंगुली करना’ जैसे वाक्य भी रोजमर्रा की बोलचाल में शामिल हो गई ऐसी ही प्रतिक्रियाएं हैं, जिनका प्रयोग युवा पीढ़ी बिना निहीतार्थ जाने खूब कर रही है। जो लोग अभिव्यक्ति के स्तर पर भाषाई शुचिता के पैरोकार हैं, उनके लिए तो हिंदी का हिंग्लिश हो जाना भी कम परेशानी का सबब नहीं है। भाषा के नाम पर अंग्रेजी और हिंदी की ऐसी खिचड़ी कुछ अखबार तक परोसने लगे हैं। खबरों के शीषर्कों में टीचरों, स्टूडेंटों, क्रिमिनलों जैसे शब्दों को देखकर अब संजीदा पाठक यह भी तय नहीं कर पाते कि वे इस खिचड़ी का आनंद लें या इसके कसैलेपन को देखकर अपना सिर पीटें।
दरअसल, भाषा केवल अभिव्यक्ति का ही माध्यम नहीं होती। वह हमारे सामाजिक सरोकारों और जीवन संस्कारों का भी प्रतिबिंब होती है। यही कारण है कि किसी समाज के सामाजिक- सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए उस समाज की भाषा का भी अध्ययन किया जाता है। भाषा एक नदी की तरह होती है। समय के प्रवाह में गतिमान रहते हुए उसमें नए-नए शब्द समाहित होते रहते हैं। नए शब्दों को आत्मसात करने की यह प्रवृत्ति किसी भी भाषा के जीवन के निर्धारण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहा भी जाता है कि बाढ़ के दिनों में जो नदी मजबूत पेड़ों को अपने साथ बहाकर ले जाती है, वह बांस को आसानी से नहीं डिगा पाती क्योंकि बांस अपनी लोचशीलता के कारण नदी के वेग को सहज ही मनमानी नहीं करने देता। स्वभाव की विनम्रता विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में बहुत मदद करती है। भाषा के संदर्भ में उसकी लोचशीलता को ही विनम्रता समझा जा सकता है। अंगे्रजी यदि दुनिया भर में सहज स्वीकार्य है तो उसका एक कारण यह भी है कि अंग्रेजी के मानक शब्दकोषों में दुनिया भर के लोकप्रिय शब्दों को शामिल किया जाता है। यही लोचशीलता हिंदी की भी ताकत है। आज अंग्रेजी, फारसी, अरबी, तुकर् ी और पुर्तगाली तक के शब्द हिंदी की समृद्धि के कारक बने हुए हैं। उर्दू तो खैर भारतीय भाषा परिवार का ही एक अंग है। हिंदी को उससे किसी भी तरह का परहेज कैसे हो सकता है?
लेकिन बदलती हुई जीवन शैली बहुत सारे तत्त्वों को शनै: शनै: प्रचलन से बाहर कर देती है और फिर उनसे जुड़े हुए शब्द भी अप्रासंगिक होकर प्रचलन से बाहर हो जाते हैं। जैसे मोबाइल फोन की लोकप्रियता ने ‘ट्रंक कॉल’ को जीवन से बाहर किया और अब किशोरों को यह समझाना पड़ता है कि ‘ट्रंक कॉल’ क्या होता है। ऐसे में क्या हम भविष्य की पीढ़ियों से यह उम्मीद कर सकेंगे कि वो ‘ट्रंक कॉल’ शब्द युग्म का उपयोग कर सकें? नवीनता के पक्षधरों का एक तर्क यह हो सकता है कि जो शब्द या जो वस्तु जीवन के लिए अप्रासंगिक ही हो गए हों, उन्हें याद रखने का औचित्य भी क्या है? लेकिन भाषा के अस्तित्व की यही तो खूबसूरती है कि वह अप्रासंगिक प्रतीत होते शब्दों को भी इतने सौंदर्य के साथ अभिव्यक्ति की सामर्थ्य सौंपती है कि सुनने वाला सम्मोहन से भर उठता है। मसलन- कौड़ियां अब वस्तु विनिमय या व्यापार का साधन नहीं रहीं लेकिन आज भी जो मारक क्षमता किसी को ‘दो कौड़ी का आदमी’ कहने में है, वह घटिया आदमी या बेकार आदमी कह देने में नहीं महसूस की जा सकती।
लेकिन भाषा का सौंदर्य किसी को दो कौड़ी का साबित करने में नहीं है। भाषा जीवन की संभावनाओं को संवारती है और संभावनाएं सदैव सौंदर्य की संवाहक होती हैं। यह तो मनुष्य का पूर्वाग्रह या दुराग्रह होता है जो सौंदर्य के प्रतिमानों को भी विकृत रूप देता है। भाषा के संस्कारों को विकृत करने वाले कारकों में एक प्रवृत्ति मुखलाघव भी होती है। मुख लाघव अर्थात अपनी सुविधा के अनुसार वास्तविक उच्चारण को परिवर्तित कर देना। राजस्थान के मेवाड़ अंचल में तो इसी कारण सहस्त्रबाहु का मंदिर सास-बहू का मंदिर हो गया है और मजेदार बात यह है कि यही नाम लोक की जुबान पर भी चढ़ गया है। मुखलाघव की प्रवृत्ति का एक बड़ा उदाहरण है ‘धोबी का कुत्ता, घर का न घाट का’ वाला मुहावरा। असली कहावत थी -धोबी का कुतका, घर का न घाट का। कुतका लोक जुबान में लकड़ी के उस धोऊणे को कहा जाता है जिससे धोते समय कपड़ों को कूटा जाता है। धोबी घर में कपड़ों को धोता नहीं है और घाट पर कपड़े धोते समय कपड़े कूटने के स्थान पर पचीट लेता है। इसलिए कुतका उसके लिए कहीं काम नहीं आता। लेकिन मुख लाघव ने कुतका को कुत्ता कर दिया और कहावत हो गई – धोबी का कुत्ता, घर का न घाट का। .
शायद यही कारण रहा कि तत्कालीन सोवियत संघ के जाने-माने लेखक रसूल हमजातोव ने अपनी बहुचर्चित कृति ‘मेरा दागिस्तान’ में एक स्थान पर लिखा था- ‘‘बोलना सीखने के लिए आदमी को दो साल की जरूरत होती है, मगर यह सीखने के लिए कि जबान को बस में कैसे रखा जाए- साठ सालों की आवश्यकता होती है।’’ रसूल हमजातोव जब साठ सालों की बात करते हैं तो वस्तुत: जीवन के प्रति सचेतन अभिव्यक्ति के अनुभव की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। तभी तो हमारे यहां ‘साठा सो पाठा’ जैसी लोकोक्तियां प्रचलित हैं। अस्तु।
रसूल हमजातोव की यह बात पिछले दिनों एक बार फिर उस समय प्रासंगिक होकर उभरी, जब भारतीय क्रिकेट टीम के दो युवा सदस्यों ने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में अपने खुलेपन को उजाकर करने के अत्युत्साह में महिलाओं के लिए अशोभनीय टिप्पणी कर दी। उन्हें सर्वत्र आलोचना का शिकार होना पड़ा। दरअसल, पिछले कुछ समय से अमर्यादित बातें करना भी लोगों के लिए अपने को विशिष्ट दर्शाने का एक माध्यम हो गया है। ग्रेशम नामक अथर्शास्त्री का एक लोकप्रिय नियम है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। बाजारवादी मानसिकता के चलते अथर्शास्त्र का यह सामान्य सिद्धांत जीवन के दूसरे क्षेत्रों की मनोवृत्ति का परिचायक हो गया है। अब लोग चर्चा में रहने के लिए सामान्य गरिमा से भी समझौता कर लेते हैं। गोया सबने गीतकार नीरज की इन पंक्तियों में अपने होने का अर्थ तलाश लिया हो- ‘‘इतने बदनाम हुए, हम तो इस जमाने में/लग जाएंगी सदियां ही- आपको भुलाने में।’’ नीरज ने गजल की इन पंक्तियों को किन्हीं अन्य अर्थों में लिखा था, लेकिन लोगों ने इसके उथले अर्थ को ही आत्मसात किया और परिणाम यह हुआ कि- ‘‘न तो पीने का सलीका, न पिलाने का शऊर/ ऐसे भी लोग चले आए हैं मयखाने में।’’ जब जीवन के हर क्षेत्र में इसी प्रवृत्ति का बोलबाला है तो भाषा सामान्यीकरण के नाम पर सरेआम ‘फट्टू’ संबोधन तक पहुंच गई तो क्या आश्चर्य?
निश्चित रूप से परिवर्तन को आत्मसात करने की प्रवृत्ति किसी भी भाषा को प्रवाहमान रखने के लिए जरूरी होती है और प्रवाह की यह गति ही नदी और भाषा की सबसे बड़ी ताकत होती है। यही ताकत भाषा को कुंठित होने से बचाती है और नदी को प्रदूषित होने से। भाषा में यदि नए शब्दों के लिए द्वार बंद कर दिये जाएंगे तो भाषा का दम घुटने लगेगा। संस्कृत जैसी सामर्थ्यवान भाषा आम आदमी से दूर होने का एक कारण यह भी है कि उसमें व्याकरण के नियम बहुत सख्त हैं। रसूल हमजातोव ने इसीलिए लिखा था- ‘‘मैं ऐसी पुस्तक लिखना चाहता हूं, जिसमें भाषा व्याकरण के अधीन न होकर व्याकरण भाषा के अधीन हो।’’ भाषाई संस्कारों के लिए पारंपरिकता का निर्वहन और नवीनता का प्रतिपालन- दोनों ही प्रवृत्तियां आवश्यक हैं लेकिन भाषा को यदि उसकी जड़ों से दूर कर दिया जाएगा तो वह अस्तित्व में रहते हुए भी कृशकाय प्रतीत होती है। नवीनता जीवन के लिए आवश्यक है लेकिन हर कीमत पर और हर प्रसंग में परिवर्तन की आतुरता अक्सर कुछ ऐसे तत्त्वों को पोषित कर देती है, जो जीवन के सहज विकास के अनुकूल साबित नहीं होते। एक विद्वान के शब्दों में- ‘‘प्रकृति का मूल आधार प्रेरणा है, किन्तु नियंत्रण के बिना वह विकृति बन जाती है।’’ यह बात भाषा के संबंध में भी सही साबित होती है। भिनसारे जैसे शब्द तो प्रचलन से बाहर होकर भी संवेदनशील लोगों के जेहन में बने रहेंगे लेकिन यदि ‘‘जिंदगी झंड करना’’ भाषा का मूल स्वर बन गया तो हम सब शायद खुद को कभी माफ नहीं कर सकेंगे। १