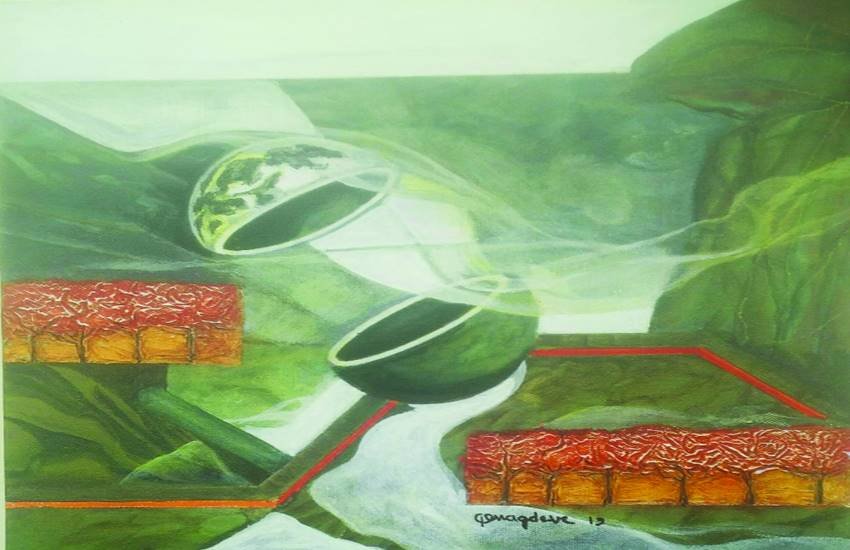रामप्रकाश कुशवाहा
हिंदी आलोचना के इतिहास में कई शीर्षस्थ विभूतियों के होते हुए भी एक लंबा दौर ऐसा रहा है, जिसे भविष्य के साहित्यिक इतिहास लेखक निस्संदेह आलोचना का नामवर काल ही कहना पसंद करेंगे। भारतीय राजनीति में नेहरू और इंदिरा के लंबे और प्रभावी कार्यकाल की तरह आजादी के बाद अज्ञेय और नामवर सिंह ही साहित्यिक नेतृत्व की दृष्टि से दो केंद्रीय व्यक्तित्व दूर और सहज रूप से दिखते हैं। यद्यपि इस बीच धर्मयुग और धर्मवीर भारती, दिनमान और रघुवीर सहाय, सारिका और कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और हंस, ज्ञानरंजन और उनकी पहल का संपादकीय नेतृत्व और अवदान भी कम प्रभावी और महत्त्वपूर्ण नहीं है। यद्यपि अपने अंतिम चरण में वे आलोचक की केंद्रस्थ प्रभावी भूमिका से स्वेच्छा से हट गए थे, लेकिन एक साहित्यिक अभिभावक का-सा प्रभामंडल अंत तक उनके साथ जुड़ा रहा।
प्रगतिशील आलोचक होते हुए भी नामवर सिंह पूरी तरह विचारधारा पर आश्रित बुद्धिधर्मी नहीं थे। विचारधारा पर पूरी तरह आधारित विचारक रहते, तो सोवियत रूस के पतन के साथ उनके लिए भी प्रासंगिकता का संकट और अवसाद का दौर शुरू होता। दरअसल, उनके वामपंथ और मार्क्सवाद का आधुनिकता और वैज्ञानिक चेतना से वैर या विरोध नहीं था। इस विचारशीलता का उन्होंने अपने लिए चयन किया था। यह प्रगतिशीलता उनकी धोती-कुर्ते वाली उत्तर भारतीय किसानों की वेशभूषा की तरह व्यक्तित्व की पोशाक थी। सहमति को लेकर एक सूक्ष्म-पूर्वाग्रही अड़ियलपन था उनमें, कुछ-कुछ अपनी ही शर्तों पर जीने वाली जिद की तरह। भाषा की सर्जनात्मकता का मानक उन्हें अपने गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से प्राप्त हुआ था। इसी कसौटी पर विचारधारा के अंतर्विरोधों की परवाह न करते हुए निर्मल वर्मा की साहित्यिक भाषा पर रीझे। ‘परिंदे’ पर उनकी रीझ कलात्मक अभिव्यक्ति और सृजनात्मक भाषा के प्रति उनका नैतिक समर्थन ही था।
ऐसे नामवर के प्रस्थान और आलोचना में उनके युग के अवसान के बाद हिंदी आलोचना का जो वर्तमान सामने आया है, उसमें अब भी उनकी प्रेरणा और परंपरा (दूसरी) का चिंतन-जड़त्व देखा जा सकता है। पत्रिकाओं से लेकर फेसबुक तक की कविताओं में जागृत मध्यवर्ग की असहमतिपूर्ण चेतना समझदारी के स्तर पर ही अंतर्विन्यस्त है। उनके बाद वरिष्ठ और नई पीढ़ी के अनेक समर्थ आलोचकों के होते हुए भी न जाने क्यों लगता है कि हिंदी का साहित्यिक समय अपनी सामूहिकता की लय को बहुत कुछ खो चुका है और अपने बिखराव को समेटने में असमर्थ है। नामवर जी के जाने के बाद आलोचना के विकेंद्रीकरण की संभावना तो पहले से थी, लेकिन एक अवसर भी था, एक नए लोकतांत्रिक सामूहिक साहित्यिक परिदृश्य के निर्मित होने का। सच तो यह है कि आलोचना साहित्यशास्त्र के निर्माण का सतत चलने वाला उपक्रम है। यह साहित्य की कलात्मक और संरचनात्मक प्रविधियों तथा युक्तियों के सूक्ष्म गहन अध्ययन की सतत चलने वाली परियोजना है।
यह महज संयोग नहीं है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल से लेकर नामवर सिंह और विश्वनाथ त्रिपाठी तक सभी पाठ्यक्रम और पाठ-निर्माण की समस्या से जूझते रहे हैं। यह भी सच है कि प्राध्यापकीय आलोचना अत्यंत धीमी गति से परिवर्धनशील और प्राय: पुनरावर्ती होती है, लेकिन यह भी सच है कि साहित्य के चक्रव्यूह में आखिरी द्वार उसी को खोलना है। सोशल मीडिया ने पहली बार सीधे पाठकों को भी एक अभिव्यक्ति का मंच उपलब्ध करा दिया है। शिक्षित मध्यवर्ग बढ़ा है और उसे दृश्य माध्यमों की चकाचौंध से बाहर निकाल कर वापस किताबों की ओर लाने की जरूरत है। विश्वविद्यालयों में एक समान पाठ्यक्रम पढ़ाए जाने के कारण साहित्य के शिक्षित विशेषज्ञ बढ़े हैं। अगर सही ढंग से हो, तो शोध भी आलोचना कर्म का ही विस्तार है। प्रश्न यही है कि हिंदी में नामवर युग के अवसान के बाद किसी व्यक्ति आलोचक की ताजपोशी के स्थान पर किसी संस्थागत स्थायी मूल्यांकन तंत्र का विकास, यानी पंचायती आलोचना की ओर हिंदी जगत क्यों नहीं बढ़ता।
दरअसल, आलोचना एक संस्थागत और सामूहिकता का प्रतिनिधित्व करने वाला साहित्यिक भाषा-कर्म है। लेकिन हिंदी में यह आरंभ से ही कुछ विशिष्ट प्रतिभाओं पर और लगभग व्यक्ति आश्रित रहा है। हिंदी आलोचना के कुछ बरगदों का युग समाप्त हो जाने से अन्य वनस्पतियों का युग शुरू होता तो भी अच्छा ही होता, लेकिन विडंबना यह है कि भारतीय राजनीति की तरह हिंदी की आलोचना संस्था भी व्यक्ति केंद्रित विपणन की शिकार है। इसने आलोचक की रुचि और पसंद केंद्रित एकरस लेखन को बढ़ावा दिया है। इसने आलोचना और आलोचक की मुखापेक्षी रचनाधर्मिता को बढ़ावा दिया और इसने रचनाकारों की एक बड़ी पीढ़ी को कुछ अधिक ही दमित, शमित, नियंत्रित और सुनियोजित किया।
इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह हुआ कि एक पीढ़ी के हिंदी रचनाकारों में नेतृत्व का आत्मविश्वास और नवोन्मेषी प्रयोगधर्मिता के लिए जोखिम लेने की प्रवृत्ति ही सिरे से गायब हो गई। इससे हिंदी में कुछ समय के लिए बरगदी आलोचक के सापेक्ष बोनसाई लेखकों का दौर रहा। जबकि आलोचक के प्रभुत्व के अभाव वाली अन्य भारतीय भाषाओ में इस कारक के अभाव के कारण बड़े और प्रयोगधर्मी साहित्यकारों का उभरना देखा जा सकता है।
हिंदी के इस यथार्थ के सापेक्ष अंग्रेजी साहित्य के परिदृश्य पर दृष्टिपात करें तो वैश्विक पंूजी के आधार पर होने वाले विपणन के समांतर उनका संस्थागत मूल्यांकन तंत्र सशक्त और विश्वसनीय है। अपने यहां पहले से मान लिया गया है कि इस बीच सभी शोध प्रबंध पीएच-डी की उपाधि के लिए ही लिखे गए हैं। उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यह इतिहास में दर्ज होते हुए भी कि मालवीय जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को उनके अनौपचारिक अध्ययन और कार्य के आधार पर ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में आचार्य पद दिया था। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे यहां मूल्यांकन का स्वायत्त तंत्र और विवेक नहीं है। रचनाकारों और रचनाओं के छवि-निर्माण का दायित्व पूंजीपतियों और मध्यवर्ग से आए साहित्यकारों की रीढ़ पर टिकी लघु पत्रिकाओं यानी कुल मिला कर पत्रकारिता पर ही है।
रचना ही साहित्य की आधारभूत ईकाई है। रचना एक असमाप्त वाद या मुकदमे की तरह है और पाठकों के बीच अपनी विश्वसनीयता सुरक्षित रहने तक आलोचक उस जज की तरह है, जिसके निर्णय की पुनर्परीक्षा का अधिकार भावी पीढ़ी के जज यानी आलोचक को हस्तांतरित होता जाता है।
दरअसल, रचना ही आलोचना का आधार होती है। क्योंकि आलोचना के होने या न होने के बावजूद वह स्वतंत्र रूप से अस्तित्वमान होती है। एक विरोधी आलोचना उसे खारिज करने के स्थान पर और चर्चित और लोकप्रिय बना सकती है। अमृतपान करने वाले मिथकीय चरित्र राहु की तरह ऐसे विवाद रचना की अमरता ही सुनिश्चित करते हैं। आलोचना एक परनिर्भर साहित्यिक विधा है। पाठक आलोचक की संस्तुति मानने के लिए तब तक बाध्य नही है, जब तक कि वह आलोचकीय टिप्पणी की विश्वसनीयता को लेकर आश्वस्त न हो। आलोचना विधा को साहित्यिक स्वीकृति भी पाठकों की सहमति के बाद ही मिलती है।
राजनीति की तरह आलोचना भी एक संस्थागत (सामाजिक) व्यवहार है। आलोचक की वैधता भी मानवीय मूल्यों और सरोकारों के सापेक्ष होती है। आलोचक व्यक्ति होने पर भी समाज के प्रतिनिधि के रूप में मूल्यांकन-चिंतन करता है। जब लोग असामाजिक व्यक्ति के रूप मे आलोचक होने का दंभ जीने लगेंगे, तो आलोचना के संसथागत विवेक और विश्वसनीयता को क्षतिग्रस्त करेंगे। राम की जगह समाज को रख कर भरत की जगह आलोचक को रखा जाए, तब भरत-विवेक के सदृश आलोचक के विवेक का आदर्श उपस्थित होगा।