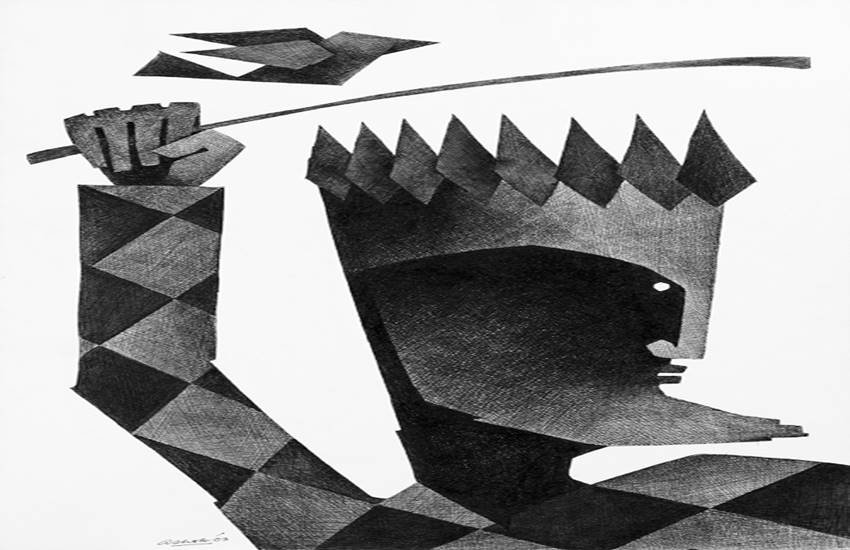दिनेश कुमार
अकसर यह कहते सुना जाता है कि समाज में उथल-पुथल है, लेकिन उस पर एक भी रचना नहीं है या बहुत कम रचनाएं लिखी जा रही हैं। इस तरह साहित्य और साहित्यकार से अपेक्षा की जाती है कि वह समाज में घट रही घटनाओं को तत्काल अपनी रचनात्मकता का हिस्सा बनाए। यह अपेक्षा रचनात्मकता को शाश्वतता की जगह तात्कालिकता में अवमूल्यित करती है। रचनात्मकता की कोई विशेष पद्धति या नियम नहीं है, जिसका पालन कर कोई व्यक्ति सृजन-कर्म में सिद्धहस्त हो सके। प्रत्येक लेखक की रचना-प्रक्रिया अलग-अलग होती है। यहां तक कि हरेक रचना की सृजन-प्रक्रिया में पर्याप्त भिन्नता होती है। पर एक बात निश्चित है कि कोई भी महान सृजन-कर्म तात्कालिकता से परे जाकर ही संभव होता है। तात्कालिकता से बंध कर कोई भी महान रचना नहीं लिखी जा सकती। एक घटना के बाद दूसरी घटना के होते ही जैसे पहली घटना स्मृति से गायब हो जाती है, वैसा ही हश्र इन घटनाओं पर लिखी गई रचनाओं का भी होता है।
देश-समाज में घट रही घटनाएं- जैसे कि कोई आंदोलन, चुनावी राजनीति, सांप्रदायिक तनाव, भ्रष्टाचार, घोटाला, बालात्कार, मंहगाई आदि- पर जो तुरत-फुरत रचनाएं लिखी जाती हैं वे रचना कम, प्रोपेगैंडा अधिक होती हैं। ऐसी रचनाओं का प्रभाव क्षणभंगुर होता है और वे अंतत: हमारे साहित्यिक संस्कार और रुचि को विकृत करती हैं। साहित्य और प्रचारात्मक सामग्री या नारेबाजी में अंतर होता है। घटनाओं पर तात्कालिक प्रतिक्रिया को साहित्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।
साहित्यकारों का जो वर्ग तात्कालिक घटनाओं, आंदोलनों और स्थितियों पर साहित्य-सृजन की वकालत करता है, वह मूलत: साहित्य को उपयोगितावादी दृष्टि से देखता है। साहित्य उसके लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन मात्र है। उसके लिए साहित्य और जरूरत की दूसरी वस्तुओं में कोई फर्क नहीं है। जब आप साहित्य को उपयोगिता की वस्तु मान लेते हैं तो फिर, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता कि उसका उपयोग कोई भष्टाचार विरोधी आंदोलन के लिए कर रहा है या मजदूर आंदोलन के लिए या धार्मिक, राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए। अगर उपयोगिता का तर्क सही है, तो वह सबके लिए सही होगा। उपयोगितावादी दृष्टिकोण मूलत: सत्तावादी दृष्टिकोण है। यह अकारण नहीं है कि प्रत्येक सत्ता, चाहे वह दक्षिणपंथी हो या वामपंथी, अपने विचारों और उद्देश्यों के लिए उपयोगी साहित्य को तो महत्त्वपूर्ण मानती है, लेकिन दूसरे प्रत्येक साहित्य को खारिज करती या कमतर मानती है।
इसलिए असल सवाल सृजनात्मकता के सही या गलत उपयोग का नहीं, बल्कि सृजनात्मकता के प्रति किसी भी तरह के उपयोगितावादी दृष्टि के निषेध का है। उपयोगितावादी दृष्टि साहित्य को जरूरी और गैर-जरूरी में बांटती है। जरूरी और गैर-जरूरी का यह निर्धारण हमेशा उस समय की वर्चस्वशाली विचारधारा द्वारा होता है। इसलिए साहित्य की उपयोगितावादी दृष्टि साहित्य के अस्तित्व को सिर्फ अपने फायदे के लिए स्वीकार करती है। यहां एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए कि साहित्य के लिए उसका अस्तित्व और अस्मिता दोनों जरूरी है। उपयोगितावादी दृष्टि उसके अस्तित्व को एकांगी ही सही, स्वीकार तो करती है पर, उसकी अस्मिता को बिल्कुल ही अनदेखा कर देती है। अस्मिता को खोते ही साहित्य का अस्तित्व भी धीरे-धीरे समाप्त हो जाता है।
ऐसे में एक बड़ा प्रश्न यह उठता है कि क्या साहित्य समाज-निरपेक्ष होता है? समाज में उसकी कोई भूमिका नहीं होती? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। साहित्य का जन्म समाज में होता है। वह समाज निरपेक्ष कभी हो ही नहीं सकता है। इसी तरह उसका उद्देश्य स्वभावत: मानव-कल्याण होता है। मानवीय गरिमा की प्रतिष्ठा ही उसका लक्ष्य है। इसके लिए सचेत प्रयास की जरूरत नहीं है। अगर कोई सचेत प्रयास से अपनी रचनात्मकता को समाज-सापेक्ष और मानव-कल्याणकारी बना रहा है, तो वह निश्चय ही नकली साहित्यकार है।
दरअसल, साहित्य का काम सत्य को अभिव्यक्त करना है, उपयोगिता देखना नहीं। उपयोगिता के तर्क से परे जाकर साहित्य और साहित्यकार का काम सच को अभिव्यक्त करना है। जो सच होगा वह निश्चय ही मानव समाज के हित में होगा। साहित्य की समाज सापेक्षता और उसकी मानव कल्याणकारी भूमिका सचेत नहीं, बल्कि स्वभावत: होती है। श्रेष्ठ साहित्य की कसौटी उसकी उपयोगिता नहीं, बल्कि उसमें अभिव्यक्त सत्य होता है।
किसी भी अच्छी रचना में भाव और विचार, जिसे मुक्तिबोध के शब्दों में कहें तो संवेदना ओर ज्ञान का समन्वय होता है। किसी घटना-विशेष पर तत्काल रचना लिखने से यह समन्वय पूरी तरह गड़बड़ा जाता है। किसी घटना के घटित होने के तुरंत बाद या किसी स्थिति विशेष का प्रथम अनुभव होते ही जब लेखक कोई रचना लिखता है, तो वह रचना उस घटना या स्थिति विशेष के प्रति उसकी भावात्मक या संवेदनात्मक प्रतिक्रिया मात्र होती है। उस रचना में भावुकता अधिक होती है और यथार्थ के प्रति संतुलित दृष्टि कम होती है। ऐसी रचना किसी वांछित उद्देश्य के लिए उपयोगी तो हो सकती है, पर वह सत्य को अभिव्यक्त करने वाली नहीं होगी। जाहिर है, ऐसी रचनाओं की उम्र भी लंबी नहीं होती है। वे जिस परिस्थिति विशेष की उपज होती हैं, उस परिस्थिति विशेष के बदलते ही उनकी भी लगभग मृत्यु हो जाती है।
रचनाकार का प्राथमिक काम निजी अनुभव को सार्वजनिक अनुभव में तब्दील करना होता है। उसे अपने अनुभव को सबका अनुभव बनाना होता है। इसके लिए रचनाकार में तटस्थता का भाव आवश्यक है। यानी भोक्ता और स्रष्टा के बीच में एक द्रष्टा की भी भूमिका होती है। भोक्ता और स्रष्टा के बीच इस द्रष्टा की भूमिका जितनी अधिक होगी रचना विशेष अनुभव से सामान्य अनुभव में उतनी ही अधिक रूपांतरित होगी। जब हम किसी घटना विशेष पर प्रतिक्रिया देते हैं तो यही द्रष्टा भाव अनुपस्थित होता है और रचना निहायत भावुक बन कर रह जाती है। परिवेश के प्रति भावुकता या आक्रोश दोनों ही श्रेष्ठ साहित्य के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हैं। तात्कालिक रचनाओं में या तो भावुकता होती है या आक्रोश।
अतिशय क्रांतिकारिता के दबाव में हम यह भूल जाते हैं कि साहित्यकार होना और एक्टिविस्ट होना, ये दो अलग-अलग स्थितियां हैं। प्रत्येक एक्टिविस्ट लेखक नहीं होता, इसी तरह प्रत्येक लेखक भी एक्टिविस्ट नहीं होता। साहित्यकार का मूल्यांकन उसकी रचनाओं से होगा और रचनाओं का मूल्यांकन साहित्य की कसौटी पर होगा। कोई इसलिए महान रचनाकार नहीं हो सकता कि वह बहुत बड़ा आंदोलनधर्मी है। हिंदी में लेखक संगठनों की राजनीति ने रचनाकार की साहित्यिक उत्कृष्टता को द्वितीयक बनाया और राजनीतिक पहचान को प्राथमिक बनाया। अब इन संगठनों में लेखक बहुत कम और अलेखक अधिक हैं। ऐसे ही अलेखक तात्कालिक घटनाओं पर तात्कालिक कविता आदि लिख कर रचनाकार बनने का प्रयास करते रहते हैं।
दरअसल, ऐसे लोग अपने नागरिक जीवन में संघर्ष के अभाव की पूर्ति अपनी रचनाओं से करते हैं। एक नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करने की जगह ये साहित्य में क्रांतिकारी बनने का छद्म करते हैं। फेसबुक की रचनाशीलता और क्रांतिकारिता भी इसी श्रेणी में आती है। इस तरह का तात्कालिक लेखन नागरिक जीवन में प्रतिरोध न कर पाने के पश्चात्ताप से मुक्त करता है। तात्कालिक लेखन साहित्य के लिए नकारात्मक तो है ही, समाज में भी प्रतिरोध की व्यापकता को सीमित करता है।