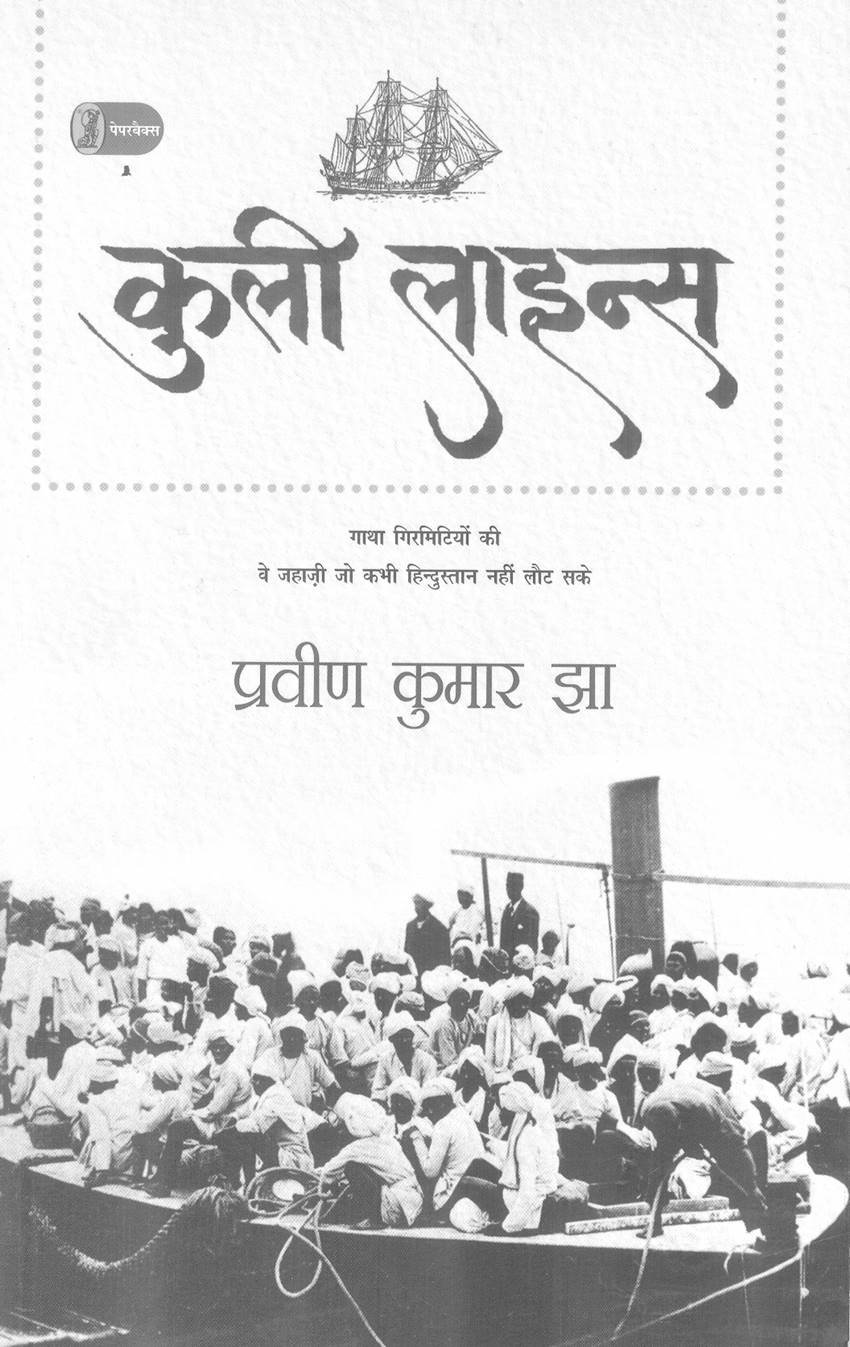मल्लिका
मल्लिका आधुनिक हिंदी के निर्माता भारतेंदु हरिश्चंद्र की वह प्रेमिका थी, जिसके संबंध में इतिहास और साहित्य मौन हैं। भारतेंदु के घर के पास रहने वाली बाल-विधवा, मल्लिका ने भारतेंदु से हिंदी पढ़ना-लिखना सीख कर बांग्ला के तीन उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद किया। उन्हीं अनुवादों ने भारतेंदु को ‘उपन्यास’ विधा से परिचित करवाया और इसी से प्रेरणा पाकर वे आधुनिक हिंदी के निर्माता बने। लेकिन भाग्य की ऐसी विडंबना कि मल्लिका ने जो स्वयं मौलिक उपन्यास लिखा, उसका कहीं कोई जिक्र तक नहीं मिलता; जबकि उनका वह उपन्यास हिंदी का प्रथम उपन्यास माने जाने वाले, ‘परीक्षागुरु’, से पहले का है। इतिहास के धुंधलके से गल्प के सहारे मनीषा ने उसी विस्मृत और उपेक्षित नायिका को खोज निकाला है और उसके जीवन पर एक काल्पनिक जीवनीपरक उपन्यास रचा है।
‘मल्लिका’ की कथा गल्प होते हुए भी ऐसे संपूर्ण व्यक्ति की कहानी है जो हाड़-मांस से बना, किन्हीं वक्तों में जीता हुआ, सांस लेता था। उसके होने के अल्प ही सही, ओझल ही सही, मगर प्रमाण हैं। वे प्रमाण इतने क्षीण हैं कि वह किसी महानतम की छाया का व्यंग्य मात्र बन कर रह जाती है। उसके बारे में जो अनिश्चित और रिक्त स्थान हैं उन्हें उसके वायवीय चौखटे पर कल्पना के सूत्रों से एक संपूर्ण व्यक्तित्व की संरचना से भरने/ बुनने का काम लेखिका ने किया है। गल्प से निर्मित इस कृति में इसका खास खयाल रखा गया है कि ‘वह’ उस विशिष्ट और महत्त्वपूर्ण भूमिका को वहन करे, उसके जीवन का हर पहलू विचारणीय बने, जिसका प्रतिनिधित्व उसने यकीनन अपने ओझल समय में किया होगा।
मल्लिका : मनीषा कुलश्रेष्ठ; राजपाल एंड संज, 1590, मदरसा रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली; 235 रुपए।
अनासक्त आस्तिक
जैनेंद्र कुमार हिंदी के केवल मूर्धन्य कथाकार नहीं, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक-विचारक भी हैं। वे हिंदी भाषा में सोचने-विचारने वाले अन्यतम व्यावहारिक भारतीय दार्शनिक भी हैं, तो भारत सहित वैश्विक राजनीति पर गहरी दृष्टि रखने वाले प्रबुद्ध राजनीतिक विशेषज्ञ भी। वे स्वाधीनता आंदोलन के तपोनिष्ठ सत्याग्रही भी रहे, जिन्होंने स्वाधीनता मिलने के बाद भी अपने समग्र जीवन और लेखन को सत्याग्रह बनाया। अपने पूरे जीवन में अनासक्त रहते हुए उन्होंने जो लिखा और जिया, वह हमेशा एक नई राह की खोज का कारण बना। कहानी और उपन्यास को नई भाषा, शिल्प तथा अधुनातन प्रविधियों में ढालकर जैनेंद्र ने उन विषयों को प्रमुखता दी, जिन पर विचार करने का साहस पहले न किया जा सका। इसमें प्रमुखता से वह स्त्री उभरी, जिसे सदियों से उत्पीड़ित किया जाता रहा है।
अपने दर्शन में आत्म को प्रतिष्ठित करने वाले, विचारों में भारतीय राष्ट्र-राज्य को अधिकाधिक सर्वोदय में देखने वाले तथा जीवन में एक गृहस्थ संन्यासी का आदर्श प्रस्तुत करने वाले जैनेंद्र कुमार का महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे, राधाकृष्णन, जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी आदि राष्ट्रीय नेताओं से सीधा संवाद था। पर यह संवाद राष्ट्रीय हितों के लिए था, निजी स्वार्थों के लिए नहीं। ऐसे जैनेंद्र कुमार के विराट व्यक्तित्व को उनकी जीवनी ‘अनासक्त आस्तिक’ में देखने और उनके क्रमिक विकास को परखने का एक बड़ा प्रयत्न है, जो निश्चय ही उन्हें नए सिरे से समझने में सहायक होगा।
अनासक्त आस्तिक : ज्योतिष जोशी; राजकमल प्रकाशन, 1-बी, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली; 795 रुपए।
अब मैं सांस ले रहा हूं
हिंदी दलित कविता में असंगघोष एक चर्चित नाम हैं। उनके इस संग्रह की कविताएं एक ओर हमारी मानवीय संवेदनाओं को झकझोरती हैं, तो दूसरी ओर अन्याय, शोषण और असमानता के विरुद्ध प्रतिकार की चेतना का संचार करती हैं। इन कविताओं में सर्वत्र मनुष्यता की पहचान, मनुष्यता की मांग और मनुष्यता की कामना है। कवि का हृदय वर्जनाओं से मुक्त होकर बगावत करने के लिए व्याकुल है। इस व्याकुलता में उसके ‘अंतर्मन से निकलते हैं नफरतों भरे/ बगावत के गीत’ और इन गीतों को वह खुद पर ही आजमाता है। इन गीतों की अपनी भाषा है, अपनी लय, छंद, जिनमें समता और स्वातंत्र्य की चाह और मनुष्यता की राह है। कवि समाज को यह अहसास कराना चाहता है कि समाज में सब कुछ सुंदर नहीं है। बहुत कुछ असुंदर और वीभत्स भी है, किंतु इस असुंदर और वीभत्स पर पर्दा है। असंगघोष की कविताएं इस पर्दे को उघाड़ कर समाज के उस असुंदर और वीभत्स यथार्थ को अभिव्यक्त करती हैं। साथ ही, भेड़ की खाल में भेड़िए की पहचान, अभिजात्यता के आवरण में छिपे जातिवाद की पहचान, छद्म राष्ट्रवाद और देशभक्ति की पहचान भी ये कविताएं कराती हैं।
कवि का हृदय जातिगत भेदभाव के जनक और पोषण ब्राह्मण वर्ग के प्रति आक्रोश और प्रतिशोध से भरा है। वह ब्राह्मणवाद को एक दुश्मन की तरह देखता है, पर अन्य दलित कवियों की तरह हिंदुत्व से बाहर निकलने के बजाय वह हिंदू ही बने रहना चाहता है और घोषणा करता है कि ‘मैं तब तक हिंदू ही रहूंगा/ जब तक कि उसकी श्रेष्ठता को जमीन में/ गाड़ न दूं/ सौ फुट नीचे/ तब तक मैं हिंदू हूं/ और हिंदू ही रहूंगा।’ हिंदुत्व से मुक्ति का यह भी एक रूप है।
अब मैं सांस ले रहा हूं : असंगघोष; वाणी प्रकाशन, 4695, 21-ए, दरियागंज, नई दिल्ली; 250 रुपए।
दस्तक देती यादें
सूर्यनगरी जोधपुर जितना ऐतिहासिक रूप में सुपरिचित है, उतनी ही बड़ी पहचान लिए है एक कारोबारी स्थल के रूप में भी। यहां पुष्करण ब्राह्मणों का समाज लंबे समय से रहता चला आया है। इसी समाज की भीतरी सच्चाइयों का क्लोजअप विश्वंभर पुरोहित की इन कहानियों में पढ़ने को मिलेगा। अपनी रसवान पठनीय भाषा में वे इस समाज की अपरिवर्तनशील जड़ मानसिकता को अपनी कहानियों का विषय अनेक कोणों से बनाते हैं। संग्रह की कहानियां परिवेश का वर्णन रिपोर्ताज शैली में करती हैं। वर्णनात्मकता इनका गुण भी है और सीमा भी। समाज की परिभाषा का दायरा भले ही यहां व्यापक न हो, परंतु सीमित दायरे के भीतर खूब पैठ कर देखा गया है। लेखक का अनुभव यहां पूरी धमक के साथ मौजूद है। स्वयं पर्याप्त निरपेक्षता भी है। आत्मविश्लेषण इन कहानियों में इतना नहीं है, जितना कि अनुभवजन्य आंखिन देखा सत्य। अपने मूल उद्यम को संजोए रखने की व्यग्रता में भी लेखक उन कुरीतियों पर वार करता है, जो एक खास समाज को आज भी जकड़े हुए हैं। जहां बहुएं आज भी अपनी सास से पर्दा करती हैं। पीहर में बेटियां पिता के सामने अपनी संतान को गोद में नहीं उठा सकती हैं। बहुपरतीय समाज के दृश्य भले ही यहां न हों, पर जिस समाज को यहां उभारा गया है, उसकी परख और पहचान सच्ची है। एक समय यही काम अपनी भाषा में कुमाउंनी समाज की कमियां उजागर करने के लिए मूर्धन्य कथाकार मनोहरश्याम जोशी ने किया था, जिसकी भूरि-भूरि प्रशंसा हुई थी। इस दृष्टिकोण से विश्वम्भर पुरोहित की ये कहानियां बेहद पठनीय और जरूरी संदेश लेकर उपस्थित हुई हैं।
दस्तक देती यादें : विश्वंभर पुरोहित; सामयिक प्रकाशन, 3320-21, जटवाड़ा, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली; 250 रुपए।