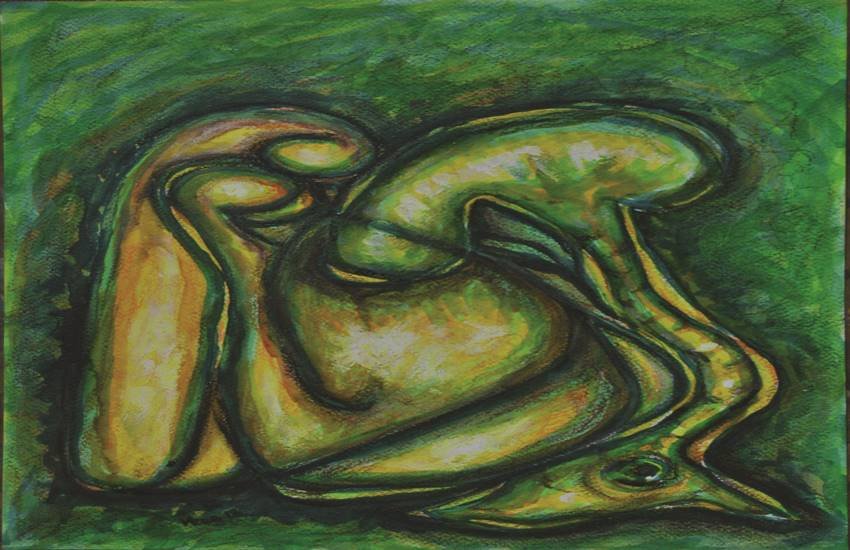विजय बहादुर सिंह
तमाम दुनिया किताबों की/ कितनी-कितनी कम लगती है/ एक पूरी जिंदगी में/… कलम के रोजगार में भी/ इतनी-इतनी चालाकियां।’-कंचन सिंह चौहान। किताबों की दुनिया के पंजीकृत नागरिकों की एक खूबसूरती तो यह होती ही है कि वे उसी को परम सत्य मान लेते हैं। वे उन्हें एक ऐसे परम विचार लोक में ले जाती हैं जो परम सत्य होता है और उसके आगे-पीछे शायद कुछ भी नहीं होता। सांप्रदायिकता वस्तुत: यहीं से शुरू होती है। इसी सांप्रदायिकता से दुनिया पहले भी त्रस्त और लहूलुहान थी, आज भी हो रही है। आज तो यह विचारों की परमता से आगे बढ़कर जातियों और कुनबों की परमता की ओर बढ़ चली है। तभी तो कवि नागार्जुन ने लिखा- ‘हमीं हम ठोस, बाकी सब फूटे ढोल।’ तब कंचन नाम की युवा कवयित्री का यह लिखना कि जिंदगी के बीहड़ अनुभवों के बीच किताबों का वैचारिक या फिर काल्पनिक संसार कितना छोटा पड़ जाता है। तब किसी बुजुर्ग पुरखे आलोचक का यह कहना कितना सही और विचारणीय लगता है कि वादों और विचारों की तो सीमा होती है लेकिन जिंदगी की ‘गतियों’ और उनसे निकली या जन्मी सच्चाइयों की नहीं। विचार का सच अगर ठहरा हुआ सच नहीं होता तो दुनिया के कई बड़े ताकतवर देश उस सच के बावजूद क्षमताहीन नहीं होते। काव्य और कलाएं इस ठहरे हुए सच को हकीकत समझ जिंदगी के नए चेहरों को पहचानने और समझने निकल पड़ती हैं। ऐसा न होता तो इस देश को एक रामायण से ही संतुष्ट हो जाना था, जबकि वह महाभारत जैसा एक और प्रतिवादी महाग्रंथ लेकर आया। इतने से भी इसका पेट कहां भरा, तो पुराण लेकर आ गया। तो क्या मान लें कि यह एक भुक्खड़ और अस्थिर चित्त का देश है या फिर समय-समय की सच्चाइयों के पीछे किसी खोजी व्याकुल वैज्ञानिक जैसे चित्तवाला देश। निरंतर बदलते जाते अनुभव-सत्य पर गहरी निगाह रखने वाला समाज। इस गतिशीलता को कुछेक जड़ जगतवादी चाहें तो देसी मानस की अस्थिरता भी कह सकते हैं या फिर धुरी से खिसका देश, पर जिनके पास सुस्थिर इतिहास, दृष्टि और समझ है वे जानते हैं कि गतिशीलता ही एकमात्र सच है। इसे आसानी से समझने के लिए या तो हमें इतिहास में चंडत्व का पर्याय बने अशोक का धम्मदूत बन उठना है या फिर छायावादी कवि पंत की कविता ‘परिवर्तन’ की ओर। समय के चेहरे पर उसके पांवों की गतियों की छाप होती है। विडंबना यह है कि कुछ लोग पांवों की गतियों को छोड़ इसी चेहरे को लेकर बैठ जाते हैं और खतरा यहीं से शुरू होता है।
एक बार मैंने अपने समय के एक जाने-माने बुद्धिजीवी के समक्ष यह जिज्ञासा की थी कि अपने यहां जब तीन पुुरुषार्थ भोग से जुड़े हैं, तब यहां के साधु-संन्यासी क्यों अध्यात्म-अध्यात्म करते रहते हैं, तो उसका जवाब कुछ उलटबासी जैसा था कि वे सब अभी संसार को लेकर अपना राग छोड़ नहीं पाए हैं इसलिए। अध्यात्म तो वस्तुत: विश्वमय विश्वरूप हो जाना है। वैदिक ग्रंथों में भूमा का बोध हो जाना है। व्यक्ति का समष्टि होना ही अध्यात्म है। अरसे बाद मैंने जब इसे ही आचार्य आलोचक से पूछा तो उन्होंने कहा- वह जिसमें गंभीर संवेदनाओं का सागर लहराता है, जिसे समूचे लोक की व्यथा सताती हो, जिसमें विश्वव्यापी करुणा हो, वही सच्चा आध्यात्मवादी है। इस रूप में बुद्ध या महावीर आध्यात्मवादी थे या फिर हमारे अपने जमाने में गांधी। वे धर्मों और जातियों में रहकर भी अपनी सोच और व्यवहार में इन दोनों ही घेरों का अतिक्रमण कर जाते थे। इसलिए उनमें अंग्रेजों को लेकर भी घृणा नहीं थी, पर उनकी अंग्रेजियत से थी। न होती तो वे ब्रिटिश बाजारों के विरुद्ध स्वदेशी जैसा मुंहतोड़ हथियार कैसे खोजते? बुद्ध की करुणा, महावीर की अहिंसा और गांधी का सत्याग्रह ही सच्चा अध्यात्म है। लेकिन यह इसी भौतिक संसार की उपलब्धि और संदेश है कि वैयक्तिकता के दायरे से ऊपर उठो। इतना ही क्यों, आजकल इस देश के कई स्वयंभू पश्चिम के धर्म को भारत में व्यवहृत धर्म मान कर चल रहे हैं। वेदों से लेकर महाभारत से होते तुलसी के मानस तक धर्म की एक ही परिभाषा दी गई है- मनुष्यत्व। इंसानीपन। इसका शायद ही कोई रिश्ता किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारे से हो। ‘परहित सरिस धर्म नहिं भाई।’ यही है। अब अगर कोई साहित्य-वकील धर्म का कोई अपना चालू या सतही कर्मकांडी अर्थ लगाता हो तो वह भारत के लोगों में खूब है। रावण से लेकर डाकू मानसिंह तक। पर इस देश में कभी उन्हें धर्म-पुरुष नहीं माना गया।
साहित्य और कलाएं इसी सच्चे, पवित्र और सूक्ष्म धार्मिक मन की उपज हैं। कभी-कभी यह मन सर्जक की अल्प प्रतिभा के कारण मानव-मन की उन गहराइयों और उसके सपनों की ऊंचाइयों तक नहीं भी पहुंच पाता, पर आता तो है इसी उदात्तता की कोख से। साहित्य से ही उदाहरण लें तो मैथिलीशरण गुप्त और प्रेमचंद का ले सकते हैं। जानने वाले जानते हैं ये दोनों राष्ट्रीय आंदोलन की ही उपज थे। पता नहीं यह खुद नवजागरण की उपज था या नहीं फिर भी इसके पीछे उत्तर भारत के आर्थिक तौर पर त्रस्त किसानों और बंगाल के जड़मूल से उखड़ चुके कपड़ा कारीगरों की भूख, यातना और विक्षोभ से उपजा विद्रोह। राष्ट्रीय आंदोलन ने ही वह जनचेतना फैलाई जिसमें ये दोनों और कई अन्य छोटे-मोटे अपनी दशा पर सोचने और उस पर विचार करने के लिए आगे आए। निश्चय ही इनमें सबसे गहरी समझ और दृष्टि तो प्रेमचंद के ही पास थी अन्यथा छायावाद युग के आलोचक आचार्य नंददुलारे वाजपेयी अपनी पुस्तक ‘राष्ट्रीय साहित्य और अन्य निबंध’ में यह कभी न लिखते कि ‘वृहत सामाजिक अन्याय के उद्घाटन को हम प्रेमचंद के कृतित्व का मूल तत्व कह सकते हैं, किंतु इस अन्याय की कसौटी। वे कहां से प्राप्त करते हैं?- मनुष्य के व्यक्तित्व में अटल और अदम्य आस्था द्वारा।’ इसी के पहले उसी पैरा में वे यह भी लिख चुके हैं कि- कथा साहित्य के क्षेत्र में विश्व के बड़े साहित्यिकों में परिणत होने योग्य हमारे प्रेमचंद हैं। अफसोस यह कि हमारे राष्ट्रकवि यथार्थ के इस धरातल की ओर झांकते ही नहीं। न ही उन्हें गतिशील जीवन सत्य की कोई चिंता है। उनके प्रशंसित और आकांक्षित मूल्य हृास ग्रस्त मध्ययुगीन समाज के हैं। ‘भारत भारती’ ही नहीं, ‘साकेत’ तक उनका यही मानस चलता है। ‘साकेत’ पर तो गांधी की ही टिप्पणी पर्याप्त है। इस दृष्टि से ‘कामायनी’ के प्रसाद जिस सूक्ष्म वैचारिक धरातल पर भोगवाद की तरफ बढ़ते इस आधुनिक विश्व का चरित्रांकन करते और आगाह करते हैं, उसको समझने के लिए ‘कामायनी’ का चिंता सर्ग ही पर्याप्त है- ‘स्वयं देव वे हम सब, तो फिर/ क्यों न विशृंखल होती सृष्टि।’ यह कैसा संसार हम बनाने निकल पड़े हैं, जहां केवल और केवल मनुष्य का अस्तित्व स्वीकार है? जीव-जंतु-नदी-नाले-वन-पहाड़-जंगल क्या अपना अस्तित्व अक्षुण्ण रखने के हकदार नहीं?
क्या मनुष्य का भोगवाद इतना हिंसक हो उठा जितना देवताओं का था, चिंता सर्ग का? नागार्जुन जैसे कवि इसका जवाब-सा सोचते हुए लिखते हैं- ‘भौतिक भोगमात्र सुलभ हों भूरि-भूरि। विवेक हो कुंठित। तन हो कनकाम, मन हो तिमिरावृतय कमलपत्री नेत्र हो बाहर-बाहर/ भीतर की आंखें निपट-निमीलित/ यह कैसे होगा, यह क्यों कर होगा?’
साहित्य यह झगड़ा शायद ही कभी करता हो कि उसका विश्वबोध ही एकमात्र विश्वबोध है। न ही वह वैचारिक संप्रदायवादियों की तरह अपने ही सच को एकमात्र सच मानता है। वह परंपरावादियों की तरह अतीतवाद को ही परंपरा मानता है। परंपरा का अर्थ ही है- गति में रह सकने वाली सनातनता या अविच्छिन्नता। एक पीढ़ी से भावी पीढ़ियों तक को ऊर्जास्वितदाय देने वाली शक्ति ही विरासत है। इस दृष्टि से स्त्रियों के संदर्भ में प्रियप्रवास की राधा समाजसेविका है। गांधी और आर्यसमाज दोनों के ही संयोग की तात्कालिक उपज। पर हम उसकी तुलना कामायनी की ‘श्रद्धा’ या ‘इड़ा’ से तो कदापि नहीं कर सकते।