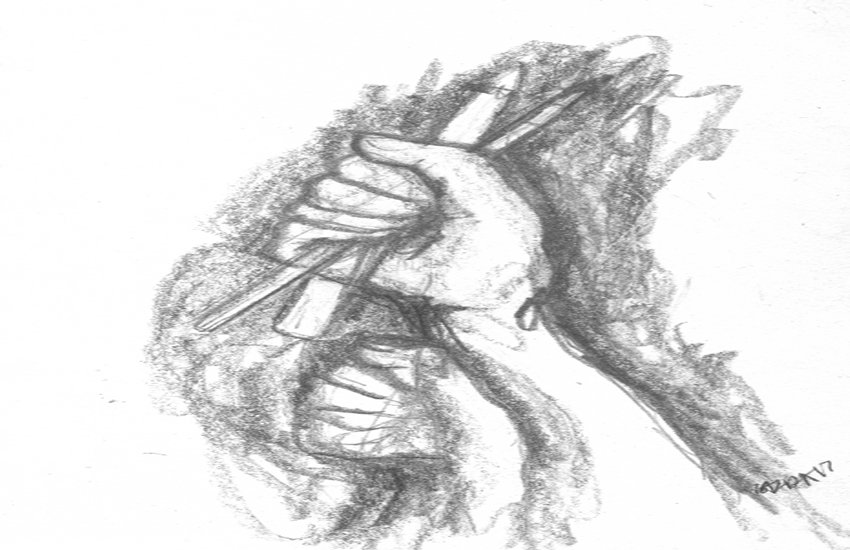राजेंद्र कुमार
सितंबर आया नहीं कि हर साल सरकारी, अर्द्ध-सरकारी संस्थानों में ‘हिंदी-हिंदी’ होने लगता है। कहीं ‘हिंदी दिवस’ तो कहीं ‘हिंदी पखवाड़ा’। आयोजन इतने होते हैं कि आमंत्रित किए जाने के लिए हिंदी के स्वनामधन्य अध्यापकों और तथाकथित हिंदी-प्रेमियों की संख्या कम पड़ने लगती है। ऐसे में कई संस्थानों में वहां के अधिकारीगण ही ‘हिंदी-हिंदी’ उगलने लगते हैं और हिंदी के खाते में अनुमोदित राशि को आपस में ही मिल बांटकर निगल जाते हैं। इससे हिंदी की श्री-वृद्धि कितनी होती है, हिंदी के प्रति वास्तविक प्रेम में कैसा और कितना इजाफा होता है, यह किससे पूछा जाए? अपना देश शायद दुनिया का अकेला देश है, जहां भाषा के नाम पर भी ‘दिवस’ मनाए जाते हैं। नहीं सुना कि दुनिया के किसी अन्य देश में वहां की किसी भाषा को बढ़ावा देने के लिए कोई ‘दिवस’ या कोई ‘पखवाड़ा’ मनाने की जरूरत पड़ती हो। ‘दिवस’ मनाने का ऐसा उत्साह कि अर्थ का अनर्थ हो रहा हो, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। तथाकथित हिंदी-प्रेम के अनेक नमूने अक्सर हमारे अनुभव का अंग बनते रहते हैं। इलाहाबाद शहर में देखा गया कि आंखों के एक अस्पताल के प्रवेश-द्वार पर अंग्रेजी में लिखा था-‘गवर्नमेंट आई हास्पिटल’। अस्पताल के प्रशासन के हृदय में हिंदी का प्यार उमड़ा। उसने अंग्रेजी की इस इबारत का हिंदीकरण किया और नागरी में यों लिखा-‘सरकारी आंख का अस्पताल।’ हिंदी बेचारी मन मसोस कर रह गई। काश, इबारत यों होती-‘आंख का सरकारी अस्पताल।’
जहां तक अंग्रेजी और हिंदी के द्वंद्व का सवाल है, तो एक बात तो यह कि अंग्रेजी का आत्यंतिक विरोध कई बार हिंदी-प्रेम का कम, अंग्रेजी में अपनी गति की सीमाओं को छिपाने का उपक्रम ज्यादा होता है। भूलना नहीं चाहिए कि राम मनोहर लोहिया ने ‘अंग्रेजी हटाओ’ आंदोलन चलाया था तो इस तथ्य के बावजूद कि उन्हें अंग्रेजी खूब अच्छी तरह आती थी। महात्मा गांधी तो ऐसी सहज-सरल अंग्रेजी लिखते-बोलते थे, जो आज भी इस बात का आदर्श नमूना है कि एक हिंदुस्तानी की अंग्रेजी वैसी होनी चाहिए, और तब उन्होंने अपने देश की भाषा के प्रति स्वाभिमान जताने के लिए कहा था कि ‘दुनिया से कह दो कि गांधी को अंग्रेजी नहीं आती।’ पर आज तो संकट यह है कि हमारे बहुत से हिंदी-प्रेमियों को कायदे से न अंग्रेजी आती है, न हिंदी। तब कुछ यह ध्वनित होता है कि अंग्रेजी क्या सीखना, वह तो पराई है, हिंदी भी क्या सीखना वह तो है ही अपनी भाषा।
दूसरी बात यह कि ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में पूरी गंभीरता से काम करने वाले हमारे भारतीय विद्वान और बौद्धिक जन, जिनको अच्छी हिंदी आती है, वे भी अंग्रेजी में लिखना ज्यादा सार्थक या ज्यादा महत्त्व की बात मानते हैं। एक गंवई कहावत है-‘पराई पतरी का बरा किसे अच्छा नहीं लगता?’ तो, अंग्रेजी ऐसी पराई पत्तल है, जिसमें अपनी विद्वत्ता परोसते रहने से ही हमारे विद्वानों में यह विश्वास जागता है कि उनके काम को श्रेष्ठ और प्रामाणिक माना जाएगा।
भाषा के स्तर पर हिंदी अगर अपने स्वाभिमान की रक्षा में आज असमर्थ दिख रही है तो साहित्य के स्तर पर भी हिंदी कम संकटग्रस्त नहीं है। ऐसे समय में, जब तथाकथित भूमंडलीकरण की आंधी हमारी सभी भाषाओं और बोलियों को अंग्रेजी के मुंह का ग्रास बनने की दिशा में उड़ाए लिए जा रही है, होना यह चाहिए था कि न सिर्फ हिंदी, बल्कि सभी भारतीय भाषाओं के शुभिंचतक और रचनाकारों में आपसी समझदारी बढ़ती। पर, हो यह रहा है कि सब अपनी-अपनी महत्त्वाकांक्षाओं के शिकार हैं। सोच-विचार के केंद्र में सही और जरूरी मुद्दों को लाने के अवसर खत्म होते जा रहे हैं। हर बात का मजा लेने के अवसर बढ़ते जा रहे हैं।
भाषा की चाल से समाज की चाल का पता चलता है। एक समय था, जब हिंदी भाषा समाज आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में आ रहा था। तब इस समाज की फिक्र यह थी कि हिंदी और उसकी बोलियों को भी किस प्रकार समर्थ बनाया जाए कि ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में आ पड़े कार्यभारों को वहन करने के लिए वे तैयार हो सकें। राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद ने पहली बार हिंदी में पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने में रुचि लेना शुरू किया था और अंग्रेजी या अन्य भाषाओं से आए पारिभाषिक शब्दों के हिंदी रूप (मसलन, ‘इंडेक्स’ के लिए ‘अनुक्रमणिका’, ‘बेस’ के लिए आधार, ‘नक्शा’ के लिए मानचित्र) हमें दिए थे। आपस की अनेक असहमतियों के बावजूद सबकी ंिचंता का बुनियादी बिंदु प्राय: यही था कि हिंदी का जो भी रूप बने, वह हिंदी की अपनी प्रकृति पर प्रहार करता हुआ नहीं, बल्कि उसकी रक्षा के सवाल को ध्यान में रखते हुए बने। भारतेंदु ने भी तभी अपना प्रसिद्ध लेख लिखा था-‘हिंदी नई चाल में ढली’।
लेकिन यह सब लगभग डेढ़-दो सौ वर्ष पहले का इतिहास है। जाहिर है, तब अंग्रेजी राज था और अंग्रेजी का वर्चस्व तब कितना भी रहा हो, पर हिंदी के अपने वाक्यों में अंग्रेजी शब्दों को अनधिकृत प्रवेश की कतई छूट न थी। अंग्रेजी से शब्द बेशक हमने बहुत से लिए थे, जैसे अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से लिए थे। लेकिन हिंदी की प्रकृति के अनुकूल बनाते हुए। अंग्रेजी का ‘हास्पिटल’ शब्द आया तो हिंदी के लिए उसे ‘अस्पताल’ बनना पड़ा। फारसी का ‘देह’ (गांव) शब्द आया तो उसे ध्यान रखना पड़ा कि हिंदी के ‘देह’ (शरीर) शब्द से टकराए नहीं। इसलिए देह का फारसी में जो बहुवचन रूप था देहात, वह हिंदी के वाक्य में एकवचन बनकर गांव के अर्थ में प्रचलित हुआ। अरबी का ‘फस्ल’ शब्द आया तो इस तथ्य का ख्याल रखते हुए आया कि अपनी संस्कृत के ‘जन्म’ और ‘भस्म’ जैसे शब्दों को जब जनम और भसम कर लेने का अपना हक हिंदी ने नहीं छोड़ा तो उसे फस्ल को फसल कर लेने का हक भी क्यों न दे दिया जाए। तो यह हिंदी का नई चाल में ढलना एक सांस्कृतिक आदान-प्रदान की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम था। यह प्रक्रिया हिंदी की अपनी प्रकृति के लचीलेपन का प्रमाण भी देती थी और साथ ही, अपनी लोकतांत्रिक चेतना से विदेशी भाषाओं के शब्दों को यह तमीज भी देती थी कि उन्हें हिंदी में आने का सहज अधिकार किस तरह पाना है। लेकिन जिस तरह आज हिंदी को एक लाचार भाषा बना देने का उपक्रम चल रहा है, वह उसे बड़े अभियान कर अंग है, जिसमें न केवल, हिंदी, बल्कि समूचे भारतीय समाज को भूमंडलीकरण के नाम पर लाचार कर देने की साजिश रची जा रही है।
राष्ट्रभाषा और राजभाषा बनने योग्य रुतबा पाने के लिए खड़ी बोली हिंदी जब मानकीकृत हुई, तो अपनी ठसक में उसने अपने परिवार की क्षेत्रीय बोलियों से अपना नाता जिस तरह तोड़ लिया, उससे हुई क्षति का जायजा अभी हमें लेना था। लेकिन तब तक हम भूमंडलीकृत समाज होने के चक्कर में आने लगे। यह जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों वाले कारपोरेट जगत के नागरिक होने का सुख भोगने को हम अब तैयार बैठे हैं, इसकी अगर कोई मानक भाषा होनी है, तो वह अंग्रेजी ही होनी है। यानी भाषा का जो भूमंडलीकृत मानक स्वरूप बन रहा है, वह अंग्रेजी आधारित ही होगा, यह लगभग तय हो चुका है। ऐसे में हिंदी से नाता टूटते जाना स्वाभाविक है। यह अपनी जड़ों से उखड़ना जैसा होगा। मध्य वर्ग का एक बड़ा तबका अभी इस संकट से बेखबर है। वह अपनी हैसियत बनाने में मगरूर है।
इधर कुछ शुद्धतावादी सलूक के उत्साह में भी हिंदी प्रेम के नाम पर जाने-अनजाने हिंदी का अहित होने की आशंका है। लगभग दो बरस पहले एनसीईआरटी को एक प्रस्ताव भेजा गया जिसमें कहा गया कि हिंदी की पाठ्य-पुस्तकें तैयार करते समय ध्यान रखा जाए कि उनमें अंग्रेजी-उर्दू के शब्द न आने पाएं। सोचिए, यदि यह प्रस्ताव मान लिया जाए तो हमारी भाषा का क्या हश्र होगा। क्या होगा ‘अस्पताल’ (हास्पिटल), ‘स्कूल’ ‘कापी-किताब’ जैसे अनेक शब्दों का, जो हिंदी की गोद में पलते-पुसते रहे। अगर ‘गरीब’ की जगह ‘निर्धन’ कर देंगे तो तुलसी के राम ‘गरीब नेवाज’ न रह जाऐंगे। इस तरह की सोच और व्यवहार हावी न होने पाए, तभी हिंदी ‘हमारी हिंदी’ बनी रह, सकेगी। ‘हिंदी दिवस’ पर आयोजनों के कर्मकांडों से क्या होगा? सचमुच ‘जिन्हें नाज है हिंदी पर वे कहां हैं? ०