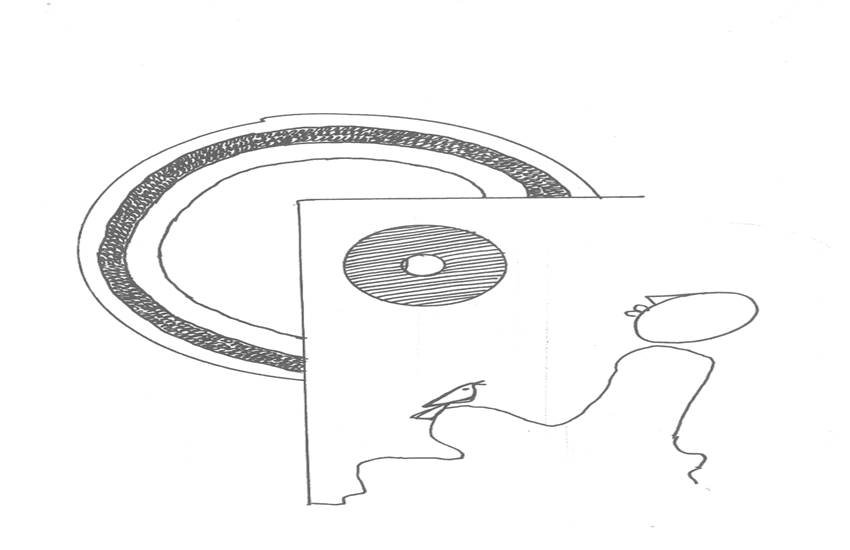हित्यिक कृतियों के मामले में आलोचना ने एक खेल का रूप अख्तियार कर लिया है। जैसे फुटबाल का खेल। फुटबाल के खिलाड़ी तरह-तरह से खेलते हैं- कोई पैर से किक मारता है, तो कोई माथे से, कोई नाक की सीध में गेंद को मारता है, तो कोई उसे उल्टी दिशा में लहरा देता है, कोई दाएं मारता है, तो कोई बाएं। गोलकीपर उसे हाथ से ही पकड़ लेता है। लगभग ऐसा ही व्यवहार विभिन्न आलोचकों का साहित्यकारों और उनकी कृतियों के साथ दिखाई देता है। हालांकि फुटबाल के खिलाड़ियों का लक्ष्य गेंद को गोलपोस्ट के भीतर करने का रहता है, जिसे देख कर खिलाड़ी और दर्शक दोनों को अपने श्रम और समय की सार्थकता का अहसास होता है, जबकि हमारे आलोचक रचनाओं के साथ जो खेल खेलते हैं उससे पाठक दुविधा का शिकार हो जाता है। किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ होता है और उसके सामने फांक ही फांक, अंतर्विरोध ही अंतर्विरोध उपस्थित हो जाते हैं
पहले हिंदी की पाठ्य पुस्तक में विद्यापति, कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, मीरा, रहीम, रसखान, बिहारी से लेकर भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिलीशरण गुप्त, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, दिनकर आदि की कविताएं होती थीं, तो गद्य साहित्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारीप्रसाद द्विवेदी के निबंध, प्रेमचंद, प्रसाद, सुदर्शन, शिवपूजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि की कहानियां होती थीं। इन साहित्यकारों को पढ़ाने वाले शिक्षकों ने बच्चों में यही बोध या संस्कार पैदा किया कि ये सभी कवि-लेखक हमारे महान, आदरणीय हैं। इनका साहित्य हमारे लिए गौरव का विषय है। इन सबके लेखन को पढ़ने से ही अनेक विद्यार्थियों में साहित्यिक अभिरुचि पैदा हुई। पर वही जब स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर पहुंचते हैं और उनका आलोचनात्मक लेखन से वास्ता पड़ता है, तो उनके इस संस्कार में दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं, बढ़ती ही जाती हैं।
हिंदी आलोचना के शुक्लोत्तर काल के बाद इस फांकवादी आलोचना का चलन खूब बढ़ा। कुछेक आलोचक कबीर आदि निर्गुणिया कवियों को संत कोटि में रखते हुए विद्रोही, क्रांतिकारी बताने लगे, तो उत्तर भारत की जनता के हृदय पर राज करने वाले तुलसीदास को प्रतिगामी, ब्राह्मणवादी, शूद्र और स्त्री-विरोधी सिद्ध करने लगे। राष्ट्रप्रेम का स्वर मुखरित करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र को राजभक्त बताया जाने लगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी को महज नैतिकतावादी, स्थूलता का पोषक बता कर उपहास उड़ाया जाने लगा, तो राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त को हिंदू पुनरुत्थान का कवि बता कर उनका कद छोटा किया जाने लगा। छायावाद को पलायन की काव्यधारा मानने वालों से आगे बढ़ कर उसे हिंदू महासभा और मुसलिम लीग से भी ज्यादा घातक बताया गया। आलोचकों की एक टीम रामचंद्र शुक्ल को ब्राह्मणवादी, सामंतवादी बताने में पिल पड़ी, तो दलित विमर्श के नाम पर तैयार हुई टीम रामविलास शर्मा, नामवर सिंह जैसे ख्यात प्रगतिवादियों को सवर्णवादी सिद्ध करने लगी। निराला को इस बात के लिए कोसा जाने लगा कि उन्होंने ‘शंबूक वध’ के बजाय ‘राम की शक्ति पूजा’ पर क्यों कविता लिखी। जीवन भर सामंती मूल्यों की धज्जियां उड़ाने वाले प्रेमचंद को ‘सामंत का मुंशी’ सिद्ध किया जाने लगा। दलित और स्त्री विमर्श के नाम पर उभरी आलोचनाओं ने संपूर्ण भारतीय साहित्य को ही सवर्णवादी और पुरुष-वर्चस्ववादी साहित्य सिद्ध करने में अपनी प्रतिभा झोंक दी।
हर आलोचक अपनी नियमावली बना कर कृति के साथ खेल खेलता है, जिसका नतीजा होता है कि कृति के वस्तु-सत्य पर धुंध छाती जाती है और सहृदय पाठक इसके पार जाने वाली दृष्टि से वंचित रहने के कारण अपना माथा पकड़ कर बैठ जाता है। वह तय नहीं कर पाता कि किस आलोचक की बात को सही समझे और किसकी गलत। अधिकतर आलोचनाओं में आलोचकों का विचारधारात्मक रूझान इतना प्रबल रहा है कि वे कृतियों में संप्रेषित मूल अर्थ, भाव पर अपने विचारों का रंग उड़ेलते रहे, नतीजतन हर कृति का अपना मूल कथ्य बदरंग और ओझल होता गया। कृष्णदत्त पालीवाल के शब्दों में कहें तो ‘इस विचारधारा के कसाईबाड़े में साहित्यिक कृतियों की हत्या होती रही।’
आज हर आलोचक के पास कृतियों की हत्या करने के अपने-अपने औजार हैं। किसी के पास पुराना मार्क्सवादी वर्गीय चेतना वाला हथियार है, तो किसी के पास नए औजार के रूप में दलित चेतना, स्त्री-चेतना या फिर पश्चिम से आयातित संरचनावाद, उत्तर-आधुनिकतावाद, विखंडनवाद आदि का। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिप्रेक्ष्य के नाम पर अपने-अपने व्यक्तिगत मनोभावों, विचारों के अनुरूप साहित्यिक कृतियों के वस्तु-सत्य को क्षत-विक्षत करने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वह बढ़ता ही जा रहा है। इससे खुद आलोचना की विश्वसनीयता का ही क्षरण हुआ है। दरअसल, आलोचना का काम किसी कृति को समझने की कुंजी के रूप में होना चाहिए, न कि अपनी वैचारिकी के अनुरूप उसका भाष्य प्रस्तुत करना। इस संबंध में विजयदेव नारायण साही का ‘लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस’ निबंध में आलोचना कर्म के लिए बड़ा ही सटीक सूत्र है-‘आलोचना का काम साहित्यिक कृति की संवेदना को जबर्दस्ती खींच कर पाठक तक पहुंचाना नहीं है।
आलोचना सिर्फ इतना कर सकती है कि पाठक के जो भी वैचारिक या धारणात्मक पूर्वाग्रह, जाने या अनजाने, अपनी उपस्थिति या अनुपस्थिति के कारण, पाठक को उस ओर उन्मुख होने से रोक रहे हैं, जहां से काव्य का ‘प्रभाव’ प्रवाहित हो रहा है उन्हें विनष्ट करके पाठक को एक उचित तत्परता की अवस्था में छोड़ दे। यंत्र जगत की एक स्थूल उपमा द्वारा हम यों कह सकते हैं कि रेडियो की सुई को उचित लहर मान पर लाकर लगा भर देना आलोचना का काम है, बाकी ट्रांसमीटर से आता हुआ गायन तो रेडियो सेट स्वयं पकड़ेगा। अब अगर वहां से गायन आ ही न रहा हो, या आवाज में गड़बड़ी हो तो आलोचक गाने वाले के स्वर से स्वर मिला कर गा नहीं सकता।’
साही ने सही आलोचना के लिए जिस ‘वैचारिक या धारणात्मक पूर्वाग्रह’ को विनष्ट करने की बात कही, मुक्तिबोध ने भी ‘कामायनी एक पुनर्विचार’ लिखने के बाद उसकी आवश्यकता महसूस की। अपने वैचारिक पूर्वाग्रह के कारण मुक्तिबोध कामायनी की आलोचना करने में जिस फिसलन का शिकार हुए थे, उसे उन्होंने महसूस कर लिया था। तभी उन्होंने अपने प्रसिद्ध निबंध ‘समीक्षा की समस्याएं’ में समीक्षक के लिए यह शर्त रखी- ‘समीक्षक का प्रथम कर्तव्य है कि वह किसी भी कलाकृति के अंतर्तत्त्वों को, उसके प्राण-तत्त्वों को, भावना-कल्पना को हृदयंगम करे और एक विशेष दिशा की ओर प्रवाहित अंतर्धारा की गति, और उसकी अंतिम परिणति को, सहानुभूतिपूर्वक अच्छी तरह समझे और तदुपरांत उसका विश्लेषण करे।… इसके लिए समीक्षक के पास प्रगाढ़ जीवनानुभूति, वैविध्यपूर्ण प्रगाढ़ अनुभव संपन्नता तथा मार्मिक जीवन-विवेक चाहिए।’ आचार्य शुक्ल ने भी उच्च कोटि की समालोचना के लिए ‘विस्तृत अध्ययन, सूक्ष्म अन्वीक्षण बुद्धि और मर्मग्राहिणी प्रज्ञा को अपेक्षित माना था।
जिन मुक्तिबोध ने मार्क्सवादी वैचारिकी के वशीभूत होकर कामायनीकार को समाजवादी व्यवस्था को समाधान स्वरूप न अपनाने के लिए खूब कोसा था, वही परवर्ती काल में सच्ची समालोचना के लिए विचारधारात्मक आग्रह के बदले ‘प्रगाढ़ जीवनानुभूति, वैविध्यपूर्ण प्रगाढ़ अनुभव संपन्नता तथा मार्मिक जीवन-विवेक’ को आवश्यक मानने लगे थे। पर विडंबना यह रही कि मुक्तिबोध भक्तों का भी वैचारिक आग्रहों से मोहभंग नहीं हुआ और हिंदी आलोचना तरह-तरह की वैचारिक पटरियों पर दौड़ती रही। ऐसा नहीं कि इस वैचारिक घटाटोप से आलोचना को मुक्त करने वाला लेखन नहीं हुआ। कृष्णदत्त पालीवाल, रमेशचंद्र शाह, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, विजय बहादुर सिंह, नंदकिशोर आचार्य, विनोद शाही, रमेश दवे आदि आलोचक यह कार्य जरूर करते रहे। पर विचारधारा या अस्मितामूलक विमर्शों के तहत लिखी जा रही आलोचना का वर्चस्व ज्यादा रहा, क्योंकि इसके पास ज्यादा संगठित मंच रहा। सुकून देने वाली बात है कि नई पीढ़ी के कुछेक आलोचक ‘जड़ीभूत सत्याभिरुचि’ की वैचारिकी से मुक्त होकर अपना आलोचनात्मक लेखन कर रहे हैं। ०