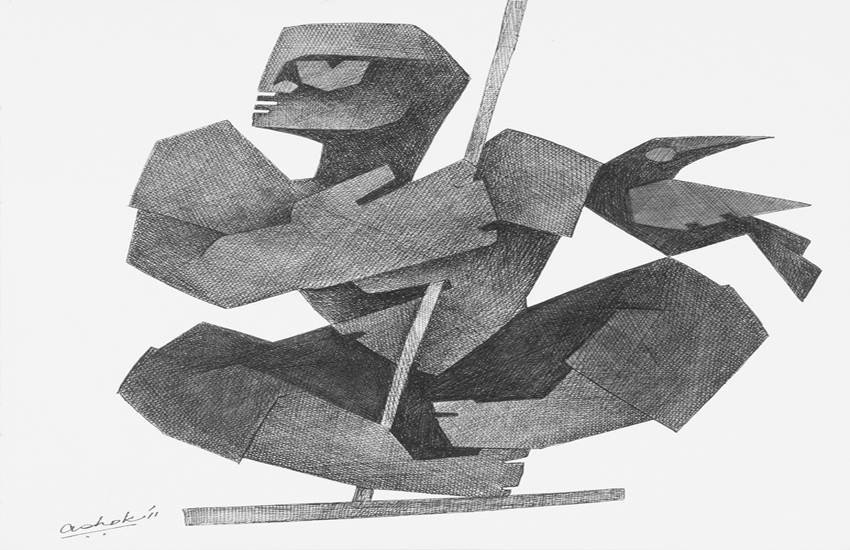कहानी और उपन्यास दोनों की जाति एक है। इन दोनों विधाओं का आरंभ भी लगभग एक साथ हुआ है। शुरू-शुरू में छोटे उपन्यास को कहानी कहा जाता था। पर, धीरे-धीरे स्थितियां बदलीं और कहानी ने अपना स्वतंत्र मार्ग बनाया। उपन्यास और कहानी में भिन्नता का आधार केवल आकार नहीं रहा। धीरे-धीरे यह निश्चित हो गया कि उपन्यास को छोटा करके न तो ‘कहानी’ बनाई जा सकती है और न ही कहानी को फुला कर उपन्यास बनाया जा सकता है। उपन्यास से स्वतंत्र होकर कहानी की कुछ विशेषताएं प्रकट हुर्इं। इन्हीं विशेषताओं को आधार बना कर कहानी का एक व्याकरण बना और विधा के रूप में कहानी को लेकर एक आम राय विकसित हुई। बहुत थोड़े ही समय बाद कहानियां लोकप्रियता की दृष्टि से उपन्यासों को टक्कर देने लगीं। इनको लोकप्रिय बनाने में पत्र-पत्रिकाओं की बड़ी भूमिका थी।
हिंदी में ‘बड़ी कहानी’ और ‘छोटी कहानी’ जैसा कोई विभाजन नहीं था। यहां कहानी का मतलब ही यही था कि वह आकार में छोटी होगी। ‘बड़ी कहानी’ जैसी किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं था। या तो कोई रचना उपन्यास है या तो कहानी। बीच का कोई मामला ही नहीं था। छोटी कहानी शब्द का प्रचलन अंग्रेजी के ‘शॉर्ट टेल’ के अनुवाद के तौर पर हुआ। हिंदी में इस विशेषण (छोटी) की कोई जरूरत नहीं थी। वह तो स्वत: सिद्ध था। इसीलिए, कालांतर में ‘छोटी कहानी’ की जगह सिर्फ ‘कहानी’ शब्द प्रचलन में रहा। इधर तीन-चार दशकों से कुछ ऐसी कहानियां लिखी जाने लगी हैं, जिनका आकार बहुत बड़ा हो रहा है। ऐसी कहानियों को ‘लंबी कहानी’ कहा जाता है। जो कहानियां हिंदी में लिखी गर्इं और अत्यंत लोकप्रिय हुर्इं, उनके आधार पर यह तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि किसी भी अच्छी कहानी के लिए कथा तत्त्व का होना अनिवार्य है। हिंदी में ऐसी एक भी श्रेष्ठ और लोकप्रिय कहानी ढूंढनी मुश्किल हो जाएगी, जिसमें कथा न हो। लंबी कहानियों के लिए तो कथा प्राणतत्त्व है। यहां तक कि लंबी कविताओं के लिए भी कथा का होना अनिवार्य है। यह अलग बात है कि वह कथा व्यक्ति की भी हो सकती है और देश की भी। जहां तक कहानी का प्रश्न है, वह तो कथा के बिना हो ही नहीं सकती है चाहे वह ‘कहानी’ हो या ‘लंबी कहानी’। लोगों को प्राय: यह कहते सुना जाता है कि ‘कहानी तो कहानी होती है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी।’ यह बात वैसे तो ठीक है, पर जैसे ही कहानी सामान्य से अधिक लंबी हो तब हमें यह अवश्य देखना चाहिए कि कहानी कथा-वस्तु के कारण लंबी हुई है या अवान्तर विवरणों के कारण। कथा-वस्तु के कारण कहानी लंबी या छोटी हो सकती है और उससे कहानी की सेहत पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बिना अपेक्षित कथा-वस्तु के कोई कहानी लंबी हो तो वह पाठकों के लिए उबाऊ होती है और वह अंतत: एक विफल कहानी होती है।
कहानी को ‘छोटी मुंह बड़ी बात’ के रूप में परिभाषित किया गया। इसी तर्ज पर कहा जाए तो लंबी कहानी एक तरह से ‘बड़ी मुंह बड़ी बात’ है। यानी, कहानी (छोटी मुंह) के माध्यम से जो बड़ी बात कही जा रही है उसे कहने के लिए अगर किसी को ‘लंबी कहानी’ (बड़ी मुंह) लिखनी पड़ रही है तो यह उसकी रचनात्मक न्यूनता का द्योतक है। लेकिन बात यहीं तक होती तो फिर भी गनीमत थी। आज की लंबी कहानियां प्राय: ‘बड़ी मुंह छोटी बात’ हो गई हैं। एक बड़ा प्रश्न यह है कि वर्तमान दौर में कहानियां लंबी क्यों हो रही हैं? हिंदी कहानी ‘छोटी मुंह बड़ी बात’ से ‘बड़ी मुंह छोटी बात’ तक कैसे पहुंच गई? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उपन्यास और कहानी के अंतर को भुला दिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि हिंदी कहानी की सौ साल की यात्रा को अप्रासंगिक बना कर हम फिर से आरंभ में पहुंच गए हैं जहां उपन्यास छोटा हो जाए तो उसे कहानी कह दें। हमें यह समझना चाहिए कि उपन्यास से अलग कहानी की अपनी अस्मिता है और उसकी कुछ अपनी शर्तें भी हैं। तभी तो, दोनों विधाओं में एक साथ लिखने वाले कुछ रचनाकारों को कहानी में अधिक सफलता मिलती है, तो कुछ को उपन्यास में। दरअसल, कहानी में कथ्य बहुत महत्त्वपूर्ण होता है। उसी के अनुरूप वह पात्रों और घटनाओं का चयन करता है। फिर इनको एक सूत्र में बांधता है। यह सूत्र ही कथानक है। कथ्य के अनुरूप अगर वह कथानक का निर्माण कर लेता है तो वह उसकी सफलता है और कहानी भी बेहतरीन बनती है। कहानी में कथ्य के अनुरूप कथानक को गढ़ना होता है। कथानक का एकमात्र लक्ष्य कथ्य को अभिव्यक्त करना होता है। घटना, पात्र, संवाद सब कथ्य के अधीन होते हैं। उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता और न ही वे स्वतंत्र रूप से विकसित हो सकते हैं। इसीलिए कहानी में ढेर सारे विवरणों, घटनाओं और पात्रों के लिए अवकाश नहीं रहता। ऐसा करने से कथानक में बिखराव पैदा होता है, जिसके फलस्वरूप कहानी लंबी होती जाती है और अपने उद्देश्य या कथ्य को भी ठीक से अभिव्यक्त नहीं कर पाती है। उपन्यास में लेखक के पास यह जरूर अवकाश रहता है कि वह अधिकाधिक विवरणों, घटनाओं और पात्रों की योजना कर सके। उपन्यास में इनके स्वतंत्र विकास के अवसर होते हैं।
पर्याप्त विषय-वस्तु के बिना कहानी का लंबा होना कहानीकार की आत्ममुग्धता का परिचायक है। कहानीकार जो कुछ भी जानता है उसे वह कहानी में प्रदर्शित कर देना चाहता है। यह एक तरह से अपने जाने हुए को कहानी के माध्यम से पाठकों पर थोप देना है। कहानी लिखना एक कला है। जैसे दर्जी कपड़े को काट-छांट कर कोई वस्त्र बनाता है उसी तरह कहानीकार का काम अपने अनुभव क्षेत्र के यथार्थ को काट-छांट कर कहानी बनाना है। अगर कोई कहानीकार यह कहे कि उसका अनुभव और ज्ञान बहुत मूल्यवान है और इसलिए वह उसे बिना काट-छांट के ही प्रस्तुत करेगा तो फिर उससे कहानी तो नहीं ही बन पाएगी। आजकल यही अधिक हो रहा है। कहानीकार बहुत जरूरी और मूल्यवान होने के नाम पर यर्थाथ को कहानी के अनुरूप बिना कटाई-छंटाई के ही प्रस्तुत कर दे रहा है। वह अपनी कहानी को चाहे कितना ही मूल्यवान माने, पर पाठकों की दृष्टि में उसकी रचना एक विफल कहानी बन कर रह जाती है। वर्तमान दौर में कहानी लंबी इसलिए नहीं हो रही है कि आज का कहानीकार पहले के कहानीकारों की तुलना में अपनी कहानियों के माध्यम से किसी अधिक बड़े सत्य को अभिव्यक्त कर रहा है, बल्कि लंबी इसलिए हो रही है कि वह यर्थाथ को काट-छांट कर कहानी बनाने में अकुशल हो गया है। वह कहानी से उपन्यास का काम लेना चाहता है। ऐसे में उसकी स्थिति बहुत दयनीय बन जाती है। उसकी रचना न उपन्यास बन पाती है, न कहानी। लंबी कहानी उसके लिए सुरक्षा कवच की तरह होती है। पर्याप्त कथावस्तु और कथा रस से भरपूर कुछ लंबी कहानियों को छोड़ दें तो इधर लिखी जा रही लंबी कहानियां कहानी हैं ही नहीं। कोई कहानी सफल है या नहीं उसकी पहली कसौटी यही है जैसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि ‘कहानी कहने वाले ने कहानी ठीक-ठीक सुनाई है या नहीं और वह शुरू से अंत तक सुनने वाले की उत्सुकता जागृत रखने में नाकामयाब तो नहीं रहा।’ यह कहानी की प्राथमिक कसौटी है। इस कसौटी पर खरा उतरने के बाद ही बाकी चीजों की बारी आती है। इधर कहानियां पहली ही कसौटी पर विफल साबित हो रही हैं। इस कसौटी पर विफल होकर बाकी कसौटियों पर सफल होने का कोई अर्थ नहीं है।