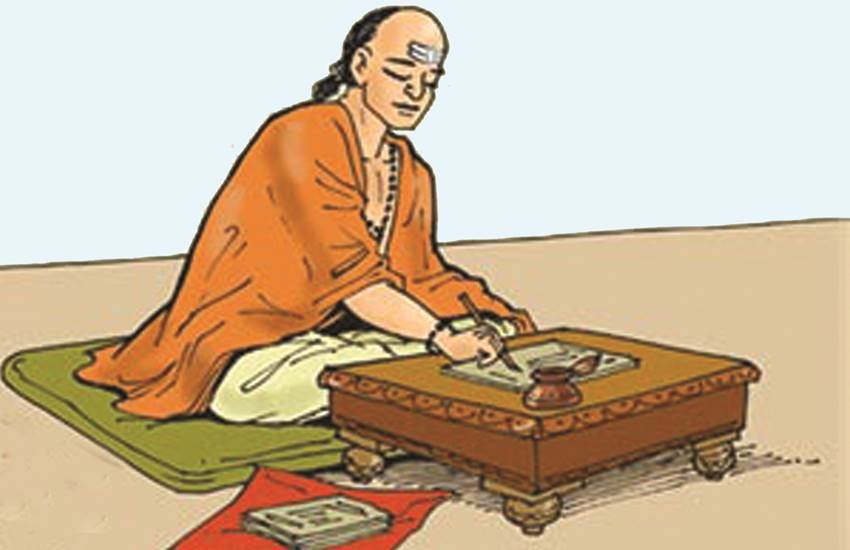शास्त्री कोसलेंद्रदास
आजादी के बाद देश को विदेशी भाषाओं के प्रभाव से मुक्त करने के लिए देशज भाषाओं के उत्थान के प्रयास हुए। जिसके परिणाम में केंद्र सरकार ने भारतीय भाषाओं को बढ़ाने और बचाने के लिए विशेष ‘दिवस’ मनाने शुरू किए। मुख्यत: ये दिवस दो भाषाओं के हैं। पहला है हिंदी दिवस, जो प्रतिवर्ष 14 सिंतबर को आता है। दूसरा है, रक्षाबंधन के दिन मनाया जाना वाला संस्कृत दिवस। संस्कृत दिवस का इतिहास पचास वर्ष पुराना है। 1968 में एक प्रस्ताव बना कि केंद्र और राज्य सरकारें हर साल ‘संस्कृत दिवस’ मनाएं। तत्कालीन शिक्षामंत्री डॉ. वीकेआर वरदराजराव ने इस दिशा में मजबूत काम किया। इसका नतीजा 1969 में आया, जब संस्कृत दिवस मनाने का सरकारी परिपत्र जारी हुआ। डॉ. राव उच्च कोटि के शिक्षाविद और सांस्कृतिक परंपराओं के गहरे जानकार थे। इसीलिए उन्होंने संस्कृत दिवस के लिए श्रावण माह की पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन का दिन चुना।
एक पर्व, तीन नाम
संस्कृत दिवस के लिए रक्षाबंधन का दिन चुनने के पीछे जो रहस्य है, वह शाश्वत परंपरा से जुड़ा है। मनुस्मृति में ‘श्रावण्यां प्रौष्ठपद्यां वा उपाकृत्य यथाविधि’ यानी यह दिन सदियों से गुरुकुलों में वेदों की शाखाएं दोहराने का है। यही दिन पुरोहितों द्वारा तीर्थों में ‘उपाकर्म’ करने का है, जिसे ‘श्रावणी’ कहा जाता है। उपाकर्म यानी शास्त्र पढ़ने की शुरुआत। मान्यता है कि गुरुकुलों में श्रावणी पूर्णिमा से शैक्षणिक सत्र आरंभ होता था। दूसरे लोगों का कहना है कि माघ महीने से चले आ रहे शैक्षणिक सत्र का समापन दिन श्रावणी है। जो भी कारण रहा हो, पर गुरुकुलों में यह दिन अध्ययन और अध्यापन के हिसाब से सबसे महत्त्व का रहा है। इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया भी जाता है। यही कारण था कि डॉ. राव ने इस दिन को ‘संस्कृत दिवस’ के रूप में चुना, जिससे इस दिन की पारंपरिक महत्ता जीवित रखी जा सके।
संस्कृत दिवस मनाना संस्कृत भाषा पर उपकार नहीं, बल्कि यह इस अमर भाषा के प्रति आभार प्रकट करने का दिन है। नई पीढ़ी को संस्कृत का ऐतिहासिक महत्त्व समझाने के लिए है, जिससे वह संस्कृत के ज्ञान-विज्ञान और साहित्य को समझ कर इसका उपयोग कर सके। संस्कृत में आदर्श और अनुशासन का मेल है। आध्यात्मिक और नैतिक स्तर पर व्यक्ति को मजबूत करने का साधन है। धन और शक्ति के बजाय ज्ञान के वर्चस्व की स्थापना है। उसके आदर्श ऊंचे हैं, जैसे- शुल्क लेकर पढ़ाना पाप है, जो ऐसा करता है वह मनुष्य अधम है। क्या आज यह आदर्श स्थापित हो सकता है?
संस्कृत आयोग का गठन
आजादी के बाद भारतीय भाषाओं की स्रोत भाषा संस्कृत के जमीनी हालात जानने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में संस्कृत आयोग बनाया। इसके अध्यक्ष भाषाविद सुनीति कुमार चटर्जी थे। वी. राघवन, विश्वबंधु शास्त्री और आरएन दांडेकर जैसे मनीषी इस आयोग के सदस्य थे। आयोग ने लंबे विचार-विमर्श के बाद शिक्षामंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद को 30 नवंबर, 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। आयोग की रिपोर्ट में संस्कृत के पारंपरिक अध्ययन-अध्यापन और उसे फैलाने को लेकर अनेक सुझाव थे।
संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए पंडित नेहरू ने 1961 में तिरुपति (आंध्र प्रदेश) में एक केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ खोला। 1 अप्रैल, 1967 को लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना दिल्ली में हुई। 1970 में इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए देश भर में संस्कृत महाविद्यालय खोलने के लिए दिल्ली में केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ स्थापित किया। अब यह राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है, जिसके अधीन तेरह संस्कृत शिक्षण केंद्र विभिन्न प्रांतों में संचालित हैं। 1987 में राजीव गांधी सरकार ने उज्जैन में महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान स्थापित किया। इस तरह संस्कृत आयोग की सिफारिशों के हिसाब से संस्कृत को मजबूत करने के निर्णय हुए, जिसके बेहतर परिणाम सामने आए।
पैंतीस सालों से संस्कृत समाचार
सन 1969 में कर्ण सिंह और सरोजनी महिषी के नेतृत्व में एक संसदीय दल जर्मनी गया। दल ने भारत आकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जो प्रतिवेदन दिया, उसमें एक सुझाव यह भी था कि जर्मनी के संचार साधनों से संस्कृत कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। इसी तर्ज पर भारत में भी आकाशवाणी और दूरदर्शन से संस्कृत समाचार और कार्यक्रम प्रसारित करने की योजना बनाई जाए। इंद्रकुमार गुजराल जब सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, तब 30 जून, 1974 को पहली बार आकाशवाणी से संस्कृत समाचार बुलेटिन शुरू हुआ। संस्कृत दिवस के अवसर पर 21 अगस्त, 1994 को दूरदर्शन से संस्कृत समाचार बुलेटिन शुरू हुआ, जिसे जाने-माने संस्कृत समाचार वाचक डॉ. बलदेवानंद सागर ने अपनी आवाज दी थी।
विरोधों का समन्वय है संस्कृत
प्राचीन काल में गुरुकुल के आचार्यों और अंतेवासियों (शिष्यों) ने आत्मकेंद्रित होकर भिक्षाटन से जीवन चला कर विशाल साहित्य का लेखन और संरक्षण किया। आयुर्वेद, गणितीय प्रणाली, संगीत, शिल्प शास्त्र, वास्तु शास्त्र, कृषि शास्त्र, अर्थशास्त्र तथा खगोल विज्ञान को समृद्ध करने में अनुपम अनुसंधान किए। संस्कृत की खासियत है कि उसमें बहुरंगी विचारों का समावेश है। उसके दर्शनशास्त्र में आस्तिक और नास्तिक का मेल है। अहिंसा, सत्य, चोरी न करना और सामाजिक समानता जैसे आध्यात्मिक और नैतिक आदर्श स्थापित है। पर क्या यह विडंबना नहीं है कि आधुनिकता के नाम पर इस धरोहर भाषा के विरोध में यदा-कदा घृणा की आवाज सुनाई देती है। भौतिकता के अहंकार में संस्कृत को बिना समझने उसका उपहास किया जाता है। उसे दकियानूसी विचारों से जोड़ दिया जाता है। जबकि हकीकत में सामाजिक अंतर्विरोधों और विचारों के संघर्ष और समन्वय का सर्वोत्तम चित्रण संस्कृत के पास है।
यजुर्वेद के इस मंत्र में उदात्त भावना देखिए, ‘आ नो भद्रा: क्रतवो यन्तु विश्वत:’ यानी अच्छे विचार चारों ओर से आने दो। संस्कृत में दर्शन, अध्यात्म और लौकिक ज्ञान-विज्ञान तथा मानवतावादी साहित्य का खजाना है। ऐसे में संस्कृत को प्रतिक्रियावादी राजनीति के डंडे से हांकना कहां तक उचित है? क्या संस्कृत विरोध की राजनीति करना उसमें निहित सनातन ज्ञान और विज्ञान का विरोध नहीं है? क्या संस्कृत को हिंदुत्व के मकड़जाल में फंसा कर उस पर धर्मगत भाषा का ठप्पा लगाना ठीक है? याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने 1986 में फैसला दिया था कि अरबी और फारसी के बिना संस्कृत भाषा को पढ़ाना धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ नहीं है।
आयोग का सुझाव था कि संस्कृत अध्ययन की देखभाल के लिए प्रत्येक राज्य में संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए, जिसमें सरकारी हस्तक्षेप न हो। देश भर के विश्वविद्यालयों में संस्कृत विभाग स्थापित हो। आयोग ने संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने के दो उद्देश्य बताए। पहला, संस्कृत की पारंपरिक पढ़ाई को विशेष तरीके से आगे बढ़ाया जाए। दूसरा, पारंपरिक संस्कृत अध्ययन को आधुनिक शिक्षा के साथ अपग्रेड करके शास्त्री और आचार्य उपाधियों को उनके बराबर लाया जाए। इस सुझाव से देश भर में सोलह संस्कृत विश्वविद्यालय खुले। इनमें केंद्र के चार और राज्य सरकारों के बारह विश्वविद्यालय हैं। वाराणसी का संपूणार्नंद संस्कृत विश्वविद्यालय सबसे पुराना है, जिसकी स्थापना ब्रिटिश राज में गर्वनर जोनाथन डंकन ने 1791 ईस्वी में गवर्नमेंट संस्कृत पाठशाला के रूप में की थी। वहीं, हरियाणा के कैथल में खुल रहा महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय सबसे नया है।
यह अप्रिय सच है कि आज अधिकतर संस्कृत विश्वविद्यालय ‘वेंटीलेटर’ पर हैं। इन्हें कहीं सरकारी अनदेखी बर्बाद कर रही है, तो कहीं राजनीतिक उठापटक। शिक्षकों के आधे से अधिक पद रिक्त हैं। शोध और अनुसंधान रसातल में चला गया है। संस्कृत के अनुसंधान उसी ढर्रे से हो रहे हैं, जिससे शोध पुरातन काल के प्रतीत होते हैं। अगर किसी संस्कृत विद्वान से संस्कृत के मौजूदा हालात की बात करें, तो वह इसके शास्त्रीय स्वरूप पर ‘प्रवचन’ देने लगता है। ऐसे प्रवचनों से ही संस्कृत पुराकाल की भाषा बन कर रह गई है।
सनातन है संस्कृत
आज संस्कृत शिक्षा के बारे में एक धूमिल-सी धारणा है। इसकी शास्त्रीय परंपरा जो भी रही हो, पर आम आदमी इसे पूजा-पाठ की भाषा से अधिक नहीं मानता। संस्कृत की यह अपनी समस्या है, जिसे हल करने का काम अग्रणी विद्वानों का है। यह जरूरी है कि संस्कृत के बारे में लोगों में भ्रम न रहे। उन्हें बताया जाए कि संस्कृत एक परंपरा है। वह धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान की वाहक है। उसका इतिहास किसी से मत पूछिए। यह सनातन है। ठीक उसी प्रकार जैसे सनातन धर्म है। कौन जानता है कि सनातन धर्म कब से है! जितनी संस्कृतियां भारत में जन्मी और पली-बढ़ी, संस्कृत उनकी नींव है। दर्शन, विज्ञान और कला का साहित्य संस्कृत में रचा गया। संस्कृत के उपकरण वे आदर्श हैं, जो परंपरा से चले आ रहे हैं। वे आस्थावान बनने की प्रेरणा देते हैं। मनुष्य होने का मर्म बताते हैं। आनंद की परिभाषा समझाते हैं। ‘मनुर्भव’ का संदेश देते हैं। 2007 में यूनेस्को की घोषणा के बाद ऋग्वेद मानव सभ्यता का सबसे पुराना दस्तावेज बैठता है। इससे संस्कृत वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक पुरातन भाषा सिद्ध होती है।
अभी संस्कृत उपेक्षित-सी है। इसके बारे में घोर अज्ञान है। वेदों से यह शुरू होती है। लेकिन इसकी बड़ी समस्या यह है कि इसकी शाखाएं खुद तना बन गई हैं। हर शाखा ने वृक्ष का रूप ले लिया है, मूल मरता चला गया। इसे नया आकार देने का दायित्व आज की पीढ़ी का है। पर संस्कृत की गौरवशाली परंपरा को समझे बगैर यह संभव नहीं है। संस्कृत का दायरा किसी पंथ, परंपरा या विधान का अनुगामी नहीं है। वह सार्वभौम तथा सार्वकालिक है। तभी तो ‘सत्यमेव जयते’ जैसे अमर वाक्य का सिद्धांत किस धर्म, पंथ, परंपरा या राष्ट्र को स्वीकृत नहीं है?
संस्कृत को बेहतरी का इंतजार
वर्तमान सरकार आई तो विश्वास जगा कि संस्कृत के दिन बहुरेंगे। पर इस सरकार ने जो प्रयास किए, वे पर्याप्त नहीं हैं। संस्कृत के हालात बिगड़ रहे हैं। इसका एक कारण हो सकता है कि संस्कृत के पास अपना वोट बैंक नहीं है। राजनीति के लोग जानते हैं कि उर्दू, सिंधी, गुजराती, पंजाबी या दूसरी भाषाओं की तुलना में संस्कृत भाषाई धरातल पर मजबूत नहीं है। 2011 की जनगणना के हिसाब से संस्कृत की स्थिति बेहद खराब है। संविधान में सूचीबद्ध बाईस भाषाओं में संस्कृत सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है। देश भर में सिर्फ 24821 लोगों ने संस्कृत को अपनी मातृभाषा बताया है। साफ है, सरकारी और सामाजिक बेरुखी के चलते संस्कृत नीचे के पायदान पर है। ऐसे में यक्ष प्रश्न है कि क्या केंद्र और राज्य सरकारें संस्कृत के पारंपरिक ज्ञान को बचाने के लिए ठोस प्रयास कर रही हैं? अगर इसका जबाव हां है तो फिर संस्कृत की स्थिति लगातार बद से बदतर क्यों हो रही है?
अटल बिहारी वाजपेयी संस्कृत को बचाने के ऐतिहासिक दायित्व के प्रति सचेत थे। उन्होंने संस्कृत के लिए बुनियादी कामों की शुरुआत की थी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग खोला। वर्ष 2003 को संस्कृत वर्ष के रूप में घोषित किया। ज्योतिष शास्त्र के विज्ञान को खोजने के लिए अनेक विश्वविद्यालयों में ज्योतिर्विज्ञान केंद्र खोले। तीन संस्कृत विद्यापीठों को मानित विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया। संस्कृत की पांडुलिपियों को बचाने के लिए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन 2003 में स्थापित किया। दिल्ली में एक विश्व संस्कृत सम्मेलन का आयोजन करवाया, जिसमें उन्होंने कहा था, संस्कृत को मृत भाषा कहना पूरी सनातन संस्कृति का अपमान है क्योंकि संस्कृत और संस्कृति अविभाज्य हैं। यह 5 अप्रेल, 2001 की बात है। पद्मभूषण आचार्य सत्यव्रत शास्त्री की अध्यक्षता में 10 जनवरी, 2014 को दूसरा संस्कृत आयोग बना। कलानाथ शास्त्री, डॉ. मानवेंदु बनर्जी और प्रो. वी. कुटुंब शास्त्री जैसे विद्वान आयोग के सदस्य थे। आयोग ने जुलाई, 2015 में विस्तृत रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्री को सौंपी।
संस्कृत को बढ़ाने के सुझाव
दूसरे संस्कृत आयोग ने संस्कृत को लेकर जो सुझाव दिए, उनमें स्कूली शिक्षा में चार भाषा फॉर्मूला प्रस्तावित है। आयोग का मानना है कि कक्षा छह से दस तक के छात्रों के लिए संस्कृत अनिवार्य विषय बनाया जाए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संस्थानों में संस्कृत के अनिवार्य पेपर के साथ कृषि विश्वविद्यालयों, वास्तुकला संस्थान, आइआइटी, आइआइएम और कानूनी पढ़ाई में संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों को जोड़ा जाए। राजनीति विज्ञान के छात्रों के लिए शुक्रनीति, विदुरनीति और महाभारत जैसे पुरातन ग्रंथों के अध्ययन की व्यवस्था की जाए। कृषि के विद्यार्थियों को ‘वृक्षायुर्वेद’ जैसे ग्रंथ पढ़ाए जाएं। आयोग ने संस्कृत शिक्षा के स्कूल और प्रत्येक राज्य में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना पर जोर दिया है।
केन्द्रीय संस्कृत विद्यालयों की स्थापना, निजी चैनलों और रेडियो स्टेशनों द्वारा संस्कृत कार्यक्रमों का प्रसारण, वेद-विद्यालयों जैसे पारंपरिक केंद्रों के छात्रों के लिए आधुनिक सुविधाएं, दिल्ली के राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान के रूप में विकसित करने और संस्कृत में एक टीवी चैनल शुरू करने के सुझाव हैं। वर्तमान सरकार ने यूपीए सरकार के बनाए संस्कृत आयोग के जवाब में 18 नवंबर, 2015 को तेरह सदस्यों की एक संस्कृत सुझाव समिति बनाई। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के कुलाधिपति एन. गोपालस्वामी समिति के अध्यक्ष थे। गोपालस्वामी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। समिति को तीन महीने में अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया, ताकि संस्कृत का दस सालों का रोडमैप बन सके। समिति ने अपनी रिपोर्ट में संस्कृत के आधुनिक और पारंपरिक अध्ययन को लेकर सुझाव दिए हैं, जिनको क्रियान्वित करना बाकी है। हालांकि मोदी सरकार ने दो साल पहले जामिया मिल्लिया इस्लामिया में संस्कृत विभाग खोल कर संस्कृत को वहां पहुंचाने का ऐतिहासिक काम किया है।
संस्कृत का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप
देशज बोलियों ने संस्कृत से अपनी शब्दावली ग्रहण की है। एक भाषायी शोध के अनुसार दक्षिण-पूर्व एशिया की भाषाओं में संस्कृत शब्द अच्छी तादाद में हैं। मूल उच्चारण में थोड़ा-बहुत अंतर वैसे ही है, जैसे भारत में ‘घट’ का ‘घड़ा’ है। ‘दक्षिण-पूर्व’ दिशा के लिए शब्द है- आखने, जो संस्कृत के ‘आग्रेय’ शब्द का परिवर्तित रूप है। ऐसे थाई भाषा में दक्षिण-पूर्व कहना हो तो कहा जाएगा ‘आसया आखने’।
थाईलैंड में नौ विश्वविद्यालय हैं, जिनमें सात के नाम संस्कृत में हैं और दो के राजाओं पर। एक विश्वविद्यालय का नाम है- धर्मशास्त्र विश्वविद्यालय, तो दूसरे का शिल्पाकर विश्वविद्यालय। एक है- कसेरसात विश्वविद्यालय यानी कृषिशास्त्र विश्वविद्यालय। लाओ भाषा में ‘वन-वे’ के लिए ‘एक-दिशा मार्ग’ है। संस्कृत के हजारों शब्द दक्षिण-पूर्व एशिया में प्रचलित हैं। ‘वर्ल्ड बैंक’ के लिए ‘लोक धनागार’ शब्द है। मलय भाषा में हवाई जहाज के लिए ‘आकाश यान’ शब्द है। इंडोनेशिया में हाथी ‘गज’ है, तो महिला के लिए ‘वनिता’ शब्द है। शहद के लिए ‘मधु’ तथा गार्डन के लिए ‘उद्यान’ शब्द हैं। चिड़ियाघर के लिए ‘उद्यान लोकसत्व’ शब्द है, वहीं फोटो के लिए ‘रूप’ है। मध्य एशिया के सेमेटिक परिवार की अरबी भाषा में संस्कृत शब्दों का भरपूर प्रचलन है। यथा इलायची के लिए एल, पान के लिए तंबूल और मृत्यु (अंतकाल) के लिए इंतकाल। भाषाई अध्ययन के मुताबिक चीनी भाषा में लगभग छत्तीस सौ शब्द संस्कृत के हैं।
संस्कृत के विकास में मुसलमानों और ईसाइयों का बड़ा योगदान है। ईसाइयों ने तो श्रीमद्भगवद्गीता की तर्ज पर ‘ख्रिस्तु गीता’ लिखी है। केरल के पीसी देवस्सिआ ने छत्तीस सर्गों में महाकाव्य लिखा है ‘ख्रिस्तुभागवतम्’, जिस पर उन्हें 1980 में साहित्य अकादेमी पुरस्कार मिला। इसी तरह ‘यीशुचरितम्’, ‘यीशुमाहात्म्यम्’ और ‘यीशुसौरभम्’ जैसे ग्रंथ लिखे गए हैं। यहां तक की ‘विष्णुसहस्रनामस्तोत्र’ की तरह ‘ख्रिस्तुसहस्रनामस्तोत्र’ लिखा गया। प्राचीन काल से ही मुसलिम विद्वानों ने संस्कृत पर लेखनी चलाई है। अब्दुल रहीम खानेखाना ने ‘खेटकौतुकमे’ और ‘रहीमकाव्यम्’ लिखे, जो बहुत प्रसिद्ध हैं। मुंबई में दरगाह के मुतवल्ली पंडित गुलाम दस्तगीर बिराजदार संस्कृत में गजल गाते हैं। उनका कहना है, ‘देश की सभी शास्त्रीय भाषाओं, विशेषकर संस्कृत का संरक्षण सरकार का काम है और सरकार को इसके लिए मजबूर करना हमारा काम।’ बिराजदार शान से खुद को ‘संस्कृत का गुलाम’ ही कहते हैं।