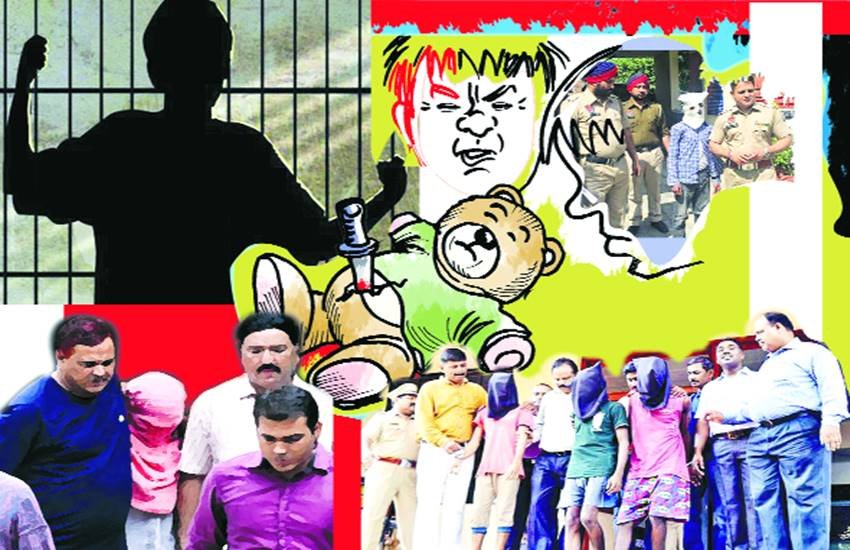उम्र सीमा कम किए जाने के बावजूद किशोर-अपराधों में कोई कमी नहीं आई है। कानूनन वे सहानुभूति के हकदार हैं लेकिन सवाल उठता है कि क्या उम्र के आधार पर किसी अपराधी के प्रति सहानुभूति दिखा कर उसके शिकार हुए लोगों को सही मायने में न्याय मिलता है? उम्र कम होने के आधार पर किसी के कुकृत्य को कमतर क्यों माना जाए? जायजा ले रहे हैं ‘श्रीशचंद्र मिश्र’।
इस बात से असहमत होने की कोई वजह नहीं है कि अपराधी को उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। अपराध बड़ा हो तो सजा भी उतनी ही कड़ी। इसमें उम्र को आधार बनाने का मानवीय संकोच करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है? संशोधित कानून में यही किया गया है। लेकिन इससे किशोरों द्वारा किए जाने वाले अपराधों में कोई कमी नहीं आ पाई है। कानून बना कर कभी अपराध खत्म नहीं किए जा सके हैं। पिछले एक दशक में किशोर अपराधियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। अठारह साल की उम्र तक के अपराधी को किशोर मान कर किसी भी तरह के अपराध के लिए उसे अधिकतम तीन साल आम जेल से अलग बाल सुधारगृह में रखने की पुरानी व्यवस्था की वजह से तो ऐसा नहीं हुआ है। जाहिर है कि इसके कुछ मानसिक कारण भी हैं जो अपराधी की सामाजिक व पारिवारिक परिस्थितियों से जुड़े हैं।
आर्थिक कारण इसमें महत्त्वपूर्ण नहीं हैं क्योंकि पिछले एक दशक में जो किशोर अपराध दर्ज हुए हैं उनमें ज्यादा संख्या यौन अपराधों की है।महिला सशक्तीकरण पर बनी संसद की संयुक्त समिति का भी मानना है कि महिलाओं के प्रति यौन अपराध करने वाले सोलह से अठारह साल के उम्र के किशोरों की संख्या बढ़ी है। इसी आधार पर सोलह साल की उम्र तक के अपराधी को किशोर अपराधी मानने का कानून बनाने की मांग उठी। बहरहाल अब सवाल यह है कि दो साल उम्र घटा कर क्या किशोर अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकेगा? हाल फिलहाल में ही कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें सोलह साल से कम उम्र के लड़के यौन अपराधों में शामिल पाए गए। दिल्ली में ही इस तरह के दो मामले पिछले दिनों सामने आए। इससे यह बड़ा सवाल उठता है कि महिलाओं के प्रति अपराध में किशोरों की बढ़ती भूमिका की वजह क्या है? उनमें यह विकृति क्या समाज के बदले माहौल से आई है?
पंद्रह साल पहले जब किशोर न्याय (बाल सुरक्षा व संरक्षण) कानून बनाया गया था तो उसके पीछे विचार यह था कि किशोर उत्तेजना, भावावेग या किसी उकसावे में आकर अपराध कर बैठते हैं। वे शातिर अपराधी नहीं होते। उनके व्यवहार और मानसिकता में सुधार किया जा सकता है। लिहाजा ऐसे अपराधियों की सजा दंडात्मक नहीं सुधारात्मक होनी चाहिए। यह सिर्फ भारत में ही नहीं हुआ। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में जो सहमति बनी थी उसमें 190 देशों ने अपराधी को वयस्क मानने की उम्र सीमा अठारह साल तय कर दी थी। 2000 के कानून में व्यवस्था थी कि अठारह साल या उससे कम उम्र का अपराधी किशोर माना जाएगा और किशोर अदालत में उस पर मुकदमा चलेगा। इसमें यह व्यवस्था भी थी कि जघन्यतम अपराध करने वाले किशोर को भी अठारह साल की उम्र पार करते ही रिहा कर दिया जाए। 2006 में पिछले कानून की इस धारा को हटा दिया गया।
यह संयोग नहीं है कि किशोर कानून बनने के बाद से किशोर अपराधों की संख्या तेजी से बढ़ी है। शायद इसलिए कि किसी भी तरह का अपराध करते समय किशोर आश्वस्त रहता है कि उसे कम सजा मिलेगी और उसे सामान्य जेल में भी रहना नहीं पड़ेगा। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी का मानना है कि गंभीर अपराधों में शामिल सोलह साल से ऊपर के पचास फीसद से ज्यादा अपराधी कानून के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2014 में किशोर अपराध उससे पिछले साल की तुलना में 132 फीसद बढ़े हैं। बलात्कार की घटनाओं में साठ फीसद की बढ़ोतरी हुई। ऐसे अपराधों में 16 से 18 साल की उम्र के 66 फीसद से ज्यादा किशोर शामिल पाए गए। बाल अधिकारों के संरक्षण के दिल्ली आयोग ने गैरसरकारी संगठन ह्यबटरफ्लाइजह्ण के साथ मिल कर अध्ययन किया कि आखिर बच्चे अपराध क्यों करते हैं ?
निचोड़ यह निकला कि उत्पीड़न, गरीबी, अशिक्षा और ठीक से संरक्षण न मिल पाने की वजह से ऐसा होता है। इस अध्ययन में बताया गया कि कम उम्र में अपराध करने वालों के शातिर अपराधी बनने की आशंका अधिक उम्र में अपराध शुरू करने वालों से ज्यादा होती है। छोटी उम्र में बच्चों को मजदूरी में लगा दिए जाने से उनमें आपराधिक प्रवृत्ति पनपने की संभावना ज्यादा रहती है। लेकिन यह धारणा भी पूरी तरह सही नहीं है कि गरीबी, निरक्षरता, अभाव व खराब पारिवारिक पृष्ठभूमि किशोरों को अपराध करने के लिए प्रेरित करती है। संभ्रात परिवार के और पढ़े-लिखे किशोरों में आपराधिक प्रवृत्तियां पिछले कुछ समय में तेजी से बढ़ी हैं। हाल के आंकड़े तो और चौंकाने वाले है। 2014 में किशोरों ने केवल दिल्ली में 120 बलात्कार किए। 15 दिसंबर 2015 तक बलात्कार के आरोप में 149 नाबालिग पकड़े गए। पूरे देश की बात करे तो 2012 से 2014 के बीच किशोरों ने बलात्कार और महिलाओं के उत्पीड़न की 8676 वारदातें की।
बढ़ते अपराधों की सबसे बड़ी वजह अपराधियों को कम उम्र की वजह से उपयुक्त सजा न मिल पाना है। 2014 में 18 साल से कम उम्र के जिन साठ हजार से ज्यादा अपराधियों को पकड़ा गया उनमें से 14.5 फीसद यानी करीब 8,700 को ही बाल सुधार गृह भेजा गया। 7345 को सलाह देकर या फटकार लगा कर घर भेज दिया गया। 8,159 को प्रोबेशन पर रिहा कर माता-पिता या किसी अभिभावक की देख-रेख में रखा गया। 22,276 को विभिन्न संस्थानों के हवाले कर दिया गया। 3,509 पर आरोप साबित नहीं हो पाए और 1,857 पर सिर्फ जुर्माना लगाया गया।
किशोर कानून में संशोधन होने बाद भी यह सवाल उठाने वालों की कमी नहीं है कि अपराधियों पर उम्र के लिहाज से रहम क्यों किया जाए? इसके लिए ब्रिटेन का उदाहरण दिया जाता है जहां सात से सोलह साल की उम्र के अपराधियों के लिए चार वर्ग बनाए गए हैं। अपराध के हिसाब से उन्हें सजा दी जाती है। भारत में किशोर अपराधी को यह सुविधा भी प्राप्त है कि बाल सुधारगृह से रिहा होने के बाद अगर वह कोई अपराध करता है तो उसका पिछला अपराध, चाहे वह कितना ही जघन्यतम क्यों न हो, संज्ञान में नहीं लाया जाएगा।
ऐसे अपराधियों की क्रिमिनल हिस्ट्री दर्ज नहीं होती। संशोधित कानून में भी इसका कोई प्रावधान नहीं है। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी का मानना है कि यौन अपराधी भले ही दस बारह साल का क्यों न हो, राष्ट्रीय यौन अपराधी रजिस्टर में उसका नाम दर्ज होना चाहिए। उनका प्रस्ताव यह भी है कि रिहा होने के बाद किशोर को हर महीने पुलिस के सामने हाजिरी देना और अपना अता-पता प्रमाणित करना अनिवार्य होना चाहिए। नाबालिग अपराधियों पर रहम दिखा कर उन्हें सुधरने का मौका देने की ब्रिटिशकाल की अवधारणा को जकड़े बैठी न्यायिक व्यवस्था की खामी का फायदा उठाकर पिछले करीब एक दशक में ही कथित अल्पवयस्क अपराधियों ने तांडव मचा रखा है। चिकित्सकीय व मनोवैज्ञानिक तरीके से नाबालिग अपराधी की मानसिकता बदलने का प्रयोग करने वाली दिल्ली की बाल जेलों में समय-समय पर बाल अपराधियों ने जिस तरह उत्पात मचाया है, उससे साफ है कि एक बार अपराध करने के बाद उनमें ग्लानि का भाव कतई नहीं आया।
भारत में अदालतों को यह अधिकार देने की मांग पर भी बहस उठी है कि वह यह तय करे कि जघन्य अपराधों के मामले में बाल अपराधियों को वयस्क मान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए या नहीं। यह देखते हुए कि समाज में तेजी से बदलाव आ रहा है और बच्चे बहुत कुछ जानने समझने लगे हैं, विशिष्ट मामलों में कानून को उम्र की सीमा फिर से निर्धारित करनी चाहिए। बेहतर तरीका यह है कि बाल न्याय बोर्ड को अपराध की गंभीरता तय करने दिया जाए। इससे उसे बाल अपराधी की मानसिक स्थिति समझ कर अपराध के अनुकूल सजा दे पाने में मदद मिलेगी। इस तरह के मामलों में सजा देना ही काफी नहीं है। ऐसे अपराधियों की उपयुक्त काउंसलिंग, पुनर्वास की पर्याप्त दिशा देने वाले बेहतर सुधारगृह और बाल अपराधियों में सुधार की नियमित समीक्षा जैसे कदम उठाए जाने भी जरूरी हैं। ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं कि कितने बाल अपराधी सुधरे।
मौजूदा कानून इस संभावना पर बने हैं कि बाल अपराधी को अगर ठीक सलाह और अवसर मुहैया कराए जाए तो उसे सुधारा जा सकता है। हालांकि उसके लक्षण कुछ ही अपराधियों में दिखे हैं। छह साल की बच्ची से बलात्कार कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देने वाले वहशी की मौत की सजा बदलने के पीछे दिल्ली हाईकोर्ट ने कम उम्र को जो आधार बनाया, उस पर एक महिला वकील ऋचा कपूर ने सरकार से मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की गुजारिश की थी। सुझाव दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट से इस बात पर विचार करने का आग्रह किया जाना चाहिए कि क्या अदालतों को यह तय करने का अधिकार है कि वह आरोपी के व्यवहार व उसके अपराध की जघन्यता पर उम्र संबंधी मेडिकल सबूत हावी न होने दे। उम्र का मेडिकल सबूत हमेशा निर्णायक नहीं हो सकता। वह क्षेत्र, खुराक और वर्ण के आधार पर अलग अलग हो सकता है। अगर अपराध से लगे कि वह योजनाबद्ध तरीके से सोच समझ कर किया गया है तो ऐसे में तथाकथित कम उम्र के अपराधी को बाल अपराधी नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई।
कुल मिला कर आमराय तो यही है कि कम उम्र होने को आधार बना कर खतरनाक अपराधी को कम सजा देने वाले कानून में और संशोधन कर उम्र की बंदिश खत्म की जाए। हालांकि बाल अधिकारों के लिए काम करने वालों में इस मुद्दे पर सहमति नहीं है। कुछ का तर्क है कि बाल अपराधी के लिए निर्धारित न्यूनतम उम्र को यथावत रखते हुए विशेष मामलों में बाल अपराधी को कड़ी सजा दी जाए। कुछ का मानना है कि सजा देने से ऐसे अपराधियों को सुधारा नहीं जा सकेगा। उनका तर्क है कि इस तरह के ज्यादातर अपराधी ऐसे माहौल में पलते हैं जहां उनकी उपेक्षा होती है या मानसिक, शारीरिक और यौन-उत्पीड़न किया जाता है। लेकिन इस तर्क के दो पहलू हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। नाबालिगों द्वारा बलात्कार के जो मामले सामने आए हैं उनमें से आधे से ज्यादा मामलों में दोनों पक्षों की सहमति से शारीरिक संबंध बने लेकिन लड़की के अल्पवयस्क होने की वजह से इन्हें बलात्कार का मामला माना गया। बाल न्याय बोर्ड के सामने लाए गए बाल अपराधियों में से करीब एक चौथाई ने फिर अपराध नहीं किया।
काउंसलिंग से उनमें सुधार आया। विशेषज्ञ इसे अच्छा संकेत मानते हैं और उनका कहना है कि बाकियों को शिक्षा व काउंसलिंग के साथ रोजगार का भी कोई विकल्प मुहैया कराना चाहिए ताकि उन्हें आपराधिक गतिविधियों से अलग किया जा सके। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि बाल न्याय बोर्ड के सामने लाए जाने वाले कई बाल अपराधी आपराधिक मनोवृत्ति के होते हैं और उन्हें किसी भी हालत में सुधारा नहीं जा सकता। बाल न्याय कानून की वजह से वे कड़ी सजा से बच जाते हैं। इनमें से ज्यादातर निम्न आय वर्ग के परिवार के होते है। बाल अधिकार के लिए काम करने वाले लोगों का सुझाव है कि जब बाल न्याय बोर्ड के सामने किसी बाल अपराधी को पेश किया जाता है तो उसके साथ साथ उसके माता-पिता व अन्य परिजनों की काउंसिलिंग भी होनी चाहिए। लेकिन बाल अपराधियों के सुधार और पुनर्वास के लिए की गई व्यवस्था नाकाफी है। बाल अपराधियों को जहां रखा जाता है वहां से उनके साथ भेदभाव, दुर्व्यवहार और हिंसा होने की खबरें भी आए दिन सामने आती हैं।
पिछले कुछ सालों ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनसे साबित हुआ कि बाल अपराधी होने की वजह से जघन्य अपराध की बेहद मामूली सजा पाने वाले सुधरते नहीं हैं बल्कि रिहा होने के बाद और हिंसक हो जाते हैं। पड़ोस की लड़की से बलात्कार कर उसकी हत्या करने के बावजूद अल्पवयस्क होने की वजह से एक किशोर को तीन साल की सजा मिली। सजा काटने के बाद वह और ज्यादा खतरनाक हो गया। उसी लड़की के पिता को वह धमकी देने पहुंच गया कि उसकी दूसरी बेटी के साथ भी वही करेगा जो पहली बेटी के साथ किया। ऐसी ही एक घटना ने बता दिया कि नाबालिग होने के बावजूद कैसे किशोरों को अपराध करने में आनंद आता है। बाल सुधार गृह से भागने के करीब एक महीने बाद ही पांच किशोरों ने एक महिला की हत्या कर पचास किलोग्राम चांदी के जेवर और दस लाख रुपए लूटने में जरा सी भी हिचक नहीं दिखाई। शातिर तरीके से अपराध को अंजाम देने के बाद उन्होंने भंडारे के लिए 35 हजार रुपए दिए और अपने एक साथी के जन्मदिन पर जश्न मनाया। नोएडा में उन्होंने शानोशौकत से रहना शुरू कर दिया।
गिरफ्तारी के बाद उन्होंने पुलिस को बताया कि वे एक संगठित गिरोह का हिस्सा हैं। गिरोह का मुखिया उन्हें मासिक वेतन देता था और पकड़े जाने पर उन्हें कानूनी सहायता उपलब्ध कराता था। ऐसे गिरोह दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में निश्चित रूप से काफी होंगे जो किशोरों को बहला फुसला कर अपराध की दुनिया में धकेल रहे हैं। देश भर में ऐसे नाबालिग बच्चों की संख्या करीब बीस लाख है जो बेसहारा हैं, उपेक्षित हैं और जिनका आय का जरिया कोई नहीं है। ऐसे बच्चों को आपराधिक गतिविधियों की तरफ आसानी से धकेला जा सकता है। सवाल यह है कि इसे रोका कैसे जाए? कच्ची उम्र में अपराध के आकर्षण में फंस जाने वाले किशोरों को उस दलदल से बाहर निकाल कर सही दिशा में कैसे मोड़ा जाए? यह सिर्फ सामाजिक समस्या भर नहीं है।
प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर भी इसका निदान खोजा जाना जरूरी है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सोलह साल साल की अधिकतम उम्र के अपराधी को बाल अपराधी की श्रेणी में रखने का दायरा बदलने से भी समस्या का हल नहीं हो सकता। इससे बाल अपराधियों की मानसिकता नहीं बदली जा सकती। सजा उम्र से नहीं अपराध की जघन्यता से तय हो। साथ ही सामान्य अपराधियों के पुनर्वास की संवेदनशील व्यवस्था हो।